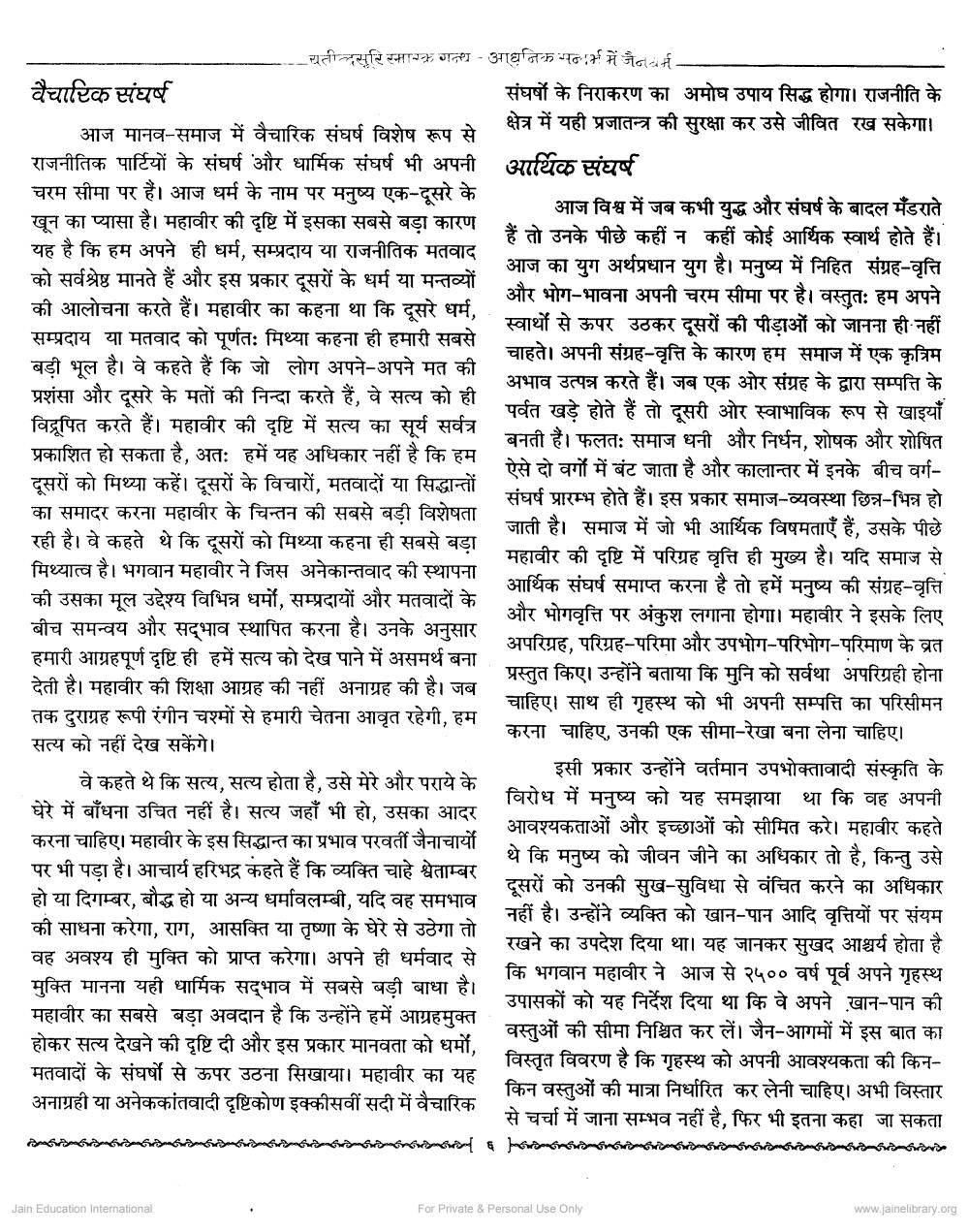________________
____ यतीन्दसूरि रमारक गत्य - आधुनिक मन में जैनबर्न - वैचारिक संघर्ष
संघर्षों के निराकरण का अमोघ उपाय सिद्ध होगा। राजनीति के
क्षेत्र में यही प्रजातन्त्र की सुरक्षा कर उसे जीवित रख सकेगा। आज मानव-समाज में वैचारिक संघर्ष विशेष रूप से राजनीतिक पार्टियों के संघर्ष और धार्मिक संघर्ष भी अपनी आर्थिक संघर्ष चरम सीमा पर हैं। आज धर्म के नाम पर मनुष्य एक-दूसरे के
आज विश्व में जब कभी युद्ध और संघर्ष के बादल मँडराते खून का प्यासा है। महावीर की दृष्टि में इसका सबसे बड़ा कारण
हैं तो उनके पीछे कहीं न कहीं कोई आर्थिक स्वार्थ होते हैं। यह है कि हम अपने ही धर्म, सम्प्रदाय या राजनीतिक मतवाद
आज का युग अर्थप्रधान युग है। मनुष्य में निहित संग्रह-वृत्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और इस प्रकार दूसरों के धर्म या मन्तव्यों
और भोग-भावना अपनी चरम सीमा पर है। वस्तुतः हम अपने की आलोचना करते हैं। महावीर का कहना था कि दसरे धर्म. .
स्वार्थों से ऊपर उठकर दूसरों की पीडाओं को जानना ही नहीं सम्प्रदाय या मतवाद को पूर्णतः मिथ्या कहना ही हमारी सबसे
चाहते। अपनी संग्रह-वृत्ति के कारण हम समाज में एक कृत्रिम बड़ी भूल है। वे कहते हैं कि जो लोग अपने-अपने मत की
अभाव उत्पन्न करते हैं। जब एक ओर संग्रह के द्वारा सम्पत्ति के प्रशंसा और दूसरे के मतों की निन्दा करते हैं, वे सत्य को ही
पर्वत खड़े होते हैं तो दूसरी ओर स्वाभाविक रूप से खाइयाँ विद्रपित करते हैं। महावीर की दृष्टि में सत्य का सर्य सर्वत्र
बनती है। फलतः समाज धनी और निर्धन, शोषक और शोषित प्रकाशित हो सकता है, अतः हमें यह अधिकार नहीं है कि हम
ऐसे दो वर्गों में बंट जाता है और कालान्तर में इनके बीच वर्गदूसरों को मिथ्या कहें। दूसरों के विचारों, मतवादों या सिद्धान्तों
संघर्ष प्रारम्भ होते हैं। इस प्रकार समाज-व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो का समादर करना महावीर के चिन्तन की सबसे बड़ी विशेषता
जाती है। समाज में जो भी आर्थिक विषमताएँ हैं, उसके पीछे रही है। वे कहते थे कि दूसरों को मिथ्या कहना ही सबसे बड़ा
महावीर की दृष्टि में परिग्रह वृत्ति ही मुख्य है। यदि समाज से मिथ्यात्व है। भगवान महावीर ने जिस अनेकान्तवाद की स्थापना
आर्थिक संघर्ष समाप्त करना है तो हमें मनुष्य की संग्रह-वृत्ति की उसका मूल उद्देश्य विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों और मतवादों के
और भोगवृत्ति पर अंकुश लगाना होगा। महावीर ने इसके लिए बीच समन्वय और सद्भाव स्थापित करना है। उनके अनुसार
अपरिग्रह, परिग्रह-परिमा और उपभोग-परिभोग-परिमाण के व्रत हमारी आग्रहपूर्ण दृष्टि ही हमें सत्य को देख पाने में असमर्थ बना
प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि मुनि को सर्वथा अपरिग्रही होना देती है। महावीर की शिक्षा आग्रह की नहीं अनाग्रह की है। जब
चाहिए। साथ ही गृहस्थ को भी अपनी सम्पत्ति का परिसीमन तक दुराग्रह रूपी रंगीन चश्मों से हमारी चेतना आवृत रहेगी, हम
करना चाहिए, उनकी एक सीमा-रेखा बना लेना चाहिए। सत्य को नहीं देख सकेंगे।
इसी प्रकार उन्होंने वर्तमान उपभोक्तावादी संस्कृति के वे कहते थे कि सत्य, सत्य होता है. उसे मेरे और पराये के।
विरोध में मनुष्य को यह समझाया था कि वह अपनी घेरे में बाँधना उचित नहीं है। सत्य जहाँ भी हो, उसका आदर
आवश्यकताओं और इच्छाओं को सीमित करे। महावीर कहते करना चाहिए। महावीर के इस सिद्धान्त का प्रभाव परवर्ती जैनाचार्यों
थे कि मनुष्य को जीवन जीने का अधिकार तो है, किन्तु उसे पर भी पड़ा है। आचार्य हरिभद्र कहते हैं कि व्यक्ति चाहे श्वेताम्बर
दूसरों को उनकी सुख-सुविधा से वंचित करने का अधिकार हो या दिगम्बर, बौद्ध हो या अन्य धर्मावलम्बी, यदि वह समभाव
नहीं है। उन्होंने व्यक्ति को खान-पान आदि वृत्तियों पर संयम की साधना करेगा, राग, आसक्ति या तृष्णा के घेरे से उठेगा तो
रखने का उपदेश दिया था। यह जानकर सुखद आश्चर्य होता है वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त करेगा। अपने ही धर्मवाद से
कि भगवान महावीर ने आज से २५०० वर्ष पूर्व अपने गृहस्थ मुक्ति मानना यही धार्मिक सद्भाव में सबसे बड़ी बाधा है।
उपासकों को यह निर्देश दिया था कि वे अपने खान-पान की महावीर का सबसे बड़ा अवदान है कि उन्होंने हमें आग्रहमुक्त
वस्तुओं की सीमा निश्चित कर लें। जैन-आगमों में इस बात का होकर सत्य देखने की दृष्टि दी और इस प्रकार मानवता को धमों, मतवादों के संघर्षों से ऊपर उठना सिखाया। महावीर का यह ।
विस्तृत विवरण है कि गृहस्थ को अपनी आवश्यकता की किन
किन वस्तुओं की मात्रा निर्धारित कर लेनी चाहिए। अभी विस्तार अनाग्रही या अनेककांतवादी दृष्टिकोण इक्कीसवीं सदी में वैचारिक
से चर्चा में जाना सम्भव नहीं है, फिर भी इतना कहा जा सकता
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org