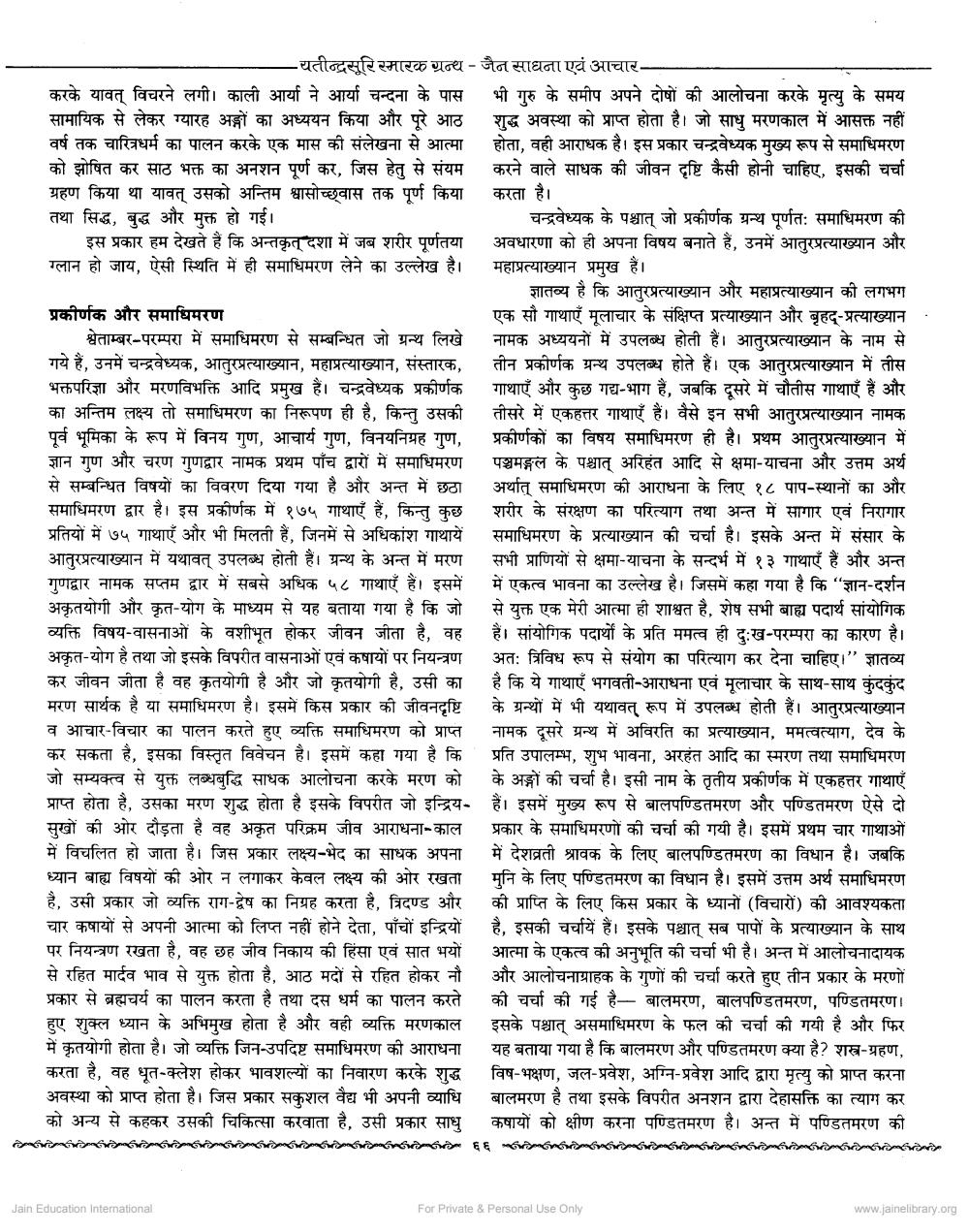________________
- यतीन्द्रसूरि स्मारक ग्रन्थ करके यावत् विचरने लगी। काली आय ने आर्या चन्दना के पास सामायिक से लेकर ग्यारह अनों का अध्ययन किया और पूरे आठ वर्ष तक चारित्रधर्म का पालन करके एक मास की संलेखना से आत्मा को झोषित कर साठ भक्त का अनशन पूर्ण कर, जिस हेतु से संयम ग्रहण किया था यावत् उसको अन्तिम श्वासोच्छ्वास तक पूर्ण किया तथा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गई।
इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्तकृत् दशा में जब शरीर पूर्णतया ग्लान हो जाय, ऐसी स्थिति में ही समाधिमरण लेने का उल्लेख है।
प्रकीर्णक और समाधिमरण
.
श्वेताम्बर परम्परा में समाधिमरण से सम्बन्धित जो ग्रन्थ लिखे गये हैं, उनमें चन्द्रवेयक आतुरप्रत्याख्यान, महाप्रत्याख्यान, संस्तारक, भक्तपरिज्ञा और मरणविभक्ति आदि प्रमुख हैं । चन्द्रवेध्यक प्रकीर्णक का अन्तिम लक्ष्य तो समाधिमरण का निरूपण ही है, किन्तु उसकी पूर्व भूमिका के रूप में विनय गुण, आचार्य गुण, विनयनिग्रह गुण, ज्ञान गुण और चरण गुणद्वार नामक प्रथम पाँच द्वारों में समाधिमरण से सम्बन्धित विषयों का विवरण दिया गया है और अन्त में छठा समाधिमरण द्वार है। इस प्रकीर्णक में १७५ गाथाएँ हैं, किन्तु कुछ प्रतियों में ७५ गाथाएँ और भी मिलती है, जिनमें से अधिकांश गाथायें आतुरप्रत्याख्यान में यथावत् उपलब्ध होती हैं। ग्रन्थ के अन्त में मरण गुणद्वार नामक सप्तम द्वार में सबसे अधिक ५८ गाथाएँ हैं। इसमें अकृतयोगी और कृतत-योग के माध्यम से यह बताया गया है कि जो व्यक्ति विषय-वासनाओं के वशीभूत होकर जीवन जीता है, वह अकृत योग है तथा जो इसके विपरीत वासनाओं एवं कषायों पर नियन्त्रण कर जीवन जीता है वह कतयोगी है और जो कृतयोगी है, उसी का मरण सार्थक है या समाधिमरण है। इसमें किस प्रकार की जीवनदृष्टि व आचार-विचार का पालन करते हुए व्यक्ति समाधिमरण को प्राप्त कर सकता है, इसका विस्तृत विवेचन है। इसमें कहा गया है कि जो सम्यक्त्व से युक्त लब्धबुद्धि साधक आलोचना करके मरण को प्राप्त होता है, उसका मरण शुद्ध होता है इसके विपरीत जो इन्द्रिय सुखों की ओर दौड़ता है वह अकृत परिक्रम जीव आराधना-काल में विचलित हो जाता है। जिस प्रकार लक्ष्य-भेद का साधक अपना ध्यान बाह्य विषयों की ओर न लगाकर केवल लक्ष्य की ओर रखता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति राग-द्वेष का निग्रह करता है, त्रिदण्ड और चार कषायों से अपनी आत्मा को लिप्त नहीं होने देता, पाँचों इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखता है, वह छह जीव निकाय की हिंसा एवं सात भयों से रहित मार्दव भाव से युक्त होता है, आठ मदों से रहित होकर नी प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करता है तथा दस धर्म का पालन करते हुए शुक्ल ध्यान के अभिमुख होता है और वही व्यक्ति मरणकाल में कृतयोगी होता है। जो व्यक्ति जिन उपदिष्ट समाधिमरण की आराधना करता है, वह धूत-क्लेश होकर भावशल्यों का निवारण करके शुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। जिस प्रकार सकुशल वैद्य भी अपनी व्याधि को अन्य से कहकर उसकी चिकित्सा करवाता है, उसी प्रकार साधु
Jain Education International
जैन साधना एवं आचार
भी गुरु के समीप अपने दोषों की आलोचना करके मृत्यु के समय शुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। जो साधु मरणकाल में आसक्त नहीं होता, वही आराधक है। इस प्रकार चन्द्रवेध्यक मुख्य रूप से समाधिमरण करने वाले साधक की जीवन दृष्टि कैसी होनी चाहिए, इसकी चर्चा करता है।
६६
चन्द्रवेध्यक के पश्चात् जो प्रकीर्णक ग्रन्थ पूर्णतः समाधिमरण की अवधारणा को ही अपना विषय बनाते हैं, उनमें आतुरप्रत्याख्यान और महाप्रत्याख्यान प्रमुख हैं । ज्ञातव्य है कि आतुरप्रत्याख्यान और महाप्रत्याख्यान की लगभग एक सौ गाथाएँ मूलाचार के संक्षिप्त प्रत्याख्यान और बृहद् - प्रत्याख्यान नामक अध्ययनों में उपलब्ध होती हैं। आतुरप्रत्याख्यान के नाम से तीन प्रकीर्णक ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। एक आतुरप्रत्याख्यान में तीस गाथाएँ और कुछ गद्य-भाग हैं, जबकि दूसरे में चौतीस गाथाएँ हैं और तीसरे में एकहत्तर गाथाएँ हैं। वैसे इन सभी आतुरप्रत्याख्यान नामक प्रकीर्णकों का विषय समाधिमरण ही है। प्रथम आतुरप्रत्याख्यान में पञ्चमङ्गल के पश्चात् अरिहंत आदि से क्षमा याचना और उत्तम अर्थ अर्थात् समाधिमरण की आराधना के लिए १८ पाप-स्थानों का और शरीर के संरक्षण का परित्याग तथा अन्त में सागार एवं निरागार समाधिमरण के प्रत्याख्यान की चर्चा है। इसके अन्त में संसार के सभी प्राणियों से क्षमा याचना के सन्दर्भ में १३ गाथाएँ हैं और अन्त में एकत्व भावना का उल्लेख है। जिसमें कहा गया है कि "ज्ञान-दर्शन से युक्त एक मेरी आत्मा ही शाश्वत है, शेष सभी बाह्य पदार्थ सांयोगिक है। सांयोगिक पदार्थों के प्रति ममत्व ही दुःख-परम्परा का कारण है। अतः त्रिविध रूप से संयोग का परित्याग कर देना चाहिए।” ज्ञातव्य है कि ये गाथाएं भगवती आराधना एवं मूलाचार के साथ-साथ कुंदकुंद के ग्रन्थों में भी यथावत् रूप में उपलब्ध होती हैं। आतुरप्रत्याख्यान नामक दूसरे ग्रन्थ में अविरति का प्रत्याख्यान, ममत्वत्याग, देव के प्रति उपालम्भ, शुभ भावना, अरहंत आदि का स्मरण तथा समाधिमरण के अङ्गों की चर्चा है। इसी नाम के तृतीय प्रकीर्णक में एकहत्तर गाथाएं हैं। इसमें मुख्य रूप से बालपण्डितमरण और पण्डितमरण ऐसे दो प्रकार के समाधिमरणों की चर्चा की गयी है। इसमें प्रथम चार गाथाओं में देशव्रती श्रावक के लिए बालपण्डितमरण का विधान है। जबकि मुनि के लिए पण्डितमरण का विधान है। इसमें उत्तम अर्थ समाधिमरण की प्राप्ति के लिए किस प्रकार के ध्यानों (विचारों) की आवश्यकता है, इसकी चर्चायें हैं। इसके पश्चात् सब पापों के प्रत्याख्यान के साथ आत्मा के एकत्व की अनुभूति की चर्चा भी है। अन्त में आलोचनादायक और आलोचना ग्राहक के गुणों की चर्चा करते हुए तीन प्रकार के मरणों की चर्चा की गई है- बालमरण, वालपण्डितमरण, पण्डितमरण इसके पश्चात् असमाधिमरण के फल की चर्चा की गयी है और फिर यह बताया गया है कि बालमरण और पण्डितमरण क्या है? शस्त्र ग्रहण, विष - भक्षण, जल-प्रवेश, अग्नि प्रवेश आदि द्वारा मृत्यु को प्राप्त करना बालमरण है तथा इसके विपरीत अनशन द्वारा देहासक्ति का त्याग कर कषायों को क्षीण करना पण्डितमरण है। अन्त में पण्डितमरण की
For Private & Personal Use Only
Eviantar
www.jainelibrary.org