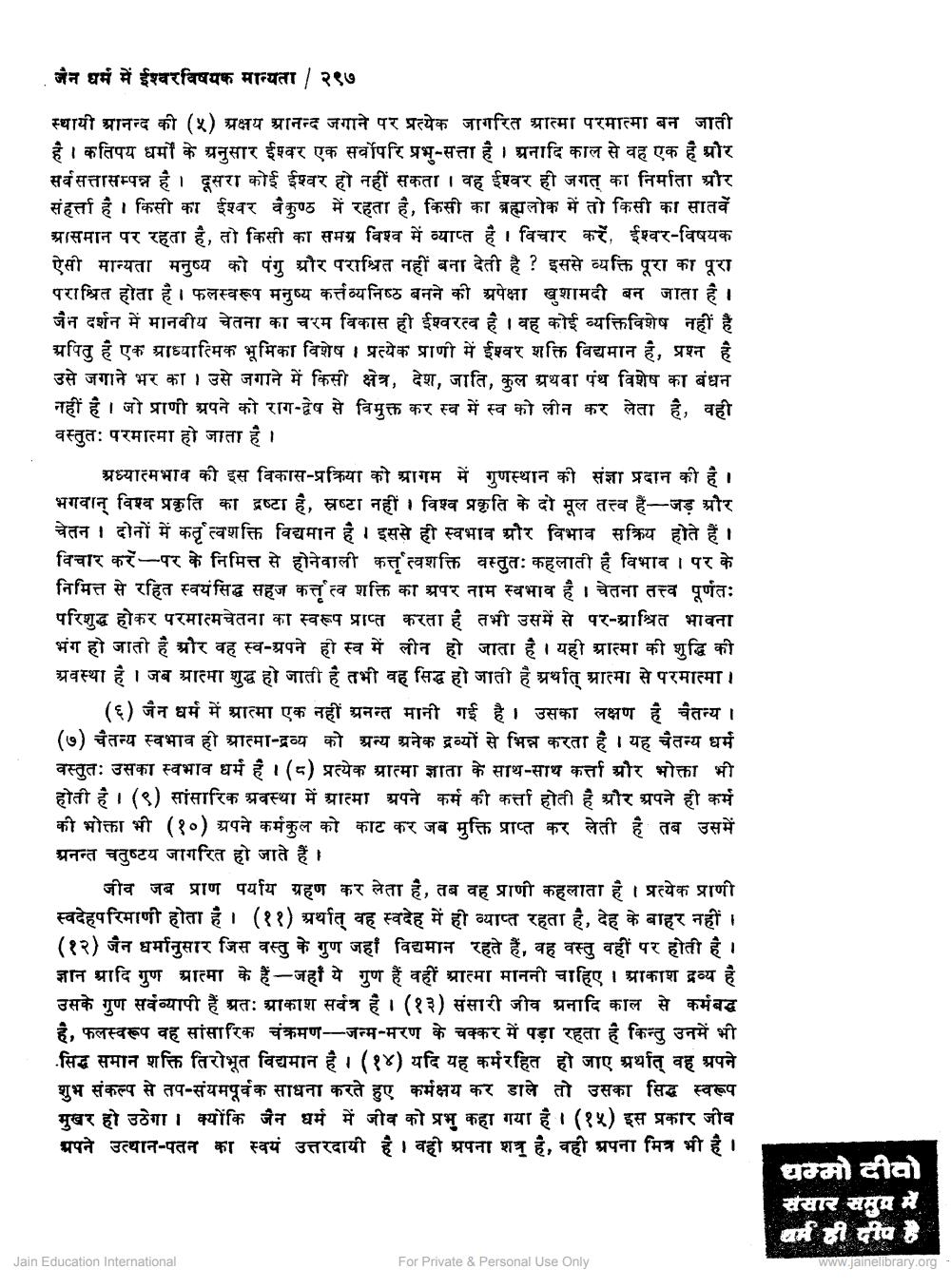________________
जैन धर्म में ईश्वरविषयक मान्यता | २९७
स्थायी प्रानन्द की (५) अक्षय प्रानन्द जगाने पर प्रत्येक जागरित आत्मा परमात्मा बन जाती है । कतिपय धर्मों के अनुसार ईश्वर एक सर्वोपरि प्रभु-सत्ता है । अनादि काल से वह एक है और सर्वसत्तासम्पन्न है। दूसरा कोई ईश्वर हो नहीं सकता । वह ईश्वर ही जगत् का निर्माता और संहर्ता है। किसी का ईश्वर वैकुण्ठ में रहता है, किसी का ब्रह्मलोक में तो किसी का सातवें
आसमान पर रहता है, तो किसी का समग्र विश्व में व्याप्त है । विचार करें, ईश्वर-विषयक ऐसी मान्यता मनुष्य को पंगू और पराश्रित नहीं बना देती है ? इससे व्यक्ति पूरा का पूरा पराश्रित होता है। फलस्वरूप मनुष्य कर्तव्यनिष्ठ बनने की अपेक्षा खुशामदी बन जाता है। जैन दर्शन में मानवीय चेतना का चरम विकास ही ईश्वरत्व है । वह कोई व्यक्तिविशेष नहीं है अपितु है एक प्राध्यात्मिक भूमिका विशेष । प्रत्येक प्राणी में ईश्वर शक्ति विद्यमान है, प्रश्न है उसे जगाने भर का। उसे जगाने में किसी क्षेत्र, देश, जाति, कुल अथवा पंथ विशेष का बंधन नहीं है। जो प्राणी अपने को राग-द्वेष से विमुक्त कर स्व में स्व को लीन कर लेता है, वही वस्तुत: परमात्मा हो जाता है।
अध्यात्मभाव की इस विकास-प्रक्रिया को आगम में गुणस्थान की संज्ञा प्रदान की है। भगवान् विश्व प्रकृति का द्रष्टा है, स्रष्टा नहीं। विश्व प्रकृति के दो मूल तत्त्व हैं-जड़ और चेतन । दोनों में कर्तृत्वशक्ति विद्यमान है। इससे ही स्वभाव और विभाव सक्रिय होते हैं। विचार करें-पर के निमित्त से होनेवाली कर्तृत्वशक्ति वस्तुतः कहलाती है विभाव । पर के निमित्त से रहित स्वयं सिद्ध सहज कर्तृत्व शक्ति का अपर नाम स्वभाव है । चेतना तत्त्व पूर्णतः परिशुद्ध होकर परमात्मचेतना का स्वरूप प्राप्त करता है तभी उसमें से पर-प्राश्रित भावना भंग हो जाती है और वह स्व-अपने ही स्व में लीन हो जाता है। यही आत्मा की शुद्धि की अवस्था है । जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तभी वह सिद्ध हो जाती है अर्थात् प्रात्मा से परमात्मा।
(६) जैन धर्म में प्रात्मा एक नहीं अनन्त मानी गई है। उसका लक्षण है चैतन्य । (७) चैतन्य स्वभाव ही आत्मा-द्रव्य को अन्य अनेक द्रव्यों से भिन्न करता है। यह चैतन्य धर्म वस्तुतः उसका स्वभाव धर्म है । (८) प्रत्येक प्रात्मा ज्ञाता के साथ-साथ कर्ता और भोक्ता भी होती है । (९) सांसारिक अवस्था में आत्मा अपने कर्म की कर्ता होती है और अपने ही कर्म की भोक्ता भी (१०) अपने कर्मकूल को काट कर जब मुक्ति प्राप्त कर लेती है तब उसमें अनन्त चतुष्टय जागरित हो जाते हैं।
जीव जब प्राण पर्याय ग्रहण कर लेता है, तब वह प्राणी कहलाता है । प्रत्येक प्राणी स्वदेहपरिमाणी होता है। (११) अर्थात् वह स्वदेह में ही व्याप्त रहता है, देह के बाहर नहीं । (१२) जैन धर्मानुसार जिस वस्तु के गुण जहाँ विद्यमान रहते हैं, वह वस्तु वहीं पर होती है। ज्ञान प्रादि गुण आत्मा के हैं-जहाँ ये गुण हैं वहीं प्रात्मा माननी चाहिए । अाकाश द्रव्य है उसके गुण सर्वव्यापी हैं अतः आकाश सर्वत्र है । (१३) संसारी जीव अनादि काल से कर्मबद्ध है, फलस्वरूप वह सांसारिक चंक्रमण-जन्म-मरण के चक्कर में पड़ा रहता है किन्तु उनमें भी सिद्ध समान शक्ति तिरोभूत विद्यमान है। (१४) यदि यह कर्मरहित हो जाए अर्थात् वह अपने शुभ संकल्प से तप-संयमपूर्वक साधना करते हुए कर्मक्षय कर डाले तो उसका सिद्ध स्वरूप मुखर हो उठेगा। क्योंकि जैन धर्म में जीव को प्रभु कहा गया है। (१५) इस प्रकार जीव अपने उत्थान-पतन का स्वयं उत्तरदायी है। वही अपना शत्रु है, वही अपना मित्र भी है ।
धम्मो दीवो संसार समुद्र में वर्म ही दीप है
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org