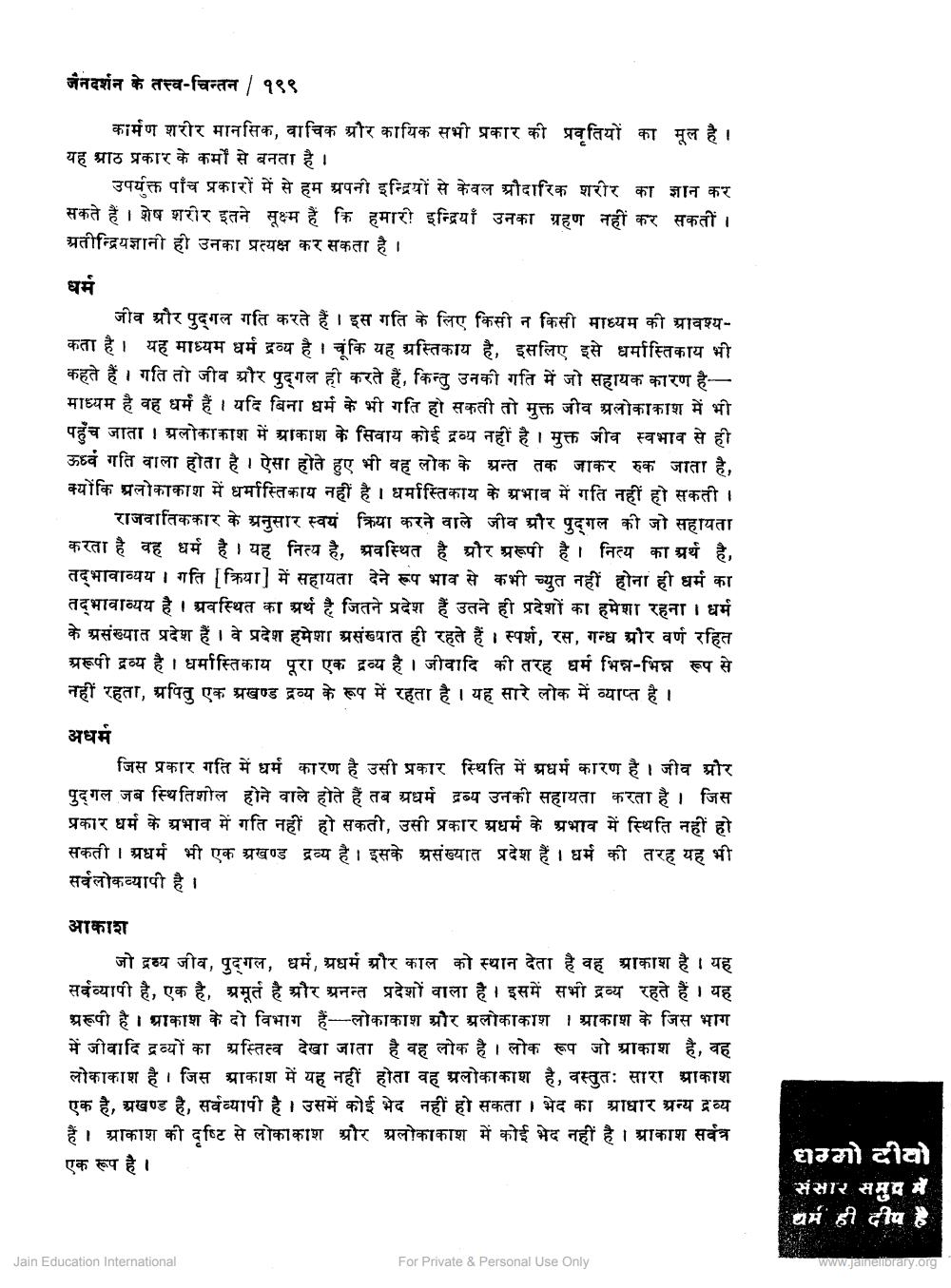________________
जैनदर्शन के तत्व-चिन्तन | १९९
कार्मण शरीर मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार की प्रवृतियों का मूल है। यह पाठ प्रकार के कर्मों से बनता है।
उपर्यक्त पाँच प्रकारों में से हम अपनी इन्द्रियों से केवल प्रौदारिक शरीर का ज्ञान कर सकते हैं। शेष शरीर इतने सूक्ष्म हैं कि हमारी इन्द्रियाँ उनका ग्रहण नहीं कर सकतीं। अतीन्द्रियज्ञानी ही उनका प्रत्यक्ष कर सकता है।
धर्म
जीव और पुद्गल गति करते हैं । इस गति के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता है। यह माध्यम धर्म द्रव्य है। चूंकि यह अस्तिकाय है, इसलिए इसे धर्मास्तिकाय भी कहते हैं। गति तो जीव और पुद्गल ही करते हैं, किन्तु उनकी गति में जो सहायक कारण हैमाध्यम है वह धर्म हैं। यदि बिना धर्म के भी गति हो सकती तो मुक्त जीव अलोकाकाश में भी पहुँच जाता । अलोकाकाश में आकाश के सिवाय कोई द्रव्य नहीं है। मुक्त जीव स्वभाव से ही ऊध्वं गति वाला होता है। ऐसा होते हुए भी वह लोक के अन्त तक जाकर रुक जाता है, क्योंकि प्रलोकाकाश में धर्मास्तिकाय नहीं है। धर्मास्तिकाय के अभाव में गति नहीं हो सकती।
राजवातिककार के अनुसार स्वयं क्रिया करने वाले जीव और पुद्गल की जो सहायता करता है वह धर्म है। यह नित्य है, अवस्थित है और प्ररूपी है। नित्य का अर्थ है, तद्भावाव्यय । गति [क्रिया में सहायता देने रूप भाव से कभी च्युत नहीं होना ही धर्म का तद्भावाव्यय है । अवस्थित का अर्थ है जितने प्रदेश हैं उतने ही प्रदेशों का हमेशा रहना । धर्म के असंख्यात प्रदेश हैं। वे प्रदेश हमेशा असंख्यात ही रहते हैं। स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण रहित अरूपी द्रव्य है। धर्मास्तिकाय पूरा एक द्रव्य है । जीवादि की तरह धर्म भिन्न-भिन्न रूप से नहीं रहता, अपितु एक अखण्ड द्रव्य के रूप में रहता है । यह सारे लोक में व्याप्त है ।
अधर्म
जिस प्रकार गति में धर्म कारण है उसी प्रकार स्थिति में अधर्म कारण है। जीव और पुद्गल जब स्थितिशील होने वाले होते हैं तब अधर्म द्रब्य उनकी सहायता करता है। जिस प्रकार धर्म के अभाव में गति नहीं हो सकती, उसी प्रकार अधर्म के प्रभाव में स्थिति नहीं हो सकती । अधर्म भी एक अखण्ड द्रव्य है। इसके असंख्यात प्रदेश हैं । धर्म की तरह यह भी सर्वलोकव्यापी है।
आकाश
जो द्रव्य जीव, पूदगल, धर्म, अधर्म और काल को स्थान देता है वह आकाश है । यह सर्वव्यापी है, एक है, अमूर्त है और अनन्त प्रदेशों वाला है। इसमें सभी द्रव्य रहते हैं। यह प्ररूपी है। प्राकाश के दो विभाग हैं-लोकाकाश और अलोकाकाश । आकाश के जिस भाग में जीवादि द्रव्यों का अस्तित्व देखा जाता है वह लोक है। लोक रूप जो आकाश है, वह लोकाकाश है। जिस आकाश में यह नहीं होता वह प्रलोकाकाश है, वस्तुत: सारा आकाश एक है, अखण्ड है, सर्वव्यापी है। उसमें कोई भेद नहीं हो सकता। भेद का प्राधार अन्य द्रव्य हैं। आकाश की दृष्टि से लोकाकाश और अलोकाकाश में कोई भेद नहीं है। आकाश सर्वत्र एक रूप है।
धम्मो दीवो संसार समुद्र में धर्म ही दीय है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jaimellorary.org