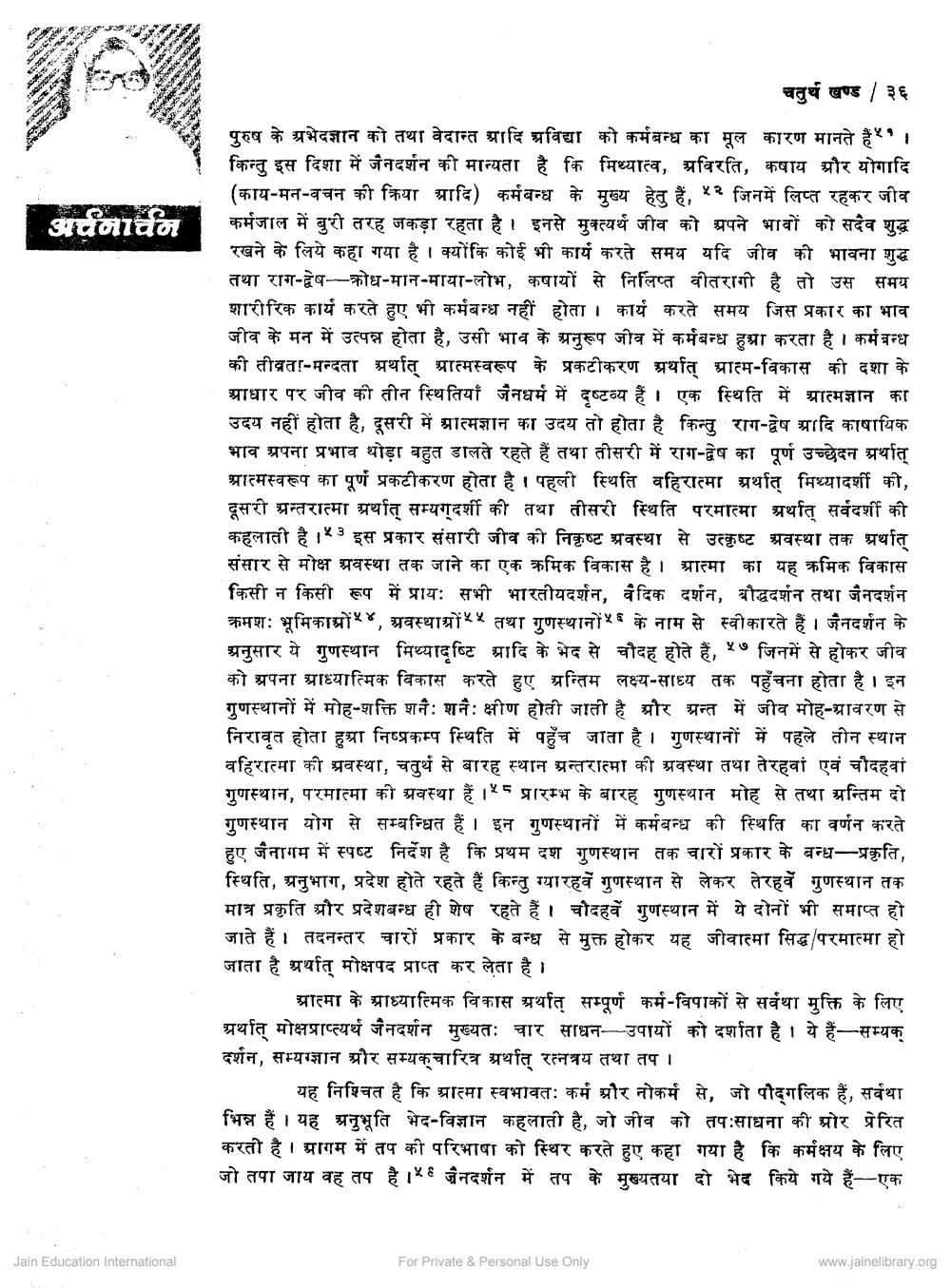________________
kinesirevieKIN
चतुर्थ खण्ड | ३६
raam
H imansopra Sanwar
HODicareer
amavar
Koxipar d eshe Spark
Budidat
पुरुष के अभेदज्ञान को तथा वेदान्त आदि अविद्या को कर्मबन्ध का मूल कारण मानते हैं । किन्तु इस दिशा में जैनदर्शन की मान्यता है कि मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगादि (काय-मन-वचन की क्रिया आदि) कर्मबन्ध के मुख्य हेतु हैं, ५२ जिनमें लिप्त रहकर जीव कर्मजाल में बुरी तरह जकड़ा रहता है। इनसे मुक्त्यर्थ जीव को अपने भावों को सदैव शुद्ध रखने के लिये कहा गया है । क्योंकि कोई भी कार्य करते समय यदि जीव की भावना शुद्ध तथा राग-द्वेष-क्रोध-मान-माया-लोभ, कषायों से निलिप्त वीतरागी है तो उस समय शारीरिक कार्य करते हुए भी कर्मबन्ध नहीं होता। कार्य करते समय जिस प्रकार का भाव जीव के मन में उत्पन्न होता है, उसी भाव के अनुरूप जीव में कर्मबन्ध हुआ करता है। कर्मबन्ध की तीव्रता-मन्दता अर्थात् प्रात्मस्वरूप के प्रकटीकरण अर्थात् आत्म-विकास की दशा के आधार पर जीव की तीन स्थितियाँ जैनधर्म में दृष्टव्य हैं। एक स्थिति में आत्मज्ञान का उदय नहीं होता है, दूसरी में आत्मज्ञान का उदय तो होता है किन्तु राग-द्वेष आदि काषायिक भाव अपना प्रभाव थोड़ा बहुत डालते रहते हैं तथा तीसरी में राग-द्वेष का पूर्ण उच्छेदन अर्थात् प्रात्मस्वरूप का पूर्ण प्रकटीकरण होता है । पहली स्थिति बहिरात्मा अर्थात् मिथ्यादर्शी की, दूसरी अन्तरात्मा अर्थात् सम्यग्दर्शी की तथा तीसरी स्थिति परमात्मा अर्थात् सर्वदर्शी की कहलाती है। ५३ इस प्रकार संसारी जीव की निकृष्ट अवस्था से उत्कृष्ट अवस्था तक अर्थात् संसार से मोक्ष अवस्था तक जाने का एक क्रमिक विकास है। आत्मा का यह क्रमिक विकास किसी न किसी रूप में प्रायः सभी भारतीयदर्शन, वैदिक दर्शन, बौद्धदर्शन तथा जैनदर्शन क्रमशः भूमिकामों५४, अवस्थानों५५ तथा गुणस्थानों५६ के नाम से स्वीकारते हैं। जैनदर्शन के अनुसार ये गुणस्थान मिथ्यादृष्टि प्रादि के भेद से चौदह होते हैं, ५७ जिनमें से होकर जीव को अपना आध्यात्मिक विकास करते हुए अन्तिम लक्ष्य-साध्य तक पहुँचना होता है । इन गुणस्थानों में मोह-शक्ति शनैः शनैः क्षीण होती जाती है और अन्त में जीव मोह-यावरण से निरावृत होता हुआ निष्प्रकम्प स्थिति में पहुँच जाता है। गुणस्थानों में पहले तीन स्थान वहिरात्मा की अवस्था, चतुर्थ से बारह स्थान अन्तरात्मा की अवस्था तथा तेरहवां एवं चौदहवां गुणस्थान, परमात्मा की अवस्था हैं।५८ प्रारम्भ के बारह गुणस्थान मोह से तथा अन्तिम दो गुणस्थान योग से सम्बन्धित हैं। इन गुणस्थानों में कर्मबन्ध की स्थिति का वर्णन करते हए जैनागम में स्पष्ट निर्देश है कि प्रथम दश गुणस्थान तक चारों प्रकार के बन्ध-प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश होते रहते हैं किन्तु ग्यारहवें गुणस्थान से लेकर तेरहवें गुणस्थान तक मात्र प्रकृति और प्रदेशबन्ध ही शेष रहते हैं। चौदहवें गुणस्थान में ये दोनों भी समाप्त हो जाते हैं। तदनन्तर चारों प्रकार के बन्ध से मुक्त होकर यह जीवात्मा सिद्ध परमात्मा हो जाता है अर्थात् मोक्षपद प्राप्त कर लेता है।
आत्मा के प्राध्यात्मिक विकास अर्थात् सम्पूर्ण कर्म-विपाकों से सर्वथा मुक्ति के लिए अर्थात् मोक्षप्राप्त्यर्थ जैनदर्शन मुख्यत: चार साधन-उपायों को दर्शाता है। ये हैं-सम्यक दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र अर्थात् रत्नत्रय तथा तप ।
यह निश्चित है कि प्रात्मा स्वभावतः कर्म और नोकर्म से, जो पौद्गलिक हैं, सर्वथा भिन्न हैं। यह अनुभूति भेद-विज्ञान कहलाती है, जो जीव को तपःसाधना की प्रोर प्रेरित करती है । प्रागम में तप की परिभाषा को स्थिर करते हुए कहा गया है कि कर्मक्षय के लिए जो तपा जाय वह तप है।५६ जनदर्शन में तप के मुख्यतया दो भेद किये गये हैं-एक
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org