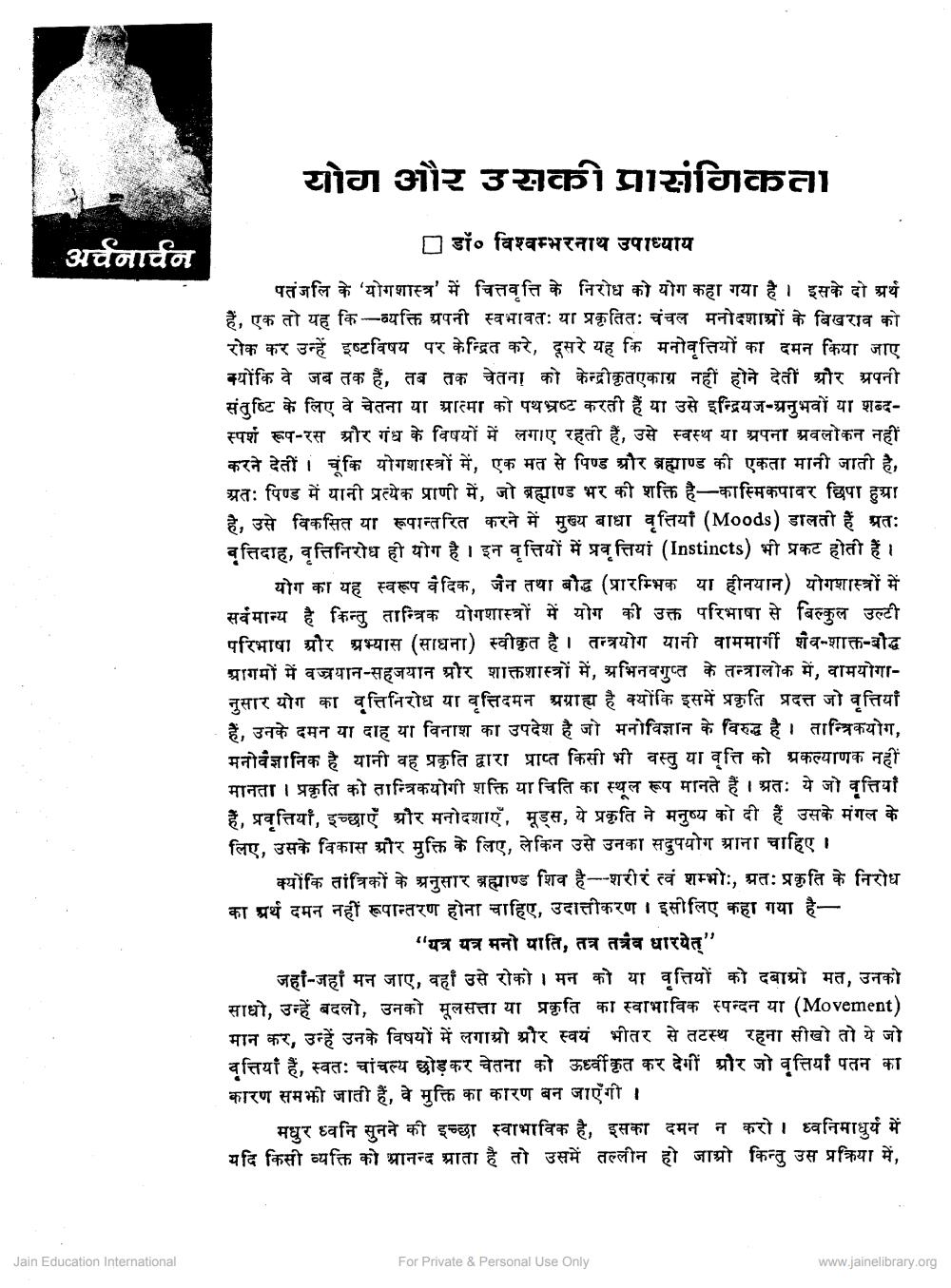________________
योग और उसकी प्रासंगिकता
अर्चनार्चन
डॉ० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय
पतंजलि के 'योगशास्त्र' में चित्तवृत्ति के निरोध को योग कहा गया है। इसके दो अर्थ हैं, एक तो यह कि-व्यक्ति अपनी स्वभावत: या प्रकृतित: चंचल मनोदशात्रों के बिखराव को रोक कर उन्हें इष्टविषय पर केन्द्रित करे, दूसरे यह कि मनोवृत्तियों का दमन किया जाए क्योंकि वे जब तक हैं, तब तक चेतना को केन्द्रीकृतएकाग्र नहीं होने देतीं और अपनी संतुष्टि के लिए वे चेतना या प्रात्मा को पथभ्रष्ट करती हैं या उसे इन्द्रियज-अनुभवों या शब्दस्पर्श रूप-रस और गंध के विषयों में लगाए रहती हैं, उसे स्वस्थ या अपना अवलोकन नहीं करने देतीं। चूंकि योगशास्त्रों में, एक मत से पिण्ड और ब्रह्माण्ड की एकता मानी जाती है, अतः पिण्ड में यानी प्रत्येक प्राणी में, जो ब्रह्माण्ड भर की शक्ति है-कास्मिकपावर छिपा हुग्रा है, उसे विकसित या रूपान्तरित करने में मुख्य बाधा वृत्तियां (Moods) डालती हैं प्रतः वत्तिदाह, वत्तिनिरोध ही योग है। इन वृत्तियों में प्रवृत्तियां (Instincts) भी प्रकट होती हैं।
योग का यह स्वरूप वैदिक, जैन तथा बौद्ध (प्रारम्भिक या हीनयान) योगशास्त्रों में सर्वमान्य है किन्तु तान्त्रिक योगशास्त्रों में योग की उक्त परिभाषा से बिल्कुल उल्टी परिभाषा और अभ्यास (साधना) स्वीकृत है। तन्त्रयोग यानी वाममार्गी शैव-शाक्त-बौद्ध प्रागमों में वज्रयान-सहजयान और शाक्तशास्त्रों में, अभिनवगुप्त के तन्त्रालोक में, वामयोगानुसार योग का वृत्तिनिरोध या वृत्तिदमन अग्राह्य है क्योंकि इसमें प्रकृति प्रदत्त जो वृत्तियां हैं, उनके दमन या दाह या विनाश का उपदेश है जो मनोविज्ञान के विरुद्ध है। तान्त्रिकयोग, मनोवैज्ञानिक है यानी वह प्रकृति द्वारा प्राप्त किसी भी वस्तु या वृत्ति को अकल्याणक नहीं मानता । प्रकृति को तान्त्रिकयोगी शक्ति या चिति का स्थल रूप मानते हैं । अतः ये जो वत्तियाँ हैं, प्रवृत्तियाँ, इच्छाएँ और मनोदशाएँ, मूड्स, ये प्रकृति ने मनुष्य को दी हैं उसके मंगल के लिए, उसके विकास और मुक्ति के लिए, लेकिन उसे उनका सदुपयोग पाना चाहिए ।
क्योंकि तांत्रिकों के अनुसार ब्रह्माण्ड शिव है--शरीरं त्वं शम्भोः, अतः प्रकृति के निरोध का अर्थ दमन नहीं रूपान्तरण होना चाहिए, उदात्तीकरण । इसीलिए कहा गया है
__"यत्र यत्र मनो याति, तत्र तत्रैव धारयेत्" । जहां-जहाँ मन जाए, वहाँ उसे रोको। मन को या वत्तियों को दबायो मत, उनको साधो, उन्हें बदलो, उनको मूलसत्ता या प्रकृति का स्वाभाविक स्पन्दन या (Movement) मान कर, उन्हें उनके विषयों में लगाओ और स्वयं भीतर से तटस्थ रहना सीखो तो ये जो वृत्तियां हैं, स्वत: चांचल्य छोड़ कर चेतना को ऊर्वीकृत कर देगी और जो वृत्तियाँ पतन का कारण समझी जाती हैं, वे मुक्ति का कारण बन जाएंगी।
मधुर ध्वनि सुनने की इच्छा स्वाभाविक है, इसका दमन न करो। ध्वनिमाधुर्य में यदि किसी व्यक्ति को प्रानन्द प्राता है तो उसमें तल्लीन हो जानो किन्तु उस प्रक्रिया में,
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org