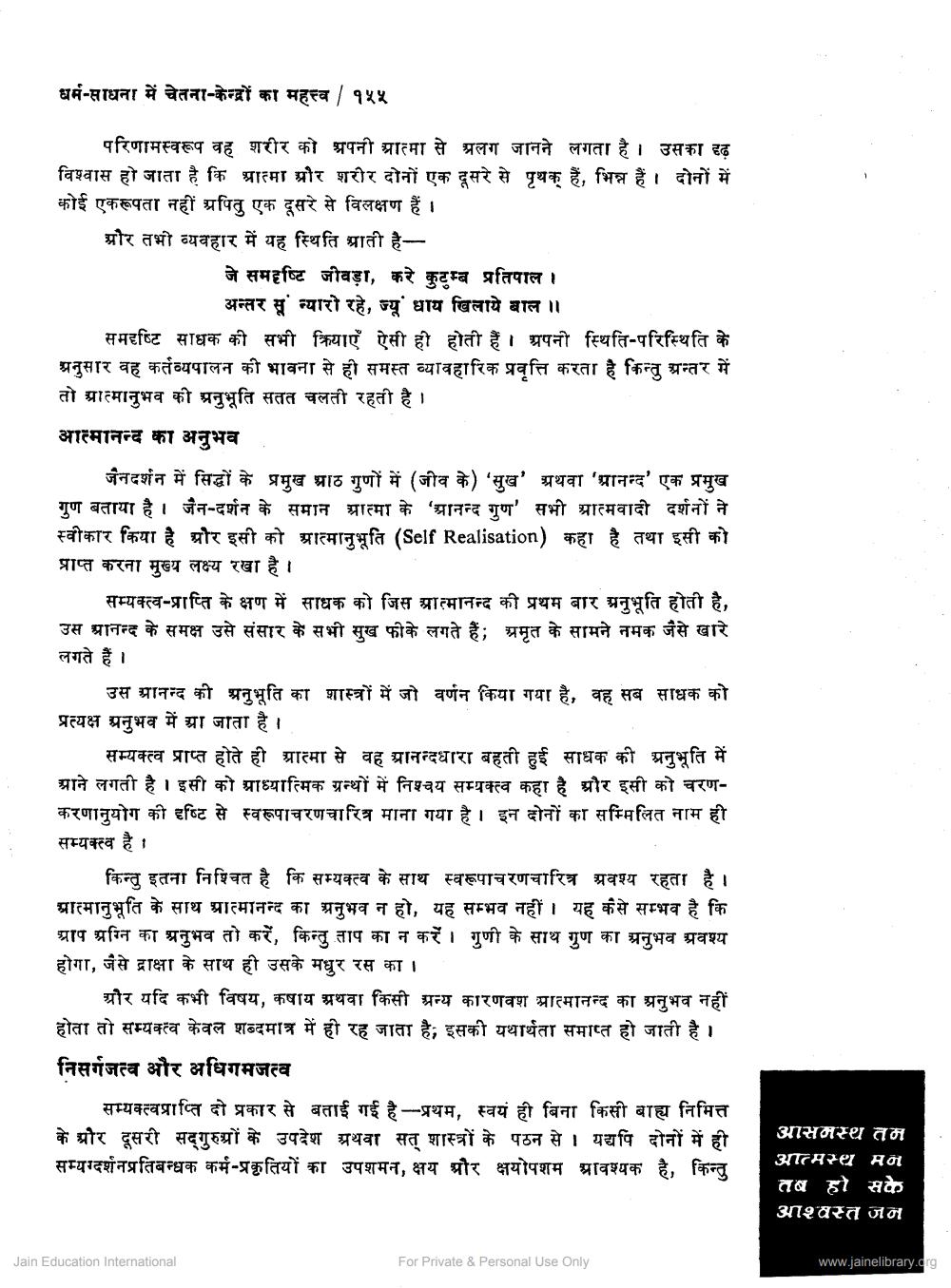________________
धर्म-साधना में चेतना-केन्द्रों का महत्त्व | १५५
परिणामस्वरूप वह शरीर को अपनी प्रात्मा से अलग जानने लगता है। उसका दृढ़ विश्वास हो जाता है कि प्रात्मा और शरीर दोनों एक दूसरे से पृथक हैं, भिन्न हैं। दोनों में कोई एकरूपता नहीं अपितु एक दूसरे से विलक्षण हैं। और तभी व्यवहार में यह स्थिति आती है
जे समदृष्टि जीवड़ा, करे कुटुम्ब प्रतिपाल ।
___ अन्तर सून्यारो रहे, ज्यू धाय खिलाये बाल ॥ समष्टि साधक की सभी क्रियाएँ ऐसी ही होती हैं। अपनी स्थिति-परिस्थिति के अनुसार वह कर्तव्यपालन की भावना से ही समस्त व्यावहारिक प्रवृत्ति करता है किन्तु अन्तर में तो प्रात्मानुभव की अनुभूति सतत चलती रहती है। आत्मानन्द का अनुभव
जनदर्शन में सिद्धों के प्रमुख पाठ गुणों में (जीव के) 'सुख' अथवा 'पानन्द' एक प्रमुख गुण बताया है। जैन-दर्शन के समान प्रात्मा के 'मानन्द गुण' सभी प्रात्मवादी दर्शनों ने स्वीकार किया है और इसी को प्रात्मानुभूति (Self Realisation) कहा है तथा इसी को प्राप्त करना मुख्य लक्ष्य रखा है।
सम्यक्त्व-प्राप्ति के क्षण में साधक को जिस आत्मानन्द की प्रथम बार अनुभूति होती है, उस आनन्द के समक्ष उसे संसार के सभी सुख फीके लगते हैं; अमृत के सामने नमक जैसे खारे लगते हैं।
उस आनन्द की अनुभूति का शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है, वह सब साधक को प्रत्यक्ष अनुभव में आ जाता है।
सम्यक्त्व प्राप्त होते ही प्रात्मा से वह प्रानन्दधारा बहती हुई साधक की अनुभूति में आने लगती है। इसी को आध्यात्मिक ग्रन्थों में निश्चय सम्यक्त्व कहा है और इसी को चरणकरणानुयोग की दृष्टि से स्वरूपाचरणचारित्र माना गया है। इन दोनों का सम्मिलित नाम ही सम्यक्त्व है।
किन्तु इतना निश्चित है कि सम्यक्त्व के साथ स्वरूपाचरणचारित्र अवश्य रहता है। प्रात्मानुभूति के साथ प्रात्मानन्द का अनुभव न हो, यह सम्भव नहीं। यह कैसे सम्भव है कि पाप अग्नि का अनुभव तो करें, किन्तु ताप का न करें। गुणी के साथ गुण का अनुभव अवश्य होगा, जैसे द्राक्षा के साथ ही उसके मधुर रस का।
और यदि कभी विषय, कषाय अथवा किसी अन्य कारणवश आत्मानन्द का अनुभव नहीं होता तो सम्यक्त्व केवल शब्दमात्र में ही रह जाता है। इसकी यथार्थता समाप्त हो जाती है। निसर्गजत्व और अधिगमजत्व
सम्यक्त्वप्राप्ति दो प्रकार से बताई गई है-प्रथम, स्वयं ही बिना किसी बाह्य निमित्त के और दूसरी सद्गुरुपों के उपदेश अथवा सत् शास्त्रों के पठन से । यद्यपि दोनों में ही सम्यग्दर्शनप्रतिबन्धक कर्म-प्रकृतियों का उपशमन, क्षय और क्षयोपशम प्रावश्यक है, किन्तु
आसमस्थ तम आत्मस्थ मन तब हो सके आश्वस्त जन
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org