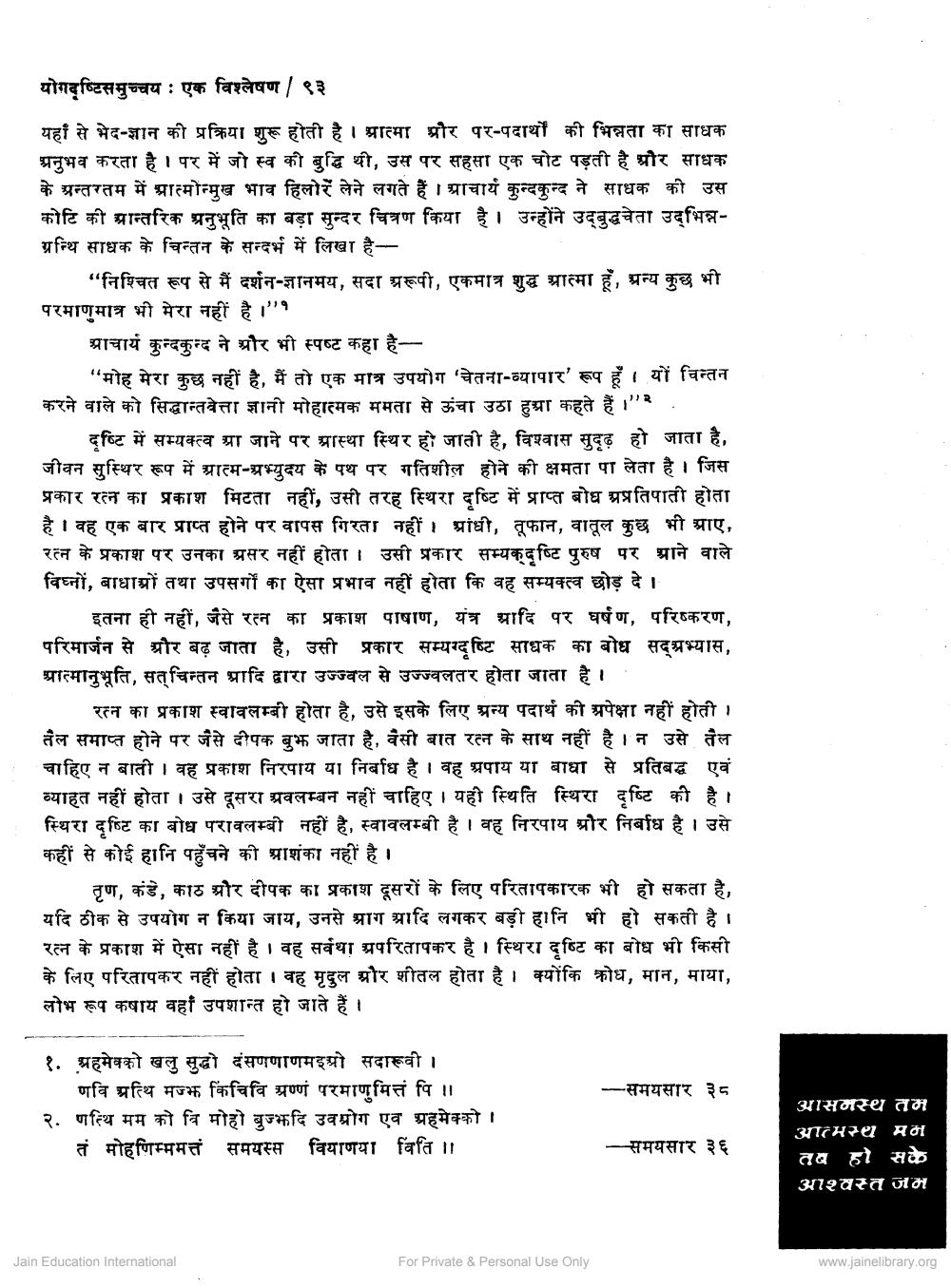________________
योगदृष्टिसमुच्चय : एक विश्लेषण / ९३
यहाँ से भेद-ज्ञान की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रात्मा और पर-पदार्थों की भिन्नता का साधक अनुभव करता है। पर में जो स्व की बुद्धि थी, उस पर सहसा एक चोट पड़ती है और साधक के अन्तरतम में प्रात्मोन्मुख भाव हिलोरें लेने लगते हैं। प्राचार्य कुन्दकुन्द ने साधक की उस कोटि की प्रान्तरिक अनुभूति का बड़ा सून्दर चित्रण किया है। उन्होंने उद्बुद्धचेता उभिन्नग्रन्थि साधक के चिन्तन के सन्दर्भ में लिखा है
"निश्चित रूप से मैं दर्शन-ज्ञानमय, सदा अरूपी, एकमात्र शुद्ध प्रात्मा हूँ, अन्य कुछ भी परमाणुमात्र भी मेरा नहीं है।"१
प्राचार्य कुन्दकुन्द ने और भी स्पष्ट कहा है
"मोह मेरा कुछ नहीं है, मैं तो एक मात्र उपयोग 'चेतना-व्यापार' रूप हूँ। यों चिन्तन करने वाले को सिद्धान्तवेत्ता ज्ञानी मोहात्मक ममता से ऊंचा उठा हुअा कहते हैं।"३ .
दृष्टि में सम्यक्त्व प्रा जाने पर आस्था स्थिर हो जाती है, विश्वास सुदृढ़ हो जाता है, जीवन सुस्थिर रूप में प्रात्म-अभ्युदय के पथ पर गतिशील होने की क्षमता पा लेता है। जिस प्रकार रत्न का प्रकाश मिटता नहीं, उसी तरह स्थिरा दष्टि में प्राप्त बोध अप्रतिपाती होता है । वह एक बार प्राप्त होने पर वापस गिरता नहीं। प्रांधी, तूफान, वातूल कुछ भी आए, रत्न के प्रकाश पर उनका असर नहीं होता। उसी प्रकार सम्यकदृष्टि पुरुष पर पाने वाले विघ्नों, बाधाओं तथा उपसर्गों का ऐसा प्रभाव नहीं होता कि वह सम्यक्त्व छोड़ दे।।
इतना ही नहीं, जैसे रत्न का प्रकाश पाषाण, यंत्र आदि पर घर्षण, परिष्करण, परिमार्जन से और बढ़ जाता है. उसी प्रकार सम्यग्दष्टि साधक का बोध सदनभ्य आत्मानुभूति, सतचिन्तन प्रादि द्वारा उज्ज्वल से उज्ज्वलतर होता जाता है।
रत्न का प्रकाश स्वावलम्बी होता है, उसे इसके लिए अन्य पदार्थ की अपेक्षा नहीं होती। तैल समाप्त होने पर जैसे दीपक बुझ जाता है, वैसी बात रत्न के साथ नहीं है । न उसे तैल चाहिए न बाती। वह प्रकाश निरपाय या निर्बाध है । वह अपाय या बाधा से प्रतिबद्ध एवं व्याहत नहीं होता। उसे दूसरा अवलम्बन नहीं चाहिए । यही स्थिति स्थिरा दृष्टि की है। स्थिरा दृष्टि का बोध परावलम्बी नहीं है, स्वावलम्बी है । वह निरपाय और निर्बाध है। उसे कहीं से कोई हानि पहुँचने की आशंका नहीं है।
तृण, कंडे, काठ और दीपक का प्रकाश दूसरों के लिए परितापकारक भी हो सकता है, यदि ठीक से उपयोग न किया जाय, उनसे आग आदि लगकर बड़ी हानि भी हो सकती है। रत्न के प्रकाश में ऐसा नहीं है। वह सर्वथा अपरितापकर है। स्थिरा दृष्टि का बोध भी किसी के लिए परितापकर नहीं होता । वह मृदुल और शीतल होता है। क्योंकि क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कषाय वहाँ उपशान्त हो जाते हैं।
-समयसार ३८
१. अहमेवको खलु सुद्धो दंसणणाणमइयो सदारूवी।
णवि अस्थि मज्झ किचिवि अण्णं परमाणु मित्तं पि ।। २. णस्थि मम को वि मोहो बुज्झदि उवप्रोग एव अहमेक्को ।
तं मोहणिम्ममत्तं समयस्स वियाणया विति ।।
-समयसार ३६
आसनस्थ तम आत्मस्थ मम तब हो सके आश्वस्त जम
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org