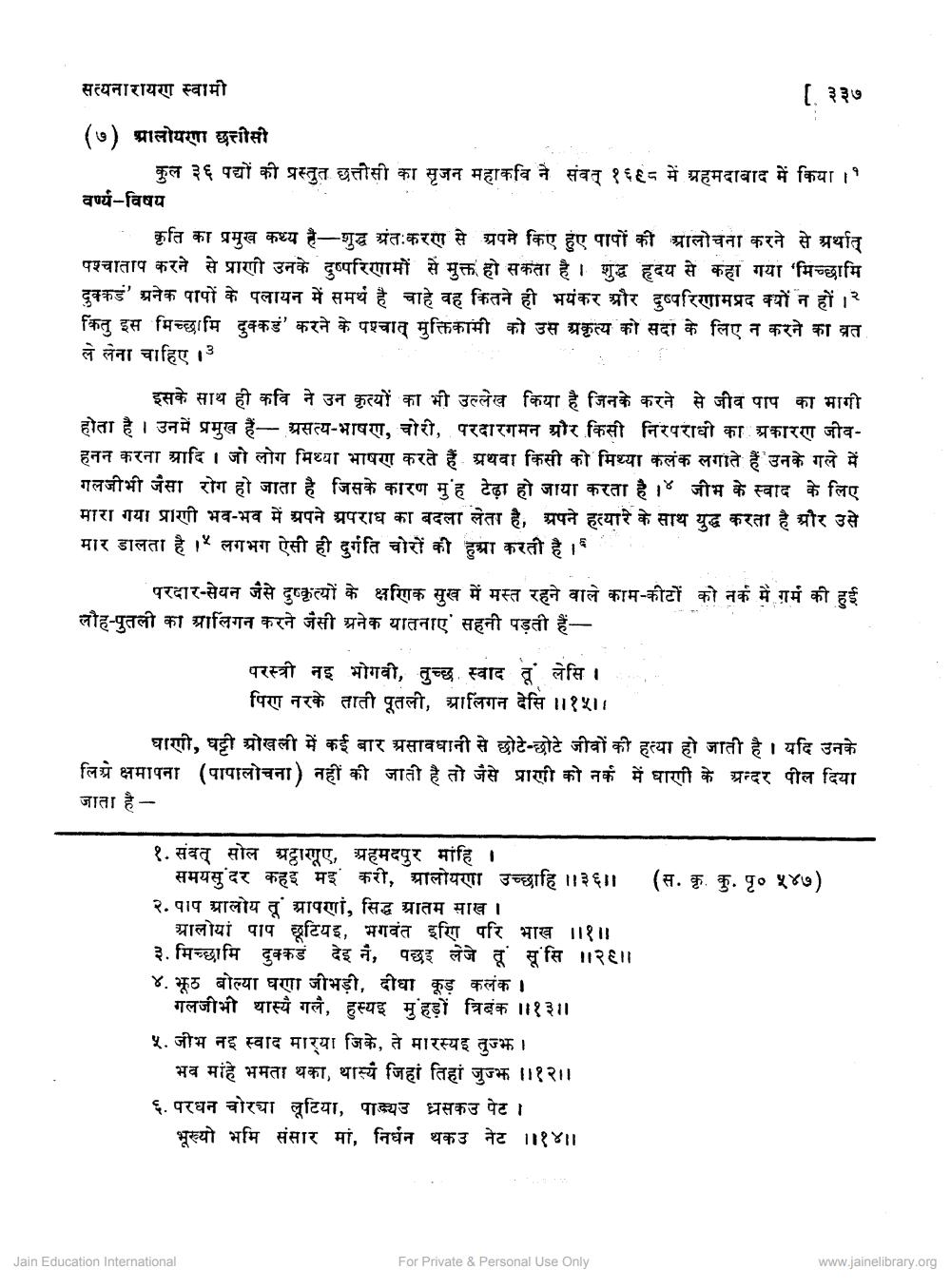________________
सत्यनारायण स्वामी
(७) श्रालोयरणा छत्तीसी
कुल ३६ पद्यों की प्रस्तुत छत्तीसी का सृजन महाकवि ने संवत् १९२६ में महमदाबाद में किया।"
वर्ण्य विषय
कृति का प्रमुख कथ्य है-शुद्ध अंतःकरण से अपने किए हुए पापों की आलोचना करने से अर्थात् पश्चाताप करने से प्राणी उनके दुष्परिणामों से मुक्त हो सकता है। शुद्ध हृदय से कहा गया 'मिच्छामि दुक्कड' अनेक पापों के पलायन में समर्थ है चाहे वह कितने ही भयंकर और दुष्परिणामप्रद क्यों न हों। २ किंतु इस मिच्छामि दुक्कडं' करने के पश्चात् मुक्तिकामी को उस प्रकृत्य को सदा के लिए न करने का व्रत ले लेना चाहिए।"
इसके साथ ही कवि ने उन कृत्यों का भी उल्लेख किया है जिनके करने से जीव पाप का भागी होता है । उनमें प्रमुख हैं— असत्य भाषण, चोरी, परदारगमन और किसी निरपराधी का प्रकारण जीवहनन करना आदि । जो लोग मिथ्या भाषण करते हैं प्रथवा किसी को मिथ्या कलंक लगाते हैं उनके गले में गलजीभी जैसा रोग हो जाता है जिसके कारण मुंह टेढ़ा हो जाया करता है। * जीम के स्वाद के लिए मारा गया प्राणी भव भव में अपने अपराध का बदला लेता है, अपने हत्यारे के साथ युद्ध करता है और उसे मार डालता है । लगभग ऐसी ही दुर्गति चोरों की हुआ करती है ।'
६
परदार- सेवन जैसे दुष्कृत्यों के क्षणिक सुख में मस्त रहने वाले काम-कीटों को नर्क में गर्म की हुई जीह-पुतली का प्रालिंगन करने जैसी अनेक यातनाएं सहनी पड़ती है
परस्त्री नइ भोगवी, तुच्छ स्वाद तू लेसि । पिण नरके ताती पूतली, आलिंगन देसि ॥। १५ ।।
[ ३३७
धारणी, घट्टी प्रोखली में कई बार असावधानी से छोटे-छोटे जीवों की हत्या हो जाती है । यदि उनके लिये क्षमापना (पापालोचना) नहीं की जाती है तो जैसे में धारणी के अन्दर पील दिया जाता है
प्राणी को नर्क
,
१. संवत् सोल अट्टाए, अहमदपुर मांहि । समयसुंदर कहई मद करी पालोयरणा उच्छाहि ||३६| २. पाप पालोय तू आपणां सिद्ध प्रातम साल घालोयां पाप छूटिबद्द भगवंत इरि परि भाख ॥१॥ ३. मिच्छामि दुक्कड़े देइ नै पद लेजे तू सि ॥२६॥
४. झूठ बोल्या पणा जीभड़ी, दीघा कूड़ कलंक | गलजीभी थास्यै गलै, हुस्यइ मुंहड़ों त्रिबंक ||१३||
५. जीभ नह स्वाद मार्या जिके ते मारस्यइ तुज्झ ।
भव मांहे भमता थका, थास्यं जिहां तिहां जुज्झ ।।१२।। ६. परधन चोरचा लूटिया, पाठ्यउ धसकउ पेट | भूस्यो भमि संसार मां, निर्धन
थकत नेट ।।१४।।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
( स. कृ. कु. पृ० ५४७ )
www.jainelibrary.org