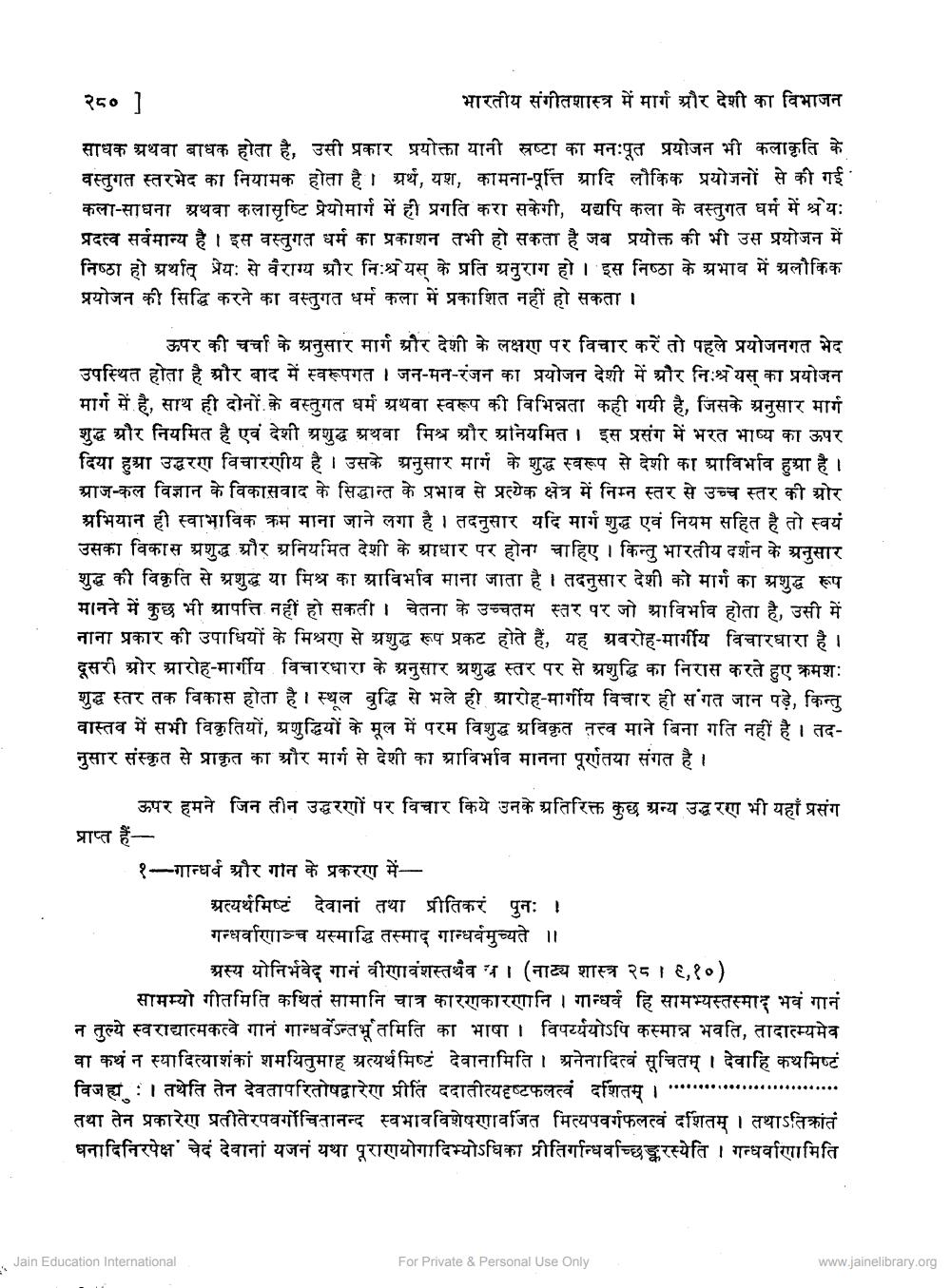________________
२८० ]
भारतीय संगीतशास्त्र में मार्ग और देशी का विभाजन
साधक अथवा बाधक होता है, उसी प्रकार प्रयोक्ता यानी स्रष्टा का मनःपूत प्रयोजन भी कलाकृति के वस्तुगत स्तरभेद का नियामक होता है। अर्थ, यश, कामना-पूत्ति आदि लौकिक प्रयोजनों से की गई कला-साधना अथवा कलासृष्टि प्रेयोमार्ग में ही प्रगति करा सकेगी, यद्यपि कला के वस्तुगत धर्म में श्रेयः प्रदत्व सर्वमान्य है। इस वस्तुगत धर्म का प्रकाशन तभी हो सकता है जब प्रयोक्त की भी उस प्रयोजन में निष्ठा हो अर्थात् प्रेयः से वैराग्य और निःश्रेयस् के प्रति अनुराग हो। इस निष्ठा के अभाव में अलौकिक प्रयोजन की सिद्धि करने का वस्तुगत धर्म कला में प्रकाशित नहीं हो सकता।
ऊपर की चर्चा के अनुसार मार्ग और देशी के लक्षण पर विचार करें तो पहले प्रयोजनगत भेद उपस्थित होता है और बाद में स्वरूपगत । जन-मन-रंजन का प्रयोजन देशी में और निःश्रेयस का प्रयोजन मार्ग में है, साथ ही दोनों के वस्तुगत धर्म अथवा स्वरूप की विभिन्नता कही गयी है, जिसके अनुसार मार्ग शुद्ध और नियमित है एवं देशी अशुद्ध अथवा मिश्र और अनियमित। इस प्रसंग में भरत भाष्य का ऊपर दिया हा उद्धरण विचारणीय है। उसके अनुसार मार्ग के शूद्ध स्वरूप से देशी का आविर्भाव हया है। आज-कल विज्ञान के विकासवाद के सिद्धान्त के प्रभाव से प्रत्येक क्षेत्र में निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर अभियान ही स्वाभाविक क्रम माना जाने लगा है। तदनुसार यदि मार्ग शुद्ध एवं नियम सहित है तो स्वयं उसका विकास अशुद्ध और अनियमित देशी के आधार पर होना चाहिए। किन्तु भारतीय दर्शन के अनुसार शुद्ध की विकृति से अशुद्ध या मिश्र का आविर्भाव माना जाता है। तदनुसार देशी को मार्ग का अशुद्ध रूप मानने में कुछ भी आपत्ति नहीं हो सकती। चेतना के उच्चतम स्तर पर जो आविर्भाव होता है, उसी में नाना प्रकार की उपाधियों के मिश्रण से अशुद्ध रूप प्रकट होते हैं, यह अवरोह-मार्गीय विचारधारा है । दूसरी ओर आरोह-मार्गीय विचारधारा के अनुसार अशुद्ध स्तर पर से अशुद्धि का निरास करते हए क्रमशः शुद्ध स्तर तक विकास होता है। स्थूल बुद्धि से भले ही आरोह-मार्गीय विचार ही संगत जान पड़े, किन्तु वास्तव में सभी विकृतियों, अशुद्धियों के मूल में परम विशुद्ध अविकृत तत्त्व माने बिना गति नहीं है । तदनुसार संस्कृत से प्राकृत का और मार्ग से देशी का आविर्भाव मानना पूर्णतया संगत है।
ऊपर हमने जिन तीन उद्धरणों पर विचार किये उनके अतिरिक्त कुछ अन्य उद्धरण भी यहाँ प्रसंग प्राप्त हैं१-गान्धर्व और गोन के प्रकरण में
प्रत्यर्थमिष्टं देवानां तथा प्रीतिकरं पुनः । गन्धर्वाणाञ्च यस्माद्धि तस्माद् गान्धर्वमुच्यते ॥
अस्य योनिर्भवेद गानं वीणावंशस्तथैव च। (नाट्य शास्त्र २८ । ६,१०) सामम्यो गीतमिति कथितं सामानि चात्र कारणकारणानि । गान्धर्व हि सामभ्यस्तस्माद् भवं गानं न तुल्ये स्वराद्यात्मकत्वे गानं गान्धर्वेऽन्तर्भूतमिति का भाषा। विपर्ययोऽपि कस्मान्न भवति, तादात्म्यमेव वा कथं न स्यादित्याशंकां शमयितुमाह अत्यर्थ मिष्टं देवानामिति । अनेनादित्वं सूचितम् । देवाहि कथमिष्टं विज ह्य : । तथेति तेन देवतापरितोषद्वारेण प्रीतिं ददातीत्यदृष्टफलत्वं दर्शितम् । ................" तथा तेन प्रकारेण प्रतीतेरपवर्गोचितानन्द स्वभावविशेषणावजित मित्यपवर्गफलत्वं दर्शितम् । तथाऽतिक्रांतं धनादिनिरपेक्ष चेदं देवानां यजनं यथा पूरागयोगादिभ्योऽधिका प्रीतिर्गान्धर्वाच्छङ्करस्येति । गन्धर्वारणामिति
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org