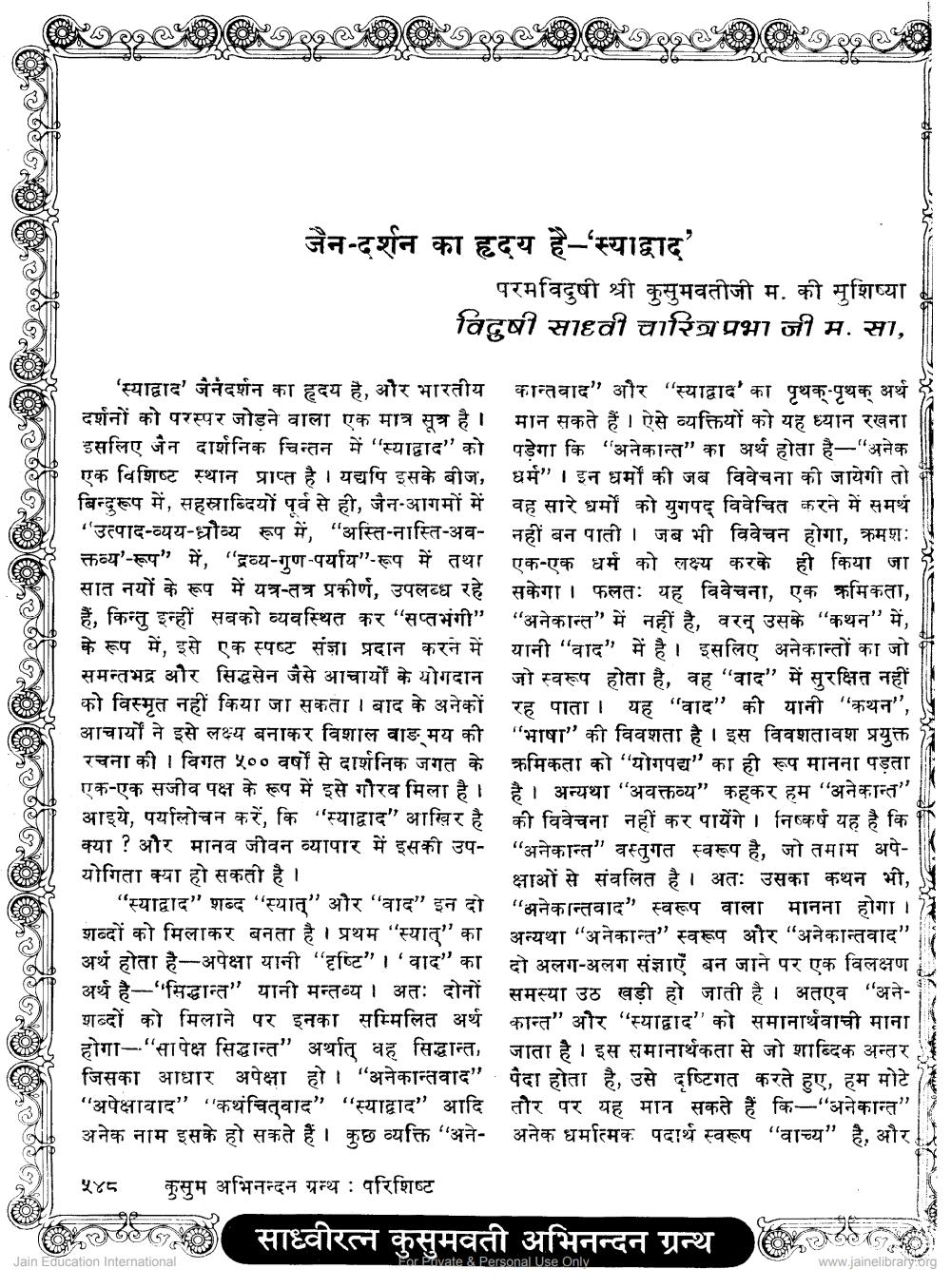________________
जैन-दर्शन का हृदय है-'स्याद्वाद'
परमविदुषी श्री कुसुमवतीजी म. की सुशिष्या । विदुषी साध्वी चारित्र प्रभा जी म. सा,
0000000000000000000
'स्याद्वाद' जनदर्शन का हृदय है, और भारतीय कान्तवाद" और "स्याद्वाद' का पृथक्-पृथक् अर्थ दर्शनों को परस्पर जोड़ने वाला एक मात्र सूत्र है। मान सकते हैं । ऐसे व्यक्तियों को यह ध्यान रखना इसलिए जैन दार्शनिक चिन्तन में "स्याद्वाद" को पडेगा कि "अनेकान्त" का अर्थ होता
नेकान्त" का अर्थ होता है-"अनेक ॥ एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। यद्यपि इसके बीज, धर्म" | इन धर्मों की जब विवेचना की जायेगी तो बिन्दुरूप में, सहस्राब्दियों पूर्व से ही, जैन-आगमों में वह सारे धर्मों को युगपद् विवेचित करने में समर्थ "उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य रूप में, "अस्ति-नास्ति-अव- नहीं बन पाती। जब भी विवेचन होगा, क्रमशः क्तव्य'-रूप" में, "द्रव्य-गुण-पर्याय"-रूप में तथा एक-एक धर्म को लक्ष्य करके ही किया जा सात नयों के रूप में यत्र-तत्र प्रकीर्ण, उपलब्ध रहे सकेगा। फलतः यह विवेचना, एक ऋमिकता, | हैं, किन्तु इन्हीं सबको व्यवस्थित कर “सप्तभंगी" "अनेकान्त" में नहीं है, वरन् उसके “कथन" में, || के रूप में, इसे एक स्पष्ट संज्ञा प्रदान करने में यानी "वाद" में है। इसलिए अनेकान्तों का जो | समन्तभद्र और सिद्धसेन जैसे आचार्यों के योगदान जो स्वरूप होता है, वह "वाद" में सुरक्षित नहीं । को विस्मृत नहीं किया जा सकता । बाद के अनेकों रह पाता। यह "वाद" की यानी "कथन", आचार्यों ने इसे लक्ष्य बनाकर विशाल वाङमय की "भाषा" की विवशता है । इस विवशतावश प्रयुक्त रचना की । विगत ५०० वर्षों से दार्शनिक जगत के ऋमिकता को "योगपद्य" का ही रूप मानना पड़ता एक-एक सजीव पक्ष के रूप में इसे गौरव मिला है। है। अन्यथा “अवक्तव्य" कहकर हम "अनेकान्त" आइये, पर्यालोचन करें, कि "स्याद्वाद" आखिर है की विवेचना नहीं कर पायेंगे । निष्कर्ष यह है कि क्या ? और मानव जीवन व्यापार में इसकी उप- "अनेकान्त" वस्तुगत स्वरूप है, जो तमाम अपेयोगिता क्या हो सकती है।
क्षाओं से संवलित है। अतः उसका कथन भी, ___"स्याद्वाद" शब्द "स्यात्" और "वाद" इन दो "अनेकान्तवाद" स्वरूप वाला मानना होगा। शब्दों को मिलाकर बनता है। प्रथम "स्यात्" का अन्यथा “अनेकान्त" स्वरूप और “अनेकान्तवाद" अर्थ होता है-अपेक्षा यानी “दृष्टि"। 'वाद" का दो अलग-अलग संज्ञाएँ बन जाने पर एक विलक्षण अर्थ है-"सिद्धान्त" यानी मन्तव्य । अतः दोनों समस्या उठ खड़ी हो जाती है। अतएव “अनेशब्दों को मिलाने पर इनका सम्मिलित अर्थ कान्त" और "स्याद्वाद" को समानार्थवाची माना! होगा-“सापेक्ष सिद्धान्त" अर्थात् वह सिद्धान्त, जाता है। इस समानार्थकता से जो शाब्दिक अन्तर। जिसका आधार अपेक्षा हो । “अनेकान्तवाद" - पैदा होता है, उसे दृष्टिगत करते हुए, हम मोटे "अपेक्षावाद" "कथंचित्वाद" "स्याद्वाद" आदि तौर पर यह मान सकते हैं कि-"अनेकान्त" अनेक नाम इसके हो सकते हैं। कुछ व्यक्ति "अने- अनेक धर्मात्मक पदार्थ स्वरूप “वाच्य" है, और।
५४८ कुसुम अभिनन्दन ग्रन्थ : परिशिष्ट 06 साध्वीरत्न कुसुमवती अभिनन्दन ग्रन्थ
AB3
Jain Education International
For Puvate & Personal Use Only
www.jainelibrary.org