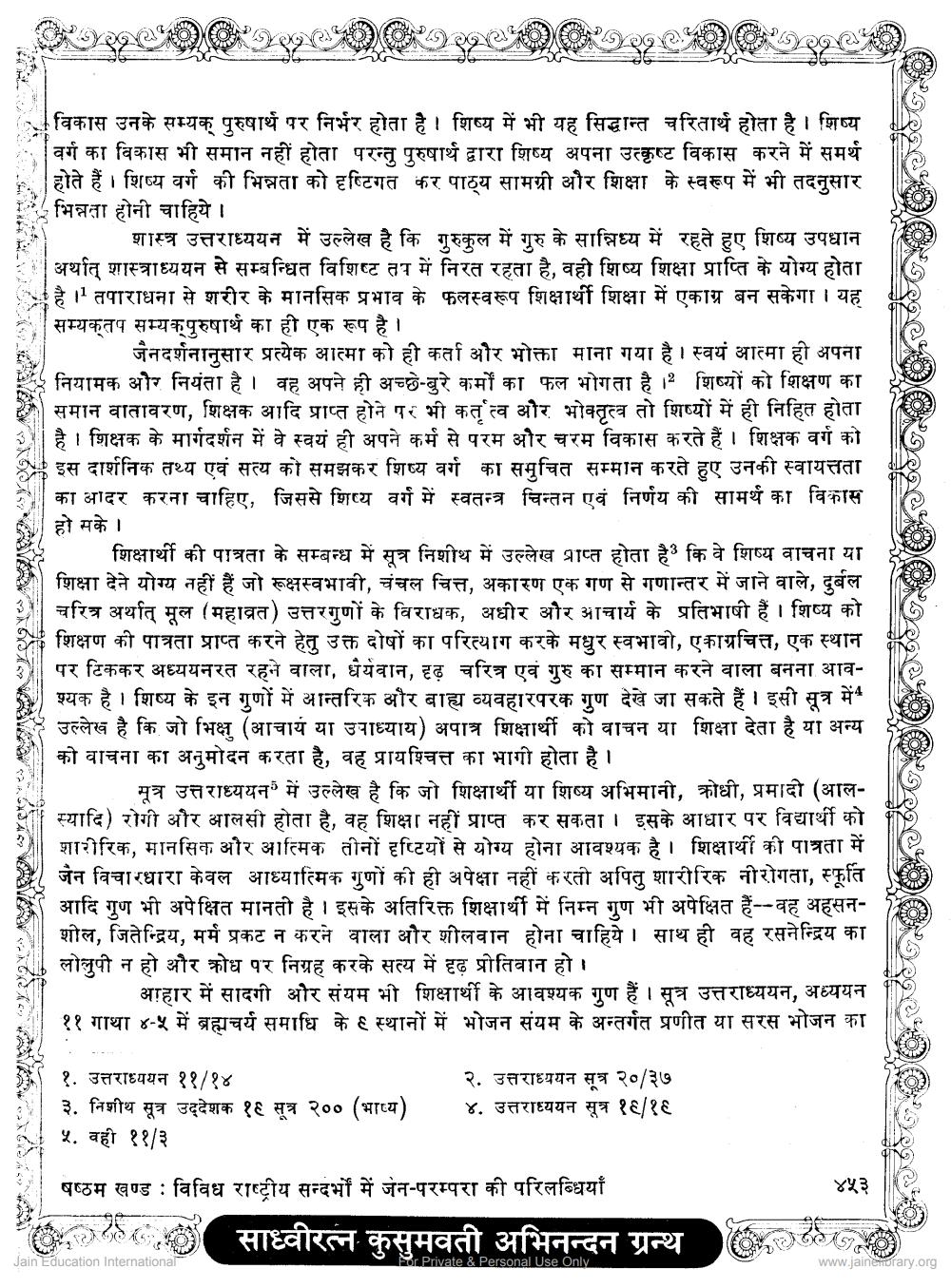________________
विकास उनके सम्यक् पुरुषार्थ पर निर्भर होता है। शिष्य में भी यह सिद्धान्त चरितार्थ होता है । शिष्य वर्ग का विकास भी समान नहीं होता परन्तु पुरुषार्थ द्वारा शिष्य अपना उत्कृष्ट विकास करने में समर्थ होते हैं । शिष्य वर्ग की भिन्नता को दृष्टिगत कर पाठ्य सामग्री और शिक्षा के स्वरूप में भी तदनुसार भिन्नता होनी चाहिये।
शास्त्र उत्तराध्ययन में उल्लेख है कि गुरुकुल में गुरु के सान्निध्य में रहते हुए शिष्य उपधान अर्थात् शास्त्राध्ययन से सम्बन्धित विशिष्ट तप में निरत रहता है, वही शिष्य शिक्षा प्राप्ति के योग्य होता है । तपाराधना से शरीर के मानसिक प्रभाव के फलस्वरूप शिक्षार्थी शिक्षा में एकाग्न बन सकेगा। यह सम्यक्तप सम्यक्पुरुषार्थ का ही एक रूप है।
जैनदर्शनानुसार प्रत्येक आत्मा को ही कर्ता और भोक्ता माना गया है। स्वयं आत्मा ही अपना नियामक और नियंता है। वह अपने ही अच्छे-बुरे कर्मों का फल भोगता है। शिष्यों को शिक्षण का
समान वातावरण, शिक्षक आदि प्राप्त होने पर भी कतत्व और भोक्तृत्व तो शिष्यों में ही निहित होता 37 है। शिक्षक के मार्गदर्शन में वे स्वयं ही अपने कर्म से परम और चरम विकास करते हैं। शिक्षक वर्ग को
इस दार्शनिक तथ्य एवं सत्य को समझकर शिष्य वर्ग का समुचित सम्मान करते हुए उनकी स्वायत्तता का आदर करना चाहिए, जिससे शिष्य वर्ग में स्वतन्त्र चिन्तन एवं निर्णय की सामर्थ का विकास हो सके।
शिक्षार्थी की पात्रता के सम्बन्ध में सत्र निशीथ में उल्लेख प्राप्त होता है कि वे शिष्य वाचना या है। शिक्षा देने योग्य नहीं हैं जो रूक्षस्वभावी, चंचल चित्त, अकारण एक गण से गणान्तर में जाने वाले, दुर्बल
चरित्र अर्थात् मूल (महाव्रत) उत्तरगुणों के विराधक, अधीर और आचार्य के प्रतिभाषी हैं । शिष्य को * शिक्षण की पात्रता प्राप्त करने हेतु उक्त दोषों का परित्याग करके मधुर स्वभावो, एकाग्रचित्त, एक स्थान पर टिककर अध्ययनरत रहने वाला, धैर्यवान, दृढ चरित्र एवं गुरु का सम्मान करने वाला बनना आवश्यक है । शिष्य के इन गुणों में आन्तरिक और बाह्य व्यवहारपरक गुण देखे जा सकते हैं । इसी सूत्र में उल्लेख है कि जो भिक्षु (आचार्य या उपाध्याय) अपात्र शिक्षार्थी को वाचन या शिक्षा देता है या अन्य को वाचना का अनुमोदन करता है, वह प्रायश्चित्त का भागी होता है।
मूत्र उत्तराध्ययन में उल्लेख है कि जो शिक्षार्थी या शिष्य अभिमानी, क्रोधी, प्रमादो (आलस्यादि) रोगी और आलसी होता है, वह शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता। इसके आधार पर विद्यार्थी को BAI शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों दृष्टियों से योग्य होना आवश्यक है। शिक्षार्थी की पात्रता में
जैन विचारधारा केवल आध्यात्मिक गुणों की ही अपेक्षा नहीं करती अपितु शारीरिक नीरोगता, स्फूर्ति आदि गुण भी अपेक्षित मानती है । इसके अतिरिक्त शिक्षार्थी में निम्न गुण भी अपेक्षित हैं--वह अहसनशोल, जितेन्द्रिय, मर्म प्रकट न करने वाला और शीलवान होना चाहिये। साथ ही वह रसनेन्द्रिय का लोलुपी न हो और क्रोध पर निग्रह करके सत्य में दृढ़ प्रीतिवान हो।
आहार में सादगी और संयम भी शिक्षार्थी के आवश्यक गुण हैं । सूत्र उत्तराध्ययन, अध्ययन ११ गाथा ४-५ में ब्रह्मचर्य समाधि के ६ स्थानों में भोजन संयम के अन्तर्गत प्रणीत या सरस भोजन का
SMOKHABHIREM
१. उत्तराध्ययन ११/१४ ३. निशीथ सूत्र उद्देशक १६ सूत्र २०० (भाष्य) ५. वही ११/३
२. उत्तराध्ययन सूत्र २०/३७ ४. उत्तराध्ययन सूत्र १६/१६
षष्ठम खण्ड : विविध राष्ट्रीय सन्दर्भो में जेन-परम्परा की परिलब्धियाँ 07 साध्वीरत्न कुसुमवती अभिनन्दन ग्रन्थ
Jain Education International
stor Private & Personal Use Only
www.jainemorary.org