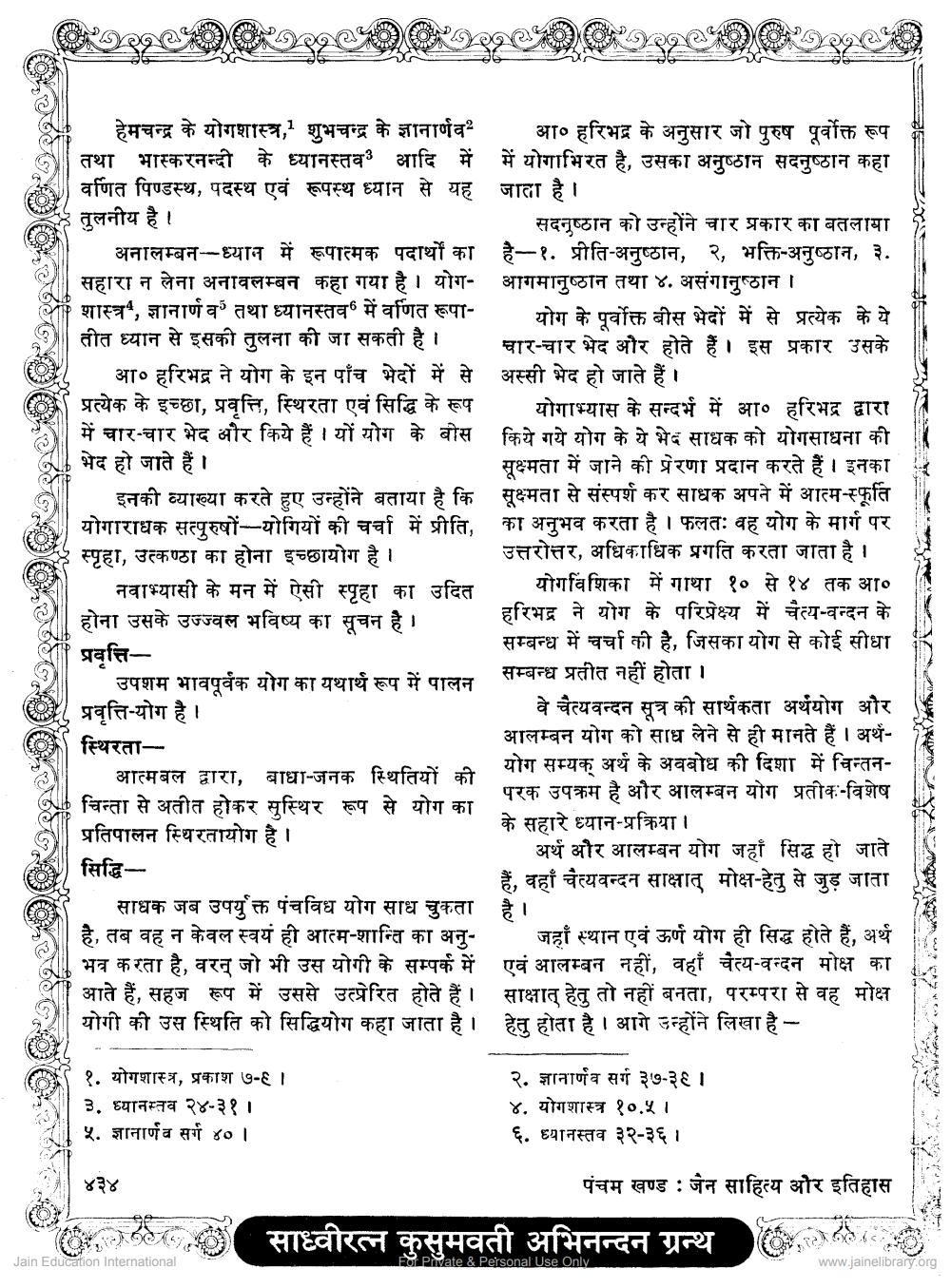________________
हेमचन्द्र के योगशास्त्र, ' शुभचन्द्र के ज्ञानार्णव' तथा भास्करनन्दी के ध्यानस्तव आदि में वर्णित पिण्डस्थ, पदस्थ एवं रूपस्थ ध्यान से यह तुलनीय है ।
अनालम्बन - ध्यान में रूपात्मक पदार्थों का सहारा न लेना अनावलम्बन कहा गया है । योगशास्त्र', ज्ञानार्णव' तथा ध्यानस्तव' में वर्णित रूपातीत ध्यान से इसकी तुलना की जा सकती है ।
० हरिभद्र ने योग के इन पाँच भेदों में से प्रत्येक के इच्छा, प्रवृत्ति, स्थिरता एवं सिद्धि के रूप में चार-चार भेद और किये हैं । यों योग के बीस भेद हो जाते हैं ।
इनकी व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया है कि योगाराधक सत्पुरुषों - योगियों की चर्चा में प्रीति, स्पृहा, उत्कण्ठा का होना इच्छायोग है ।
नवाभ्यासी के मन में ऐसी स्पृहा का उदित होना उसके उज्ज्वल भविष्य का सूचन है । प्रवृत्ति -
उपशम भावपूर्वक योग का यथार्थ रूप में पालन प्रवृत्ति योग है ।
स्थिरता
आत्मबल द्वारा, बाधा जनक स्थितियों की चिन्ता से अतीत होकर सुस्थिर रूप से योग का प्रतिपालन स्थिरतायोग है ।
सिद्धि -
साधक जब उपर्युक्त पंचविध योग साध चुकता है, तब वह न केवल स्वयं ही आत्म-शान्ति का अनुभव करता है, वरन् जो भी उस योगी के सम्पर्क में आते हैं, सहज रूप में उससे उत्प्रेरित होते हैं । योगी की उस स्थिति को सिद्धियोग कहा जाता है ।
१. योगशास्त्र, प्रकाश ७-६ ।
३. ध्यानस्तव २४-३१ । ५. ज्ञानार्णव सर्ग ४० ।
४३४
Jain Education International
० हरिभद्र के अनुसार जो पुरुष पूर्वोक्त रूप में योगाभिरत है, उसका अनुष्ठान सदनुष्ठान कहा जाता है ।
सदनुष्ठान को उन्होंने चार प्रकार का बतलामा है - १. प्रीति- अनुष्ठान, २, भक्ति - अनुष्ठान, ३. आगमानुष्ठान तथा ४. असंगानुष्ठान ।
योग के पूर्वोक्त बीस भेदों में से प्रत्येक के ये चार-चार भेद और होते हैं । इस प्रकार उसके अस्सी भेद हो जाते हैं ।
योगाभ्यास के सन्दर्भ में आ० हरिभद्र द्वारा किये गये योग के ये भेद साधक को योगसाधना की सूक्ष्मता में जाने की प्रेरणा प्रदान करते हैं । इनका सूक्ष्मता से संस्पर्श कर साधक अपने में आत्म-स्फूर्ति का अनुभव करता है । फलतः वह योग के मार्ग पर उत्तरोत्तर, अधिकाधिक प्रगति करता जाता है ।
योगविंशिका में गाथा १० से १४ तक आ० हरिभद्र ने योग के परिप्रेक्ष्य में चैत्य-वन्दन के सम्बन्ध में चर्चा की है, जिसका योग से कोई सीधा सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता ।
वे चैत्यवन्दनसूत्र की सार्थकता अर्थंयोग और आलम्बन योग को साध लेने से ही मानते हैं । अर्थयोग सम्यक् अर्थ के अवबोध की दिशा में चिन्तनपरक उपक्रम है और आलम्बन योग प्रतीक - विशेष के सहारे ध्यान- प्रक्रिया |
अर्थ और आलम्बन योग जहाँ सिद्ध हो जाते हैं, वहाँ चैत्यवन्दन साक्षात् मोक्ष हेतु से जुड़ जाता है ।
जहाँ स्थान एवं ऊर्ण योग ही सिद्ध होते हैं, अर्थ एवं आलम्बन नहीं, वहाँ चैत्य-वन्दन मोक्ष का साक्षात् हेतु तो नहीं बनता, परम्परा से वह मोक्ष हेतु होता है । आगे उन्होंने लिखा है -
२. ज्ञानार्णव सर्ग ३७-३६ ।
४. योगशास्त्र १०.५ ।
६. ध्यानस्तव ३२-३६ ।
पंचम खण्ड : जैन साहित्य और इतिहास
साध्वीरत्न कुसुमवती अभिनन्दन ग्रन्थ
For Private & Personal Use Only
कतिले
www.jainelibrary.org