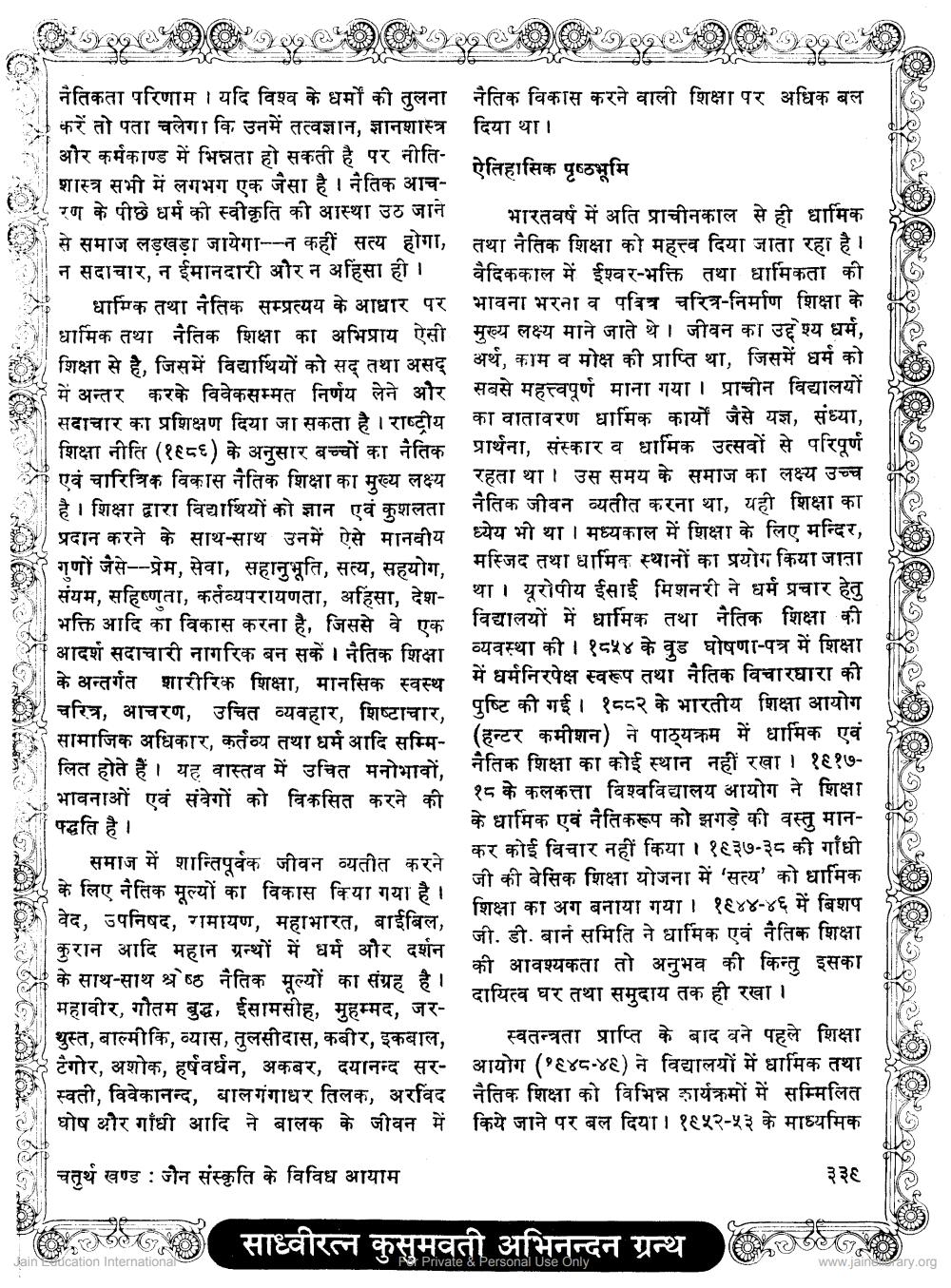________________
नैतिकता परिणाम | यदि विश्व के धर्मों की तुलना करें तो पता चलेगा कि उनमें तत्वज्ञान, ज्ञानशास्त्र और कर्मकाण्ड में भिन्नता हो सकती है पर नीतिशास्त्र सभी में लगभग एक जैसा है। नैतिक आचरण के पीछे धर्म की स्वीकृति की आस्था उठ जाने से समाज लड़खड़ा जायेगा - न कहीं सत्य होगा, न सदाचार, न ईमानदारी और न अहिंसा ही ।
धार्मिक तथा नैतिक सम्प्रत्यय के आधार पर धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा का अभिप्राय ऐसी शिक्षा से है, जिसमें विद्यार्थियों को सद् तथा असद् में अन्तर करके विवेकसम्मत निर्णय लेने और सदाचार का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (१९८६) के अनुसार बच्चों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास नैतिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है । शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों को ज्ञान एवं कुशलता प्रदान करने के साथ-साथ उनमें ऐसे मानवीय 'गुणों जैसे--प्रेम, सेवा, सहानुभूति, सत्य, सहयोग, संयम, सहिष्णुता, कर्तव्यपरायणता, अहिंसा, देशभक्ति आदि का विकास करना है, जिससे वे एक आदर्श सदाचारी नागरिक बन सकें । नैतिक शिक्षा के अन्तर्गत शारीरिक शिक्षा, मानसिक स्वस्थ चरित्र, आचरण, उचित व्यवहार, शिष्टाचार, सामाजिक अधिकार, कर्तव्य तथा धर्म आदि सम्मि - लित होते हैं । यह वास्तव में उचित मनोभावों, भावनाओं एवं संवेगों को विकसित करने की पद्धति है ।
समाज में शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए नैतिक मूल्यों का विकास किया गया है । वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, बाईबिल, कुरान आदि महान ग्रन्थों में धर्म और दर्शन के साथ-साथ श्र ेष्ठ नैतिक मूल्यों का संग्रह है । महावीर, गौतम बुद्ध, ईसामसीह, मुहम्मद, जरथुस्त, बाल्मीकि, व्यास, तुलसीदास, कबीर, इकबाल, टैगोर, अशोक, हर्षवर्धन, अकबर, दयानन्द सरस्वती, विवेकानन्द, बालगंगाधर तिलक, अरविंद घोष और गाँधी आदि ने बालक के जीवन में
चतुर्थ खण्ड : जैन संस्कृति के विविध आयाम
Jain dication International
नैतिक विकास करने वाली शिक्षा पर अधिक बल दिया था ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारतवर्ष में अति प्राचीनकाल से ही धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा को महत्त्व दिया जाता रहा है। वैदिककाल में ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना भरना व पवित्र चरित्र निर्माण शिक्षा के मुख्य लक्ष्य माने जाते थे । जीवन का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति था, जिसमें धर्म को सबसे महत्त्वपूर्ण माना गया। प्राचीन विद्यालयों का वातावरण धार्मिक कार्यों जैसे यज्ञ, संध्या, प्रार्थना, संस्कार व धार्मिक उत्सवों से परिपूर्ण रहता था । उस समय के समाज का लक्ष्य उच्च नैतिक जीवन व्यतीत करना था, यही शिक्षा का ध्येय भी था । मध्यकाल में शिक्षा के लिए मन्दिर, मस्जिद तथा धार्मिक स्थानों का प्रयोग किया जाता था । यूरोपीय ईसाई मिशनरी ने धर्म प्रचार हेतु विद्यालयों में धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की । १८५४ के वुड घोषणा-पत्र में शिक्षा में धर्मनिरपेक्ष स्वरूप तथा नैतिक विचारधारा की पुष्टि की गई । १८८२ के भारतीय शिक्षा आयोग ( हन्टर कमीशन) ने पाठ्यक्रम में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा का कोई स्थान नहीं रखा । १६१७१८ के कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने शिक्षा के धार्मिक एवं नैतिकरूप को झगड़े की वस्तु मानकर कोई विचार नहीं किया । १६३७-३८ की गाँधी जी की बेसिक शिक्षा योजना में 'सत्य' को धार्मिक शिक्षा का अंग बनाया गया । १६४४-४६ में बिशप जी. डी. बार्न समिति ने धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की आवश्यकता तो अनुभव की किन्तु इसका दायित्व घर तथा समुदाय तक ही रखा ।
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद बने पहले शिक्षा आयोग (१९४८-४९ ) ने विद्यालयों में धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा को विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित किये जाने पर बल दिया । १९५२-५३ के माध्यमिक
साध्वीरत्न ग्रन्थ
Private & Personal Use Only
३३६
www.jainsarary.org