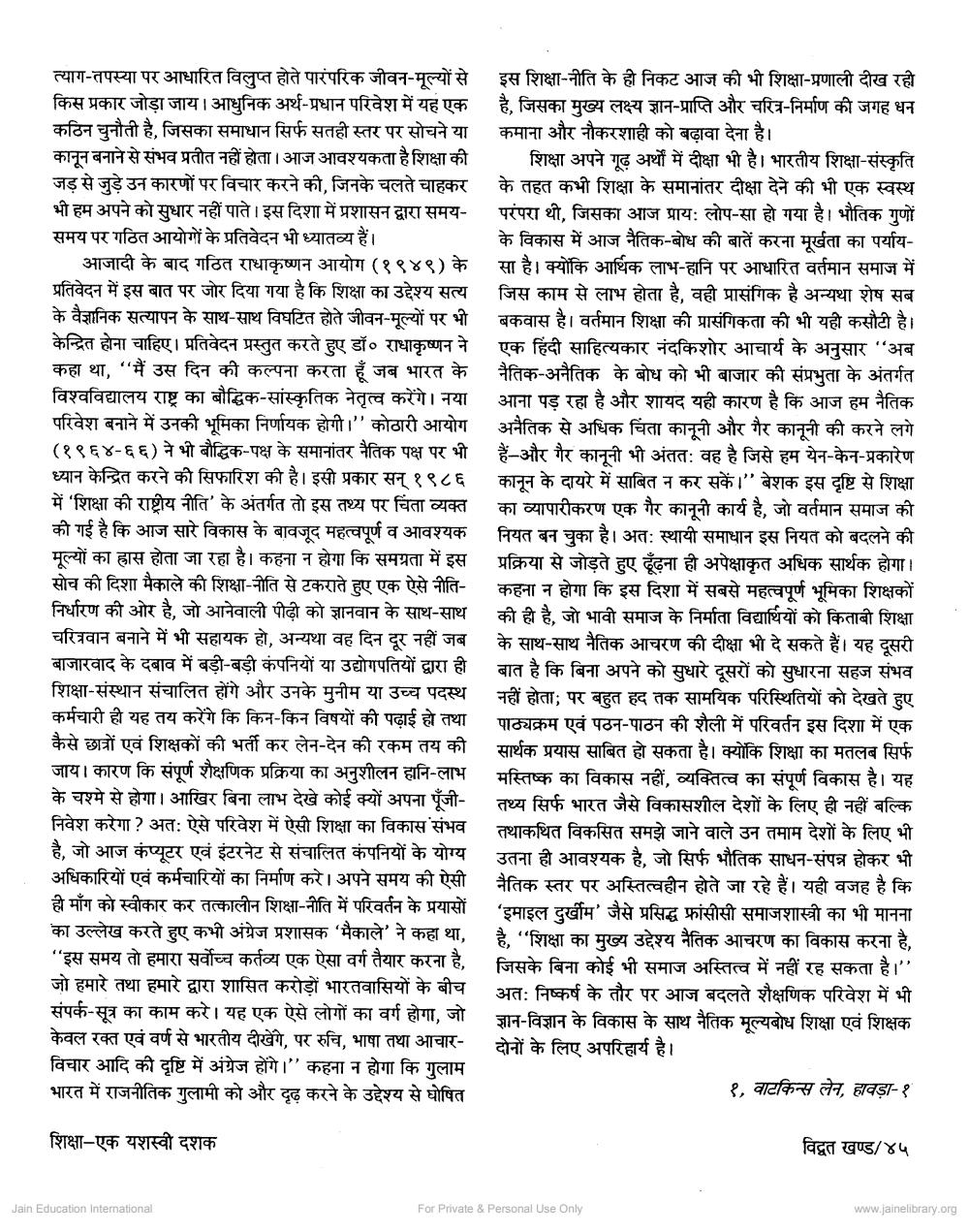________________
त्याग-तपस्या पर आधारित विलुप्त होते पारंपरिक जीवन-मूल्यों से इस शिक्षा-नीति के ही निकट आज की भी शिक्षा-प्रणाली दीख रही किस प्रकार जोड़ा जाय। आधुनिक अर्थ-प्रधान परिवेश में यह एक है, जिसका मुख्य लक्ष्य ज्ञान-प्राप्ति और चरित्र-निर्माण की जगह धन कठिन चुनौती है, जिसका समाधान सिर्फ सतही स्तर पर सोचने या कमाना और नौकरशाही को बढ़ावा देना है। कानून बनाने से संभव प्रतीत नहीं होता।आज आवश्यकता है शिक्षा की शिक्षा अपने गूढ़ अर्थों में दीक्षा भी है। भारतीय शिक्षा-संस्कृति जड़ से जुड़े उन कारणों पर विचार करने की, जिनके चलते चाहकर के तहत कभी शिक्षा के समानांतर दीक्षा देने की भी एक स्वस्थ भी हम अपने को सुधार नहीं पाते। इस दिशा में प्रशासन द्वारा समय- परंपरा थी, जिसका आज प्रायः लोप-सा हो गया है। भौतिक गुणों समय पर गठित आयोगों के प्रतिवेदन भी ध्यातव्य हैं।
के विकास में आज नैतिक-बोध की बातें करना मूर्खता का पर्यायआजादी के बाद गठित राधाकृष्णन आयोग (१९४९) के सा है। क्योंकि आर्थिक लाभ-हानि पर आधारित वर्तमान समाज में प्रतिवेदन में इस बात पर जोर दिया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य सत्य जिस काम से लाभ होता है, वही प्रासंगिक है अन्यथा शेष सब के वैज्ञानिक सत्यापन के साथ-साथ विघटित होते जीवन-मूल्यों पर भी बकवास है। वर्तमान शिक्षा की प्रासंगिकता की भी यही कसौटी है। केन्द्रित होना चाहिए। प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए डॉ० राधाकृष्णन ने एक हिंदी साहित्यकार नंदकिशोर आचार्य के अनुसार “अब कहा था, "मैं उस दिन की कल्पना करता हूँ जब भारत के नैतिक-अनैतिक के बोध को भी बाजार की संप्रभुता के अंतर्गत विश्वविद्यालय राष्ट्र का बौद्धिक-सांस्कृतिक नेतृत्व करेंगे। नया आना पड़ रहा है और शायद यही कारण है कि आज हम नैतिक परिवेश बनाने में उनकी भूमिका निर्णायक होगी।" कोठारी आयोग अनैतिक से अधिक चिंता कानूनी और गैर कानूनी की करने लगे (१९६४-६६) ने भी बौद्धिक-पक्ष के समानांतर नैतिक पक्ष पर भी हैं और गैर कानूनी भी अंतत: वह है जिसे हम येन-केन-प्रकारेण ध्यान केन्द्रित करने की सिफारिश की है। इसी प्रकार सन् १९८६ कानून के दायरे में साबित न कर सकें।" बेशक इस दृष्टि से शिक्षा में 'शिक्षा की राष्ट्रीय नीति' के अंतर्गत तो इस तथ्य पर चिंता व्यक्त का व्यापारीकरण एक गैर कानूनी कार्य है, जो वर्तमान समाज की की गई है कि आज सारे विकास के बावजूद महत्वपूर्ण व आवश्यक नियत बन चुका है। अत: स्थायी समाधान इस नियत को बदलने की मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। कहना न होगा कि समग्रता में इस प्रक्रिया से जोड़ते हुए ढूँढना ही अपेक्षाकृत अधिक सार्थक होगा। सोच की दिशा मैकाले की शिक्षा-नीति से टकराते हुए एक ऐसे नीति- कहना न होगा कि इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षकों निर्धारण की ओर है, जो आनेवाली पीढ़ी को ज्ञानवान के साथ-साथ की ही है, जो भावी समाज के निर्माता विद्यार्थियों को किताबी शिक्षा चरित्रवान बनाने में भी सहायक हो, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब के साथ-साथ नैतिक आचरण की दीक्षा भी दे सकते हैं। यह दूसरी बाजारवाद के दबाव में बड़ी-बड़ी कंपनियों या उद्योगपतियों द्वारा ही बात है कि बिना अपने को सुधारे दूसरों को सुधारना सहज संभव शिक्षा-संस्थान संचालित होंगे और उनके मुनीम या उच्च पदस्थ नहीं होता; पर बहुत हद तक सामयिक परिस्थितियों को देखते हुए कर्मचारी ही यह तय करेंगे कि किन-किन विषयों की पढ़ाई हो तथा पाठ्यक्रम एवं पठन-पाठन की शैली में परिवर्तन इस दिशा में एक कैसे छात्रों एवं शिक्षकों की भर्ती कर लेन-देन की रकम तय की सार्थक प्रयास साबित हो सकता है। क्योंकि शिक्षा का मतलब सिर्फ जाय। कारण कि संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया का अनुशीलन हानि-लाभ । मस्तिष्क का विकास नहीं, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास है। यह के चश्मे से होगा। आखिर बिना लाभ देखे कोई क्यों अपना पूँजी- तथ्य सिर्फ भारत जैसे विकासशील देशों के लिए ही नहीं बल्कि निवेश करेगा? अत: ऐसे परिवेश में ऐसी शिक्षा का विकास संभव तथाकथित विकसित समझे जाने वाले उन तमाम देशों के लिए भी है, जो आज कंप्यूटर एवं इंटरनेट से संचालित कंपनियों के योग्य उतना ही आवश्यक है. जो सिर्फ भौतिक साधन-संपन्न होकर भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का निर्माण करे। अपने समय की ऐसी नैतिक स्तर पर अस्तित्वहीन होते जा रहे हैं। यही वजह है कि ही माँग को स्वीकार कर तत्कालीन शिक्षा-नीति में परिवर्तन के प्रयासों
___'इमाइल दुर्थीम' जैसे प्रसिद्ध फ्रांसीसी समाजशास्त्री का भी मानना का उल्लेख करते हुए कभी अंग्रेज प्रशासक 'मैकाले' ने कहा था, "इस समय तो हमारा सर्वोच्च कर्तव्य एक ऐसा वर्ग तैयार करना है, जिसके बिना कोई भी समाज अस्तित्व में नहीं रह सकता है।" जो हमारे तथा हमारे द्वारा शासित करोड़ों भारतवासियों के बीच अत: निष्कर्ष के तौर पर आज बदलते शैक्षणिक परिवेश में भी संपर्क-सूत्र का काम करे। यह एक ऐसे लोगों का वर्ग होगा, जो ज्ञान-विज्ञान के विकास के साथ नैतिक मल्यबोध शिक्षा एवं शिक्षक केवल रक्त एवं वर्ण से भारतीय दीखेंगे, पर रुचि, भाषा तथा आचार- दोनों के लिए अपरिहार्य है। विचार आदि की दृष्टि में अंग्रेज होंगे।" कहना न होगा कि गुलाम भारत में राजनीतिक गुलामी को और दृढ़ करने के उद्देश्य से घोषित
१, वाटकिन्स लेन, हावड़ा-१
शिक्षा-एक यशस्वी दशक
विद्वत खण्ड/४५
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org