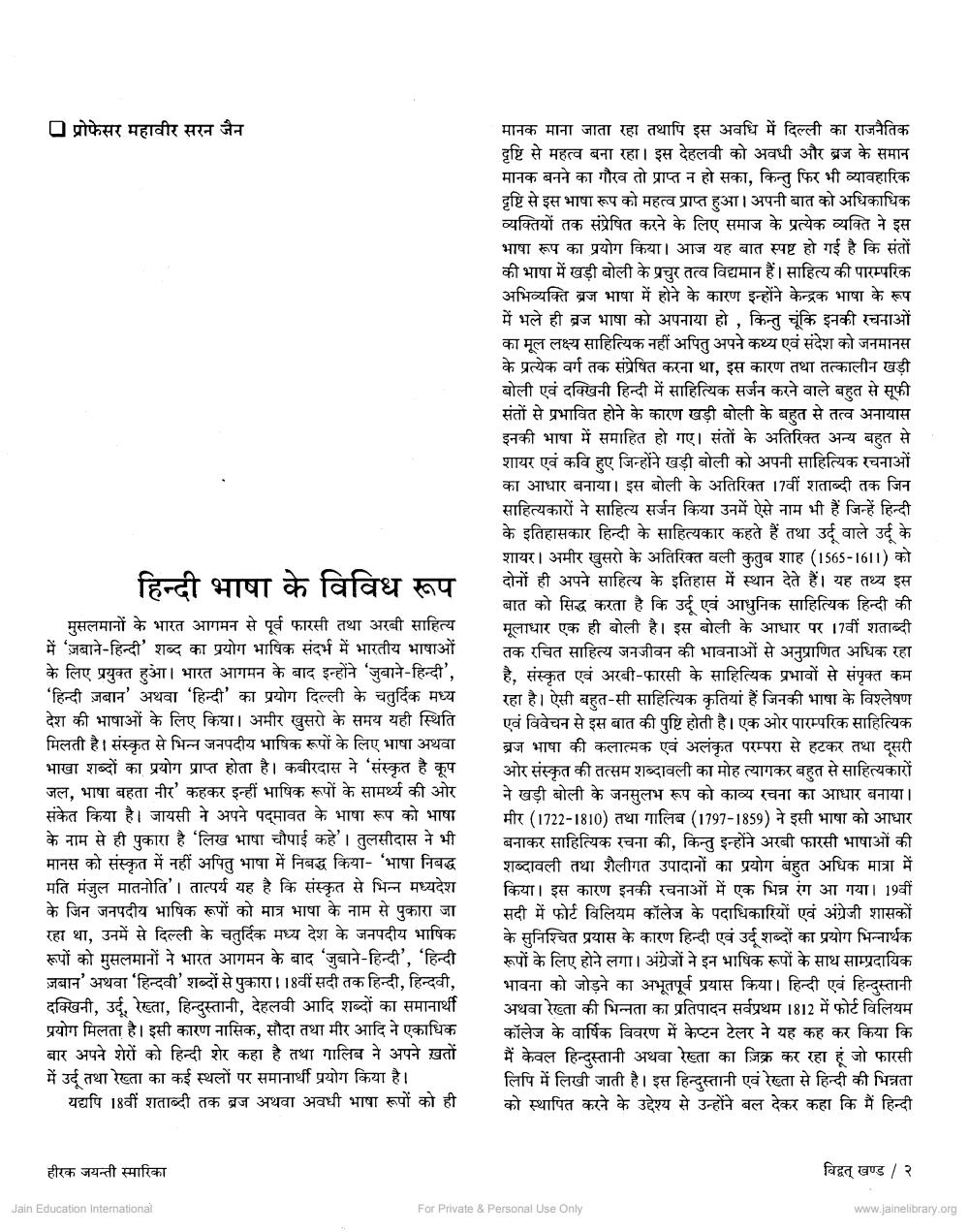________________
प्रोफेसर महावीर सरन जैन
हिन्दी भाषा के विविध रूप मुसलमानों के भारत आगमन से पूर्व फारसी तथा अरबी साहित्य में 'ज़बाने-हिन्दी' शब्द का प्रयोग भाषिक संदर्भ में भारतीय भाषाओं के लिए प्रयुक्त हुआ। भारत आगमन के बाद इन्होंने 'जुबाने-हिन्दी', 'हिन्दी ज़बान' अथवा 'हिन्दी' का प्रयोग दिल्ली के चतुर्दिक मध्य देश की भाषाओं के लिए किया। अमीर खुसरो के समय यही स्थिति मिलती है। संस्कृत से भिन्न जनपदीय भाषिक रूपों के लिए भाषा अथवा भाखा शब्दों का प्रयोग प्राप्त होता है। कबीरदास ने 'संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर' कहकर इन्हीं भाषिक रूपों के सामर्थ्य की ओर संकेत किया है। जायसी ने अपने पद्मावत के भाषा रूप को भाषा के नाम से ही पुकारा है 'लिख भाषा चौपाई कहें'। तुलसीदास ने भी मानस को संस्कृत में नहीं अपितु भाषा में निबद्ध किया- 'भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति'। तात्पर्य यह है कि संस्कृत से भिन्न मध्यदेश के जिन जनपदीय भाषिक रूपों को मात्र भाषा के नाम से पुकारा जा रहा था, उनमें से दिल्ली के चतुर्दिक मध्य देश के जनपदीय भाषिक रूपों को मुसलमानों ने भारत आगमन के बाद 'जुबाने-हिन्दी', 'हिन्दी ज़बान' अथवा 'हिन्दवी' शब्दों से पुकारा। 18वीं सदी तक हिन्दी, हिन्दवी, दक्खिनी, उर्दू, रेख्ता, हिन्दुस्तानी, देहलवी आदि शब्दों का समानार्थी प्रयोग मिलता है। इसी कारण नासिक, सौदा तथा मीर आदि ने एकाधिक बार अपने शेरों को हिन्दी शेर कहा है तथा गालिब ने अपने ख़तों में उर्दू तथा रेख्ता का कई स्थलों पर समानार्थी प्रयोग किया है।
यद्यपि 18वीं शताब्दी तक ब्रज अथवा अवधी भाषा रूपों को ही
मानक माना जाता रहा तथापि इस अवधि में दिल्ली का राजनैतिक दृष्टि से महत्व बना रहा। इस देहलवी को अवधी और ब्रज के समान मानक बनने का गौरव तो प्राप्त न हो सका, किन्तु फिर भी व्यावहारिक दृष्टि से इस भाषा रूप को महत्व प्राप्त हुआ।अपनी बात को अधिकाधिक व्यक्तियों तक संप्रेषित करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने इस भाषा रूप का प्रयोग किया। आज यह बात स्पष्ट हो गई है कि संतों की भाषा में खड़ी बोली के प्रचुर तत्व विद्यमान हैं। साहित्य की पारम्परिक अभिव्यक्ति ब्रज भाषा में होने के कारण इन्होंने केन्द्रक भाषा के रूप में भले ही ब्रज भाषा को अपनाया हो , किन्तु चूंकि इनकी रचनाओं का मूल लक्ष्य साहित्यिक नहीं अपितु अपने कथ्य एवं संदेश को जनमानस के प्रत्येक वर्ग तक संप्रेषित करना था, इस कारण तथा तत्कालीन खड़ी बोली एवं दक्खिनी हिन्दी में साहित्यिक सर्जन करने वाले बहुत से सूफी संतों से प्रभावित होने के कारण खड़ी बोली के बहुत से तत्व अनायास इनकी भाषा में समाहित हो गए। संतों के अतिरिक्त अन्य बहुत से शायर एवं कवि हुए जिन्होंने खड़ी बोली को अपनी साहित्यिक रचनाओं का आधार बनाया। इस बोली के अतिरिक्त 17वीं शताब्दी तक जिन साहित्यकारों ने साहित्य सर्जन किया उनमें ऐसे नाम भी हैं जिन्हें हिन्दी के इतिहासकार हिन्दी के साहित्यकार कहते हैं तथा उर्दू वाले उर्दू के शायर। अमीर खुसरो के अतिरिक्त वली कुतुब शाह (1565-1611) को दोनों ही अपने साहित्य के इतिहास में स्थान देते हैं। यह तथ्य इस बात को सिद्ध करता है कि उर्दू एवं आधुनिक साहित्यिक हिन्दी की मूलाधार एक ही बोली है। इस बोली के आधार पर 17वीं शताब्दी तक रचित साहित्य जनजीवन की भावनाओं से अनुप्राणित अधिक रहा है, संस्कृत एवं अरबी-फारसी के साहित्यिक प्रभावों से संपृक्त कम रहा है। ऐसी बहुत-सी साहित्यिक कृतियां हैं जिनकी भाषा के विश्लेषण एवं विवेचन से इस बात की पुष्टि होती है। एक ओर पारम्परिक साहित्यिक ब्रज भाषा की कलात्मक एवं अलंकृत परम्परा से हटकर तथा दूसरी
ओर संस्कत की तत्सम शब्दावली का मोह त्यागकर बहत से साहित्यकारों ने खड़ी बोली के जनसुलभ रूप को काव्य रचना का आधार बनाया। मीर (1722-1810) तथा गालिब (1797-1859) ने इसी भाषा को आधार बनाकर साहित्यिक रचना की, किन्तु इन्होंने अरबी फारसी भाषाओं की शब्दावली तथा शैलीगत उपादानों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया। इस कारण इनकी रचनाओं में एक भिन्न रंग आ गया। 19वीं सदी में फोर्ट विलियम कॉलेज के पदाधिकारियों एवं अंग्रेजी शासकों के सुनिश्चित प्रयास के कारण हिन्दी एवं उर्दु शब्दों का प्रयोग भिन्नार्थक रूपों के लिए होने लगा। अंग्रेजों ने इन भाषिक रूपों के साथ साम्प्रदायिक भावना को जोड़ने का अभूतपूर्व प्रयास किया। हिन्दी एवं हिन्दुस्तानी अथवा रेख्ता की भिन्नता का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1812 में फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में केप्टन टेलर ने यह कह कर किया कि मैं केवल हिन्दुस्तानी अथवा रेख्ता का ज़िक्र कर रहा हूं जो फारसी लिपि में लिखी जाती है। इस हिन्दुस्तानी एवं रेख्ता से हिन्दी की भिन्नता को स्थापित करने के उद्देश्य से उन्होंने बल देकर कहा कि मैं हिन्दी
हीरक जयन्ती स्मारिका
विद्वत् खण्ड /२
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org