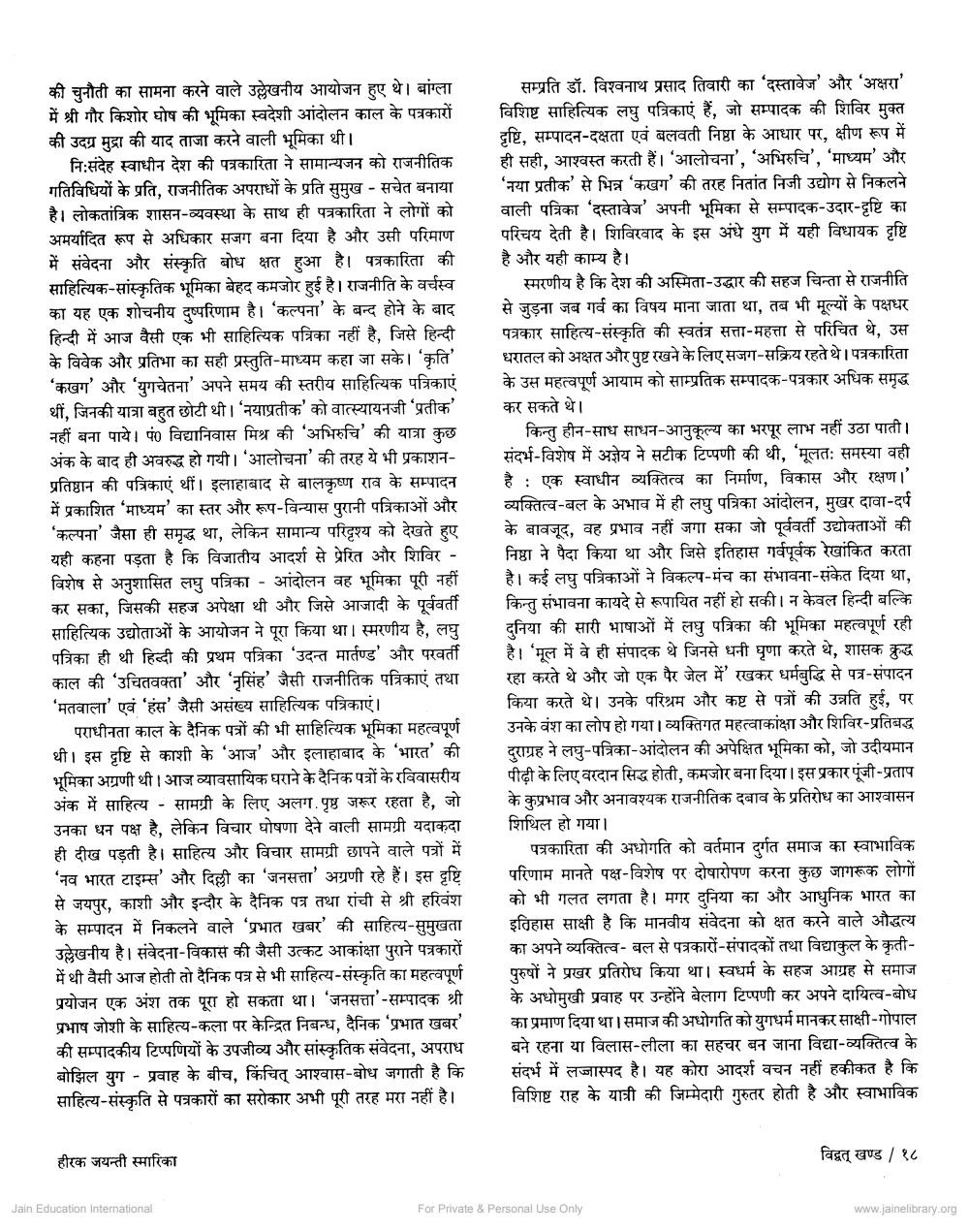________________
की चुनौती का सामना करने वाले उल्लेखनीय आयोजन हुए थे। बांग्ला में श्री गौर किशोर घोष की भूमिका स्वदेशी आंदोलन काल के पत्रकारों की उदग्र मुद्रा की याद ताजा करने वाली भूमिका थी।
नि:संदेह स्वाधीन देश की पत्रकारिता ने सामान्यजन को राजनीतिक गतिविधियों के प्रति, राजनीतिक अपराधों के प्रति सुमुख - सचेत बनाया है। लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था के साथ ही पत्रकारिता ने लोगों को अमर्यादित रूप से अधिकार सजग बना दिया है और उसी परिमाण में संवेदना और संस्कृति बोध क्षत हुआ है। पत्रकारिता की साहित्यिक-सांस्कृतिक भूमिका बेहद कमजोर हुई है। राजनीति के वर्चस्व का यह एक शोचनीय दुष्परिणाम है। 'कल्पना' के बन्द होने के बाद हिन्दी में आज वैसी एक भी साहित्यिक पत्रिका नहीं है, जिसे हिन्दी के विवेक और प्रतिभा का सही प्रस्तुति-माध्यम कहा जा सके। 'कृति' 'कखग' और 'युगचेतना' अपने समय की स्तरीय साहित्यिक पत्रिकाएं थीं, जिनकी यात्रा बहुत छोटी थी। 'नयाप्रतीक' को वात्स्यायनजी प्रतीक' नहीं बना पाये। पं0 विद्यानिवास मिश्र की 'अभिरुचि' की यात्रा कुछ अंक के बाद ही अवरुद्ध हो गयी। 'आलोचना' की तरह ये भी प्रकाशनप्रतिष्ठान की पत्रिकाएं थीं। इलाहाबाद से बालकृष्ण राव के सम्पादन में प्रकाशित 'माध्यम' का स्तर और रूप-विन्यास पुरानी पत्रिकाओं और 'कल्पना' जैसा ही समृद्ध था, लेकिन सामान्य परिदृश्य को देखते हुए यही कहना पड़ता है कि विजातीय आदर्श से प्रेरित और शिविर - विशेष से अनुशासित लघु पत्रिका - आंदोलन वह भूमिका पूरी नहीं कर सका, जिसकी सहज अपेक्षा थी और जिसे आजादी के पूर्ववर्ती साहित्यिक उद्योताओं के आयोजन ने पूरा किया था। स्मरणीय है, लघु पत्रिका ही थी हिन्दी की प्रथम पत्रिका 'उदन्त मार्तण्ड' और परवर्ती काल की 'उचितवक्ता' और 'नृसिंह' जैसी राजनीतिक पत्रिकाएं तथा 'मतवाला' एवं 'हंस' जैसी असंख्य साहित्यिक पत्रिकाएं।
पराधीनता काल के दैनिक पत्रों की भी साहित्यिक भूमिका महत्वपूर्ण थी। इस दृष्टि से काशी के 'आज' और इलाहाबाद के 'भारत' की भूमिका अग्रणी थी। आज व्यावसायिक घराने के दैनिक पत्रों के रविवासरीय अंक में साहित्य - सामग्री के लिए अलग. पृष्ठ जरूर रहता है, जो उनका धन पक्ष है, लेकिन विचार घोषणा देने वाली सामग्री यदाकदा ही दीख पड़ती है। साहित्य और विचार सामग्री छापने वाले पत्रों में 'नव भारत टाइम्स' और दिल्ली का 'जनसत्ता' अग्रणी रहे हैं। इस दृष्टि से जयपुर, काशी और इन्दौर के दैनिक पत्र तथा रांची से श्री हरिवंश के सम्पादन में निकलने वाले 'प्रभात खबर' की साहित्य-सुमुखता उल्लेखनीय है। संवेदना-विकास की जैसी उत्कट आकांक्षा पुराने पत्रकारों में थी वैसी आज होती तो दैनिक पत्र से भी साहित्य-संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रयोजन एक अंश तक पूरा हो सकता था। 'जनसत्ता'-सम्पादक श्री प्रभाष जोशी के साहित्य-कला पर केन्द्रित निबन्ध, दैनिक 'प्रभात खबर' की सम्पादकीय टिप्पणियों के उपजीव्य और सांस्कृतिक संवेदना, अपराध बोझिल युग - प्रवाह के बीच, किंचित् आश्वास-बोध जगाती है कि साहित्य-संस्कृति से पत्रकारों का सरोकार अभी पूरी तरह मरा नहीं है।
सम्प्रति डॉ. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का 'दस्तावेज' और 'अक्षरा' विशिष्ट साहित्यिक लघु पत्रिकाएं हैं, जो सम्पादक की शिविर मुक्त दृष्टि, सम्पादन-दक्षता एवं बलवती निष्ठा के आधार पर, क्षीण रूप में ही सही, आश्वस्त करती हैं। आलोचना', 'अभिरुचि', 'माध्यम' और 'नया प्रतीक' से भिन्न कखग' की तरह नितांत निजी उद्योग से निकलने वाली पत्रिका 'दस्तावेज' अपनी भूमिका से सम्पादक-उदार-दृष्टि का परिचय देती है। शिविरवाद के इस अंधे युग में यही विधायक दृष्टि है और यही काम्य है।
स्मरणीय है कि देश की अस्मिता-उद्धार की सहज चिन्ता से राजनीति से जुड़ना जब गर्व का विषय माना जाता था, तब भी मूल्यों के पक्षधर पत्रकार साहित्य-संस्कृति की स्वतंत्र सत्ता-महत्ता से परिचित थे, उस धरातल को अक्षत और पुष्ट रखने के लिए सजग-सक्रिय रहते थे। पत्रकारिता के उस महत्वपूर्ण आयाम को साम्प्रतिक सम्पादक-पत्रकार अधिक समृद्ध कर सकते थे।
किन्तु हीन-साध साधन-आनुकूल्य का भरपूर लाभ नहीं उठा पाती। संदर्भ-विशेष में अज्ञेय ने सटीक टिप्पणी की थी, 'मूलतः समस्या वही है : एक स्वाधीन व्यक्तित्व का निर्माण, विकास और रक्षण।' व्यक्तित्व-बल के अभाव में ही लघु पत्रिका आंदोलन, मुखर दावा-दर्प के बावजूद, वह प्रभाव नहीं जगा सका जो पूर्ववर्ती उद्योक्ताओं की निष्ठा ने पैदा किया था और जिसे इतिहास गर्वपूर्वक रेखांकित करता है। कई लघु पत्रिकाओं ने विकल्प-मंच का संभावना-संकेत दिया था, किन्तु संभावना कायदे से रूपायित नहीं हो सकी। न केवल हिन्दी बल्कि दुनिया की सारी भाषाओं में लघु पत्रिका की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। 'मूल में वे ही संपादक थे जिनसे धनी घृणा करते थे, शासक क्रुद्ध रहा करते थे और जो एक पैर जेल में रखकर धर्मबुद्धि से पत्र-संपादन किया करते थे। उनके परिश्रम और कष्ट से पत्रों की उन्नति हुई, पर उनके वंश का लोप हो गया।व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और शिविर-प्रतिबद्ध दुराग्रह ने लघु-पत्रिका-आंदोलन की अपेक्षित भूमिका को, जो उदीयमान पीढ़ी के लिए वरदान सिद्ध होती, कमजोर बना दिया। इस प्रकार पूंजी-प्रताप के कुप्रभाव और अनावश्यक राजनीतिक दबाव के प्रतिरोध का आश्वासन शिथिल हो गया।
पत्रकारिता की अधोगति को वर्तमान दुर्गत समाज का स्वाभाविक परिणाम मानते पक्ष-विशेष पर दोषारोपण करना कुछ जागरूक लोगों को भी गलत लगता है। मगर दुनिया का और आधुनिक भारत का इतिहास साक्षी है कि मानवीय संवेदना को क्षत करने वाले औद्धत्य का अपने व्यक्तित्व- बल से पत्रकारों-संपादकों तथा विद्याकुल के कृतीपुरुषों ने प्रखर प्रतिरोध किया था। स्वधर्म के सहज आग्रह से समाज के अधोमुखी प्रवाह पर उन्होंने बेलाग टिप्पणी कर अपने दायित्व-बोध का प्रमाण दिया था। समाज की अधोगति को युगधर्म मानकर साक्षी-गोपाल बने रहना या विलास-लीला का सहचर बन जाना विद्या-व्यक्तित्व के संदर्भ में लज्जास्पद है। यह कोरा आदर्श वचन नहीं हकीकत है कि विशिष्ट राह के यात्री की जिम्मेदारी गुरुतर होती है और स्वाभाविक
हीरक जयन्ती स्मारिका
विद्वत् खण्ड / १८
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org