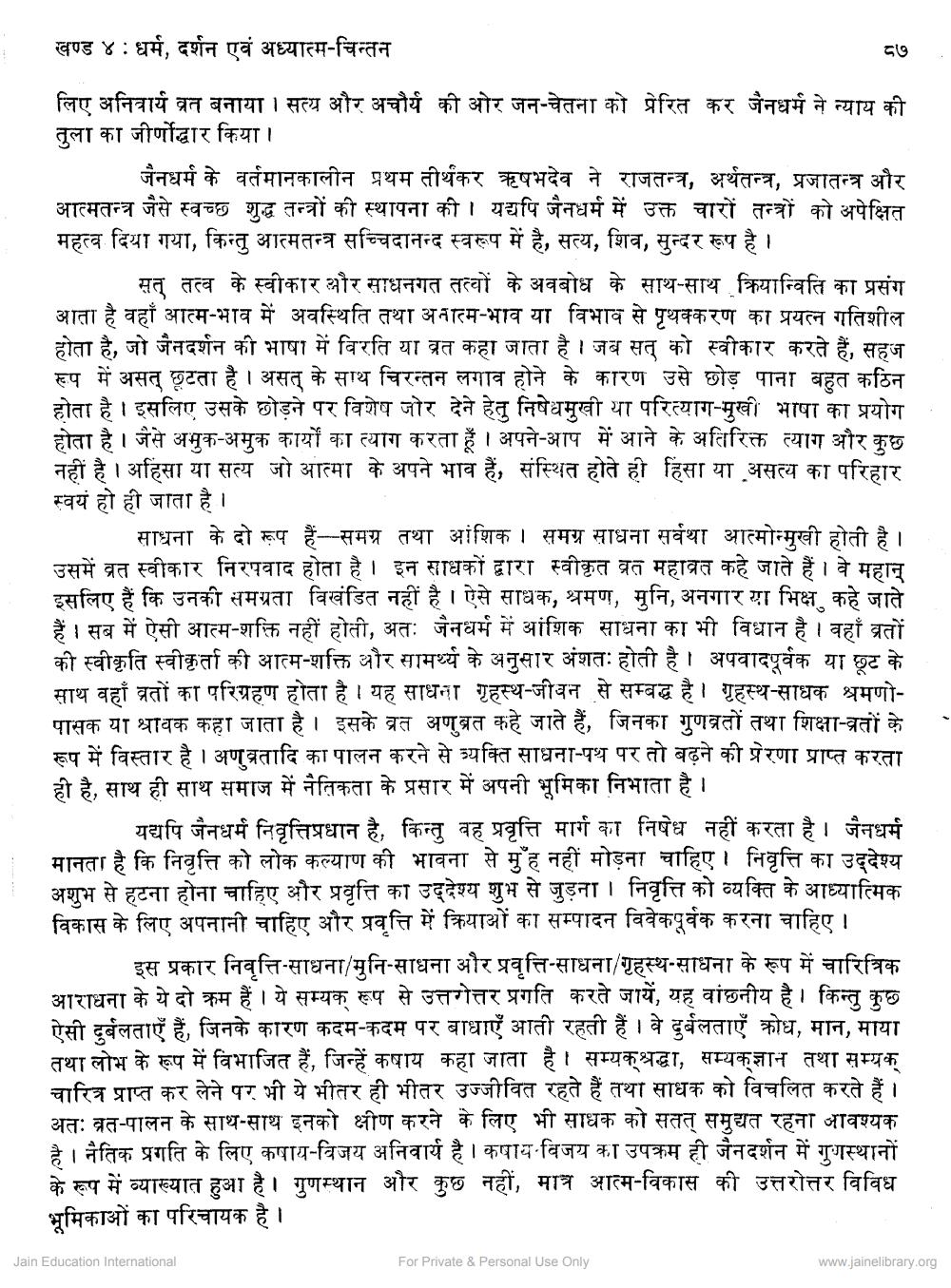________________
खण्ड ४ : धर्म, दर्शन एवं अध्यात्म-चिन्तन
लिए अनिवार्य व्रत बनाया । सत्य और अचौर्य की ओर जन-चेतना को प्रेरित कर जैनधर्म ने न्याय की तुला का जीर्णोद्धार किया।
जैनधर्म के वर्तमानकालीन प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने राजतन्त्र, अर्थतन्त्र, प्रजातन्त्र और आत्मतन्त्र जैसे स्वच्छ शुद्ध तन्त्रों की स्थापना की। यद्यपि जैनधर्म में उक्त चारों तन्त्रों को अपेक्षित महत्व दिया गया, किन्तु आत्मतन्त्र सच्चिदानन्द स्वरूप में है, सत्य, शिव, सुन्दर रूप है।
सत् तत्व के स्वीकार और साधनगत तत्वों के अवबोध के साथ-साथ क्रियान्विति का प्रसंग आता है वहाँ आत्म-भाव में अवस्थिति तथा अनात्म-भाव या विभाव से पृथक्करण का प्रयत्न गतिशील होता है, जो जैनदर्शन की भाषा में विरति या व्रत कहा जाता है। जब सत् को स्वीकार करते हैं, सहज रूप में असत् छूटता है । असत् के साथ चिरन्तन लगाव होने के कारण उसे छोड़ पाना बहुत कठिन होता है । इसलिए उसके छोड़ने पर विशेष जोर देने हेतु निषेधमुखी या परित्याग-मुखी भाषा का प्रयोग होता है । जैसे अमुक-अमुक कार्यों का त्याग करता हूँ। अपने-आप में आने के अतिरिक्त त्याग और कुछ नहीं है । अहिंसा या सत्य जो आत्मा के अपने भाव हैं, संस्थित होते ही हिंसा या असत्य का परिहार स्वयं हो ही जाता है।
साधना के दो रूप हैं-समग्र तथा आंशिक । समग्र साधना सर्वथा आत्मोन्मुखी होती है। उसमें व्रत स्वीकार निरपवाद होता है। इन साधकों द्वारा स्वीकृत व्रत महाव्रत कहे जाते हैं। वे महान् इसलिए हैं कि उनकी समग्रता विखंडित नहीं है । ऐसे साधक, श्रमण, मुनि, अनगार या भिक्ष कहे जाते हैं। सब में ऐसी आत्म-शक्ति नहीं होती, अतः जैनधर्म में आंशिक साधना का भी विधान है । वहाँ व्रतों की स्वीकृति स्वीकृर्ता की आत्म-शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार अंशतः होती है। अपवादपूर्वक या छूट के साथ वहाँ व्रतों का परिग्रहण होता है । यह साधना गृहस्थ-जीवन से सम्बद्ध है। गृहस्थ-साधक श्रमणोपासक या श्रावक कहा जाता है। इसके व्रत अणुव्रत कहे जाते हैं, जिनका गुणवतों तथा शिक्षा-व्रतों के रूप में विस्तार है । अणुव्रतादि का पालन करने से व्यक्ति साधना-पथ पर तो बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करता ही है, साथ ही साथ समाज में नैतिकता के प्रसार में अपनी भूमिका निभाता है।
यद्यपि जैनधर्म निवृत्तिप्रधान है, किन्तु वह प्रवृत्ति मार्ग का निषेध नहीं करता है। जैनधर्म मानता है कि निवृत्ति को लोक कल्याण की भावना से मुह नहीं मोड़ना चाहिए। निवृत्ति का उद्देश्य अशुभ से हटना होना चाहिए और प्रवृत्ति का उद्देश्य शुभ से जुड़ना। निवृत्ति को व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए अपनानी चाहिए और प्रवृत्ति में क्रियाओं का सम्पादन विवेकपूर्वक करना चाहिए।
इस प्रकार निवृत्ति-साधना/मुनि-साधना और प्रवृत्ति-साधना/गृहस्थ-साधना के रूप में चारित्रिक आराधना के ये दो क्रम हैं । ये सम्यक रूप से उत्तरोत्तर प्रगति करते जायें, यह वांछनीय है। किन्तु कुछ ऐसी दुर्बलताएँ हैं, जिनके कारण कदम-कदम पर बाधाएँ आती रहती हैं । वे दुर्बलताएँ क्रोध, मान, माया तथा लोभ के रूप में विभाजित हैं, जिन्हें कषाय कहा जाता है। सम्यक्श्रद्धा, सम्यक्ज्ञान तथा सम्यक चारित्र प्राप्त कर लेने पर भी ये भीतर ही भीतर उज्जीवित रहते हैं तथा साधक को विचलित करते हैं। अतः व्रत-पालन के साथ-साथ इनको क्षीण करने के लिए भी साधक को सतत् समुद्यत रहना आवश्यक है। नैतिक प्रगति के लिए कषाय-विजय अनिवार्य है । कषाय विजय का उपक्रम ही जैनदर्शन में गुणस्थानों के रूप में व्याख्यात हुआ है। गुणस्थान और कुछ नहीं, मात्र आत्म-विकास की उत्तरोत्तर विविध भूमिकाओं का परिचायक है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org