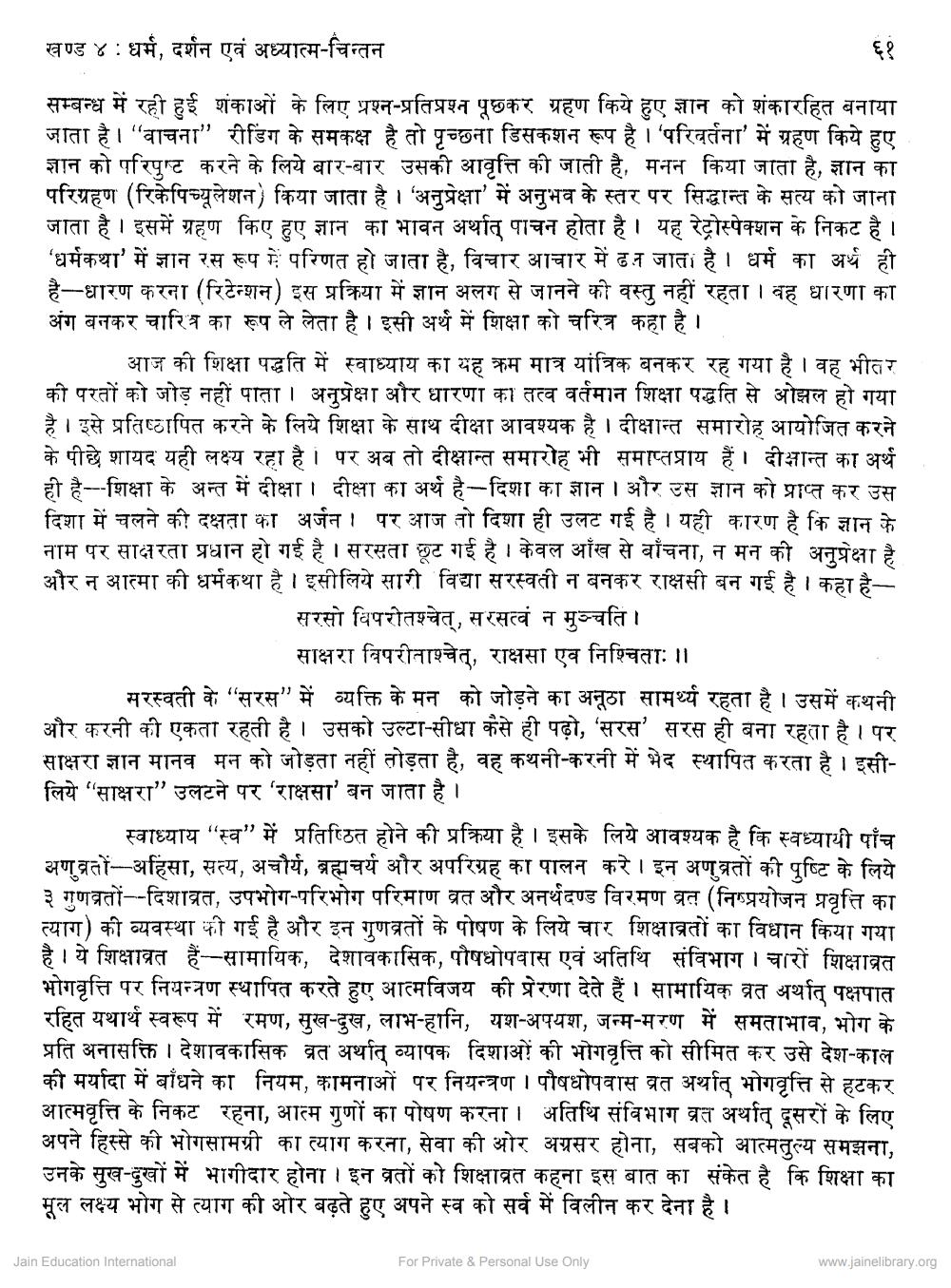________________
खण्ड ४ : धर्म, दर्शन एवं अध्यात्म-चिन्तन
सम्बन्ध में रही हुई शंकाओं के लिए प्रश्न-प्रतिप्रश्न पूछकर ग्रहण किये हुए ज्ञान को शंकारहित बनाया जाता है । "वाचना" रीडिंग के समकक्ष है तो पृच्छना डिसकशन रूप है । 'परिवर्तना' में ग्रहण किये हुए ज्ञान को परिपुष्ट करने के लिये बार-बार उसकी आवृत्ति की जाती है, मनन किया जाता है, ज्ञान का परिग्रहण (रिकेपिच्यूलेशन) किया जाता है । 'अनुप्रेक्षा' में अनुभव के स्तर पर सिद्धान्त के सत्य को जाना जाता है । इसमें ग्रहण किए हुए ज्ञान का भावन अर्थात् पाचन होता है। यह रेट्रोस्पेक्शन के निकट है । 'धर्मकथा' में ज्ञान रस रूप में परिणत हो जाता है, विचार आचार में ढल जाता है। धर्म का अर्थ ही है-धारण करना (रिटेन्शन) इस प्रक्रिया में ज्ञान अलग से जानने की वस्तु नहीं रहता । वह धारणा का अंग बनकर चारित्र का रूप ले लेता है । इसी अर्थ में शिक्षा को चरित्र कहा है।
आज की शिक्षा पद्धति में स्वाध्याय का यह क्रम मात्र यांत्रिक बनकर रह गया है । वह भीतर की परतों को जोड़ नहीं पाता। अनुप्रेक्षा और धारणा का तत्व वर्तमान शिक्षा पद्धति से ओझल हो गया है। इसे प्रतिष्ठापित करने के लिये शिक्षा के साथ दीक्षा आवश्यक है । दीक्षान्त समारोह आयोजित करने के पीछे शायद यही लक्ष्य रहा है। पर अब तो दीक्षान्त समारोह भी समाप्तप्राय हैं। दीक्षान्त का अर्थ ही है--शिक्षा के अन्त में दीक्षा। दीक्षा का अर्थ है-दिशा का ज्ञान । और उस ज्ञान को प्राप्त कर उस दिशा में चलने की दक्षता का अर्जन । पर आज तो दिशा ही उलट गई है। यही कारण है कि ज्ञान के नाम पर साक्षरता प्रधान हो गई है । सरसता छूट गई है । केवल आँख से बाँचना, न मन की अनुप्रेक्षा है और न आत्मा की धर्मकथा है । इसीलिये सारी विद्या सरस्वती न बनकर राक्षसी बन गई है। कहा है
सरसो विपरीतश्चेत्, सरसत्वं न मुञ्चति ।
साक्षरा विपरीताश्चेत्, राक्षसा एव निश्चिताः ।। सरस्वती के “सरस' में व्यक्ति के मन को जोड़ने का अनूठा सामर्थ्य रहता है । उसमें कथनी और करनी की एकता रहती है। उसको उल्टा-सीधा कैसे ही पढ़ो, 'सरस' सरस ही बना रहता है। पर साक्षरा ज्ञान मानव मन को जोड़ता नहीं तोड़ता है, वह कथनी-करनी में भेद स्थापित करता है। इसीलिये “साक्षरा" उलटने पर 'राक्षसा' बन जाता है ।।
स्वाध्याय "स्व" में प्रतिष्ठित होने की प्रक्रिया है । इसके लिये आवश्यक है कि स्वध्यायी पाँच अणुव्रतों-अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करे । इन अणुव्रतों की पुष्टि के लिये ३ गुणवतों--दिशाव्रत, उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत और अनर्थदण्ड विरमण व्रत (निष्प्रयोजन प्रवृत्ति का त्याग) की व्यवस्था की गई है और इन गुणवतों के पोषण के लिये चार शिक्षाव्रतों का विधान किया गया है । ये शिक्षाव्रत हैं-सामायिक, देशावकासिक, पौषधोपवास एवं अतिथि संविभाग । चारों शिक्षाव्रत भोगवृत्ति पर नियन्त्रण स्थापित करते हुए आत्मविजय की प्रेरणा देते हैं। सामायिक व्रत अर्थात् पक्षपात रहित यथार्थ स्वरूप में रमण, सुख-दुख, लाभ-हानि, यश-अपयश, जन्म-मरण में समताभाव, भोग के प्रति अनासक्ति । देशावकासिक व्रत अर्थात् व्यापक दिशाओं की भोगवृत्ति को सीमित कर उसे देश-काल की मर्यादा में बाँधने का नियम, कामनाओं पर नियन्त्रण । पौषधोपवास व्रत अर्थात् भोगवृत्ति से हटकर आत्मवृत्ति के निकट रहना, आत्म गुणों का पोषण करना। अतिथि संविभाग व्रत अर्थात् दूसरों के लिए अपने हिस्से की भोगसामग्री का त्याग करना, सेवा की ओर अग्रसर होना, सबको आत्मतुल्य समझना, उनके सुख-दुखों में भागीदार होना । इन व्रतों को शिक्षाव्रत कहना इस बात का संकेत है कि शिक्षा का मूल लक्ष्य भोग से त्याग की ओर बढ़ते हुए अपने स्व को सर्व में विलीन कर देना है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org