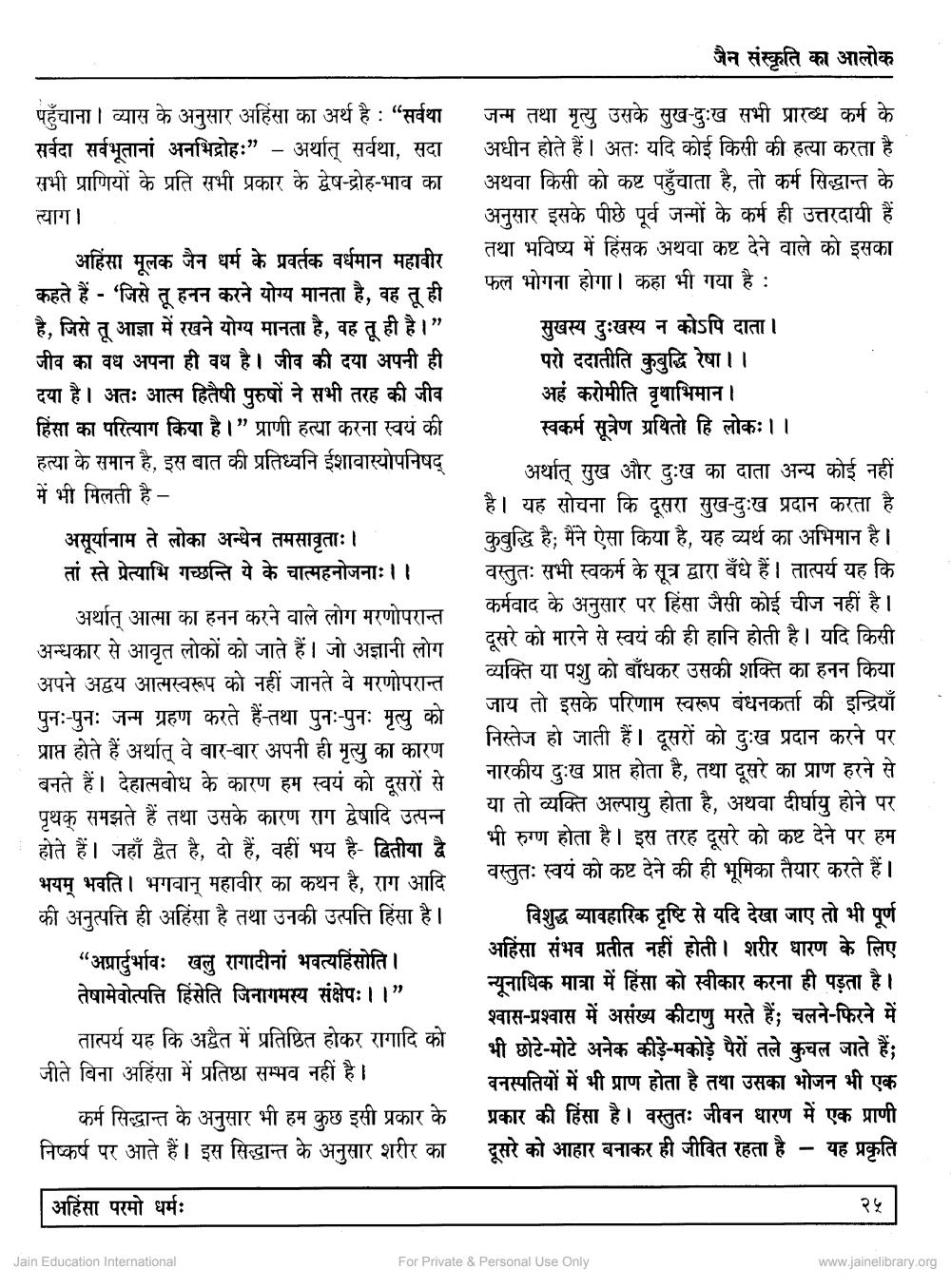________________
जैन संस्कृति का आलोक
पहुँचाना। व्यास के अनुसार अहिंसा का अर्थ है : “सर्वथा जन्म तथा मृत्यु उसके सुख-दुःख सभी प्रारब्ध कर्म के सर्वदा सर्वभूतानां अनभिद्रोहः” – अर्थात् सर्वथा, सदा अधीन होते हैं। अतः यदि कोई किसी की हत्या करता है सभी प्राणियों के प्रति सभी प्रकार के द्वेष-द्रोह-भाव का अथवा किसी को कष्ट पहुँचाता है, तो कर्म सिद्धान्त के त्याग।
अनुसार इसके पीछे पूर्व जन्मों के कर्म ही उत्तरदायी हैं अहिंसा मूलक जैन धर्म के प्रवर्तक वर्धमान महावीर
तथा भविष्य में हिंसक अथवा कष्ट देने वाले को इसका
फल भोगना होगा। कहा भी गया है : कहते हैं - 'जिसे तू हनन करने योग्य मानता है, वह तू ही है, जिसे तू आज्ञा में रखने योग्य मानता है, वह तू ही है।" सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता । जीव का वध अपना ही वध है। जीव की दया अपनी ही परो ददातीति कुबुद्धि रेषा ।। दया है। अतः आत्म हितैषी पुरुषों ने सभी तरह की जीव अहं करोमीति वृथाभिमान। हिंसा का परित्याग किया है।" प्राणी हत्या करना स्वयं की स्वकर्म सूत्रेण ग्रथितो हि लोकः।। हत्या के समान है, इस बात की प्रतिध्वनि ईशावास्योपनिषद्
अर्थात् सुख और दुःख का दाता अन्य कोई नहीं में भी मिलती है -
है। यह सोचना कि दूसरा सुख-दुःख प्रदान करता है असूर्यानाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः।
कुबुद्धि है; मैंने ऐसा किया है, यह व्यर्थ का अभिमान है। तां स्ते प्रेत्याभि गच्छन्ति ये के चात्महनोजनाः।। वस्तुतः सभी स्वकर्म के सूत्र द्वारा बँधे हैं। तात्पर्य यह कि अर्थात् आत्मा का हनन करने वाले लोग मरणोपरान्त ।
कर्मवाद के अनुसार पर हिंसा जैसी कोई चीज नहीं है। अन्धकार से आवृत लोकों को जाते हैं। जो अज्ञानी लोग दूसरे को मारने से स्वयं की ही हानि होती है। यदि किसी अपने अद्वय आत्मस्वरूप को नहीं जानते वे मरणोपरान्त
व्यक्ति या पशु को बाँधकर उसकी शक्ति का हनन किया पुनः पुनः जन्म ग्रहण करते हैं तथा पुनः-पुनः मृत्यु को
जाय तो इसके परिणाम स्वरूप बंधनकर्ता की इन्द्रियाँ प्राप्त होते हैं अर्थात् वे बार-बार अपनी ही मृत्यु का कारण
निस्तेज हो जाती हैं। दूसरों को दुःख प्रदान करने पर बनते हैं। देहात्मबोध के कारण हम स्वयं को दूसरों से ।
नारकीय दुःख प्राप्त होता है, तथा दूसरे का प्राण हरने से पृथक् समझते हैं तथा उसके कारण राग द्वेषादि उत्पन्न ।
या तो व्यक्ति अल्पायु होता है, अथवा दीर्घायु होने पर होते हैं। जहाँ द्वैत है, दो हैं, वहीं भय है- द्वितीया द्वै
भी रुग्ण होता है। इस तरह दूसरे को कष्ट देने पर हम भयम् भवति । भगवान् महावीर का कथन है, राग आदि ।
वस्तुतः स्वयं को कष्ट देने की ही भूमिका तैयार करते हैं । की अनुत्पत्ति ही अहिंसा है तथा उनकी उत्पत्ति हिंसा है। विशुद्ध व्यावहारिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो भी पूर्ण "अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसोति।
अहिंसा संभव प्रतीत नहीं होती। शरीर धारण के लिए तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः।।"
न्यूनाधिक मात्रा में हिंसा को स्वीकार करना ही पड़ता है।
श्वास-प्रश्वास में असंख्य कीटाणु मरते हैं; चलने-फिरने में तात्पर्य यह कि अद्वैत में प्रतिष्ठित होकर रागादि को भी छोटे-मोटे अनेक कीड़े-मकोड़े पैरों तले कुचल जाते हैं; जीते बिना अहिंसा में प्रतिष्ठा सम्भव नहीं है।
वनस्पतियों में भी प्राण होता है तथा उसका भोजन भी एक कर्म सिद्धान्त के अनुसार भी हम कुछ इसी प्रकार के प्रकार की हिंसा है। वस्तुतः जीवन धारण में एक प्राणी निष्कर्ष पर आते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार शरीर का दूसरे को आहार बनाकर ही जीवित रहता है - यह प्रकृति
| अहिंसा परमो धर्मः
२५
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org