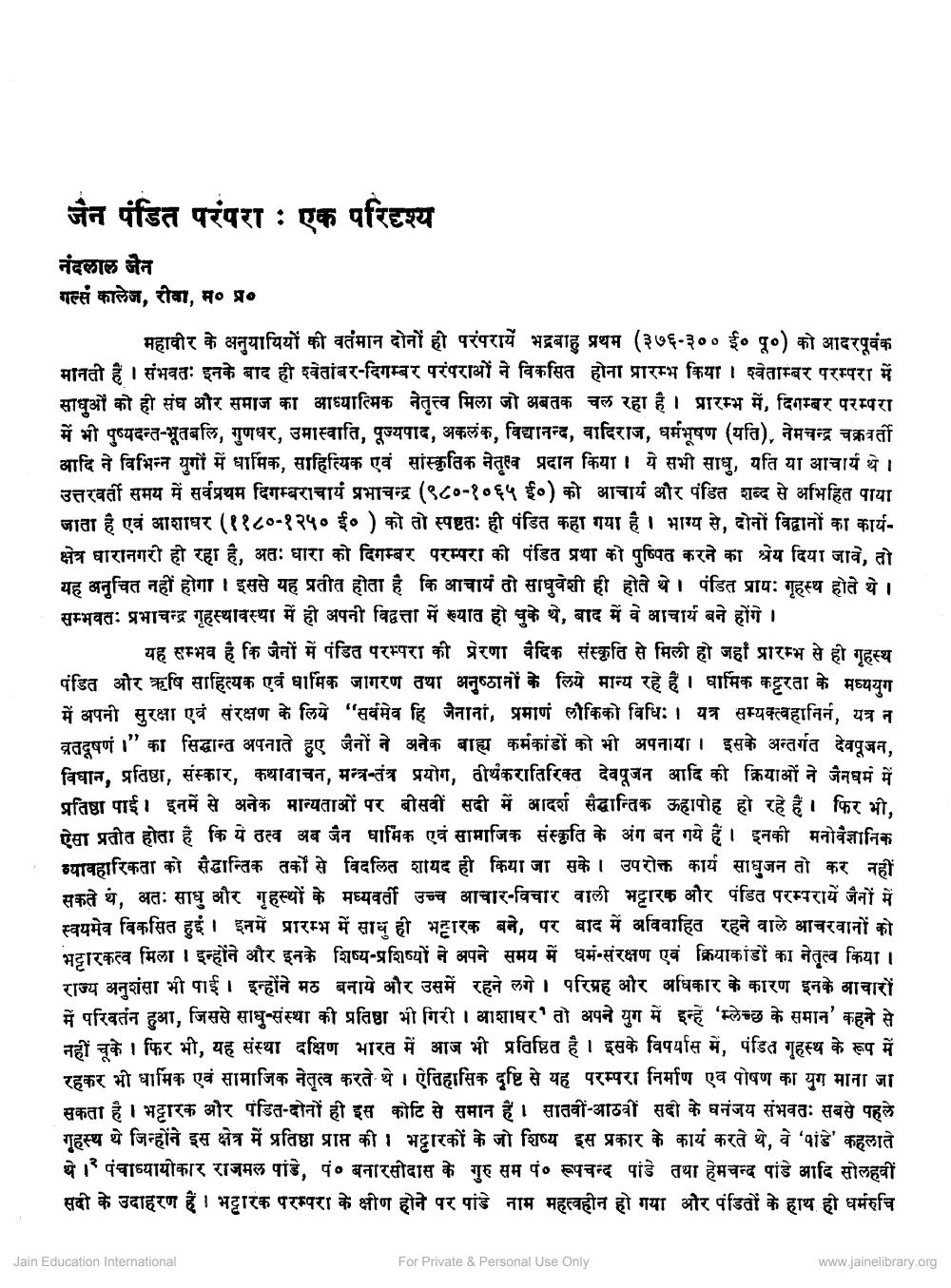________________
जैन पंडित परंपरा : एक परिदृश्य नंदलाल जैन गल्स कालेज, रीवा, म०प्र०
महावीर के अनुयायियों की वर्तमान दोनों ही परंपरायें भद्रबाहु प्रथम (३७६-३०० ई० पू०) को आदरपूर्वक मानती हैं । संभवतः इनके बाद ही श्वेतांबर-दिगम्बर परंपराओं ने विकसित होना प्रारम्भ किया। श्वेताम्बर परम्परा में साधुओं को हो संघ और समाज का आध्यात्मिक नेतृत्त्व मिला जो अबतक चल रहा है। प्रारम्भ में, दिगम्बर परम्परा में भी पुष्यदन्त-भूतबलि, गुणधर, उमास्वाति, पूज्यपाद, अकलंक, विद्यानन्द, वादिराज, धर्मभूषण (यति), नेमचन्द्र चक्रवर्ती आदि ने विभिन्न युगों में धार्मिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक नेतृत्व प्रदान किया। ये सभी साधु, यति या आचार्य थे। उत्तरवर्ती समय में सर्वप्रथम दिगम्बराचार्य प्रभाचन्द्र (९८०-१०६५ ई०) को आचार्य और पंडित शब्द से अभिहित पाया जाता है एवं आशाधर (११८०-१२५० ई.) को तो स्पष्टतः ही पंडित कहा गया है । भाग्य से, दोनों विद्वानों का कार्यक्षेत्र धारानगरी हो रहा है, अतः धारा को दिगम्बर परम्परा को पंडित प्रथा को पुष्पित करने का श्रेय दिया जावे, तो यह अनुचित नहीं होगा। इससे यह प्रतीत होता है कि आचार्य तो साधुवेशी ही होते थे। पंडित प्रायः गृहस्थ होते थे। सम्भवतः प्रभाचन्द्र गृहस्थावस्था में ही अपनी विद्वत्ता में ख्यात हो चुके थे, बाद में वे आचार्य बने होंगे।
___ यह सम्भव है कि जैनों में पंडित परम्परा की प्रेरणा वैदिक संस्कृति से मिली हो जहाँ प्रारम्भ से ही गृहस्थ पंडित और ऋषि साहित्यक एवं धार्मिक जागरण तथा अनुष्ठानों के लिये मान्य रहे हैं । धार्मिक कट्टरता के मध्ययुग में अपनी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिये “सर्वमेव हि जैनानां, प्रमाणं लौकिको विधिः । यत्र सम्यक्त्वहानिर्न, यत्र न व्रतदूषणं ।" का सिद्धान्त अपनाते हुए जैनों ने अनेक बाह्य कर्मकांडों को भी अपनाया। इसके अन्तर्गत देवपूजन, विधान, प्रतिष्ठा, संस्कार, कथावाचन, मन्त्र-तंत्र प्रयोग, तीर्थकरातिरिक्त देवपूजन आदि की क्रियाओं ने जैनधर्म में प्रतिष्ठा पाई। इनमें से अनेक मान्यताओं पर बीसवीं सदी में आदर्श सैद्धान्तिक ऊहापोह हो रहे हैं। फिर भी. ऐसा प्रतीत होता है कि ये तत्व अब जैन धार्मिक एवं सामाजिक संस्कृति के अंग बन गये हैं। इनकी मनोवैज्ञानिक व्यावहारिकता को सैद्धान्तिक तर्कों से विदलित शायद ही किया जा सके। उपरोक्त कार्य साधुजन तो कर नहीं सकते थे, अतः साधु और गृहस्थों के मध्यवर्ती उच्च आचार-विचार वाली भट्टारक और पंडित परम्परायें जैनों में स्वयमेव विकसित हुई। इनमें प्रारम्भ में साथ ही भट्टारक बने, पर बाद में अविवाहित रहने वाले आचरवानों को भट्टारकत्व मिला । इन्होंने और इनके शिष्य-प्रशिष्यों ने अपने समय में धर्म-संरक्षण एवं क्रियाकांडों का नेतृत्व किया । राज्य अनुशंसा भी पाई। इन्होंने मठ बनाये और उसमें रहने लगे। परिग्रह और अधिकार के कारण इनके आचारों में परिवर्तन हुआ, जिससे साधु-संस्था की प्रतिष्ठा भी गिरी । आशाघर' तो अपने युग में इन्हें 'म्लेच्छ के समान' कहने से नहीं चूके । फिर भी, यह संस्था दक्षिण भारत में आज भी प्रतिष्ठित है । इसके विपर्यास में, पंडित गृहस्थ के रूप में रहकर भी धार्मिक एवं सामाजिक नेतृत्व करते थे । ऐतिहासिक दृष्टि से यह परम्परा निर्माण एव पोषण का युग माना जा सकता है । भट्टारक और पंडित-दोनों ही इस कोटि से समान है। सातवीं-आठवीं सदी के धनंजय संभवतः सबसे पहले गृहस्थ थे जिन्होंने इस क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की। भट्टारकों के जो शिष्य इस प्रकार के कार्य करते थे, वे 'पांडे' कहलाते थे। पंचाध्यायोकार राजमल पांडे. पं. बनारसीदास के गुरु सम पं० रूपचन्द पांडे तथा हेमचन्द पांडे आदि सोलहवीं सदी के उदाहरण हैं । भट्टारक परम्परा के क्षीण होने पर पांडे नाम महत्वहीन हो गया और पंडितों के हाथ हो धर्मरुचि
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org