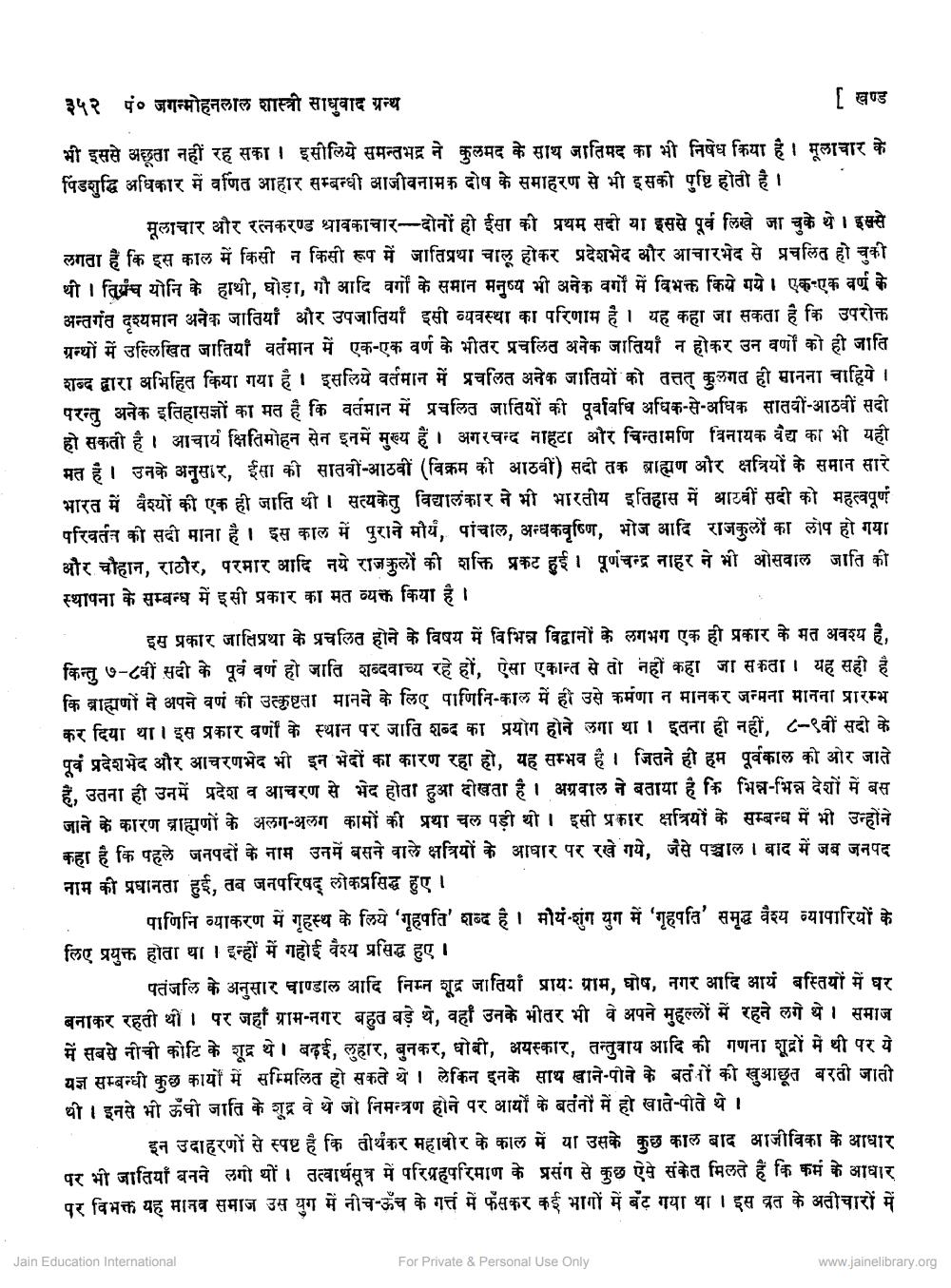________________
३५२ पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ
[खण्ड भी इससे अछूता नहीं रह सका । इसीलिये समन्तभद्र ने कुलमद के साथ जातिमद का भी निषेध किया है। मूलाचार के पिंडशुद्धि अधिकार में वर्णित आहार सम्बन्धी आजीवनामक दोष के समाहरण से भी इसको पुष्टि होती है ।
मूलाचार और रत्नकरण्ड श्रावकाचार-दोनों हो ईसा की प्रथम सदी या इससे पूर्व लिखे जा चुके थे । इससे लगता है कि इस काल में किसी न किसी रूप में जातिप्रथा चाल होकर प्रदेशभेद और आचारभेद से प्रचलित हो चुकी थी। तिसंच योनि के हाथी, घोड़ा, गौ आदि वर्गों के समान मनुष्य भी अनेक वर्गों में विभक्त किये गये। एक-एक वर्ण के अन्तर्गत दृश्यमान अनेक जातियां और उपजातियाँ इसी व्यवस्था का परिणाम है। यह कहा जा सकता है कि उपरोक्त ग्रन्थों में उल्लिखित जातियां वर्तमान में एक-एक वर्ण के भीतर प्रचलित अनेक जातियाँ न होकर उन वर्णों को ही जाति शब्द द्वारा अभिहित किया गया है । इसलिये वर्तमान में प्रचलित अनेक जातियों को तत्तत् कुलगत ही मानना चाहिये । परन्तु अनेक इतिहासज्ञों का मत है कि वर्तमान में प्रचलित जातियों की पूर्वावधि अधिक-से-अधिक सातवीं-आठवीं सदी हो सकती है। आचार्य क्षितिमोहन सेन इनमें मुख्य हैं। अगरचन्द नाहटा और चिन्तामणि विनायक वैद्य का भी यही मत है। उनके अनुसार, ईसा की सातवी-आठवीं (विक्रम की आठवीं) सदी तक ब्राह्मण और क्षत्रियों के समान सारे भारत में वैश्यों की एक ही जाति थी। सत्यकेतु विद्यालंकार ने भी भारतीय इतिहास में आठवीं सदी को महत्वपूर्ण परिवर्तन की सदी माना है। इस काल में पुराने मौर्य, पांचाल, अन्धकवृष्णि, भोज आदि राजकुलों का लोप हो गया और चौहान, राठौर, परमार आदि नये राजकुलों की शक्ति प्रकट हुई। पूर्णचन्द्र नाहर ने भी ओसवाल जाति की स्थापना के सम्बन्ध में इसी प्रकार का मत व्यक्त किया है ।
इस प्रकार जातिप्रथा के प्रचलित होने के विषय में विभिन्न विद्वानों के लगभग एक ही प्रकार के मत अवश्य है, किन्तु ७-८वीं सदी के पूर्व वर्ण हो जाति शब्दवाच्य रहे हों, ऐसा एकान्त से तो नहीं कहा जा सकता। यह सही है कि ब्राह्मणों ने अपने वर्ण की उत्कृष्टता मानने के लिए पाणिनि-काल में ही उसे कर्मणा न मानकर कर दिया था। इस प्रकार वर्गों के स्थान पर जाति शब्द का प्रयोग होने लगा था। इतना ही नहीं, ८-९वीं सदी के पूर्व प्रदेशभेद और आचरणभेद भी इन भेदों का कारण रहा हो, यह सम्भव है। जितने ही हम पूर्वकाल को ओर जाते हैं, उतना ही उनमें प्रदेश व आचरण से भेद होता हुआ दीखता है। अग्रवाल ने बताया है कि भिन्न-भिन्न देशों में बस जाने के कारण ब्राह्मणों के अलग-अलग कामों की प्रथा चल पड़ी थी। इसी प्रकार क्षत्रियों के सम्बन्ध में भी उन्होंने कहा है कि पहले जनपदों के नाम उनमें बसने वाले क्षत्रियों के आधार पर रखे गये, जैसे पञ्चाल । बाद में जब जनपद नाम की प्रधानता हुई, तब जनपरिषद् लोकप्रसिद्ध हुए।
पाणिनि व्याकरण में गृहस्थ के लिये 'गृहपति' शब्द है । मौर्य-शुंग युग में 'गृहपति' समृद्ध वैश्य व्यापारियों के लिए प्रयुक्त होता था । इन्हीं में गहोई वैश्य प्रसिद्ध हुए।
__ पतंजलि के अनुसार चाण्डाल आदि निम्न शूद्र जातियां प्रायः ग्राम, घोष, नगर आदि आर्य बस्तियों में घर बनाकर रहती थीं। पर जहाँ ग्राम-नगर बहुत बड़े थे, वहाँ उनके भीतर भी वे अपने मुहल्लों में रहने लगे थे। समाज में सबसे नीची कोटि के शूद्र थे। बढ़ई, लुहार, बुनकर, धोबी, अयस्कार, तन्तुवाय आदि की गणना शूद्रों में थी पर ये यज्ञ सम्बन्धी कुछ कार्यों में सम्मिलित हो सकते थे। लेकिन इनके साथ खाने-पीने के बर्तनों की खुआछूत बरती जाती थी। इनसे भी ऊंची जाति के शूद्र वे थे जो निमन्त्रण होने पर आर्यों के बर्तनों में हो खाते-पोते थे ।
इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि तीर्थकर महावीर के काल में या उसके कुछ काल बाद आजीविका के आधार पर भी जातियाँ बनने लगो थों। तत्वार्थसूत्र में परिग्रहपरिमाण के प्रसंग से कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि कर्म के आधार पर विभक्त यह मानव समाज उस युग में नीच-ऊँच के गर्त में फंसकर कई भागों में बंट गया था । इस व्रत के अतीचारों में
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org