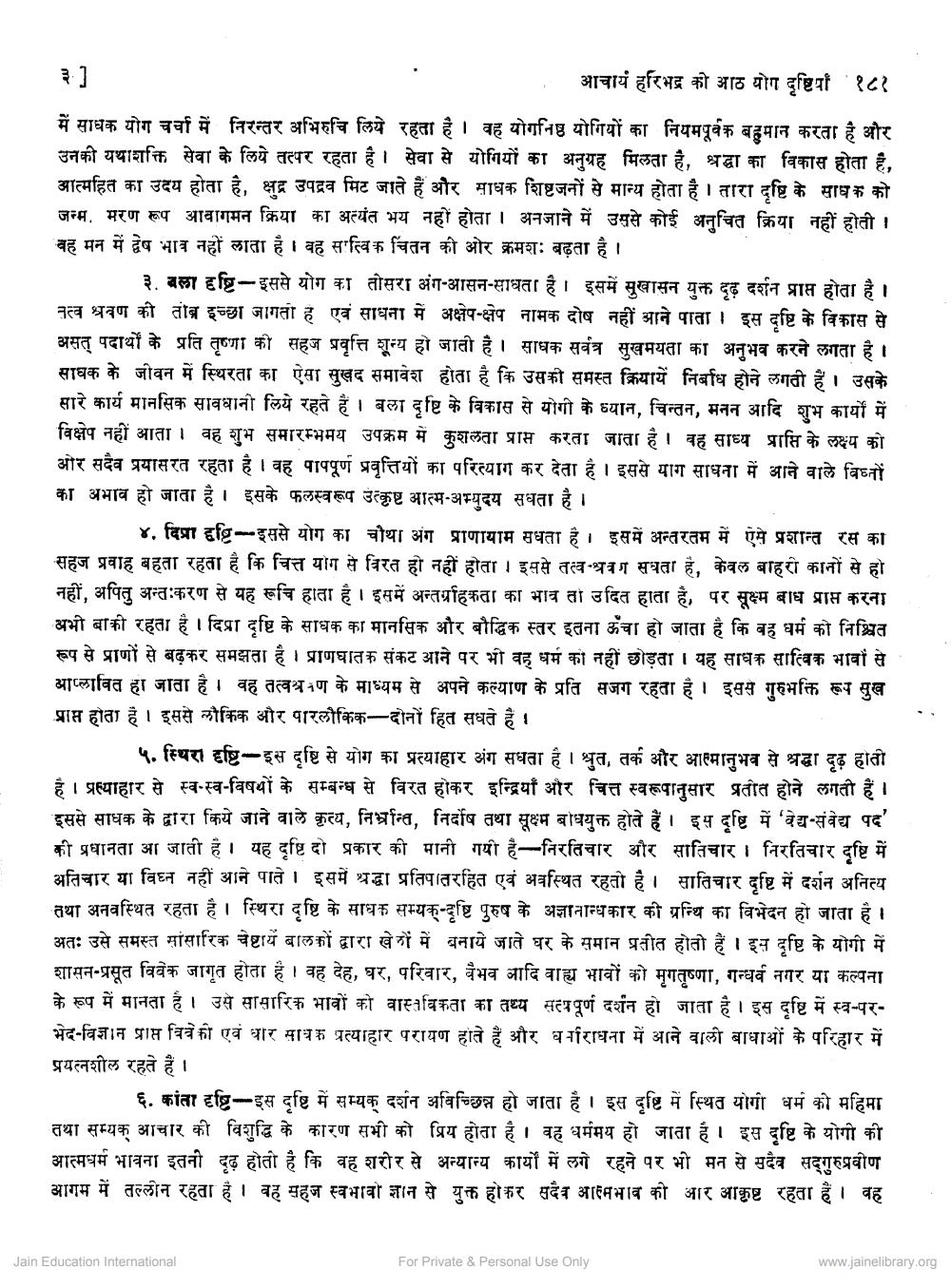________________
आचार्य हरिभद्र को आठ योग दृष्टियाँ १८१ में साधक योग चर्चा में निरन्तर अभिरुचि लिये रहता है । वह योगनिष्ठ योगियों का नियमपूर्वक बहुमान करता है और उनकी यथाशक्ति सेवा के लिये तत्पर रहता है। सेवा से योगियों का अनुग्रह मिलता है, श्रद्धा का विकास होता है, आत्महित का उदय होता है, क्षुद्र उपद्रव मिट जाते हैं और माधक शिष्टजनों से मान्य होता है जन्म. मरण रूप आवागमन क्रिया का अत्यंत भय नहीं होता। अनजाने में उससे कोई अनुचित क्रिया नहीं होती। वह मन में द्वेष भाव नहीं लाता है। वह सात्विक चिंतन की ओर क्रमशः बढ़ता है।
___३. बला दृष्टि- इससे योग का तीसरा अंग-आसन-साधता है। इसमें सुखासन युक्त दृढ़ दर्शन प्राप्त होता है। नत्व श्रवण की तीव्र इच्छा जागती है एवं साधना में अक्षेप-क्षेप नामक दोष नहीं आने पाता। इस दृष्टि के विकास से असत् पदार्थों के प्रति तृष्णा की सहज प्रवृत्ति शून्य हो जाती है। साधक सर्वत्र सुखमयता का अनुभव करने लगता है। साधक के जीवन में स्थिरता का ऐसा सुखद समावेश होता है कि उसकी समस्त क्रियायें निर्बाध होने लगती हैं। उसके सारे कार्य मानसिक सावधानी लिये रहते हैं । बला दृष्टि के विकास से योगी के ध्यान, चिन्तन, मनन आदि शुभ कार्यों में विक्षेप नहीं आता। वह शुभ समारम्भमय उपक्रम में कुशलता प्रास करता जाता है। वह साध्य प्राप्ति के लक्ष्य को
ओर सदैव प्रयासरत रहता है । वह पापपूर्ण प्रवृत्तियों का परित्याग कर देता है । इससे याग साधना में आने वाले विघ्नों का अभाव हो जाता है। इसके फलस्वरूप उत्कृष्ट आत्म-अभ्युदय सघता है ।
४. विप्रा दृष्टि-इससे योग का चौथा अंग प्राणायाम सधता है। इसमें अन्तरतम में ऐसे प्रशान्त रस का सहज प्रवाह बहता रहता है कि चित्त योग से विरत हो नहीं होता। इससे तत्व श्रवण सघता है, केवल बाहरी कानों से हो नहीं, अपितु अन्तःकरण से यह रूचि हाता है। इसमें अन्तहिकता का भाव तो उदित हाता है, पर सूक्ष्म बाध प्राप्त करना अभी बाकी रहता है । दिप्रा दृष्टि के साधक का मानसिक और बौद्धिक स्तर इतना ऊँचा हो जाता है कि वह धर्म को निश्चित रूप से प्राणों से बढ़कर समझता है। प्राणघातक संकट आने पर भी वह धर्म का नहीं छोड़ता। यह साधक सात्विक भावों से आप्लावित हा जाता है। वह तत्वश्रण के माध्यम से अपने कल्याण के प्रति सजग रहता है। इससे गुरुभक्ति रूप सुख प्राप्त होता है। इससे लौकिक और पारलौकिक-दोनों हित सधते है ।
५. स्थिरा दृष्टि-इस दृष्टि से योग का प्रत्याहार अंग सधता है । श्रुत, तर्क और आत्मानुभव से श्रद्धा दृढ़ हाती है। प्रत्याहार से स्व-स्व-विषयों के सम्बन्ध से विरत होकर इन्द्रियाँ और चित्त स्वरूपानुसार प्रतीत होने लगती हैं। इससे साधक के द्वारा किये जाने वाले कृत्य, निर्धान्त, निर्दोष तथा सूक्ष्म बोधयुक्त होते हैं। इस दृष्टि में 'वेद्य-संवेद्य पद' की प्रधानता आ जाती है। यह दृष्टि दो प्रकार की मानी गयी है-निरतिचार और सातिचार । निरतिचार दष्टि में अतिचार या विघ्न नहीं आने पाते । इसमें श्रद्धा प्रतिपातरहित एवं अवस्थित रहती है। सातिचार दृष्टि में दर्शन अनित्य तथा अनवस्थित रहता है । स्थिरा दृष्टि के साधक सम्यक्-दृष्टि पुरुष के अज्ञानान्धकार की ग्रन्थि का विभेदन हो जाता है । अतः उसे समस्त मांसारिक चेष्टायें बालकों द्वारा खेलों में बनाये जाते घर के समान प्रतीत होती हैं । इस दृष्टि के योगी में शासन-प्रसूत विवेक जागृत होता है । वह देह, घर, परिवार, वैभव आदि वाह्य भावों को मृगतृष्णा, गन्धर्व नगर या कल्पना के रूप में मानता है। उसे सासारिक भावों को वास्तविकता का तथ्य सत्यपूर्ण दर्शन हो जाता है । इस दृष्टि में स्व-परभेद-विज्ञान प्राप्त विवे की एवं धार साधक प्रत्याहार परायण हाते हैं और धर्माराधना में आने वाली बाधाओं के परिहार में प्रयत्नशील रहते हैं।
६. कांता दृष्टि-इस दृष्टि में सम्यक् दर्शन अविच्छिन्न हो जाता है । इस दृष्टि में स्थित योगी धर्म को महिमा तथा सम्यक् आचार की विशुद्धि के कारण सभी को प्रिय होता है । वह धर्ममय हो जाता है। इस दृष्टि के योगी की आत्मधर्म भावना इतनी दृढ़ होती है कि वह शरीर से अन्यान्य कार्यों में लगे रहने पर भी मन से सदैव सद्गुरुप्रवीण आगम में तल्लीन रहता है । वह सहज स्वभावो ज्ञान से युक्त होकर सदैव आत्मभाव को आर आकृष्ट रहता हैं । वह
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org