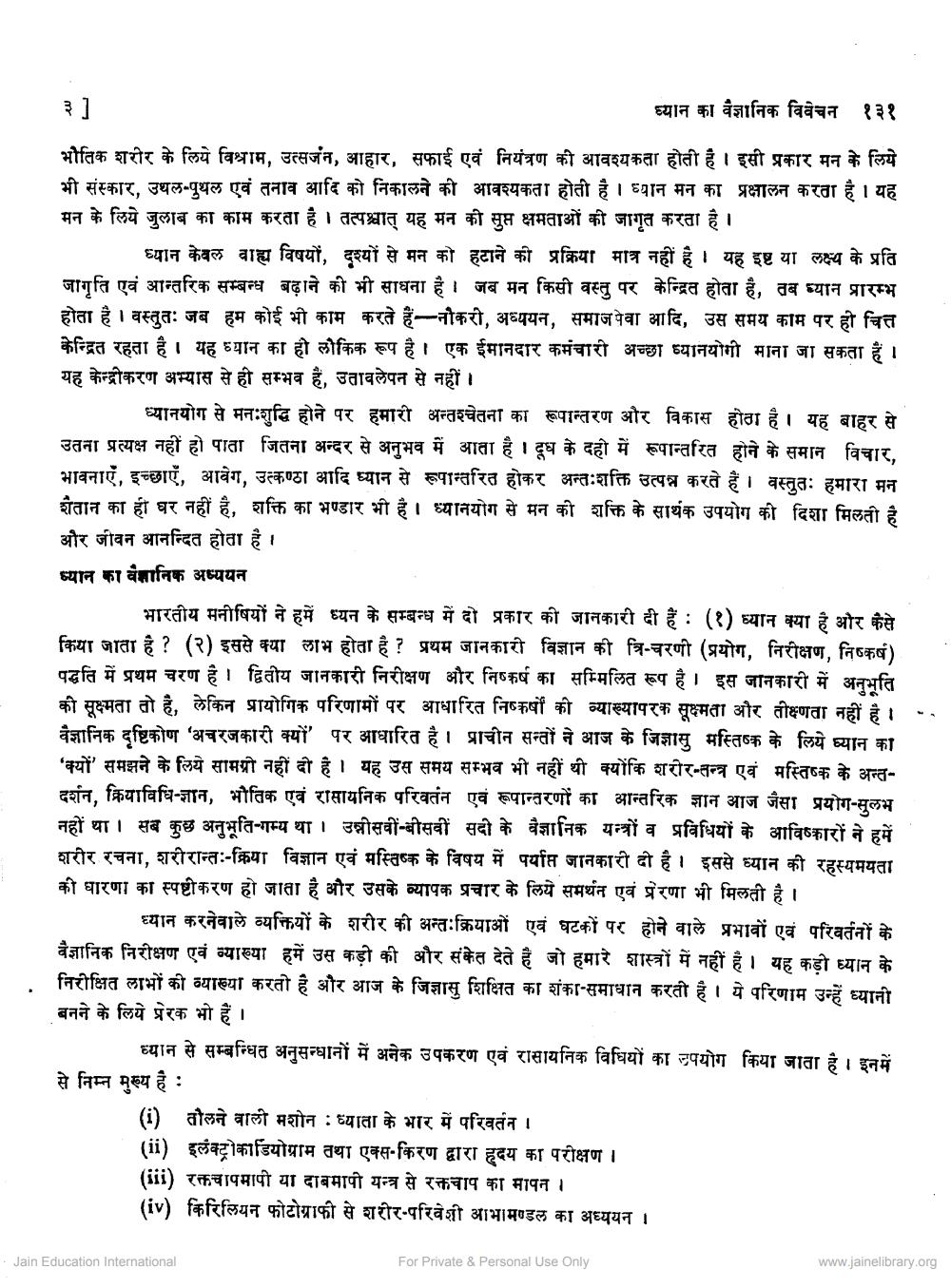________________
३]
ध्यान का वैज्ञानिक विवेचन १३१
भौतिक शरीर के लिये विश्राम, उत्सर्जन, आहार, सफाई एवं नियंत्रण की आवश्यकता होती हैं। इसी प्रकार मन के लिये भी संस्कार, उथल-पुथल एवं तनाव आदि को निकालने की आवश्यकता होती है। ध्यान मन का प्रक्षालन करता है। यह मन के लिये जुलाब का काम करता है। तत्पश्चात् यह मन की सुप्त क्षमताओं की जागृत करता है।
ध्यान केवल वाह्य विषयों, दृश्यों से मन को हटाने की प्रक्रिया मात्र नहीं है। यह इष्ट या लक्ष्य के प्रति जागृति एवं आन्तरिक सम्बन्ध बढ़ाने की भी साधना है। जब मन किसी वस्तु पर केन्द्रित होता है, तब ध्यान प्रारम्भ होता है। वस्तुतः जब हम कोई भी काम करते हैं-नौकरी, अध्ययन, समाजसेवा आदि उस समय काम पर ही चित्त केन्द्रित रहता है । यह ध्यान का ही लौकिक रूप है। एक ईमानदार कर्मचारी अच्छा ध्यानयोगी माना जा सकता हैं । यह केन्द्रीकरण अभ्यास से ही सम्भव है, उतावलेपन से नहीं।
ध्यानयोग से मनःशुद्धि होने पर हमारी अन्तश्चेतना का रूपान्तरण और विकास होता है। यह बाहर से उतना प्रत्यक्ष नहीं हो पाता जितना अन्दर से अनुभव में आता है। दूध के दही में रूपान्तरित होने के समान विचार, भावनाएं, इच्छाएँ, आवेग, उत्कण्ठा आदि ध्यान से रूपान्तरित होकर अन्तःशक्ति उत्पन्न करते हैं। वस्तुतः हमारा मन शैतान का ही घर नहीं है, शक्ति का भण्डार भी है। ध्यानयोग से मन की शक्ति के सार्थक उपयोग की दिशा मिलती है। और जीवन आनन्दित होता है ।
ध्यान का वैज्ञानिक अध्ययन
अनुभूति
भारतीय मनीषियों ने हमें ध्यन के सम्बन्ध में दो प्रकार की जानकारी दी हैं (१) ध्यान क्या है और कैसे किया जाता है ? (२) इससे क्या लाभ होता है ? प्रथम जानकारी विज्ञान की त्रि- चरणी ( प्रयोग, निरीक्षण, निष्कर्ष ) पद्धति में प्रथम चरण है। द्वितीय जानकारी निरीक्षण और निष्कर्ष का सम्मिलित रूप है । इस जानकारी में की सूक्ष्मता तो है, लेकिन प्रायोगिक परिणामों पर आधारित निष्क्रयों की व्याख्यापरक सूक्ष्मता और तीक्ष्णता नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण 'अचरजकारी क्यों' पर आधारित है। प्राचीन सन्तों ने आज के जिज्ञासु मस्तिष्क के लिये ध्यान का 'क्यों' समझने के लिये सामग्री नहीं दी है। यह उस समय सम्भव भी नहीं थी दर्शन क्रियाविधि ज्ञान, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन एवं रूपान्तरणों का
1
नहीं था । सब कुछ अनुभूति गम्य था । उन्नीसवीं-बीसवीं सदी के शरीर रचना, शरीरान्तः - क्रिया विज्ञान एवं मस्तिष्क के विषय में की धारणा का स्पष्टीकरण हो जाता है और उसके व्यापक प्रचार के
क्योंकि शरीर-तन्त्र एवं मस्तिष्क के अन्तआन्तरिक ज्ञान आज जैसा प्रयोग सुलभ वैज्ञानिक यन्त्रों व प्रविधियों के आविष्कारों ने हमें पर्याप्त जानकारी दी है । इससे ध्यान की रहस्यमयता लिये समर्थन एवं प्रेरणा भी मिलती है ।
ध्यान करनेवाले व्यक्तियों के शरीर की अन्तः क्रियाओं एवं घटकों पर होने वाले प्रभावों एवं परिवर्तनों के वैज्ञानिक निरीक्षण एवं व्याख्या हमें उस कड़ी की और संकेत देते हैं जो हमारे शास्त्रों में नहीं है। यह कड़ो ध्यान के निरीक्षित लाभों की व्याख्या करती है और आज के जिज्ञासु शिक्षित का शंका-समाधान करती है। ये परिणाम उन्हें ध्यानी बनने के लिये प्रेरक भो हैं ।
ध्यान से सम्बन्धित अनुसन्धानों में अनेक उपकरण एवं रासायनिक विधियों का उपयोग किया जाता है । इनमें से निम्न मुख्य है :
(i) तौलने वाली मशीन ध्याता के भार में परिवर्तन ।
(ii) इलैक्ट्रोकार्डियोग्राम तथा एक्स-किरण द्वारा हृदय का परीक्षण |
(iii) रक्तचापमापी या दाबमापी यन्त्र से रक्तचाप का मापन ।
(iv) किरिलियन फोटोग्राफी से शरीर परिवेशी आभामण्डल का अध्ययन |
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org