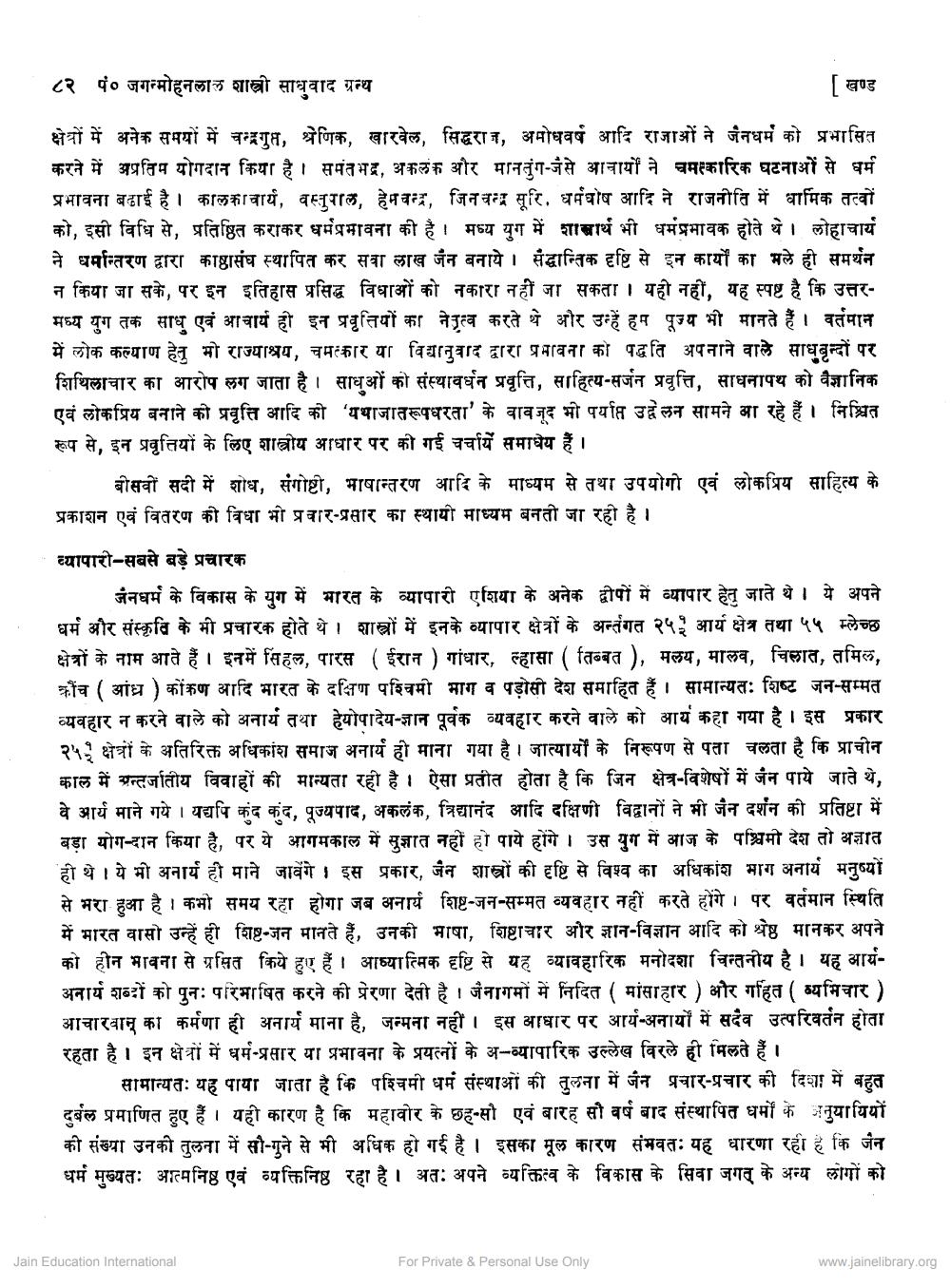________________
८२ पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ
[ खण्ड
क्षेत्रों में अनेक समयों में चन्द्रगुप्त, श्रेणिक, खारवेल, सिद्धराज, अमोधवर्ष आदि राजाओं ने जैनधर्म को प्रभासित करने में अप्रतिम योगदान किया है। समंतभद्र, अकलंक और मानतुंग-जैसे आचार्यों ने चमत्कारिक घटनाओं से धर्म प्रभावना बढ़ाई है। कालकाचार्य, वस्तुगल, हेमचन्द्र, जिन चन्द्र सूरि, धर्मघोष आदि ने राजनीति में धार्मिक तत्वों को, इसी विधि से, प्रतिष्ठित कराकर धर्मप्रभावना की है। मध्य युग में शास्त्रार्थ भी धर्मप्रभावक होते थे। लोहाचार्य ने धर्मान्तरण द्वारा काष्ठासंघ स्थापित कर सवा लाख जैन बनाये। सैद्धान्तिक दृष्टि से इन कार्यों का भले ही समर्थन न किया जा सके, पर इन इतिहास प्रसिद्ध विधाओं को नकारा नहीं जा सकता। यही नहीं, यह स्पष्ट है कि उत्तरमध्य युग तक साधु एवं आचार्य ही इन प्रवृत्तियों का नेतृत्व करते थे और उन्हें हम पूज्य भी मानते हैं। वर्तमान में लोक कल्याण हेतु भो राज्याश्रय, चमत्कार या विद्यानुवाद द्वारा प्रमावना को पद्धति अपनाने वाले साधुबृन्दों पर शिथिलाचार का आरोप लग जाता है। साधुओं को संस्थावर्धन प्रवृत्ति, साहित्य-सर्जन प्रवृत्ति, साधनापथ को वैज्ञानिक एवं लोकप्रिय बनाने की प्रवृत्ति आदि को 'यथाजातरूपधरता' के वावजूद भी पर्याप्त उद्वेलन सामने आ रहे हैं। निश्चित रूप से, इन प्रवृत्तियों के लिए शास्त्रीय आधार पर की गई चर्चायें समाधेय हैं।
बीसवीं सदी में शोध, संगोष्टी, भाषान्तरण आदि के माध्यम से तथा उपयोगी एवं लोकप्रिय साहित्य के प्रकाशन एवं वितरण की विधा भी प्रचार-प्रसार का स्थायी माध्यम बनती जा रही है।
व्यापारी-सबसे बड़े प्रचारक
जैनधर्म के विकास के युग में भारत के व्यापारी एशिया के अनेक द्वीपों में व्यापार हेतु जाते थे । ये अपने धर्म और संस्कृति के भी प्रचारक होते थे। शास्त्रों में इनके व्यापार क्षेत्रों के अन्र्तगत २५३ आर्य क्षेत्र तथा ५५ म्लेच्छ क्षेत्रों के नाम आते हैं । इनमें सिंहल, पारस ( ईरान ) गांधार, ल्हासा ( तिब्बत ), मलय, मालव, चिलात, तमिल, क्रौंच ( आंध्र) कोंकण आदि भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग व पड़ोसी देश समाहित हैं। सामान्यतः शिष्ट जन-सम्मत व्यवहार न करने वाले को अनार्य तथा हेयोपादेय-ज्ञान पूर्वक व्यवहार करने वाले को आयं कहा गया है । इस प्रकार २५, क्षेत्रों के अतिरिक्त अधिकांश समाज अनार्य ही माना गया है। जात्यार्यों के निरूपण से पता चलता है कि प्राचीन काल में अन्तर्जातीय विवाहों की मान्यता रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिन क्षेत्र-विशेषों में जैन पाये जाते थे, वे आर्य माने गये । यद्यपि कंद कंद, पूज्यपाद, अकलंक, त्रिद्यानंद आदि दक्षिणी विद्वानों ने भी जैन दर्शन की प्रतिष्टा में बड़ा योगदान किया है, पर ये आगमकाल में सुज्ञात नहीं हो पाये होंगे। उस युग में आज के पश्चिमी देश तो अज्ञात ही थे। ये भी अनार्य ही माने जावेंगे। इस प्रकार, जैन शास्त्रों की दृष्टि से विश्व का अधिकांश भाग अनार्य मनुष्यों से भरा हआ है। कभी समय रहा होगा जब अनार्य शिष्ट-जन-सम्मत व्यवहार नहीं करते होंगे। पर वर्तमान स्थिति में भारत वासो उन्हें ही शिष्ट-जन मानते हैं, उनकी भाषा, शिष्टाचार और ज्ञान-विज्ञान आदि को श्रेष्ठ मानकर अपने को हीन भावना से ग्रसित किये हए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह व्यावहारिक मनोदशा चिन्तनीय है। यह आर्यअनार्य शब्दों को पुनः परिभाषित करने की प्रेरणा देती है । जैनागमों में निदित ( मांसाहार ) और गहित ( व्यभिचार) आचारवान् का कर्मणा ही अनार्य माना है, जन्मना नहीं। इस आधार पर आर्य-अनार्यों में सदैव उत्परिवर्तन होता रहता है। इन क्षेत्रों में धर्म-प्रसार या प्रभावना के प्रयत्नों के अ-व्यापारिक उल्लेख विरले ही मिलते हैं।
सामान्यतः यह पाया जाता है कि पश्चिमी धर्म संस्थाओं की तुलना में जैन प्रचार-प्रचार की दिशा में बहत दुर्बल प्रमाणित हुए हैं। यही कारण है कि महावीर के छह-सौ एवं बारह सौ वर्ष बाद संस्थापित धर्मों के अनुयायियों की संख्या उनकी तुलना में सौ-गुने से भी अधिक हो गई है। इसका मूल कारण संभवतः यह धारणा रही है कि जैन धर्म मुख्यतः आत्मनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ रहा है। अतः अपने व्यक्तित्व के विकास के सिवा जगत् के अन्य लोगों को
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org