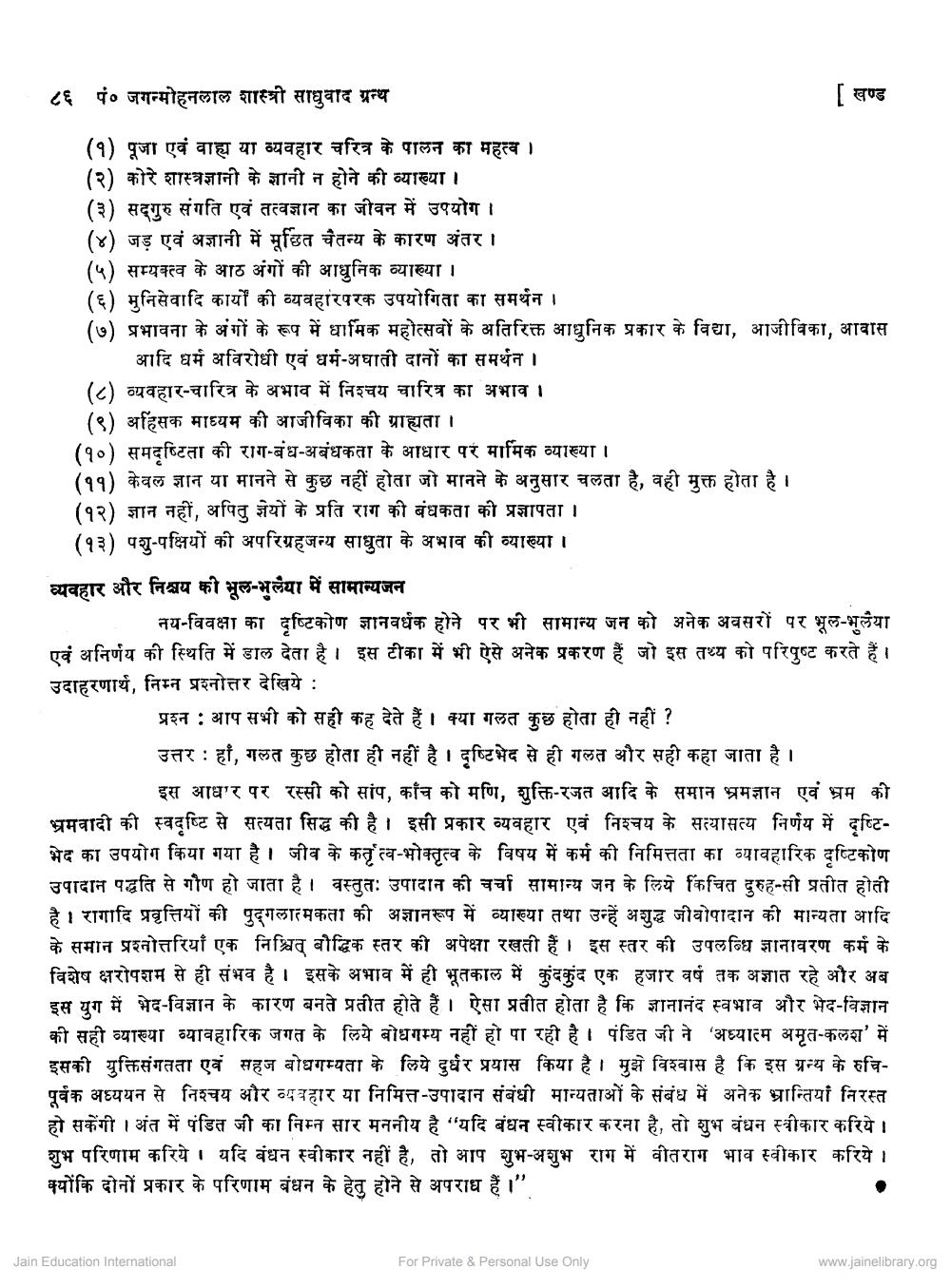________________
८६ पं० जगन्मोहनलाल शास्त्री साधुवाद ग्रन्थ
[खण्ड (१) पूजा एवं वाह्य या व्यवहार चरित्र के पालन का महत्व । (२) कोरे शास्त्रज्ञानी के ज्ञानी न होने की व्याख्या। (३) सद्गुरु संगति एवं तत्वज्ञान का जीवन में उपयोग । (४) जड़ एवं अज्ञानी में मूछित चैतन्य के कारण अंतर । (५) सम्यक्त्व के आठ अंगों की आधुनिक व्याख्या । (६) मुनिसेवादि कार्यों की व्यवहारपरक उपयोगिता का समर्थन । (७) प्रभावना के अंगों के रूप में धार्मिक महोत्सवों के अतिरिक्त आधुनिक प्रकार के विद्या, आजीविका, आवास
आदि धर्म अविरोधी एवं धर्म-अघाती दानों का समर्थन । (८) व्यवहार-चारित्र के अभाव में निश्चय चारित्र का अभाव । (९) अहिंसक माध्यम की आजीविका की ग्राह्यता। (१०) समदृष्टिता की राग-बंध-अबंधकता के आधार पर मार्मिक व्याख्या। (११) केवल ज्ञान या मानने से कुछ नहीं होता जो मानने के अनुसार चलता है, वही मुक्त होता है । (१२) ज्ञान नहीं, अपितु ज्ञेयों के प्रति राग की बंधकता की प्रज्ञापता । (१३) पशु-पक्षियों की अपरिग्रहजन्य साधुता के अभाव की व्याख्या । व्यवहार और निश्चय की भूल-भुलैया में सामान्यजन
नय-विवक्षा का दृष्टिकोण ज्ञानवर्धक होने पर भी सामान्य जन को अनेक अवसरों पर भूल-भुलैया एवं अनिर्णय की स्थिति में डाल देता है। इस टीका में भी ऐसे अनेक प्रकरण हैं जो इस तथ्य को परिपुष्ट करते हैं। उदाहरणार्थ, निम्न प्रश्नोत्तर देखिये :
प्रश्न : आप सभी को सही कह देते हैं। क्या गलत कुछ होता ही नहीं ? उत्तर : हाँ, गलत कुछ होता ही नहीं है । दृष्टिभेद से ही गलत और सही कहा जाता है।
इस आधार पर रस्सी को सांप, काँच को मणि, शुक्ति-रजत आदि के समान भ्रमज्ञान एवं भ्रम की भ्रमवादी की स्वदष्टि से सत्यता सिद्ध की है। इसी प्रकार व्यवहार एवं निश्चय के सत्यासत्य निर्णय में दष्टिभेद का उपयोग किया गया है। जीव के कर्तृत्व-भोक्तृत्व के विषय में कर्म की निमित्तता का व्यावहारिक दष्टिकोण उपादान पद्धति से गौण हो जाता है। वस्तुतः उपादान की चर्चा सामान्य जन के लिये किंचित दुरुह-सी प्रतीत होती है। रागादि प्रवृत्तियों की पुद्गलात्मकता की अज्ञानरूप में व्याख्या तथा उन्हें अशुद्ध जीवोपादान की मान्यता आदि के समान प्रश्नोत्तरियाँ एक निश्चित् बौद्धिक स्तर की अपेक्षा रखती हैं। इस स्तर की उपलब्धि ज्ञानावरण कर्म के विशेष क्षरोपशम से ही संभव है। इसके अभाव में ही भूतकाल में कुंदकुंद एक हजार वर्ष तक अज्ञात रहे और अब इस युग में भेद-विज्ञान के कारण बनते प्रतीत होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञानानंद स्वभाव और भेद-विज्ञान की सही व्याख्या व्यावहारिक जगत के लिये बोधगम्य नहीं हो पा रही है। पंडित जी ने 'अध्यात्म अमृत-कलश' में इसकी युक्तिसंगतता एवं सहज बोधगम्यता के लिये दुर्धर प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि इस ग्रन्थ के रुचिपूर्वक अध्ययन से निश्चय और व्यवहार या निमित्त-उपादान संबंधी मान्यताओं के संबंध में अ हो सकेंगी । अंत में पंडित जी का निम्न सार मननीय है "यदि बंधन स्वीकार करना है, तो शुभ बंधन स्वीकार करिये। शुभ परिणाम करिये । यदि बंधन स्वीकार नहीं है, तो आप शुभ-अशुभ राग में वीतराग भाव स्वीकार करिये। क्योंकि दोनों प्रकार के परिणाम बंधन के हेतु होने से अपराध हैं।"
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org