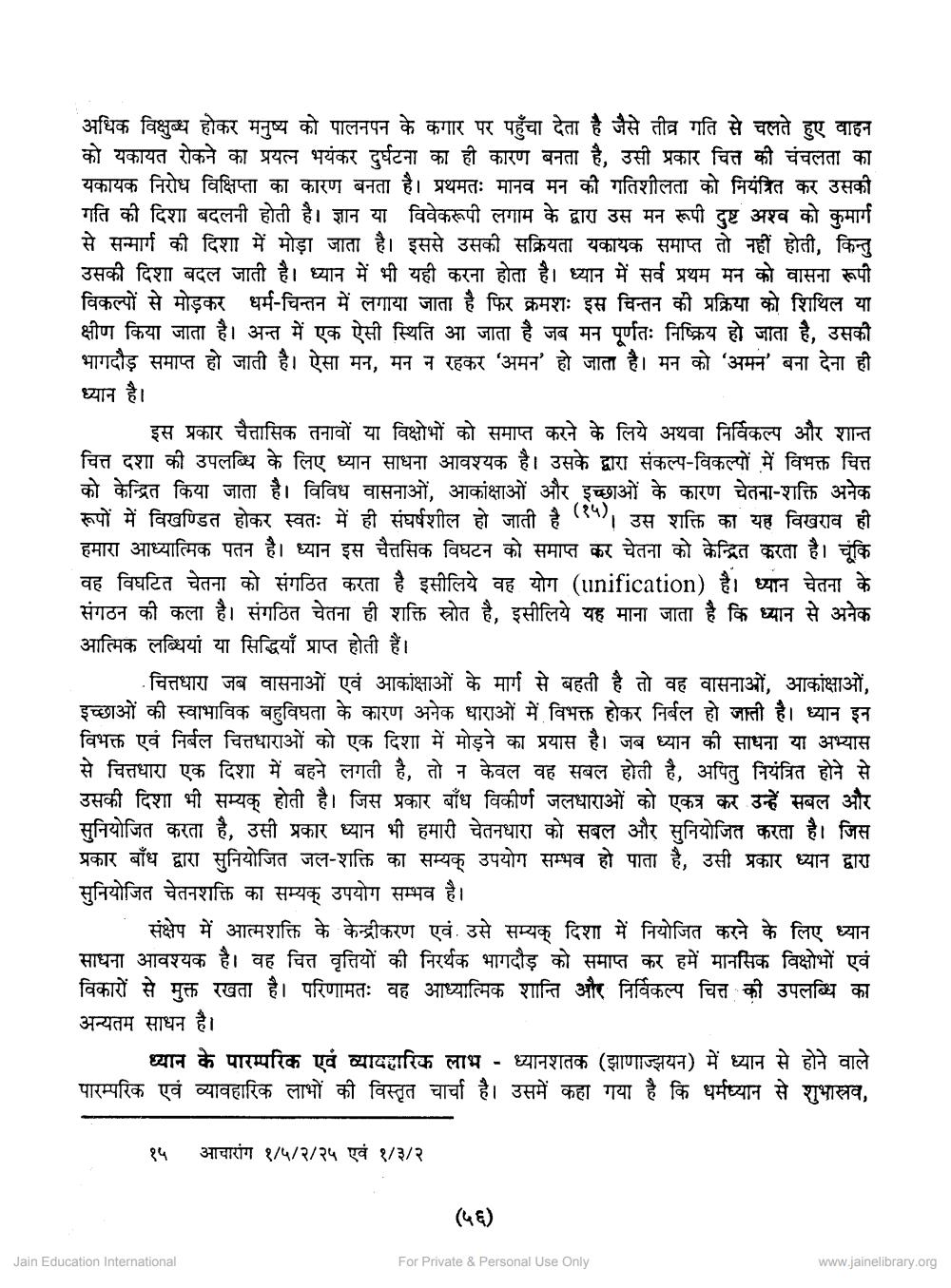________________
अधिक विक्षुब्ध होकर मनुष्य को पालनपन के कगार पर पहुँचा देता है जैसे तीव्र गति से चलते हुए वाहन को यकायत रोकने का प्रयत्न भयंकर दुर्घटना का ही कारण बनता है, उसी प्रकार चित्त की चंचलता का यकायक निरोध विक्षिप्ता का कारण बनता है। प्रथमतः मानव मन की गतिशीलता को नियंत्रित कर उसकी गति की दिशा बदलनी होती है। ज्ञान या विवेकरूपी लगाम के द्वारा उस मन रूपी दुष्ट अश्व को कुमार्ग से सन्मार्ग की दिशा में मोड़ा जाता है। इससे उसकी सक्रियता यकायक समाप्त तो नहीं होती, किन्तु उसकी दिशा बदल जाती है। ध्यान में भी यही करना होता है। ध्यान में सर्व प्रथम मन को वासना रूपी विकल्पों से मोड़कर धर्म-चिन्तन में लगाया जाता है फिर क्रमशः इस चिन्तन की प्रक्रिया को शिथिल या क्षीण किया जाता है। अन्त में एक ऐसी स्थिति आ जाता है जब मन पूर्णतः निष्क्रिय हो जाता है, उसकी भागदौड़ समाप्त हो जाती है। ऐसा मन, मन न रहकर 'अमन' हो जाता है। मन को 'अमन' बना देना ही ध्यान है।
इस प्रकार चैत्तासिक तनावों या विक्षोभों को समाप्त करने के लिये अथवा निर्विकल्प और शान्त चित्त दशा की उपलब्धि के लिए ध्यान साधना आवश्यक है। उसके द्वारा संकल्प-विकल्पों में विभक्त चित्त को केन्द्रित किया जाता है। विविध वासनाओं, आकांक्षाओं और इच्छाओं के कारण चेतना-शक्ति अनेक रूपों में विखण्डित होकर स्वतः में ही संघर्षशील हो जाती है (१५)। उस शक्ति का यह विखराव ही हमारा आध्यात्मिक पतन है। ध्यान इस चैत्तसिक विघटन को समाप्त कर चेतना को केन्द्रित करता है। चूंकि वह विघटित चेतना को संगठित करता है इसीलिये वह योग (unification) है। ध्यान चेतना के संगठन की कला है। संगठित चेतना ही शक्ति स्रोत है, इसीलिये यह माना जाता है कि ध्यान से अनेक आत्मिक लब्धियां या सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं।
चित्तधारा जब वासनाओं एवं आकांक्षाओं के मार्ग से बहती है तो वह वासनाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं की स्वाभाविक बहुविधता के कारण अनेक धाराओं में विभक्त होकर निर्बल हो जाती है। ध्यान इन विभक्त एवं निर्बल चित्तधाराओं को एक दिशा में मोड़ने का प्रयास है। जब ध्यान की साधना या अभ्यास से चित्तधारा एक दिशा में बहने लगती है, तो न केवल वह सबल होती है, अपितु नियंत्रित होने से उसकी दिशा भी सम्यक् होती है। जिस प्रकार बाँध विकीर्ण जलधाराओं को एकत्र कर उन्हें सबल और सुनियोजित करता है, उसी प्रकार ध्यान भी हमारी चेतनधारा को सबल और सुनियोजित करता है। जिस
रा सुनियोजित जल-शक्ति का सम्यक् उपयोग सम्भव हो पाता है, उसी प्रकार ध्यान द्वारा सुनियोजित चेतनशक्ति का सम्यक् उपयोग सम्भव है।
- संक्षेप में आत्मशक्ति के केन्द्रीकरण एवं उसे सम्यक् दिशा में नियोजित करने के लिए ध्यान साधना आवश्यक है। वह चित्त वृत्तियों की निरर्थक भागदौड़ को समाप्त कर हमें मानसिक विक्षोभों एवं विकारों से मुक्त रखता है। परिणामतः वह आध्यात्मिक शान्ति और निर्विकल्प चित्त की उपलब्धि का अन्यतम साधन है।
ध्यान के पारम्परिक एवं व्यावहारिक लाभ - ध्यानशतक (झाणाज्झयन) में ध्यान से होने वाले पारम्परिक एवं व्यावहारिक लाभों की विस्तृत चार्चा है। उसमें कहा गया है कि धर्मध्यान से शुभास्रव,
१५
आचारांग १/५/२/२५ एवं १/३/२
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org