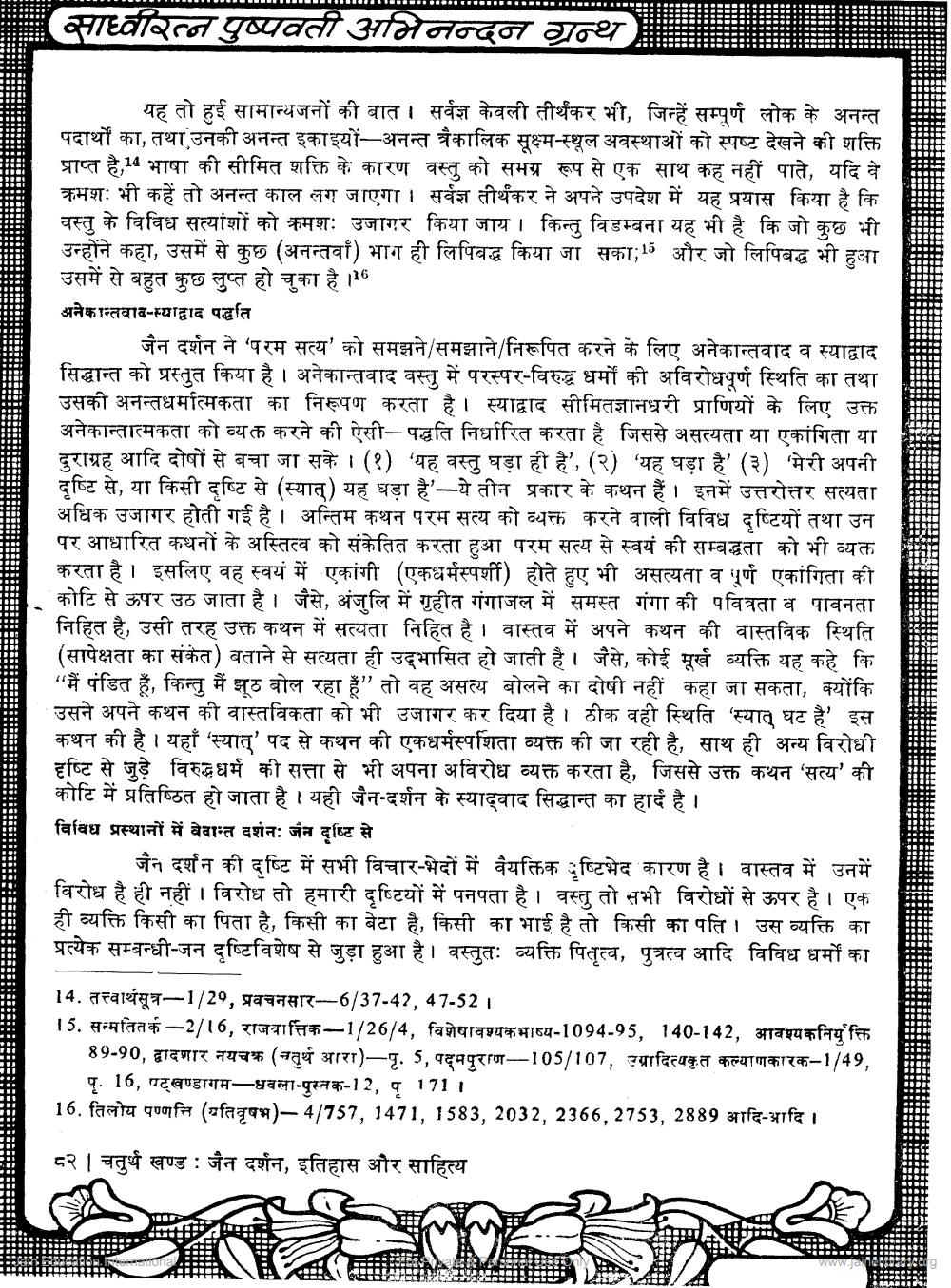________________
साध्वीरत्न पुष्पवती अभिनन्दन ग्रन्थ
यह तो हुई सामान्यजनों की बात । सर्वज्ञ केवली तीर्थंकर भी, जिन्हें सम्पूर्ण लोक के अनन्त पदार्थों का, तथा, उनकी अनन्त इकाइयों - अनन्त त्रैकालिक सूक्ष्म-स्थूल अवस्थाओं को स्पष्ट देखने की शक्ति प्राप्त है, 14 भाषा की सीमित शक्ति के कारण वस्तु को समग्र रूप से एक साथ कह नहीं पाते, यदि वे क्रमशः भी कहें तो अनन्त काल लग जाएगा। सर्वज्ञ तीर्थंकर ने अपने उपदेश में यह प्रयास किया है कि वस्तु के विविध सत्यांशों को क्रमशः उजागर किया जाय । किन्तु विडम्बना यह भी है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा, उसमें से कुछ (अनन्तवाँ ) भाग ही लिपिबद्ध किया जा सका, 15 और जो लिपिबद्ध भी हुआ उसमें से बहुत कुछ लुप्त हो चुका है । 16
अनेकान्तवाद - स्याद्वाद पद्धति
जैन दर्शन ने 'परम सत्य' को समझने / समझाने / निरूपित करने के लिए अनेकान्तवाद व स्याद्वाद सिद्धान्त को प्रस्तुत किया है । अनेकान्तवाद वस्तु में परस्पर विरुद्ध धर्मों की अविरोधपूर्ण स्थिति का तथा उसकी अनन्तधर्मात्मकता का निरूपण करता है । स्याद्वाद सीमितज्ञानधरी प्राणियों के लिए उक्त अनेकान्तात्मकता को व्यक्त करने की ऐसी पद्धति निर्धारित करता है जिससे असत्यता या एकांगिता या दुराग्रह आदि दोषों से बचा जा सके । (१) 'यह वस्तु घड़ा ही है', (२) 'यह घड़ा है' (३) 'मेरी अपनी दृष्टि से, या किसी दृष्टि से (स्यात्) यह घड़ा है' - ये तीन प्रकार के कथन हैं । इनमें उत्तरोत्तर सत्यता अधिक उजागर होती गई है । अन्तिम कथन परम सत्य को व्यक्त करने वाली विविध दृष्टियों तथा उन पर आधारित कथनों के अस्तित्व को संकेतित करता हुआ परम सत्य से स्वयं की सम्बद्धता को भी व्यक्त करता है । इसलिए वह स्वयं में एकांगी ( एकधर्मस्पर्शी) होते हुए भी असत्यता व पूर्ण एकांगिता की कोटि से ऊपर उठ जाता है । जैसे, अंजुलि में गृहीत गंगाजल में समस्त गंगा की पवित्रता व पावनता निहित है, उसी तरह उक्त कथन में सत्यता निहित है । वास्तव में अपने कथन की वास्तविक स्थिति ( सापेक्षता का संकेत ) बताने से सत्यता ही उद्भासित हो जाती है । जैसे, कोई मूर्ख व्यक्ति यह कहे कि " मैं पंडित हूँ, किन्तु मैं झूठ बोल रहा हूँ" तो वह असत्य बोलने का दोषी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने अपने कथन की वास्तविकता को भी उजागर कर दिया है । ठीक वही स्थिति 'स्यात् घट है' इस कथन की है । यहाँ 'स्यात्' पद से कथन की एकधर्मस्पर्शिता व्यक्त की जा रही है, साथ ही अन्य विरोधी दृष्टि से जुड़े विरुद्धधर्म की सत्ता से भी अपना अविरोध व्यक्त करता है, जिससे उक्त कथन 'सत्य' की प्रतिष्ठित हो जाता है । यही जैन दर्शन के स्याद्वाद सिद्धान्त का हार्द है ।
विविध प्रस्थानों में वेदान्त दर्शन: जैन दृष्टि से
जैन दर्शन की दृष्टि में सभी विचार-भेदों में वैयक्तिक दृष्टिभेद कारण है । वास्तव में उनमें विरोध है ही नहीं । विरोध तो हमारी दृष्टियों में पनपता है । वस्तु तो सभी विरोधों से ऊपर है । एक ही व्यक्ति किसी का पिता है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है तो किसी का पति । उस व्यक्ति का प्रत्येक सम्बन्धी जन दृष्टिविशेष से जुड़ा हुआ है। वस्तुतः व्यक्ति पितृत्व, पुत्रत्व आदि विविध धर्मों का
14 तत्त्वार्थसूत्र -- 1 /29, प्रवचनसार - 6/37-42, 47-521
15. सन्मतितर्क - 2 / 16, राजवार्तिक- 1 /26/4, विशेषावश्यक भाष्य 1094 95, 140-142, आवश्यक नियुक्ति 89-90, द्वादशार नयचक्र (चतुर्थ आरा ) - पृ. 5, पद्मपुराण - 105 / 107, उग्रादित्यकृत कल्याणकारक - 1 /49, पृ. 16, पट्खण्डागम - धवला - पुस्तक- 12, पृ 171 |
16. तिलोय पण्णनि ( यतिवृषभ ) - 4 / 757, 1471, 1583, 2032, 2366, 2753, 2889 आदि-आदि।
८२ | चतुर्थ खण्ड : जैन दर्शन, इतिहास और साहित्य