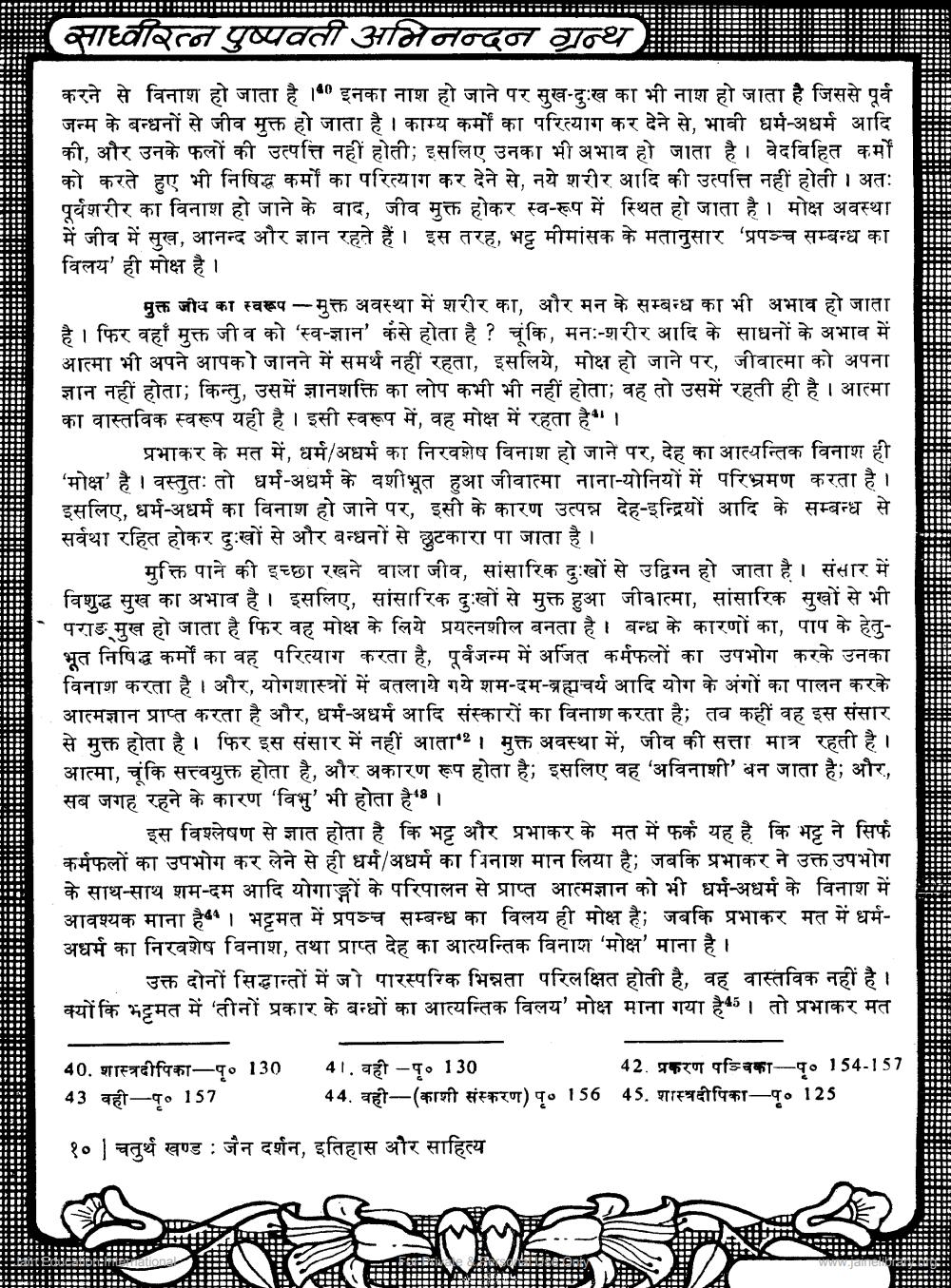________________
.....
साध्वीरत्नपुष्पवती अभिनन्दन ग्रन्थ
...
::.
करने से विनाश हो जाता है । इनका नाश हो जाने पर सुख-दुःख का भी नाश हो जाता है जिससे पूर्व जन्म के बन्धनों से जीव मुक्त हो जाता है । काम्य कर्मों का परित्याग कर देने से, भावी धर्म-अधर्म आदि की, और उनके फलों की उत्पत्ति नहीं होती; इसलिए उनका भी अभाव हो जाता है। वेदविहित कर्मों को करते हुए भी निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर देने से, नये शरीर आदि की उत्पत्ति नहीं होती। अतः पूर्वशरीर का विनाश हो जाने के बाद, जीव मुक्त होकर स्व-रूप में स्थित हो जाता है। मोक्ष अवस्था में जीव में सुख, आनन्द और ज्ञान रहते हैं। इस तरह, भट्ट मीमांसक के मतानुसार 'प्रपञ्च सम्बन्ध का विलय' ही मोक्ष है।
मुक्त जीव का स्वरूप-मुक्त अवस्था में शरीर का, और मन के सम्बन्ध का भी अभाव हो जाता है। फिर वहाँ मुक्त जीव को 'स्व-ज्ञान' कैसे होता है ? चूंकि, मनः-शरीर आदि के साधनों के अभाव में आत्मा भी अपने आपको जानने में समर्थ नहीं रहता, इसलिये, मोक्ष हो जाने पर, जीवात्मा को अपना ज्ञान नहीं होता; किन्तु, उसमें ज्ञानशक्ति का लोप कभी भी नहीं होता; वह तो उसमें रहती ही है । आत्मा का वास्तविक स्वरूप यही है । इसी स्वरूप में, वह मोक्ष में रहता है"।
प्रभाकर के मत में, धर्म/अधर्म का निरवशेष विनाश हो जाने पर, देह का आत्यन्तिक विनाश ही 'मोक्ष' है । वस्तुतः तो धर्म-अधर्म के वशीभूत हुआ जीवात्मा नाना-योनियों में परिभ्रमण करता है। इसलिए, धर्म-अधर्म का विनाश हो जाने पर, इसी के कारण उत्पन्न देह-इन्द्रियों आदि के सम्बन्ध से सर्वथा रहित होकर दुःखों से और बन्धनों से छुटकारा पा जाता है।
मुक्ति पाने की इच्छा रखने वाला जीव, सांसारिक दुःखों से उद्विग्न हो जाता है। संसार में विशुद्ध सुख का अभाव है। इसलिए, सांसारिक दुःखों से मुक्त हुआ जीवात्मा, सांसारिक सुखों से भी पराङ मुख हो जाता है फिर वह मोक्ष के लिये प्रयत्नशील बनता है। बन्ध के कारणों का, पाप के हेतुभूत निषिद्ध कर्मों का वह परित्याग करता है, पूर्वजन्म में अर्जित कर्मफलों का उपभोग करके उनका विनाश करता है। और, योगशास्त्रों में बतलाये गये शम-दम-ब्रह्मचर्य आदि योग के अंगों का पालन करके . आत्मज्ञान प्राप्त करता है और, धर्म-अधर्म आदि संस्कारों का विनाश करता है; तब कहीं वह इस संसार से मुक्त होता है। फिर इस संसार में नहीं आता। मुक्त अवस्था में, जीव की सत्ता मात्र रहती है। आत्मा, चूंकि सत्त्वयुक्त होता है, और अकारण रूप होता है, इसलिए वह 'अविनाशी' बन जाता है; और, सब जगह रहने के कारण 'विभु' भी होता है ।
इस विश्लेषण से ज्ञात होता है कि भट्ट और प्रभाकर के मत में फर्क यह है कि भट्ट ने सिर्फ कर्मफलों का उपभोग कर लेने से ही धर्म/अधर्म का विनाश मान लिया है। जबकि प्रभाकर ने उक्त उपभोग के साथ-साथ शम-दम आदि योगानों के परिपालन से प्राप्त आत्मज्ञान को भी धर्म-अधर्म के विनाश में आवश्यक माना है । भट्टमत में प्रपञ्च सम्बन्ध का विलय ही मोक्ष है। जबकि प्रभाकर मत में धर्मअधर्म का निरवशेष विनाश, तथा प्राप्त देह का आत्यन्तिक विनाश 'मोक्ष' माना है।
उक्त दोनों सिद्धान्तों में जो पारस्परिक भिन्नता परिलक्षित होती है, वह वास्तविक नहीं है। क्यों कि भट्टमत में तीनों प्रकार के बन्धों का आत्यन्तिक विलय' मोक्ष माना गया है। तो प्रभाकर मत
40. शास्त्रदीपिका-पृ० 130 41. वही -पृ. 130
42. प्रकरण पञ्चिका-प० 154-157 43 वही–पृ० 157 44. वही-(काशी संस्करण) पृ. 156 45. शास्त्रदीपिका—पृ. 125 १० | चतुर्थ खण्ड : जैन दर्शन, इतिहास और साहित्य