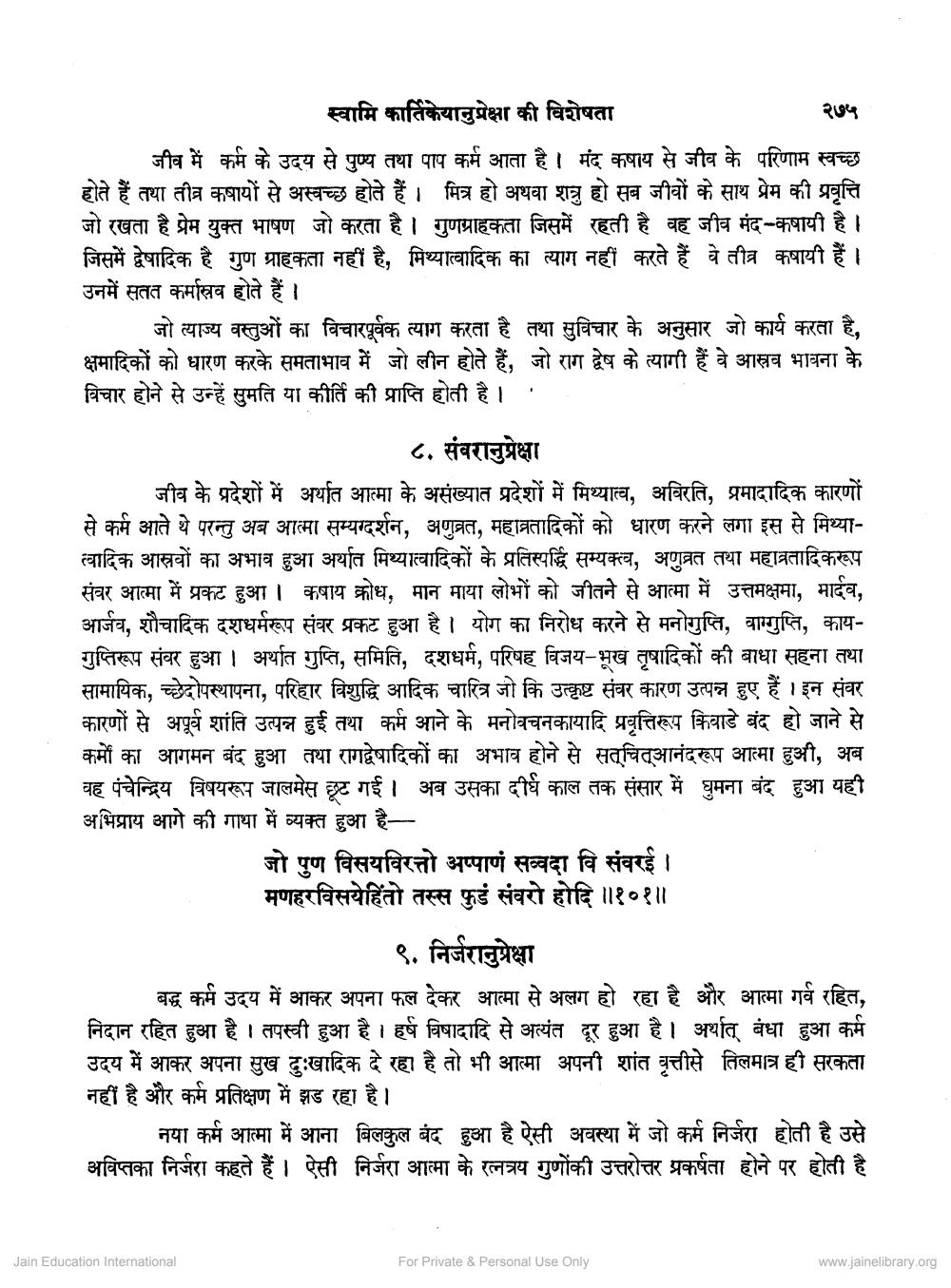________________
२७५
स्वामि कार्तिकेयानुप्रेक्षा की विशेषता जीव में कर्म के उदय से पुण्य तथा पाप कर्म आता है। मंद कषाय से जीव के परिणाम स्वच्छ होते हैं तथा तीव्र कषायों से अस्वच्छ होते हैं। मित्र हो अथवा शत्रु हो सब जीवों के साथ प्रेम की प्रवृत्ति जो रखता है प्रेम युक्त भाषण जो करता है। गुणग्राहकता जिसमें रहती है वह जीव मंद-कषायी है। जिसमें द्वेषादिक है गुण ग्राहकता नहीं है, मिथ्यात्वादिक का त्याग नहीं करते हैं वे तीव्र कषायी हैं। उनमें सतत कर्मास्रव होते हैं।
___ जो त्याज्य वस्तुओं का विचारपूर्वक त्याग करता है तथा सुविचार के अनुसार जो कार्य करता है, क्षमादिकों को धारण करके समताभाव में जो लीन होते हैं, जो राग द्वेष के त्यागी हैं वे आस्रव भावना के विचार होने से उन्हें सुमति या कीर्ति की प्राप्ति होती है। '
८. संवरानुप्रेक्षा __ जीव के प्रदेशों में अर्थात आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमादादिक कारणों से कर्म आते थे परन्तु अब आत्मा सम्यग्दर्शन, अणुव्रत, महाव्रतादिकों को धारण करने लगा इस से मिथ्यात्वादिक आस्रवों का अभाव हुआ अर्थात मिथ्यात्वादिकों के प्रतिस्पर्द्धि सम्यक्त्व, अणुव्रत तथा महाव्रतादिकरूप संवर आत्मा में प्रकट हुआ। कषाय क्रोध, मान माया लोभों को जीतने से आत्मा में उत्तमक्षमा, मार्दव, आर्जव, शौचादिक दशधर्मरूप संवर प्रकट हुआ है। योग का निरोध करने से मनोगुप्ति, वाग्गुप्ति, कायगुप्तिरूप संवर हुआ । अर्थात गुप्ति, समिति, दशधर्म, परिषह विजय-भूख तृषादिकों की बाधा सहना तथा सामायिक, च्छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि आदिक चारित्र जो कि उत्कृष्ट संवर कारण उत्पन्न हुए हैं । इन संवर कारणों से अपूर्व शांति उत्पन्न हुई तथा कर्म आने के मनोवचनकायादि प्रवृत्तिरूप किवाडे बंद हो जाने से कर्मों का आगमन बंद हुआ तथा रागद्वेषादिकों का अभाव होने से सत्चित्आनंदरूप आत्मा हुी, अब वह पंचेन्द्रिय विषयरूप जालमेस छूट गई। अब उसका दीर्घ काल तक संसार में घुमना बंद हुआ यही अभिप्राय आगे की गाथा में व्यक्त हुआ है
जो पुण विसयविरत्तो अप्पाणं सव्वदा वि संवरई । मणहरविसयेहितो तस्स फुडं संवरो होदि ॥१०१॥
९. निर्जरानुप्रेक्षा बद्ध कर्म उदय में आकर अपना फल देकर आत्मा से अलग हो रहा है और आत्मा गर्व रहित, निदान रहित हुआ है । तपस्वी हुआ है । हर्ष विषादादि से अत्यंत दूर हुआ है। अर्थात् बंधा हुआ कर्म उदय में आकर अपना सुख दुःखादिक दे रहा है तो भी आत्मा अपनी शांत वृत्तीसे तिलमात्र ही सरकता नहीं है और कर्म प्रतिक्षण में झड रहा है।
नया कर्म आत्मा में आना बिलकुल बंद हुआ है ऐसी अवस्था में जो कर्म निर्जरा होती है उसे अविप्तका निर्जरा कहते हैं। ऐसी निर्जरा आत्मा के रत्नत्रय गुणोंकी उत्तरोत्तर प्रकर्षता होने पर होती है
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org