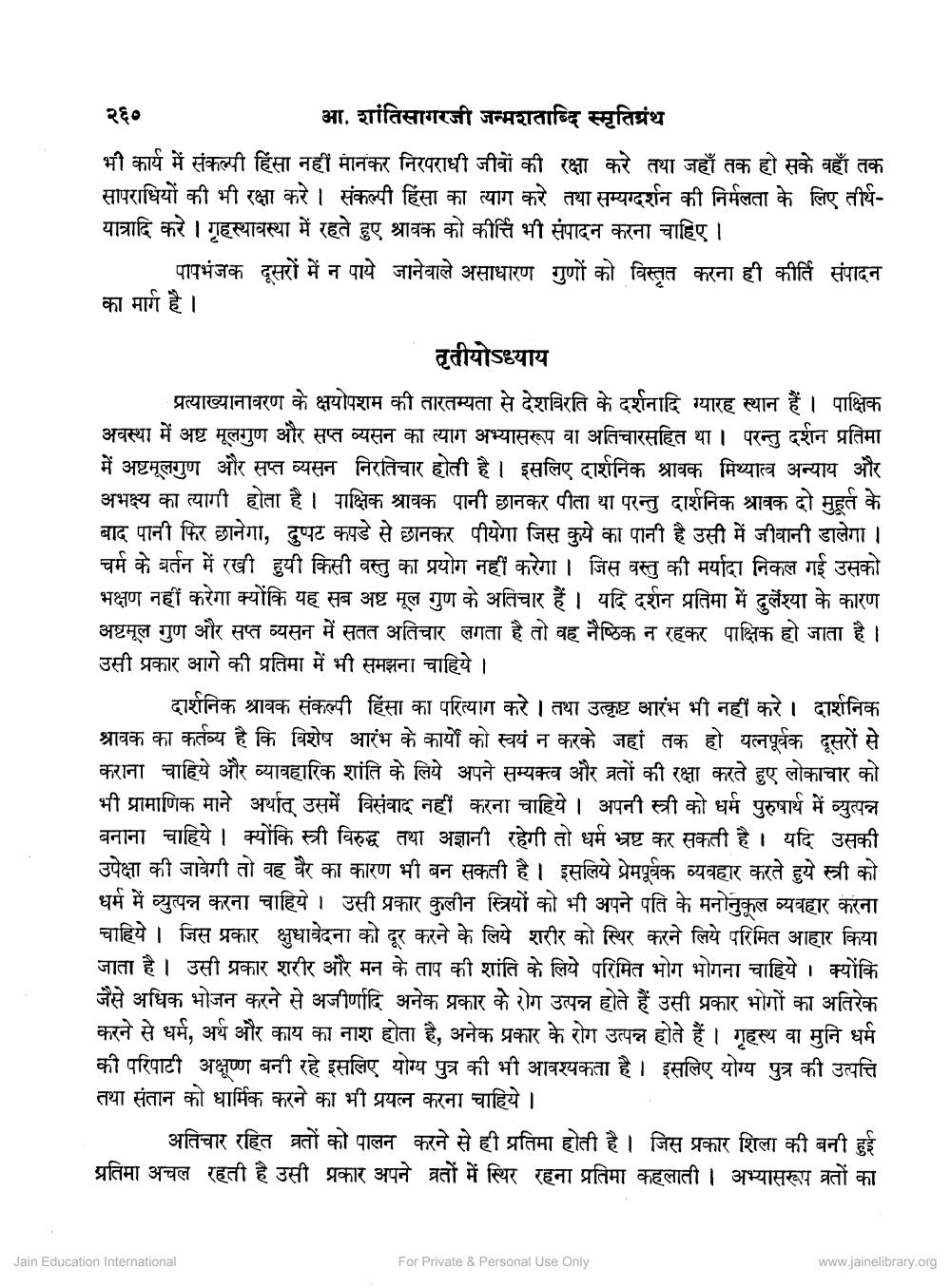________________
२६०
आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्मृतिग्रंथ भी कार्य में संकल्पी हिंसा नहीं मानकर निरपराधी जीवों की रक्षा करे तथा जहाँ तक हो सके वहाँ तक सापराधियों की भी रक्षा करे। संकल्पी हिंसा का त्याग करे तथा सम्यग्दर्शन की निर्मलता के लिए तीर्थयात्रादि करे । गृहस्थावस्था में रहते हुए श्रावक को कीर्ति भी संपादन करना चाहिए ।
पापभंजक दूसरों में न पाये जानेवाले असाधारण गुणों को विस्तृत करना ही कीर्ति संपादन का मार्ग है।
तृतीयोऽध्याय प्रत्याख्यानावरण के क्षयोपशम की तारतम्यता से देशविरति के दर्शनादि ग्यारह स्थान हैं। पाक्षिक अवस्था में अष्ट मूलगुण और सप्त व्यसन का त्याग अभ्यासरूप वा अतिचारसहित था। परन्तु दर्शन प्रतिमा में अष्टमूलगुण और सप्त व्यसन निरतिचार होती है। इसलिए दार्शनिक श्रावक मिथ्यात्व अन्याय और अभक्ष्य का त्यागी होता है। पाक्षिक श्रावक पानी छानकर पीता था परन्तु दार्शनिक श्रावक दो मुहूर्त के बाद पानी फिर छानेगा, दुप्पट कपडे से छानकर पीयेगा जिस कुये का पानी है उसी में जीवानी डालेगा। चर्म के बर्तन में रखी हुयी किसी वस्तु का प्रयोग नहीं करेगा। जिस वस्तु की मर्यादा निकल गई उसको भक्षण नहीं करेगा क्योंकि यह सब अष्ट मूल गुण के अतिचार हैं। यदि दर्शन प्रतिमा में दुर्लेश्या के कारण अष्टमूल गुण और सप्त व्यसन में सतत अतिचार लगता है तो वह नैष्ठिक न रहकर पाक्षिक हो जाता है । उसी प्रकार आगे की प्रतिमा में भी समझना चाहिये ।
दार्शनिक श्रावक संकल्पी हिंसा का परित्याग करे । तथा उत्कृष्ट आरंभ भी नहीं करे। दार्शनिक श्रावक का कर्तव्य है कि विशेष आरंभ के कार्यों को स्वयं न करके जहां तक हो यत्नपूर्वक दूसरों से कराना चाहिये और व्यावहारिक शांति के लिये अपने सम्यक्त्व और व्रतों की रक्षा करते हुए लोकाचार को भी प्रामाणिक माने अर्थात् उसमें विसंवाद नहीं करना चाहिये । अपनी स्त्री को धर्म पुरुषार्थ में व्युत्पन्न बनाना चाहिये। क्योंकि स्त्री विरुद्ध तथा अज्ञानी रहेगी तो धर्म भ्रष्ट कर सकती है। यदि उसकी उपेक्षा की जावेगी तो वह वैर का कारण भी बन सकती है। इसलिये प्रेमपूर्वक व्यवहार करते हुये स्त्री को धर्म में व्युत्पन्न करना चाहिये। उसी प्रकार कुलीन स्त्रियों को भी अपने पति के मनोनुकूल व्यवहार करना चाहिये। जिस प्रकार क्षधावेदना को दूर करने के लिये शरीर को स्थिर करने लिये परिमित आहार किया जाता है। उसी प्रकार शरीर और मन के ताप की शांति के लिये परिमित भोग भोगना चाहिये। क्योंकि जैसे अधिक भोजन करने से अजीर्णादि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार भोगों का अतिरेक करने से धर्म, अर्थ और काय का नाश होता है, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। गृहस्थ वा मुनि धर्म की परिपाटी अक्षुण्ण बनी रहे इसलिए योग्य पुत्र की भी आवश्यकता है। इसलिए योग्य पुत्र की उत्पत्ति तथा संतान को धार्मिक करने का भी प्रयत्न करना चाहिये ।
___अतिचार रहित व्रतों को पालन करने से ही प्रतिमा होती है। जिस प्रकार शिला की बनी हुई प्रतिमा अचल रहती है उसी प्रकार अपने व्रतों में स्थिर रहना प्रतिमा कहलाती। अभ्यासरूप व्रतों का
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org