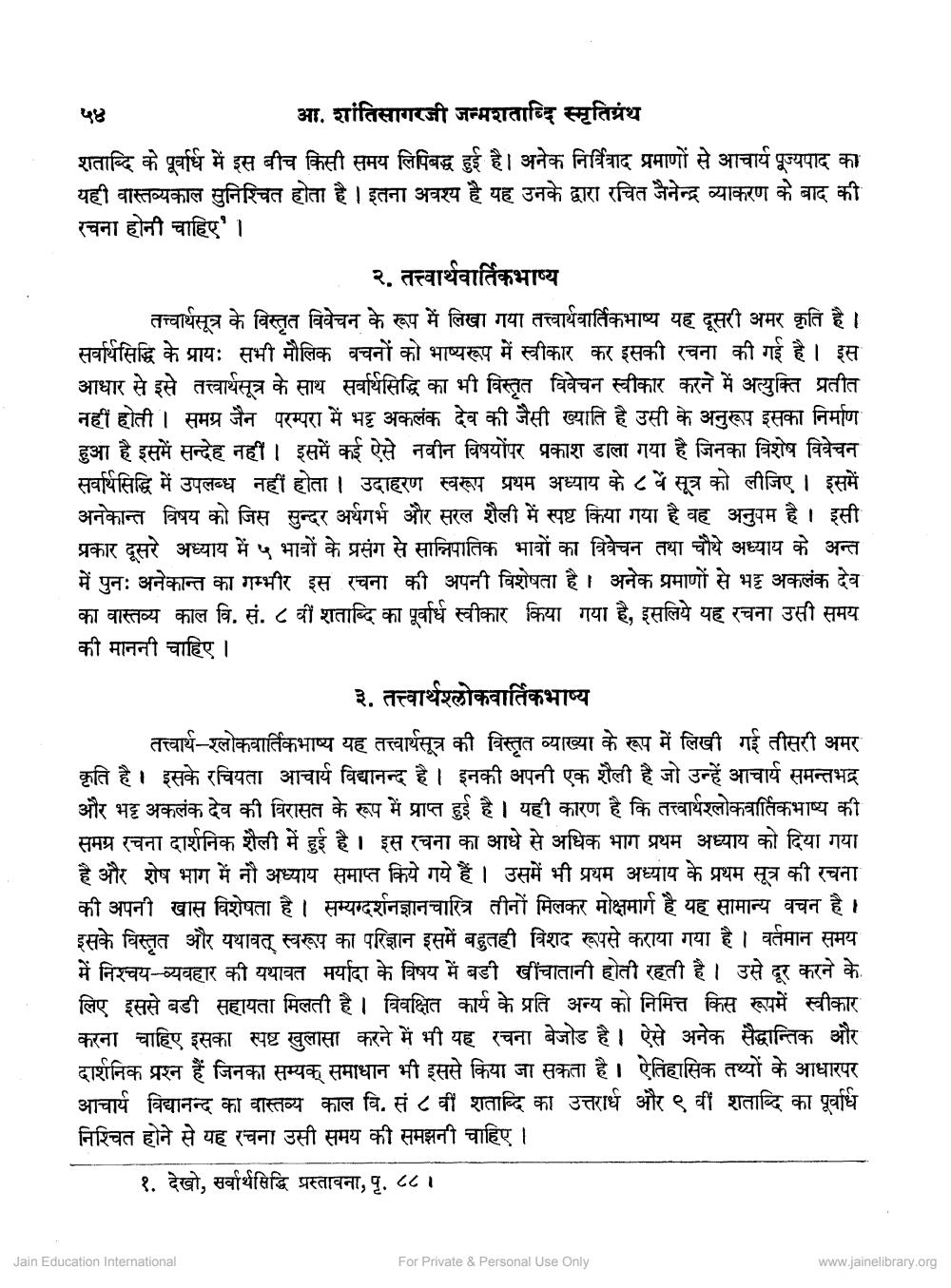________________
५४
आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्मृतिग्रंथ
शताब्दि के पूर्वार्ध में इस बीच किसी समय लिपिबद्ध हुई है । अनेक निर्विवाद प्रमाणों से आचार्य पूज्यपाद का यही वास्तव्यकाल सुनिश्चित होता है । इतना अवश्य है यह उनके द्वारा रचित जैनेन्द्र व्याकरण के बाद की रचना होनी चाहिए' ।
२. तत्त्वार्थवार्तिकभाष्य
तत्त्वार्थसूत्र के विस्तृत विवेचन के रूप में लिखा गया तत्त्वार्यवार्तिकभाष्य यह दूसरी अमर कृति है । सर्वार्थसिद्धि के प्रायः सभी मौलिक वचनों को भाष्यरूप में स्वीकार कर इसकी रचना की गई है । इस आधार से इसे तत्त्वार्थसूत्र के साथ सर्वार्थसिद्धि का भी विस्तृत विवेचन स्वीकार करने में अत्युक्ति प्रतीत नहीं होती । समग्र जैन परम्परा में भट्ट अकलंक देव की जैसी ख्याति है उसी के अनुरूप इसका निर्माण हुआ है इसमें सन्देह नहीं । इसमें कई ऐसे नवीन विषयोंपर प्रकाश डाला गया है जिनका विशेष विवेचन सर्वार्थसिद्धि में उपलब्ध नहीं होता । उदाहरण स्वरूप प्रथम अध्याय के ८ वें सूत्र को लीजिए । इसमें अनेकान्त विषय को जिस सुन्दर अर्थगर्भ और सरल शैली में स्पष्ट किया गया है वह अनुपम है । इसी प्रकार दूसरे अध्याय में ५ भावों के प्रसंग से सान्निपातिक भावों का विवेचन तथा चौथे अध्याय के अन्त में पुनः अनेकान्त का गम्भीर इस रचना की अपनी विशेषता है । अनेक प्रमाणों से भट्ट अकलंक देव का वास्तव्य काल वि. सं. ८ वीं शताब्दि का पूर्वार्ध स्वीकार किया गया है, इसलिये यह रचना उसी समय की माननी चाहिए |
३. तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकभाष्य
तत्त्वार्थ–श्लोकवार्तिकभाष्य यह तत्त्वार्थसूत्र की विस्तृत व्याख्या के रूप में लिखी गई तीसरी अमर कृति है । इसके रचियता आचार्य विद्यानन्द है । इनकी अपनी एक शैली है जो उन्हें आचार्य समन्तभद्र और भट्ट अकलंक देव की विरासत के रूप में प्राप्त हुई है । यही कारण है कि तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकभाष्य की समग्र रचना दार्शनिक शैली में हुई है। इस रचना का आधे से अधिक भाग प्रथम अध्याय को दिया गया है और शेष भाग में नौ अध्याय समाप्त किये गये हैं । उसमें भी प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र की रचना की अपनी खास विशेषता है । सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र तीनों मिलकर मोक्षमार्ग है यह सामान्य वचन है । इसके विस्तृत और यथावत् स्वरूप का परिज्ञान इसमें बहुतही विशद रूपसे कराया गया है। वर्तमान समय में निश्चय-व्यवहार की यथावत मर्यादा के विषय में बडी खींचातानी होती रहती है । उसे दूर करने के लिए इससे बडी सहायता मिलती है । विवक्षित कार्य के प्रति अन्य को निमित्त किस रूप में स्वीकार करना चाहिए इसका स्पष्ट खुलासा करने में भी यह रचना बेजोड है । ऐसे अनेक सैद्धान्तिक और दार्शनिक प्रश्न हैं जिनका सम्यक् समाधान भी इससे किया जा सकता है । ऐतिहासिक तथ्यों के आधारपर आचार्य विद्यानन्द का वास्तव्य काल वि. सं ८ वीं शताब्दि का उत्तरार्ध और ९ वीं शताब्दि का पूर्वार्ध निश्चित होने से यह रचना उसी समय की समझनी चाहिए ।
१. देखो, सर्वार्थसिद्धि प्रस्तावना, पृ. ८८ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org