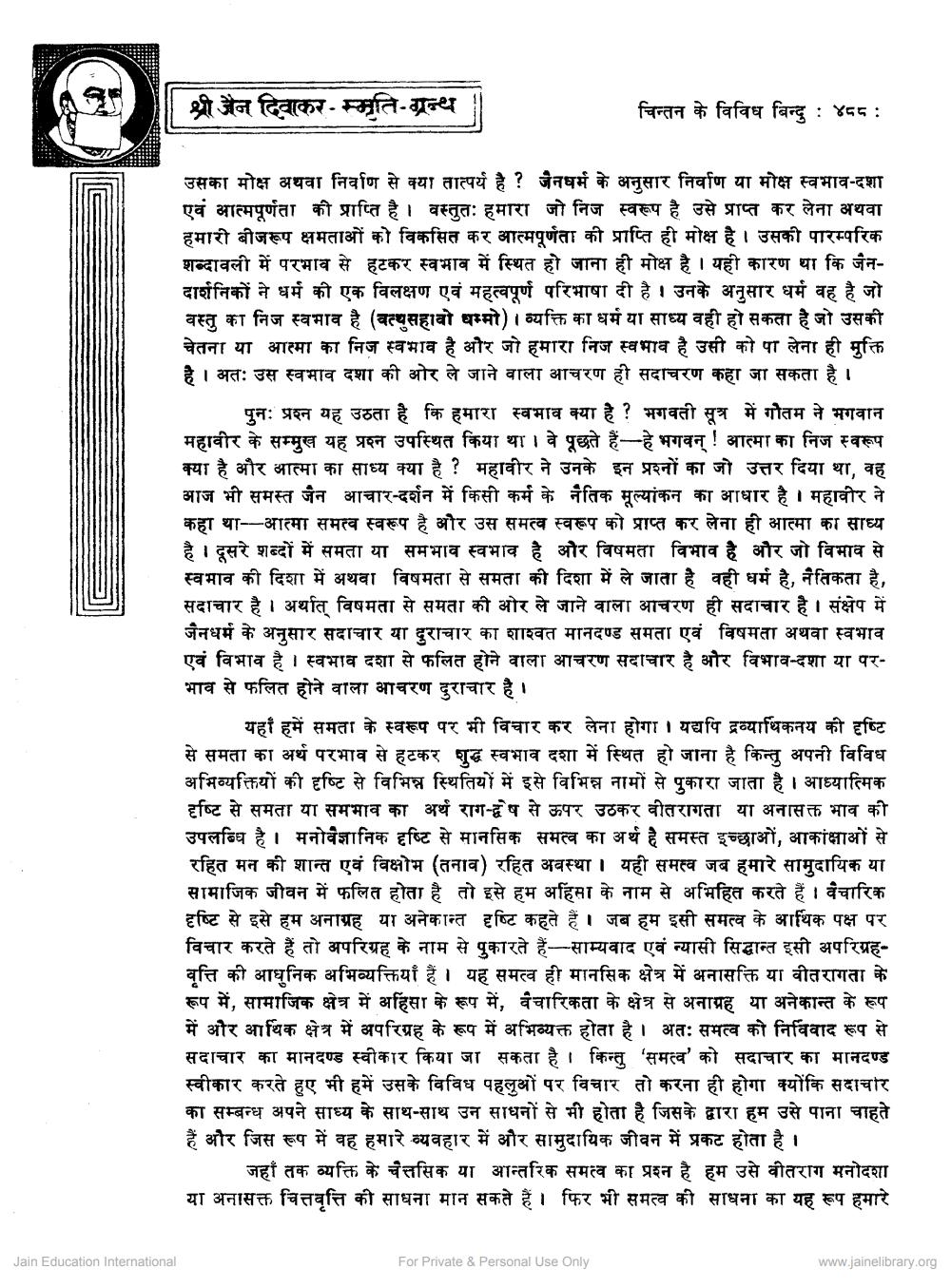________________
| श्री जैन दिवाकर म्मृति-ग्रन्थ ।।
चिन्तन के विविध बिन्दु : ४८८ :
उसका मोक्ष अथवा निर्वाण से क्या तात्पर्य है ? जैनधर्म के अनुसार निर्वाण या मोक्ष स्वभाव-दशा एवं आत्मपूर्णता की प्राप्ति है। वस्तुतः हमारा जो निज स्वरूप है उसे प्राप्त कर लेना अथवा हमारी बीजरूप क्षमताओं को विकसित कर आत्मपूर्णता की प्राप्ति ही मोक्ष है। उसकी पारम्परिक शब्दावली में परभाव से हटकर स्वभाव में स्थित हो जाना ही मोक्ष है। यही कारण था कि जैनदार्शनिकों ने धर्म की एक विलक्षण एवं महत्वपूर्ण परिभाषा दी है। उनके अनुसार धर्म वह है जो वस्तु का निज स्वभाव है (वत्थुसहावो धम्मो)। व्यक्ति का धर्म या साध्य वही हो सकता है जो उसकी चेतना या आत्मा का निज स्वभाव है और जो हमारा निज स्वभाव है उसी को पा लेना ही मुक्ति है। अतः उस स्वभाव दशा की ओर ले जाने वाला आचरण ही सदाचरण कहा जा सकता है।
पुनः प्रश्न यह उठता है कि हमारा स्वभाव क्या है ? भगवती सूत्र में गौतम ने भगवान महावीर के सम्मुख यह प्रश्न उपस्थित किया था। वे पूछते हैं-हे भगवन् ! आत्मा का निज स्वरूप क्या है और आत्मा का साध्य क्या है ? महावीर ने उनके इन प्रश्नों का जो उत्तर दिया था, वह आज भी समस्त जैन आचार-दर्शन में किसी कर्म के नैतिक मूल्यांकन का आधार है। महावीर ने कहा था-आत्मा समत्व स्वरूप है और उस समत्व स्वरूप को प्राप्त कर लेना ही आत्मा का साध्य है। दूसरे शब्दों में समता या समभाव स्वभाव है और विषमता विभाव है और जो विभाव से स्वभाव की दिशा में अथवा विषमता से समता की दिशा में ले जाता है वही धर्म है, नैतिकता है, सदाचार है । अर्थात् विषमता से समता की ओर ले जाने वाला आचरण ही सदाचार है। संक्षेप में जैनधर्म के अनुसार सदाचार या दुराचार का शाश्वत मानदण्ड समता एवं विषमता अथवा स्वभाव एवं विभाव है । स्वभाव दशा से फलित होने वाला आचरण सदाचार है और विभाव-दशा या परभाव से फलित होने वाला आचरण दुराचार है।
यहाँ हमें समता के स्वरूप पर भी विचार कर लेना होगा। यद्यपि द्रव्याथिकनय की दृष्टि से समता का अर्थ परभाव से हटकर शुद्ध स्वभाव दशा में स्थित हो जाना है किन्तु अपनी विविध अभिव्यक्तियों की दृष्टि से विभिन्न स्थितियों में इसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से समता या समभाव का अर्थ राग-द्वेष से ऊपर उठकर वीतरागता या अनासक्त भाव की उपलब्धि है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मानसिक समत्व का अर्थ है समस्त इच्छाओं, आकांक्षाओं से रहित मन की शान्त एवं विक्षोभ (तनाव) रहित अवस्था। यही समत्व जब हमारे सामुदायिक या सामाजिक जीवन में फलित होता है तो इसे हम अहिंसा के नाम से अभिहित करते हैं। वैचारिक दृष्टि से इसे हम अनाग्रह या अनेकान्त दृष्टि कहते हैं। जब हम इसी समत्व के आर्थिक पक्ष पर विचार करते हैं तो अपरिग्रह के नाम से पुकारते हैं-साम्यवाद एवं न्यासी सिद्धान्त इसी अपरिग्रहवृत्ति की आधुनिक अभिव्यक्तियाँ हैं। यह समत्व ही मानसिक क्षेत्र में अनासक्ति या वीतरागता के रूप में, सामाजिक क्षेत्र में अहिंसा के रूप में, वैचारिकता के क्षेत्र से अनाग्रह या अनेकान्त के रूप में और आर्थिक क्षेत्र में अपरिग्रह के रूप में अभिव्यक्त होता है। अतः समत्व को निर्विवाद रूप से सदाचार का मानदण्ड स्वीकार किया जा सकता है। किन्तु 'समत्व' को सदाचार का मानदण्ड स्वीकार करते हुए भी हमें उसके विविध पहलुओं पर विचार तो करना ही होगा क्योंकि सदाचार का सम्बन्ध अपने साध्य के साथ-साथ उन साधनों से भी होता है जिसके द्वारा हम उसे पाना चाहते हैं और जिस रूप में वह हमारे व्यवहार में और सामुदायिक जीवन में प्रकट होता है ।
जहाँ तक व्यक्ति के चैत्तसिक या आन्तरिक समत्व का प्रश्न है हम उसे वीतराग मनोदशा या अनासक्त चित्तवृत्ति की साधना मान सकते हैं। फिर भी समत्व की साधना का यह रूप हमारे
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org