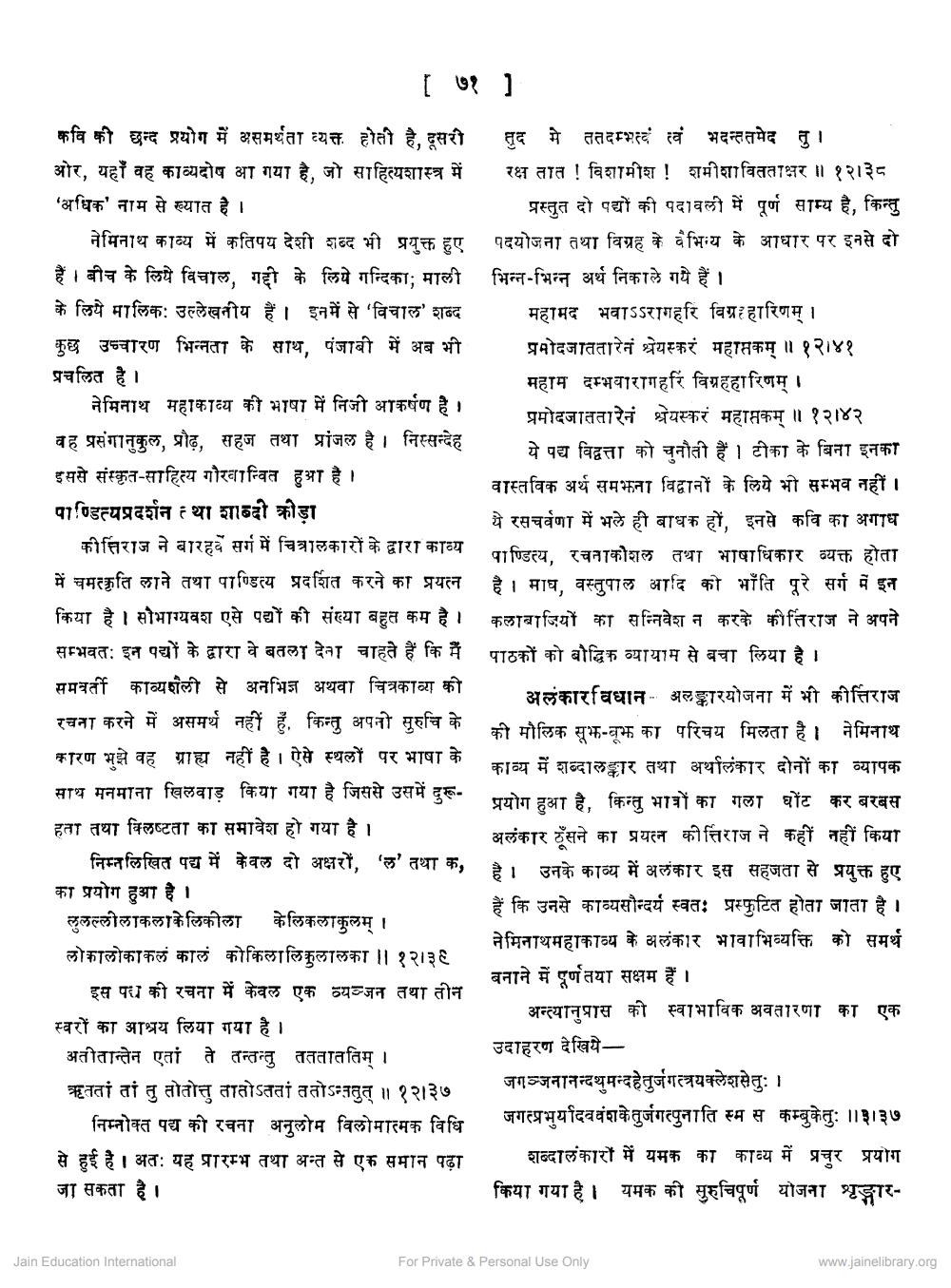________________
[
७१
]
कवि की छन्द प्रयोग में असमर्थता व्यक्त होती है, दूसरी तुद मे ततदम्भत्वं त्वं भदन्ततमेद तु। ओर, यहाँ वह काव्यदोष आ गया है, जो साहित्यशास्त्र में रक्ष तात ! विशामीश ! शमीशा वितताक्षर ॥ १२॥३८ 'अधिक' नाम से ख्यात है।
प्रस्तुत दो पद्यों की पदावली में पूर्ण साम्य है, किन्तु नेमिनाथ काव्य में कतिपय देशी शब्द भी प्रयुक्त हुए पदयोजना तथा विग्रह के वैभिन्य के आधार पर इनसे दो हैं । बीच के लिये विचाल, गद्दी के लिये गन्दिका; माली भिन्न-भिन्न अर्थ निकाले गये हैं । के लिये मालिक: उल्लेखनीय हैं। इनमें से 'विचाल' शब्द महामद भवाऽऽरागहरि विग्रहहारिणम् । कुछ उच्चारण भिन्नता के साथ, पंजाबी में अब भी प्रमोदजाततारेनं श्रेयस्करं महाप्तकम् ॥ १२॥४१ प्रचलित है।
महाम दम्भवाराग हरिं विग्रहहारिणम् । नेमिनाथ महाकाव्य की भाषा में निजी आकर्षण है।
प्रमोदजाततारेनं श्रेयस्करं महाप्तकम् ॥ १२॥४२ वह प्रसंगानुकुल, प्रौढ़, सहज तथा प्रांजल है। निस्सन्देह
ये पद्य विद्वत्ता को चुनौती हैं । टीका के बिना इनका इससे संस्कृत-साहित्य गौरवान्वित हुआ है।
वास्तविक अर्थ समझना विद्वानों के लिये भी सम्भव नहीं। पाण्डित्यप्रदर्शन था शाब्दी क्रीड़ा
ये रसचर्वणा में भले ही बाधक हों, इनसे कवि का अगाध कीतिराज ने बारह सर्ग में चित्रालकारों के द्वारा काव्य
पाण्डित्य, रचनाकौशल तथा भाषाधिकार व्यक्त होता में चमत्कृति लाने तथा पाण्डित्य प्रदर्शित करने का प्रयत्न है। माघ, वस्तुपाल आदि को भाँति पूरे सर्ग में इन किया है । सौभाग्यवश एसे पद्यों की संख्या बहुत कम है। कलाबाजियों का सन्निवेश न करके कीतिराज ने अपने सम्भवत: इन पद्यों के द्वारा वे बतला देना चाहते हैं कि मैं पाठकों को बौद्धिक व्यायाम से बचा लिया है। समवर्ती काव्यशैली से अनभिज्ञ अथवा चित्रकाव्य की
अलंकारविधान- अलङ्कारयोजना में भी कीर्तिराज रचना करने में असमर्थ नहीं हुँ, किन्तु अपनी सुरुचि के की मौलिक सूझ-बूझ का परिचय मिलता है। नेमिनाथ कारण मुझे वह ग्राह्य नहीं है । ऐसे स्थलों पर भाषा के
काव्य में शब्दालङ्कार तथा अर्थालंकार दोनों का व्यापक साथ मनमाना खिलवाड़ किया गया है जिससे उसमें दुरू
'दुल प्रयोग हुआ है, किन्तु भावों का गला घोंट कर बरबस हता तथा क्लिष्टता का समावेश हो गया है।
अलंकार हँसने का प्रयत्न कीर्तिराज ने कहीं नहीं किया निम्नलिखित पद्य में केवल दो अक्षरों, 'ल' तथा क, है। उनके काव्य में अलंकार इस सहजता से प्रयुक्त हुए का प्रयोग हुआ है।
हैं कि उनसे काव्यसौन्दर्य स्वतः प्रस्फुटित होता जाता है । लुलल्लीलाकलाके लिकीला केलिकलाकुलम् ।
नेमिनाथमहाकाव्य के अलंकार भावाभिव्यक्ति को समर्थ लोकालोकाकलं कालं कोकिलालिकुलालका ।। १२।३६
बनाने में पूर्णतया सक्षम हैं। इस पद्य की रचना में केवल एक व्यञ्जन तथा तीन
____ अन्त्यानुप्रास की स्वाभाविक अवतारणा का एक स्वरों का आश्रय लिया गया है। अतीतान्तेन एतां ते तन्तन्तु ततताततिम् ।
उदाहरण देखियेऋततां तां तु तोतोत्तु तातोऽततां ततोऽन्ततुत् ॥ १२॥३७ ।।
जगञ्जनानन्दथुमन्दहेतुर्जगत्त्रयक्लेशसेतुः । निम्नोक्त पद्य की रचना अनुलोम विलोमात्मक विधि
जगत्प्रभुर्यादववंशकेतुर्जगत्पुनाति स्म स कम्बुकेतुः ।।३।३७ से हुई है। अत: यह प्रारम्भ तथा अन्त से एक समान पढा शब्दालंकारों में यमक का काव्य में प्रचर प्रयोग जा सकता है।
किया गया है। यमक की सुरुचिपूर्ण योजना शृङ्गार
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org