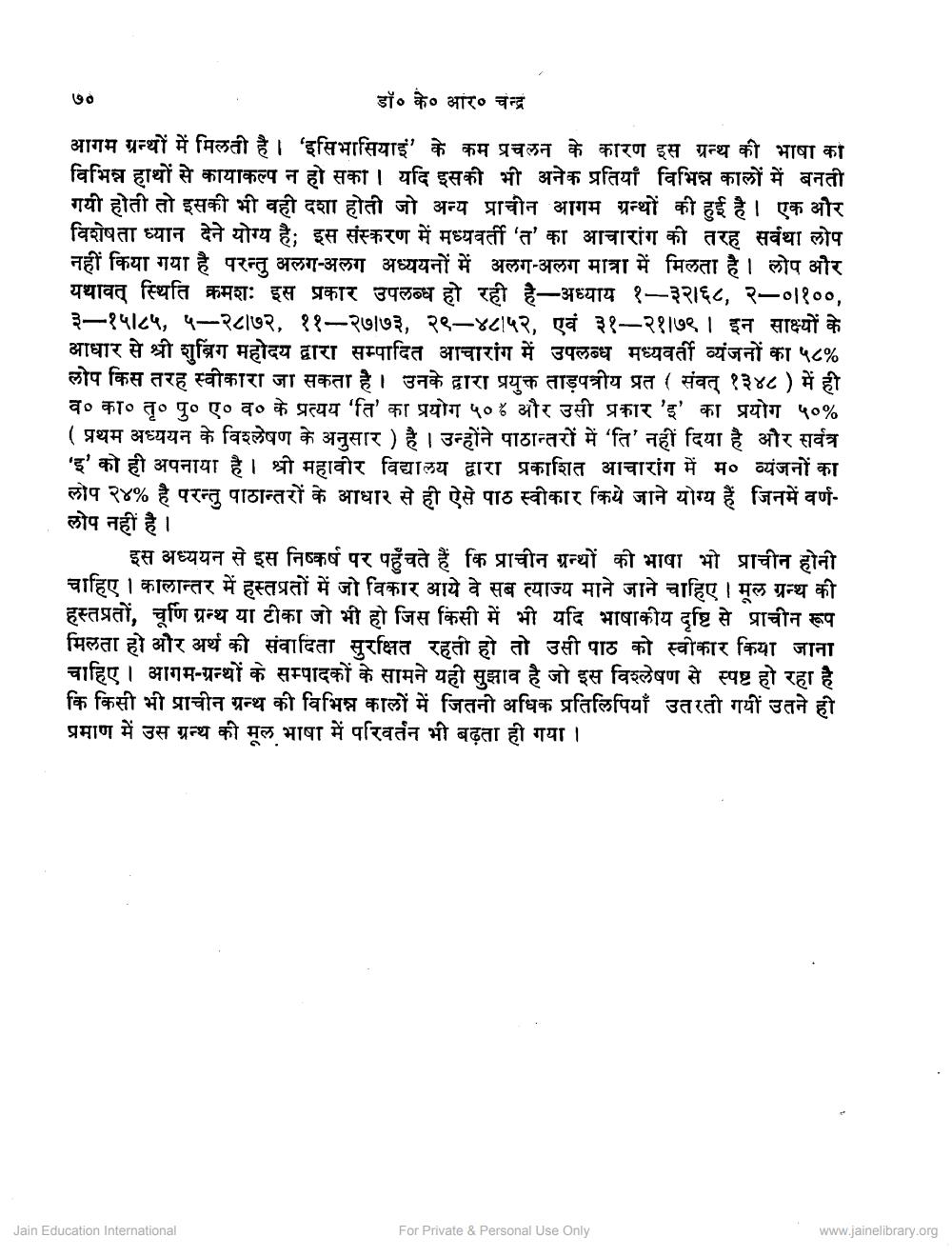________________
७०
डॉ० के० आर० चन्द्र
आगम ग्रन्थों में मिलती है। 'इसिभासियाई' के कम प्रचलन के कारण इस ग्रन्थ की भाषा का विभिन्न हाथों से कायाकल्प न हो सका । यदि इसकी भी अनेक प्रतियाँ विभिन्न कालों में बनती गयी होती तो इसकी भी वही दशा होती जो अन्य प्राचीन आगम ग्रन्थों की हुई है। एक और विशेषता ध्यान देने योग्य है। इस संस्करण में मध्यवर्ती 'त' का आचारांग की तरह सर्वथा लोप नहीं किया गया है परन्तु अलग-अलग अध्ययनों में अलग-अलग मात्रा में मिलता है। लोप और यथावत् स्थिति क्रमशः इस प्रकार उपलब्ध हो रही है-अध्याय १-३२।६८, २-०।१००, ३-१५/८५, ५-२८।७२, ११-२७।७३, २९-४८५२, एवं ३१-२१।७९ । इन साक्ष्यों के आधार से श्री शुब्रिग महोदय द्वारा सम्पादित आचारांग में उपलब्ध मध्यवर्ती व्यंजनों का ५८% लोप किस तरह स्वीकारा जा सकता है। उनके द्वारा प्रयुक्त ताड़पत्रीय प्रत ( संवत् १३४८ ) में ही व० का० त० पू० ए० व० के प्रत्यय 'ति' का प्रयोग ५०४ और उसी प्रकार 'इ' का प्रयोग ५०% ( प्रथम अध्ययन के विश्लेषण के अनुसार ) है । उन्होंने पाठान्तरों में 'ति' नहीं दिया है और सर्वत्र 'इ' को ही अपनाया है। श्री महावीर विद्यालय द्वारा प्रकाशित आचारांग में म० व्यंजनों का लोप २४% है परन्तु पाठान्तरों के आधार से ही ऐसे पाठ स्वीकार किये जाने योग्य हैं जिनमें वर्णलोप नहीं है।
इस अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्राचीन ग्रन्थों की भाषा भो प्राचीन होनी चाहिए । कालान्तर में हस्तप्रतों में जो विकार आये वे सब त्याज्य माने जाने चाहिए। मूल ग्रन्थ की हस्तप्रतों, चूणि ग्रन्थ या टीका जो भी हो जिस किसी में भी यदि भाषाकीय दृष्टि से प्राचीन रूप मिलता हो और अर्थ की संवादिता सुरक्षित रहती हो तो उसी पाठ को स्वीकार किया जाना चाहिए। आगम-ग्रन्थों के सम्पादकों के सामने यही सुझाव है जो इस विश्लेषण से स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी प्राचीन ग्रन्थ की विभिन्न कालों में जितनी अधिक प्रतिलिपियाँ उतरती गयीं उतने ही प्रमाण में उस ग्रन्थ की मल भाषा में परिवर्तन भी बढ़ता ही गया।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org