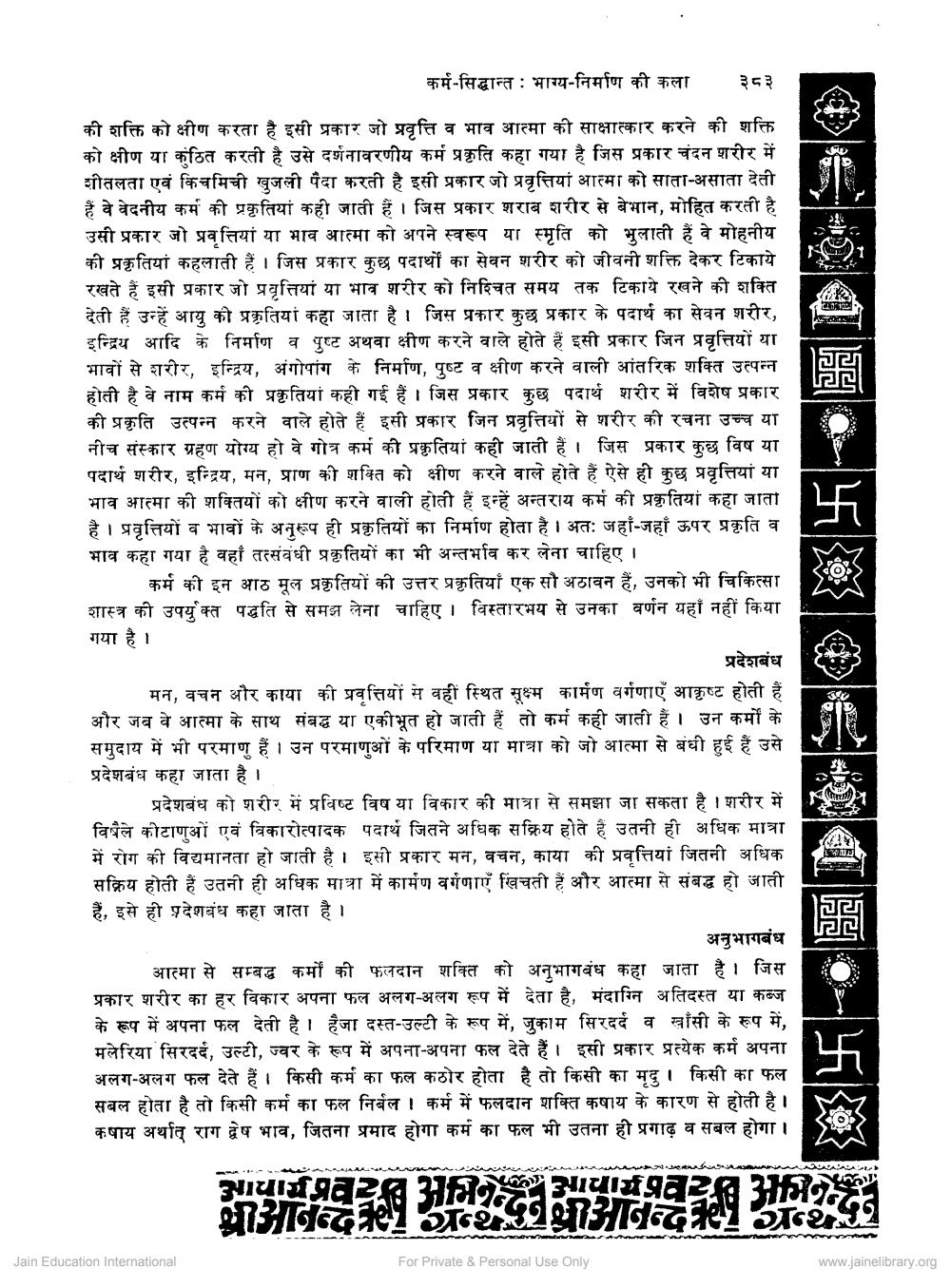________________
कर्म-सिद्धान्त : भाग्य-निर्माण की कला
३८३
का
की शक्ति को क्षीण करता है इसी प्रकार जो प्रवृत्ति व भाव आत्मा की साक्षात्कार करने की शक्ति को क्षीण या कुंठित करती है उसे दर्शनावरणीय कर्म प्रकृति कहा गया है जिस प्रकार चंदन शरीर में शीतलता एवं किचमिची खुजली पैदा करती है इसी प्रकार जो प्रवृत्तियां आत्मा को साता-असाता देती हैं वे वेदनीय कर्म की प्रकृतियां कही जाती हैं। जिस प्रकार शराब शरीर से बेभान, मोहित करती है उसी प्रकार जो प्रवृत्तियां या भाव आत्मा को अपने स्वरूप या स्मृति को भुलाती हैं वे मोहनीय की प्रकृतियां कहलाती हैं। जिस प्रकार कुछ पदार्थों का सेवन शरीर को जीवनी शक्ति देकर टिकाये रखते हैं इसी प्रकार जो प्रवृत्तियां या भाव शरीर को निश्चित समय तक टिकाये रखने की शक्ति देती हैं उन्हें आयु की प्रकृतियां कहा जाता है। जिस प्रकार कुछ प्रकार के पदार्थ का सेवन शरीर, इन्द्रिय आदि के निर्माण व पुष्ट अथवा क्षीण करने वाले होते हैं इसी प्रकार जिन प्रवृत्तियों या भावों से शरीर, इन्द्रिय, अंगोपांग के निर्माण, पुष्ट व क्षीण करने वाली आंतरिक शक्ति उत्पन्न होती है वे नाम कर्म की प्रकृतियां कही गई हैं। जिस प्रकार कुछ पदार्थ शरीर में विशेष प्रकार की प्रकृति उत्पन्न करने वाले होते हैं इसी प्रकार जिन प्रवृत्तियों से शरीर की रचना उच्च या नीच संस्कार ग्रहण योग्य हो वे गोत्र कर्म की प्रकृतियां कही जाती हैं। जिस प्रकार कुछ विष या पदार्थ शरीर, इन्द्रिय, मन, प्राण की शक्ति को क्षीण करने वाले होते हैं ऐसे ही कुछ प्रवृत्तियां या भाव आत्मा की शक्तियों को क्षीण करने वाली होती हैं इन्हें अन्तराय कर्म की प्रकृतियां कहा जाता है। प्रवृत्तियों व भावों के अनुरूप ही प्रकृतियों का निर्माण होता है । अत: जहाँ-जहाँ ऊपर प्रकृति व भाव कहा गया है वहाँ तत्संबंधी प्रकृतियों का भी अन्तर्भाव कर लेना चाहिए।
कर्म की इन आठ मूल प्रकृतियों की उत्तर प्रकृतियाँ एक सौ अठावन हैं, उनको भी चिकित्सा शास्त्र की उपर्युक्त पद्धति से समझ लेना चाहिए। विस्तारभय से उनका वर्णन यहाँ नहीं किया । गया है।
प्रदेशबंध मन, वचन और काया की प्रवृत्तियों से वहीं स्थित सुक्ष्म कार्मण वर्गणाएँ आकृष्ट होती हैं और जब वे आत्मा के साथ संबद्ध या एकीभूत हो जाती हैं तो कर्म कही जाती हैं। उन कर्मों के समुदाय में भी परमाणु हैं। उन परमाणुओं के परिमाण या मात्रा को जो आत्मा से बंधी हुई हैं उसे प्रदेशबंध कहा जाता है।
प्रदेशबंध को शरीर में प्रविष्ट विष या विकार की मात्रा से समझा जा सकता है । शरीर में विषैले कीटाणुओं एवं विकारोत्पादक पदार्थ जितने अधिक सक्रिय होते हैं उतनी ही अधिक मात्रा में रोग की विद्यमानता हो जाती है। इसी प्रकार मन, वचन, काया की प्रवृत्तियां जितनी अधिक सक्रिय होती हैं उतनी ही अधिक मात्रा में कार्मण वर्गणाएँ खिचती हैं और आत्मा से संबद्ध हो जाती हैं, इसे ही प्रदेशबंध कहा जाता है।
अनुभागबंध आत्मा से सम्बद्ध कर्मों की फलदान शक्ति को अनुभागबंध कहा जाता है। जिस प्रकार शरीर का हर विकार अपना फल अलग-अलग रूप में देता है, मंदाग्नि अतिदस्त या कब्ज के रूप में अपना फल देती है। हैजा दस्त-उल्टी के रूप में, जुकाम सिरदर्द व खाँसी के रूप में, मलेरिया सिरदर्द, उल्टी, ज्वर के रूप में अपना-अपना फल देते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक कर्म अपना अलग-अलग फल देते हैं। किसी कर्म का फल कठोर होता है तो किसी का मदु । किसी का फल सबल होता है तो किसी कर्म का फल निर्बल । कर्म में फलदान शक्ति कषाय के कारण से होती है। कषाय अर्थात् राग द्वेष भाव, जितना प्रमाद होगा कर्म का फल भी उतना ही प्रगाढ़ व सबल होगा।
COM
DareAMAA.
AnaramanupadanadaNAIAAAAAAAAAAAAAAAANAAMERAAhADJAAMAunamaASO
आपाप्रवन अभिनत्राचार्यप्रवर आम श्रीआनन्द अन्यश्रीआनन्दप्रसन्न
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org