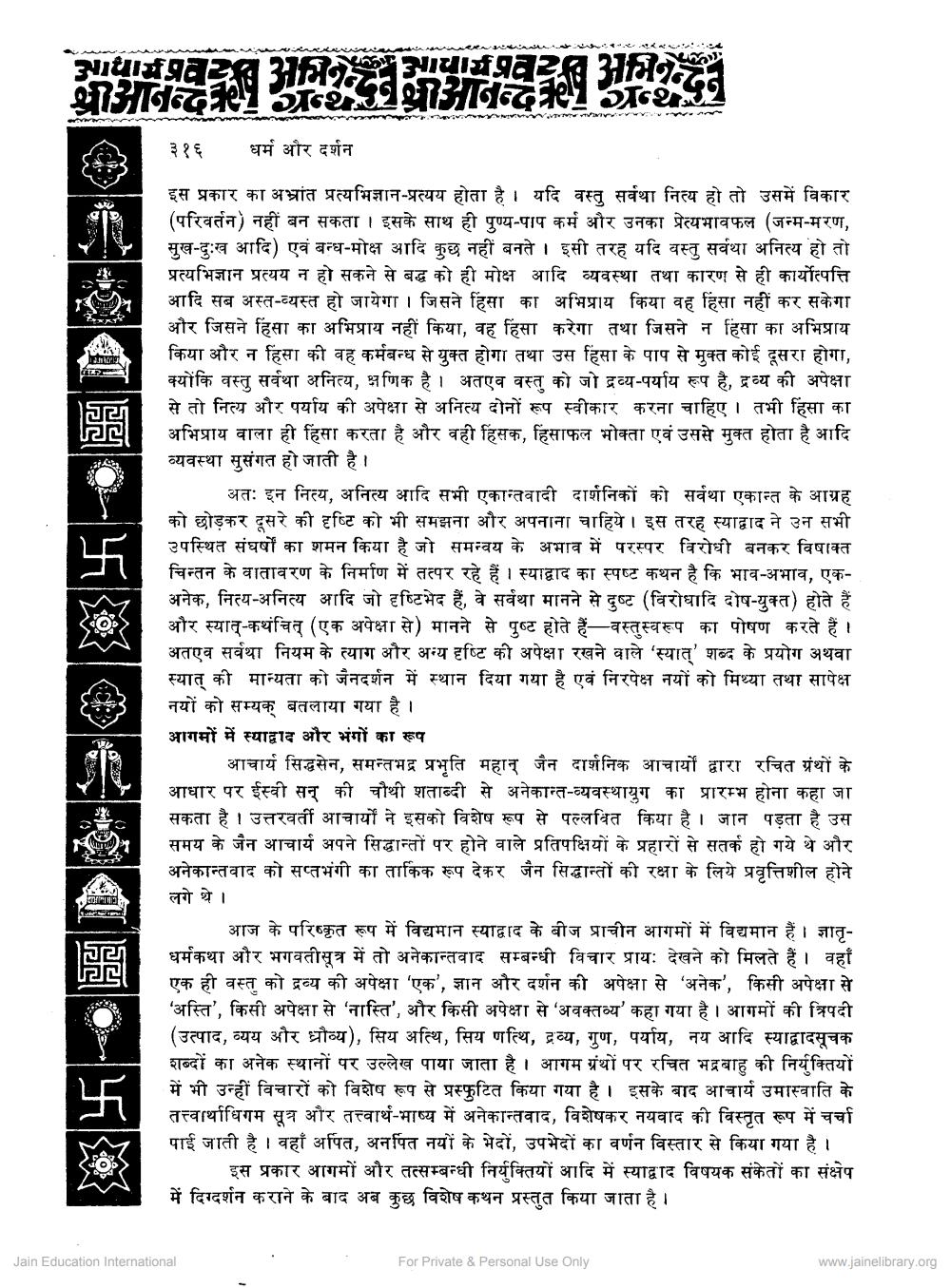________________
आधाय प्रवास अभिर्यप्र
hariot
C
३१६
धर्म और दर्शन
इस प्रकार का अभ्रांत प्रत्यभिज्ञान- प्रत्यय होता है । यदि वस्तु सर्वथा नित्य हो तो उसमें विकार ( परिवर्तन ) नहीं बन सकता । इसके साथ ही पुण्य-पाप कर्म और उनका प्रेत्यभावफल (जन्म-मरण, सुख-दुःख आदि) एवं बन्ध-मोक्ष आदि कुछ नहीं बनते । इसी तरह यदि वस्तु सर्वथा अनित्य हो तो प्रत्यभिज्ञान प्रत्यय न हो सकने से बद्ध को ही मोक्ष आदि व्यवस्था तथा कारण से ही कार्योत्पत्ति आदि सब अस्त-व्यस्त हो जायेगा । जिसने हिंसा का अभिप्राय किया वह हिंसा नहीं कर सकेगा और जिसने हिंसा का अभिप्राय नहीं किया, वह हिंसा करेगा तथा जिसने न हिंसा का अभिप्राय किया और न हिंसा की वह कर्मबन्ध से युक्त होगा तथा उस हिंसा के पाप से मुक्त कोई दूसरा होगा, क्योंकि वस्तु सर्वथा अनित्य, क्षणिक है । अतएव वस्तु को जो द्रव्य-पर्याय रूप है, द्रव्य की अपेक्षा से तो नित्य और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य दोनों रूप स्वीकार करना चाहिए। तभी हिंसा का अभिप्राय वाला ही हिंसा करता है और वही हिंसक, हिंसाफल भोक्ता एवं उससे मुक्त होता है आदि व्यवस्था सुसंगत हो जाती है ।
अभिनंदन
अतः इन नित्य, अनित्य आदि सभी एकान्तवादी दार्शनिकों को सर्वथा एकान्त के आग्रह को छोड़कर दूसरे की दृष्टि को भी समझना और अपनाना चाहिये । इस तरह स्याद्वाद ने उन सभी उपस्थित संघर्षों का शमन किया है जो समन्वय के अभाव में परस्पर विरोधी बनकर विषाक्त चिन्तन के वातावरण के निर्माण में तत्पर रहे हैं। स्याद्वाद का स्पष्ट कथन है कि भाव-अभाव, एकअनेक, नित्य-अनित्य आदि जो दृष्टिभेद हैं, वे सर्वथा मानने से दुष्ट ( विरोधादि दोष युक्त) होते हैं और स्यात् कथंचित् (एक अपेक्षा से ) मानने से पुष्ट होते हैं— वस्तुस्वरूप का पोषण करते हैं । अतएव सर्वथा नियम के त्याग और अन्य दृष्टि की अपेक्षा रखने वाले 'स्यात्' शब्द के प्रयोग अथवा स्यात् की मान्यता को जैनदर्शन में स्थान दिया गया है एवं निरपेक्ष नयों को मिथ्या तथा सापेक्ष नयों को सम्यक् बतलाया गया है ।
आगमों में स्याद्वाद और भंगों का रूप
ST आचार्य सिद्धसेन, समन्तभद्र प्रभृति महान् जैन दार्शनिक आचार्यों द्वारा रचित ग्रंथों के
आधार पर ईस्वी सन् की चौथी शताब्दी से अनेकान्त व्यवस्थायुग का प्रारम्भ होना कहा जा सकता है । उत्तरवर्ती आचार्यों ने इसको विशेष रूप से पल्लवित किया है । जान पड़ता है उस समय के जैन आचार्य अपने सिद्धान्तों पर होने वाले प्रतिपक्षियों के प्रहारों से सतर्क हो गये थे और अनेकान्तवाद को सप्तभंगी का तार्किक रूप देकर जैन सिद्धान्तों की रक्षा के लिये प्रवृत्तिशील होने लगे थे ।
आज के परिष्कृत रूप में विद्यमान स्याद्वाद के बीज प्राचीन आगमों में विद्यमान हैं । ज्ञातृधर्मकथा और भगवतीसूत्र में तो अनेकान्तवाद सम्बन्धी विचार प्रायः देखने को मिलते हैं । वहाँ एक ही वस्तु को द्रव्य की अपेक्षा 'एक', ज्ञान और दर्शन की अपेक्षा से 'अनेक', किसी अपेक्षा से 'अस्ति', किसी अपेक्षा से 'नास्ति', और किसी अपेक्षा से 'अवक्तव्य' कहा गया है । आगमों की त्रिपदी ( उत्पाद, व्यय और धौव्य), सिय अत्थि, सिय णत्थि, द्रव्य, गुण, पर्याय, नय आदि स्याद्वादसूचक शब्दों का अनेक स्थानों पर उल्लेख पाया जाता है । आगम ग्रंथों पर रचित भद्रबाहु की निर्युक्तियों में भी उन्हीं विचारों को विशेष रूप से प्रस्फुटित किया गया है । इसके बाद आचार्य उमास्वाति के तत्त्वार्थाधिगम सूत्र और तत्त्वार्थ भाष्य में अनेकान्तवाद, विशेषकर नयवाद की विस्तृत रूप में चर्चा पाई जाती है । वहाँ अर्पित, अनर्पित नयों के भेदों, उपभेदों का वर्णन विस्तार से किया गया है । इस प्रकार आगमों और तत्सम्बन्धी निर्युक्तियों आदि में स्याद्वाद विषयक संकेतों का संक्षेप में दिग्दर्शन कराने के बाद अब कुछ विशेष कथन प्रस्तुत किया जाता है ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org