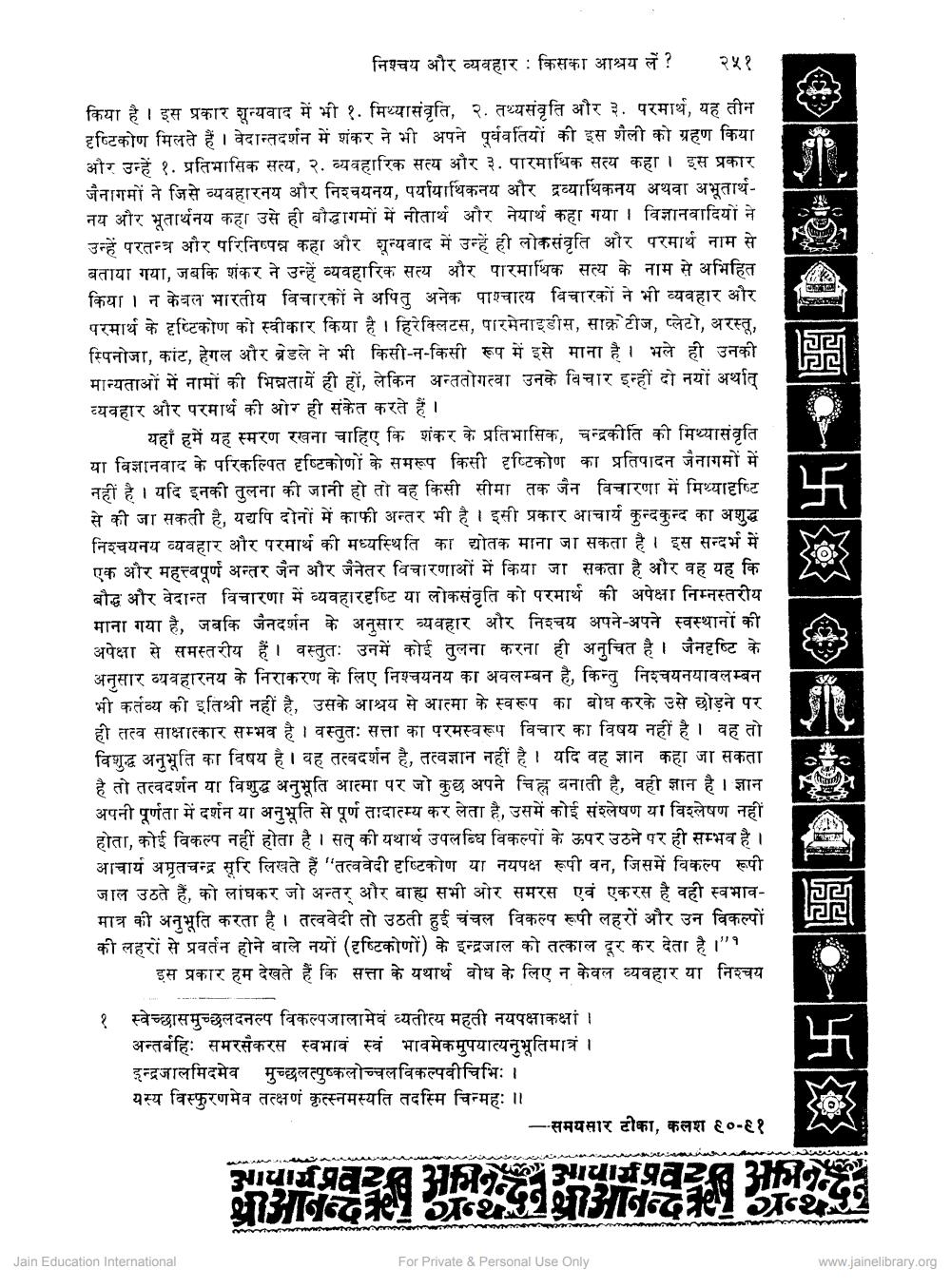________________
निश्चय और व्यवहार : किसका आश्रय लें?
२५१
RANI
किया है। इस प्रकार शून्यवाद में भी १. मिथ्यासंवृति, २. तथ्यसंवृति और ३. परमार्थ, यह तीन दृष्टिकोण मिलते हैं । वेदान्तदर्शन में शंकर ने भी अपने पूर्ववतियों की इस शैली को ग्रहण किया और उन्हें १. प्रतिभासिक सत्य, २. व्यवहारिक सत्य और ३. पारमार्थिक सत्य कहा। इस प्रकार जैनागमों ने जिसे व्यवहारनय और निश्चयनय, पर्यायाथिकनय और द्रव्याथिकनय अथवा अभूतार्थनय और भूतार्थनय कहा उसे ही बौद्धागमों में नीतार्थ और नेयार्थ कहा गया । विज्ञानवादियों ने उन्हें परतन्त्र और परिनिष्पन्न कहा और शून्यवाद में उन्हें ही लोकसंवृति और परमार्थ नाम से बताया गया, जबकि शंकर ने उन्हें व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य के नाम से अभिहित किया। न केवल भारतीय विचारकों ने अपितु अनेक पाश्चात्य विचारकों ने भी व्यवहार और परमार्थ के दृष्टिकोण को स्वीकार किया है । हिरेक्लिटस, पारमेनाइडीस, साक्र टीज, प्लेटो, अरस्तू, स्पिनोजा, कांट, हेगल और ब्रेडले ने भी किसी-न-किसी रूप में इसे माना है। भले ही उनकी मान्यताओं में नामों की भिन्नतायें ही हों, लेकिन अन्ततोगत्वा उनके विचार इन्हीं दो नयों अर्थात् व्यवहार और परमार्थ की ओर ही संकेत करते हैं।
यहाँ हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि शंकर के प्रतिभासिक, चन्द्रकीति की मिथ्यासंवृति या विज्ञानवाद के परिकल्पित दृष्टिकोणों के समरूप किसी दृष्टिकोण का प्रतिपादन जैनागमों में नहीं है। यदि इनकी तुलना की जानी हो तो वह किसी सीमा तक जैन विचारणा में मिथ्यादृष्टि से की जा सकती है, यद्यपि दोनों में काफी अन्तर भी है। इसी प्रकार आचार्य कुन्दकुन्द का अशुद्ध निश्चयनय व्यवहार और परमार्थ की मध्यस्थिति का द्योतक माना जा सकता है। इस सन्दर्भ में एक और महत्त्वपूर्ण अन्तर जैन और जैनेतर विचारणाओं में किया जा सकता है और वह यह कि बौद्ध और वेदान्त विचारणा में व्यवहारदृष्टि या लोकसंवृति को परमार्थ की अपेक्षा निम्नस्तरीय माना गया है, जबकि जैनदर्शन के अनुसार व्यवहार और निश्चय अपने-अपने स्वस्थानों की अपेक्षा से समस्तरीय हैं। वस्तुतः उनमें कोई तुलना करना ही अनुचित है। जैनदृष्टि के अनुसार व्यवहारनय के निराकरण के लिए निश्चयनय का अवलम्बन है, किन्तु निश्चयनयावलम्बन भी कर्तव्य की इतिश्री नहीं है, उसके आश्रय से आत्मा के स्वरूप का बोध करके उसे छोड़ने पर ही तत्व साक्षात्कार सम्भव है। वस्तुतः सत्ता का परमस्वरूप विचार का विषय नहीं है। वह तो विशुद्ध अनुभूति का विषय है । वह तत्वदर्शन है, तत्वज्ञान नहीं है। यदि वह ज्ञान कहा जा सकता है तो तत्वदर्शन या विशुद्ध अनुभूति आत्मा पर जो कुछ अपने चिह्न बनाती है, वही ज्ञान है । ज्ञान अपनी पूर्णता में दर्शन या अनुभूति से पूर्ण तादात्म्य कर लेता है, उसमें कोई संश्लेषण या विश्लेषण नहीं होता, कोई विकल्प नहीं होता है । सत् की यथार्थ उपलब्धि विकल्पों के ऊपर उठने पर ही सम्भव है। आचार्य अमृतचन्द्र सूरि लिखते हैं "तत्ववेदी दृष्टिकोण या नयपक्ष रूपी वन, जिसमें विकल्प रूपी जाल उठते हैं, को लांघकर जो अन्तर और बाह्य सभी ओर समरस एवं एकरस है वही स्वभावमात्र की अनुभूति करता है। तत्ववेदी तो उठती हुई चंचल विकल्प रूपी लहरों और उन विकल्पों की लहरों से प्रवर्तन होने वाले नयों (दृष्टिकोणों) के इन्द्रजाल को तत्काल दूर कर देता है।"१
इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्ता के यथार्थ बोध के लिए न केवल व्यवहार या निश्चय
GI
स्वेच्छासमुच्छलदनल्प विकल्पजालामेवं व्यतीत्य महती नयपक्षाकक्षा । अन्तर्बहिः समरसकरस स्वभावं स्वं भावमेकमुपयात्यनुभूतिमात्र । इन्द्रजालमिदमेव मुच्छलत्पुष्कलोच्चलविकल्पवीचिभिः । यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्महः ।
-समयसार टीका, कलश ६०-६१
नाaaaभियान आचार्यप्रवर अभिनन्दन यादआन्थ५१ श्रीआनन्द-मन्थश्रामा
PRMसाया।
mwwwmonawanivaarimom
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org