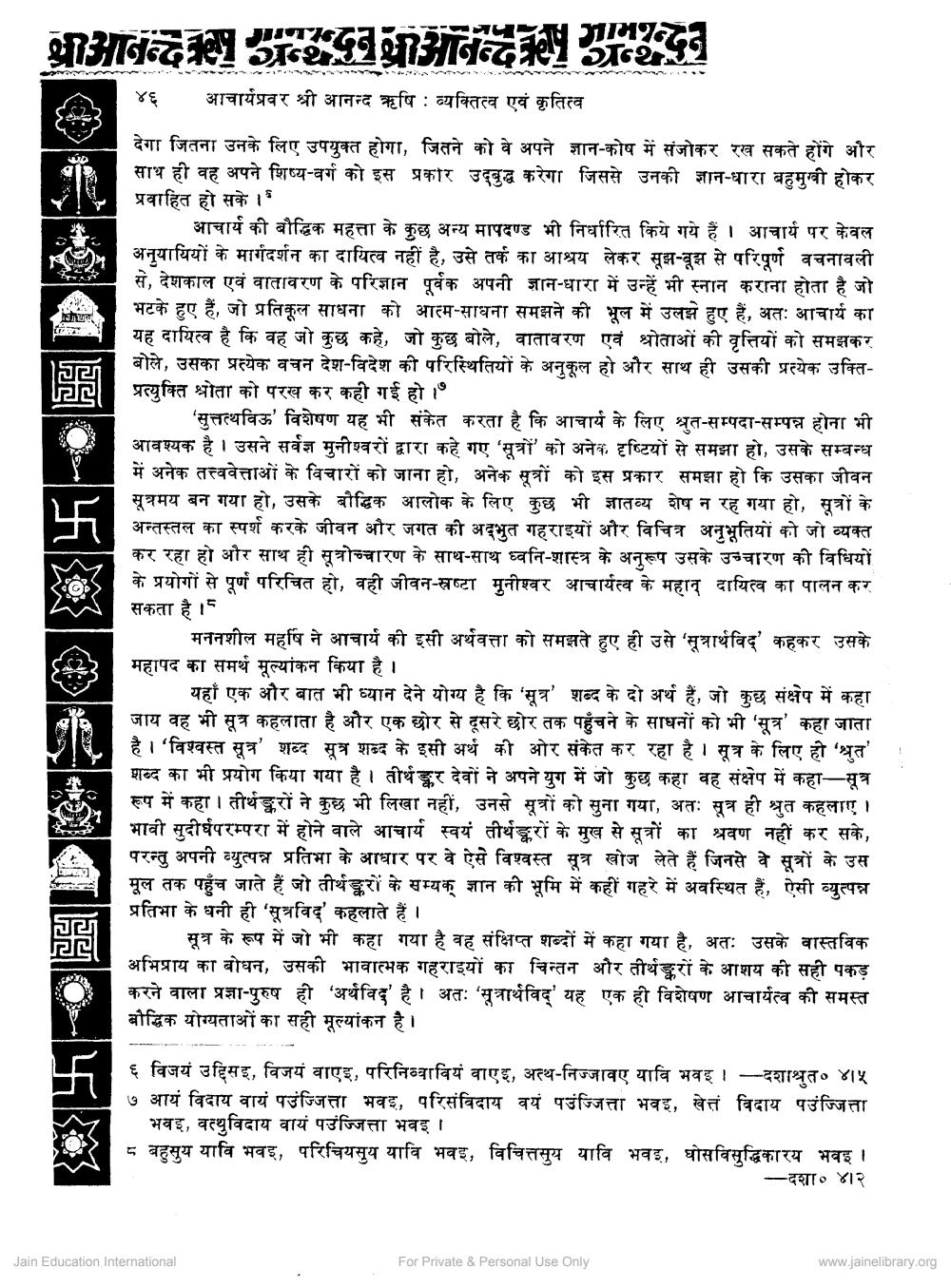________________
श्रीआनन्द
प्राआनन्द मदन
४६
आचार्यप्रवर श्री आनन्द ऋषि : व्यक्तित्व एवं कृतित्व
देगा जितना उनके लिए उपयुक्त होगा, जितने को वे अपने ज्ञान-कोष में संजोकर रख सकते होंगे और साथ ही वह अपने शिष्य-वर्ग को इस प्रकार उद्बुद्ध करेगा जिससे उनकी ज्ञान-धारा बहुमुखी होकर प्रवाहित हो सके।'
आचार्य की बौद्धिक महत्ता के कुछ अन्य मापदण्ड भी निर्धारित किये गये हैं। आचार्य पर केवल अनुयायियों के मार्गदर्शन का दायित्व नहीं है, उसे तर्क का आश्रय लेकर सूझ-बूझ से परिपूर्ण वचनावली से, देशकाल एवं वातावरण के परिज्ञान पूर्वक अपनी ज्ञान-धारा में उन्हें भी स्नान कराना होता है जो भटके हुए हैं, जो प्रतिकूल साधना को आत्म-साधना समझने की भूल में उलझे हुए हैं, अतः आचार्य का यह दायित्व है कि वह जो कुछ कहे, जो कुछ बोले, वातावरण एवं श्रोताओं की वृत्तियों को समझकर बोले, उसका प्रत्येक वचन देश-विदेश की परिस्थितियों के अनुकूल हो और साथ ही उसकी प्रत्येक उक्तिप्रत्युक्ति श्रोता को परख कर कही गई हो।
'सुत्तत्थविऊ' विशेषण यह भी संकेत करता है कि आचार्य के लिए श्रुत-सम्पदा-सम्पन्न होना भी आवश्यक है। उसने सर्वज्ञ मुनीश्वरों द्वारा कहे गए 'सूत्रों' को अनेक दृष्टियों से समझा हो, उसके सम्बन्ध में अनेक तत्त्ववेत्ताओं के विचारों को जाना हो, अनेक सूत्रों को इस प्रकार समझा हो कि उसका जीवन सूत्रमय बन गया हो, उसके बौद्धिक आलोक के लिए कुछ भी ज्ञातव्य शेष न रह गया हो, सूत्रों के अन्तस्तल का स्पर्श करके जीवन और जगत की अद्भुत गहराइयों और विचित्र अनुभूतियों को जो व्यक्त कर रहा हो और साथ ही सूत्रोच्चारण के साथ-साथ ध्वनि-शास्त्र के अनुरूप उसके उच्चारण की विधियों
से पूर्ण परिचित हो, वही जीवन-स्रष्टा मूनीश्वर आचार्यत्व के महान् दायित्व का पालन कर सकता है।
मननशील महर्षि ने आचार्य की इसी अर्थवत्ता को समझते हुए ही उसे 'सूत्रार्थविद्' कहकर उसके महापद का समर्थ मूल्यांकन किया है।
यहाँ एक और बात भी ध्यान देने योग्य है कि 'सूत्र' शब्द के दो अर्थ हैं, जो कुछ संक्षेप में कहा जाय वह भी सूत्र कहलाता है और एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने के साधनों को भी 'सूत्र' कहा जाता है। 'विश्वस्त सूत्र' शब्द सूत्र शब्द के इसी अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। सूत्र के लिए हो 'श्रुत' । शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तीर्थङ्कर देवों ने अपने युग में जो कुछ कहा वह संक्षेप में कहा-सूत्र रूप में कहा । तीर्थङ्करों ने कुछ भी लिखा नहीं, उनसे सूत्रों को सुना गया, अतः सूत्र ही श्रुत कहलाए। भावी सुदीर्घपरम्परा में होने वाले आचार्य स्वयं तीर्थङ्करों के मुख से सूत्रों का श्रवण नहीं कर सके, परन्तु अपनी व्युत्पन्न प्रतिभा के आधार पर वे ऐसे विश्वस्त सूत्र खोज लेते हैं जिनसे वे सूत्रों के उस मुल तक पहुंच जाते हैं जो तीर्थङ्करों के सम्यक् ज्ञान की भूमि में कहीं गहरे में अवस्थित हैं, ऐसी व्युत्पन्न प्रतिभा के धनी ही 'सूत्रविद्' कहलाते हैं।
सूत्र के रूप में जो भी कहा गया है वह संक्षिप्त शब्दों में कहा गया है, अतः उसके वास्तविक अभिप्राय का बोधन, उसकी भावात्मक गहराइयों का चिन्तन और तीर्थङ्करों के आशय की सही पकड़ करने वाला प्रज्ञा-पुरुष ही 'अर्थविद्' है। अतः 'सूत्रार्थविद्' यह एक ही विशेषण आचार्यत्व की समस्त बौद्धिक योग्यताओं का सही मूल्यांकन है।
६ विजयं उहिसइ, विजयं वाएइ, परिनिवावियं बाएइ, अत्थ-निज्जावए यावि भवइ। -दशाश्रुत० ४।५ ७ आयं विदाय वायं पउंज्जित्ता भवइ, परिसंविदाय वयं पउंज्जित्ता भवइ, खेत्तं विदाय पउंज्जित्ता
भवइ, वत्थुविदाय वायं पउंज्जित्ता भवइ ।। ८ बहुसुय यावि भवइ, परिचियसुय यावि भवइ, विचित्तसुय यावि भवइ, घोसविसुद्धिकारय भवइ ।
-दशा० ४।२
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org