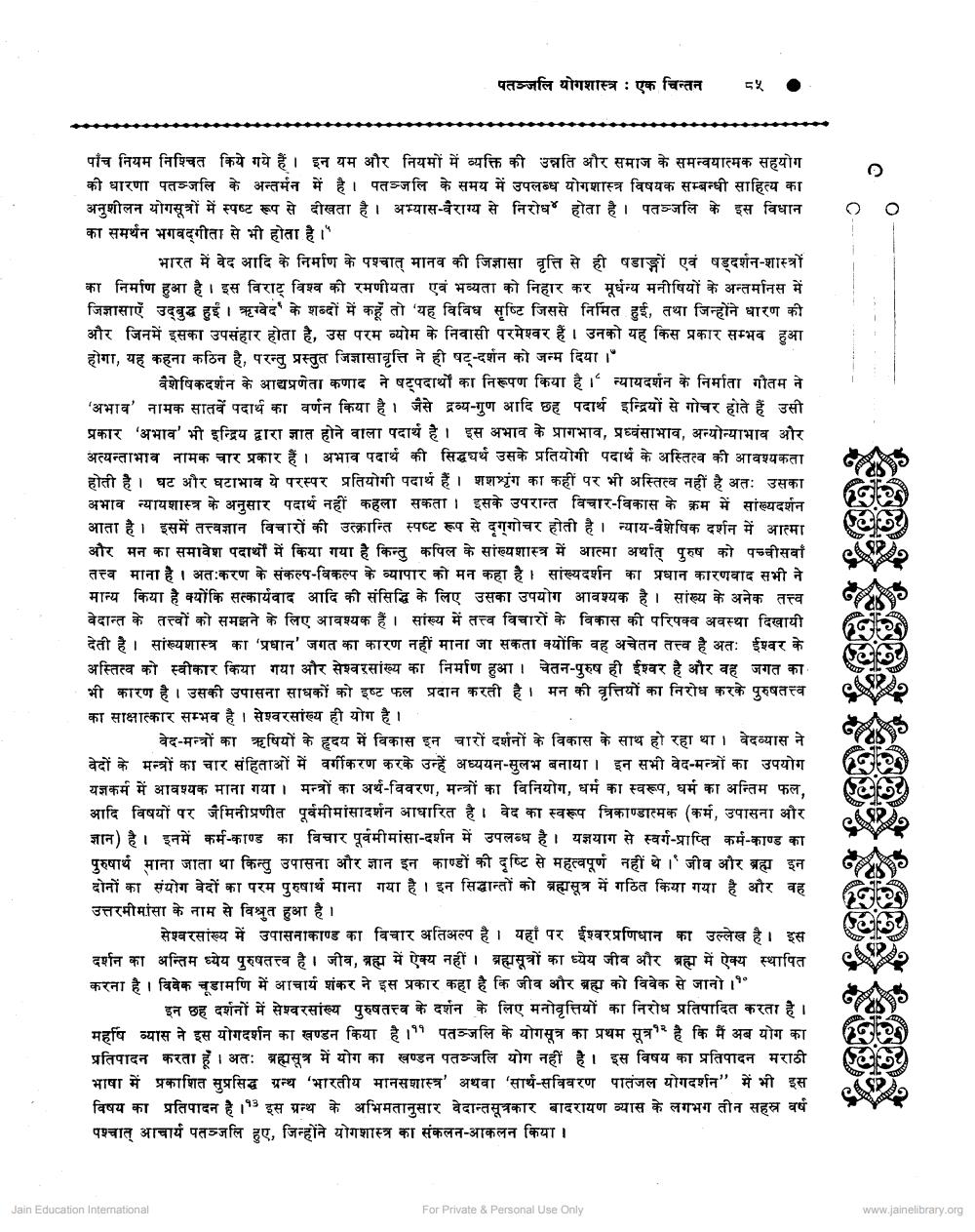________________
पतञ्जलि योगशास्त्र : एक चिन्तन
८५
.
पाँच नियम निश्चित किये गये हैं। इन यम और नियमों में व्यक्ति की उन्नति और समाज के समन्वयात्मक सहयोग की धारणा पतञ्जलि के अन्तर्मन में है। पतञ्जलि के समय में उपलब्ध योगशास्त्र विषयक सम्बन्धी साहित्य का अनुशीलन योगसूत्रों में स्पष्ट रूप से दीखता है। अभ्यास-वैराग्य से निरोध होता है। पतञ्जलि के इस विधान का समर्थन भगवद्गीता से भी होता है।
भारत में वेद आदि के निर्माण के पश्चात् मानव की जिज्ञासा बृत्ति से ही षडाङ्गों एवं षड्दर्शन-शास्त्रों का निर्माण हुआ है। इस विराट् विश्व की रमणीयता एवं भव्यता को निहार कर मूर्धन्य मनीषियों के अन्तर्मानस में जिज्ञासाएँ उद्बुद्ध हुईं। ऋग्वेद' के शब्दों में कहूँ तो 'यह विविध सृष्टि जिससे निर्मित हुई, तथा जिन्होंने धारण की और जिनमें इसका उपसंहार होता है, उस परम व्योम के निवासी परमेश्वर हैं। उनको यह किस प्रकार सम्भव हुआ होगा, यह कहना कठिन है, परन्तु प्रस्तुत जिज्ञासावृत्ति ने ही षट्-दर्शन को जन्म दिया।
वैशेषिकदर्शन के आद्यप्रणेता कणाद ने षट्पदार्थों का निरूपण किया है।' न्यायदर्शन के निर्माता गौतम ने 'अभाव' नामक सातवें पदार्थ का वर्णन किया है। जैसे द्रव्य-गुण आदि छह पदार्थ इन्द्रियों से गोचर होते हैं उसी प्रकार 'अभाव' भी इन्द्रिय द्वारा ज्ञात होने वाला पदार्थ है। इस अभाव के प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्ताभाव नामक चार प्रकार हैं। अभाव पदार्थ की सिद्धयर्थ उसके प्रतियोगी पदार्थ के अस्तित्व की आवश्यकता होती है। घट और घटाभाव ये परस्पर प्रतियोगी पदार्थ हैं। शशशृंग का कहीं पर भी अस्तित्व नहीं है अतः उसका अभाव न्यायशास्त्र के अनुसार पदार्थ नहीं कहला सकता। इसके उपरान्त विचार-विकास के क्रम में सांख्यदर्शन आता है। इसमें तत्त्वज्ञान विचारों की उत्क्रान्ति स्पष्ट रूप से दृग्गोचर होती है। न्याय-वैशेषिक दर्शन में आत्मा और मन का समावेश पदार्थों में किया गया है किन्तु कपिल के सांख्यशास्त्र में आत्मा अर्थात् पुरुष को पच्चीसवाँ तत्त्व माना है । अतःकरण के संकल्प-विकल्प के व्यापार को मन कहा है। सांख्यदर्शन का प्रधान कारणवाद सभी ने मान्य किया है क्योंकि सत्कार्यवाद आदि की संसिद्धि के लिए उसका उपयोग आवश्यक है। सांख्य के अनेक तत्त्व वेदान्त के तत्त्वों को समझने के लिए आवश्यक हैं। सांख्य में तत्त्व विचारों के विकास की परिपक्व अवस्था दिखायी देती है। सांख्यशास्त्र का 'प्रधान' जगत का कारण नहीं माना जा सकता क्योंकि वह अचेतन तत्त्व है अतः ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया और सेश्वरसांख्य का निर्माण हुआ। चेतन-पुरुष ही ईश्वर है और वह जगत का भी कारण है। उसकी उपासना साधकों को इष्ट फल प्रदान करती है। मन की वृत्तियों का निरोध करके पुरुषतत्त्व का साक्षात्कार सम्भव है । सेश्वरसांख्य ही योग है।
वेद-मन्त्रों का ऋषियों के हृदय में विकास इन चारों दर्शनों के विकास के साथ हो रहा था। वेदव्यास ने वेदों के मन्त्रों का चार संहिताओं में वर्गीकरण करके उन्हें अध्ययन-सुलभ बनाया। इन सभी वेद-मन्त्रों का उपयोग यज्ञकर्म में आवश्यक माना गया। मन्त्रों का अर्थ-विवरण, मन्त्रों का विनियोग, धर्म का स्वरूप, धर्म का अन्तिम फल, आदि विषयों पर जैमिनीप्रणीत पूर्वमीमांसादर्शन आधारित है। वेद का स्वरूप त्रिकाण्डात्मक (कर्म, उपासना और ज्ञान) है। इनमें कर्म-काण्ड का विचार पूर्वमीमांसा-दर्शन में उपलब्ध है। यज्ञयाग से स्वर्ग-प्राप्ति कर्म-काण्ड का पुरुषार्थ माना जाता था किन्तु उपासना और ज्ञान इन काण्डों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थे। जीव और ब्रह्म इन दोनों का संयोग वेदों का परम पुरुषार्थ माना गया है । इन सिद्धान्तों को ब्रह्मसूत्र में गठित किया गया है और वह उत्तरमीमांसा के नाम से विश्रुत हुआ है।
सेश्वरसांख्य में उपासनाकाण्ड का विचार अतिअल्प है। यहाँ पर ईश्वरप्रणिधान का उल्लेख है। इस दर्शन का अन्तिम ध्येय पुरुषतत्त्व है। जीव, ब्रह्म में ऐक्य नहीं। ब्रह्मसूत्रों का ध्येय जीव और ब्रह्म में ऐक्य स्थापित करना है । विवेक चूडामणि में आचार्य शंकर ने इस प्रकार कहा है कि जीव और ब्रह्म को विवेक से जानो।
इन छह दर्शनों में सेश्वरसांख्य पुरुषतत्त्व के दर्शन के लिए मनोवृत्तियों का निरोध प्रतिपादित करता है। महर्षि व्यास ने इस योगदर्शन का खण्डन किया है।११ पतञ्जलि के योगसूत्र का प्रथम सूत्र है कि मैं अब योग का प्रतिपादन करता हूँ । अतः ब्रह्मसूत्र में योग का खण्डन पतञ्जलि योग नहीं है। इस विषय का प्रतिपादन मराठी भाषा में प्रकाशित सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'भारतीय मानसशास्त्र' अथवा 'सार्थ-सविवरण पातंजल योगदर्शन" में भी इस विषय का प्रतिपादन है । इस ग्रन्थ के अभिमतानुसार वेदान्तसूत्रकार बादरायण व्यास के लगभग तीन सहस्र वर्ष पश्चात् आचार्य पतञ्जलि हुए, जिन्होंने योगशास्त्र का संकलन-आकलन किया।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org