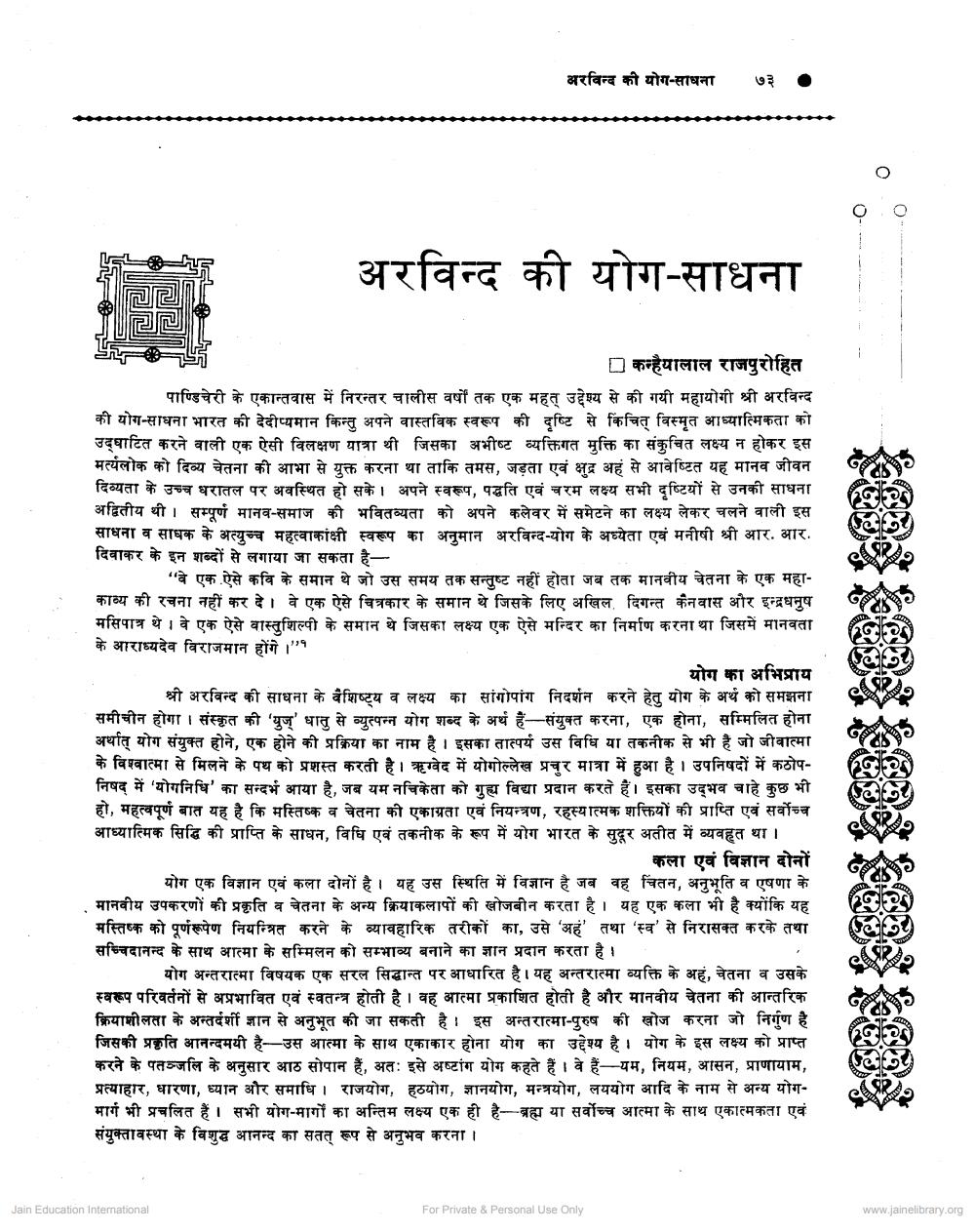________________
अरविन्द की योग-साधना
७३
अरविन्द की योग-साधना
- कन्हैयालाल राजपुरोहित पाण्डिचेरी के एकान्तवास में निरन्तर चालीस वर्षों तक एक महत् उद्देश्य से की गयी महायोगी श्री अरविन्द की योग-साधना भारत की देदीप्यमान किन्तु अपने वास्तविक स्वरूप की दृष्टि से किंचित् विस्मृत आध्यात्मिकता को उद्घाटित करने वाली एक ऐसी विलक्षण यात्रा थी जिसका अभीष्ट व्यक्तिगत मुक्ति का संकुचित लक्ष्य न होकर इस मर्त्यलोक को दिव्य चेतना की आभा से युक्त करना था ताकि तमस, जड़ता एवं क्षुद्र अहं से आवेष्टित यह मानव जीवन दिव्यता के उच्च धरातल पर अवस्थित हो सके। अपने स्वरूप, पद्धति एवं चरम लक्ष्य सभी दृष्टियों से उनकी साधना अद्वितीय थी। सम्पूर्ण मानव-समाज की भवितव्यता को अपने कलेवर में समेटने का लक्ष्य लेकर चलने वाली इस साधना व साधक के अत्युच्च महत्वाकांक्षी स्वरूप का अनुमान अरविन्द-योग के अध्येता एवं मनीषी श्री आर. आर. दिवाकर के इन शब्दों से लगाया जा सकता है
"वे एक ऐसे कवि के समान थे जो उस समय तक सन्तुष्ट नहीं होता जब तक मानवीय चेतना के एक महाकाव्य की रचना नहीं कर दे। वे एक ऐसे चित्रकार के समान थे जिसके लिए अखिल, दिगन्त कैनवास और इन्द्रधनुष मसिपात्र थे। वे एक ऐसे वास्तुशिल्पी के समान थे जिसका लक्ष्य एक ऐसे मन्दिर का निर्माण करना था जिसमें मानवता के आराध्यदेव विराजमान होंगे।"१
योग का अभिप्राय श्री अरविन्द की साधना के वैशिष्ट्य व लक्ष्य का सांगोपांग निदर्शन करने हेतु योग के अर्थ को समझना समीचीन होगा । संस्कृत की 'युज' धातु से व्युत्पन्न योग शब्द के अर्थ है-संयुक्त करना, एक होना, सम्मिलित होना अर्थात् योग संयुक्त होने, एक होने की प्रक्रिया का नाम है । इसका तात्पर्य उस विधि या तकनीक से भी है जो जीवात्मा के विश्वात्मा से मिलने के पथ को प्रशस्त करती है। ऋग्वेद में योगोल्लेख प्रचुर मात्रा में हुआ है। उपनिषदों में कठोपनिषद् में 'योगनिधि' का सन्दर्भ आया है, जब यम नचिकेता को गुह्य विद्या प्रदान करते हैं। इसका उद्भव चाहे कुछ भी हो, महत्वपूर्ण बात यह है कि मस्तिष्क व चेतना की एकाग्रता एवं नियन्त्रण, रहस्यात्मक शक्तियों की प्राप्ति एवं सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के साधन, विधि एवं तकनीक के रूप में योग भारत के सुदूर अतीत में व्यवहृत था।
कला एवं विज्ञान दोनों योग एक विज्ञान एवं कला दोनों है। यह उस स्थिति में विज्ञान है जब वह चिंतन, अनुभूति व एषणा के मानवीय उपकरणों की प्रकृति व चेतना के अन्य क्रियाकलापों की खोजबीन करता है। यह एक कला भी है क्योंकि यह मस्तिष्क को पूर्णरूपेण नियन्त्रित करने के व्यावहारिक तरीकों का, उसे 'अहं' तथा 'स्व' से निरासक्त करके तथा सच्चिदानन्द के साथ आत्मा के सम्मिलन को सम्भाव्य बनाने का ज्ञान प्रदान करता है।
योग अन्तरात्मा विषयक एक सरल सिद्धान्त पर आधारित है। यह अन्तरात्मा व्यक्ति के अहं, चेतना व उसके स्वरूप परिवर्तनों से अप्रभावित एवं स्वतन्त्र होती है । वह आत्मा प्रकाशित होती है और मानवीय चेतना की आन्तरिक क्रियाशीलता के अन्तर्दर्शी ज्ञान से अनुभूत की जा सकती है। इस अन्तरात्मा-पुरुष की खोज करना जो निर्गुण है जिसकी प्रकृति आनन्दमयी है-उस आत्मा के साथ एकाकार होना योग का उद्देश्य है। योग के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के पतञ्जलि के अनुसार आठ सोपान हैं, अतः इसे अष्टांग योग कहते हैं। वे हैं-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि । राजयोग, हठयोग, ज्ञानयोग, मन्त्रयोग, लययोग आदि के नाम से अन्य योगमार्ग भी प्रचलित हैं। सभी योग-मार्गों का अन्तिम लक्ष्य एक ही है-ब्रह्म या सर्वोच्च आत्मा के साथ एकात्मकता एवं संयुक्तावस्था के विशुद्ध आनन्द का सतत् रूप से अनुभव करना।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org