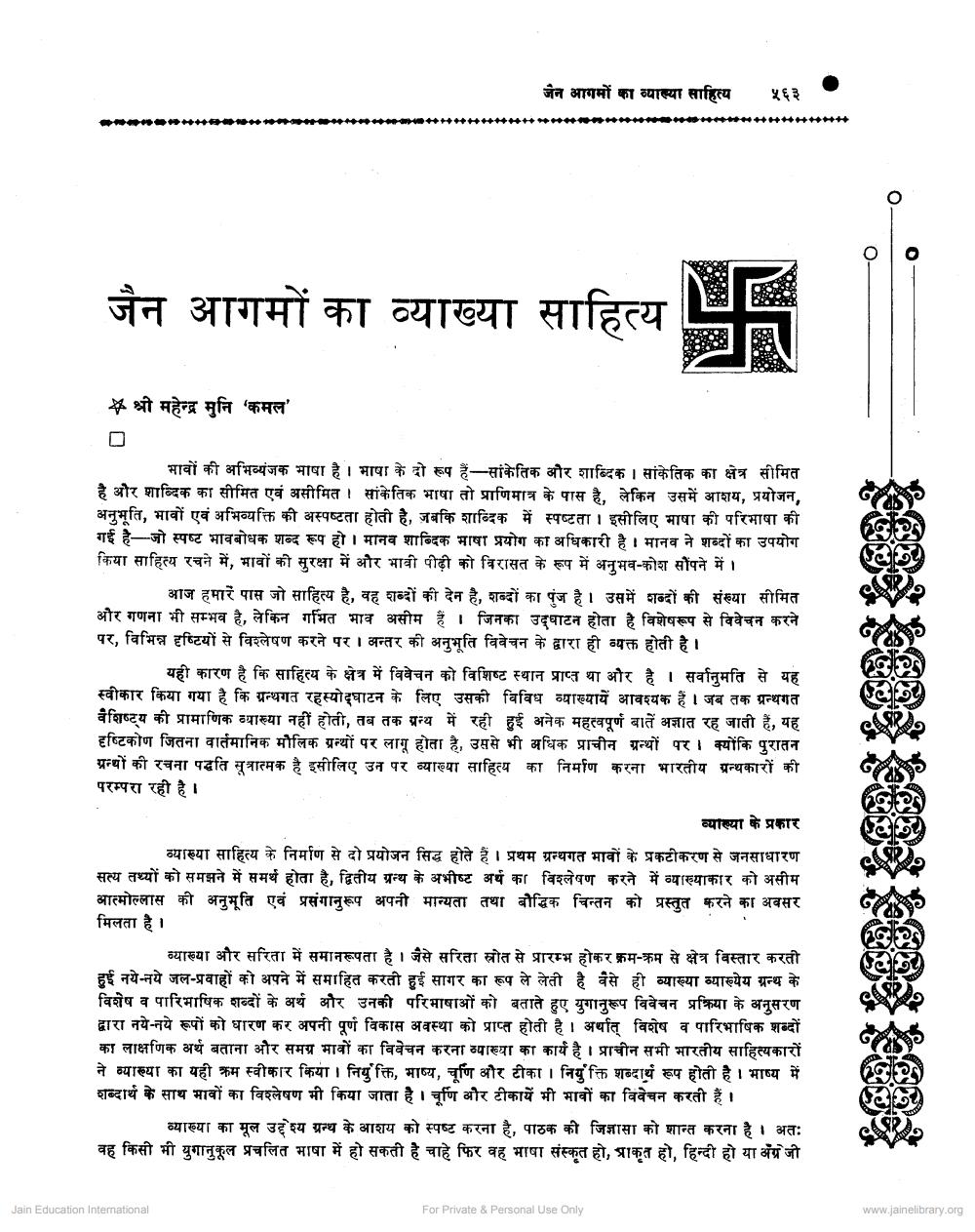________________
जैन आगमों का व्याख्या साहित्य
५६३
जैन आगमों का व्याख्या साहित्य
श्री महेन्द्र मुनि 'कमल'
भावों की अभिव्यंजक भाषा है । भाषा के दो रूप हैं-सांकेतिक और शाब्दिक । सांकेतिक का क्षेत्र सीमित है और शाब्दिक का सीमित एवं असीमित । सांकेतिक भाषा तो प्राणिमात्र के पास है, लेकिन उसमें आशय, प्रयोजन, अनुभूति, भावों एवं अभिव्यक्ति की अस्पष्टता होती है, जबकि शाब्दिक में स्पष्टता। इसीलिए भाषा की परिभाषा की गई है जो स्पष्ट भावबोधक शब्द रूप हो। मानव शाब्दिक भाषा प्रयोग का अधिकारी है। मानव ने शब्दों का उपयोग किया साहित्य रचने में, मावों की सुरक्षा में और भावी पीढ़ी को विरासत के रूप में अनुभव-कोश सौंपने में।
आज हमारे पास जो साहित्य है, वह शब्दों की देन है, शब्दों का पुंज है। उसमें शब्दों की संख्या सीमित और गणना भी सम्भव है, लेकिन गभित भाव असीम हैं । जिनका उद्घाटन होता है विशेषरूप से विवेचन करने पर, विभिन्न दृष्टियों से विश्लेषण करने पर । अन्तर की अनुभूति विवेचन के द्वारा ही व्यक्त होती है।
यही कारण है कि साहित्य के क्षेत्र में विवेचन को विशिष्ट स्थान प्राप्त था और है । सर्वानुमति से यह स्वीकार किया गया है कि ग्रन्थगत रहस्योद्घाटन के लिए उसकी विविध व्याख्या आवश्यक हैं । जब तक ग्रन्थगत वैशिष्ट्य की प्रामाणिक व्याख्या नहीं होती, तब तक ग्रन्थ में रही हुई अनेक महत्वपूर्ण बातें अज्ञात रह जाती हैं, यह दृष्टिकोण जितना वार्तमानिक मौलिक ग्रन्थों पर लागू होता है, उससे भी अधिक प्राचीन ग्रन्थों पर । क्योंकि पुरातन ग्रन्थों की रचना पद्धति सुत्रात्मक है इसीलिए उन पर व्याख्या साहित्य का निर्माण करना भारतीय ग्रन्थकारों की परम्परा रही है।
व्याख्या के प्रकार व्याख्या साहित्य के निर्माण से दो प्रयोजन सिद्ध होते हैं। प्रथम ग्रन्थगत भावों के प्रकटीकरण से जनसाधारण सत्य तथ्यों को समझने में समर्थ होता है, द्वितीय ग्रन्थ के अभीष्ट अर्थ का विश्लेषण करने में व्याख्याकार को असीम आत्मोल्लास की अनुभूति एवं प्रसंगानुरूप अपनी मान्यता तथा बौद्धिक चिन्तन को प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है।
___ व्याख्या और सरिता में समानरूपता है । जैसे सरिता स्रोत से प्रारम्भ होकर क्रम-क्रम से क्षेत्र विस्तार करती हुई नये-नये जल-प्रवाहों को अपने में समाहित करती हुई सागर का रूप ले लेती है वैसे ही व्याख्या व्याख्येय ग्रन्थ के विशेष व पारिभाषिक शब्दों के अर्थ और उनकी परिभाषाओं को बताते हुए युगानुरूप विवेचन प्रक्रिया के अनुसरण द्वारा नये-नये रूपों को धारण कर अपनी पूर्ण विकास अवस्था को प्राप्त होती है । अर्थात् विशेष व पारिभाषिक शब्दों का लाक्षणिक अर्थ बताना और समग्र भावों का विवेचन करना व्याख्या का कार्य है । प्राचीन सभी भारतीय साहित्यकारों ने व्याख्या का यही क्रम स्वीकार किया। नियुक्ति, भाष्य, चूणि और टीका । नियुक्ति शब्दार्थ रूप होती है। भाष्य में शब्दार्थ के साथ भावों का विश्लेषण भी किया जाता है। चूणि और टीकायें भी भावों का विवेचन करती हैं।
व्याख्या का मूल उद्देश्य ग्रन्थ के आशय को स्पष्ट करना है, पाठक को जिज्ञासा को शान्त करना है । अतः वह किसी भी युगानुकूल प्रचलित भाषा में हो सकती है चाहे फिर वह भाषा संस्कृत हो, प्राकृत हो, हिन्दी हो या अंग्रेजी
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org