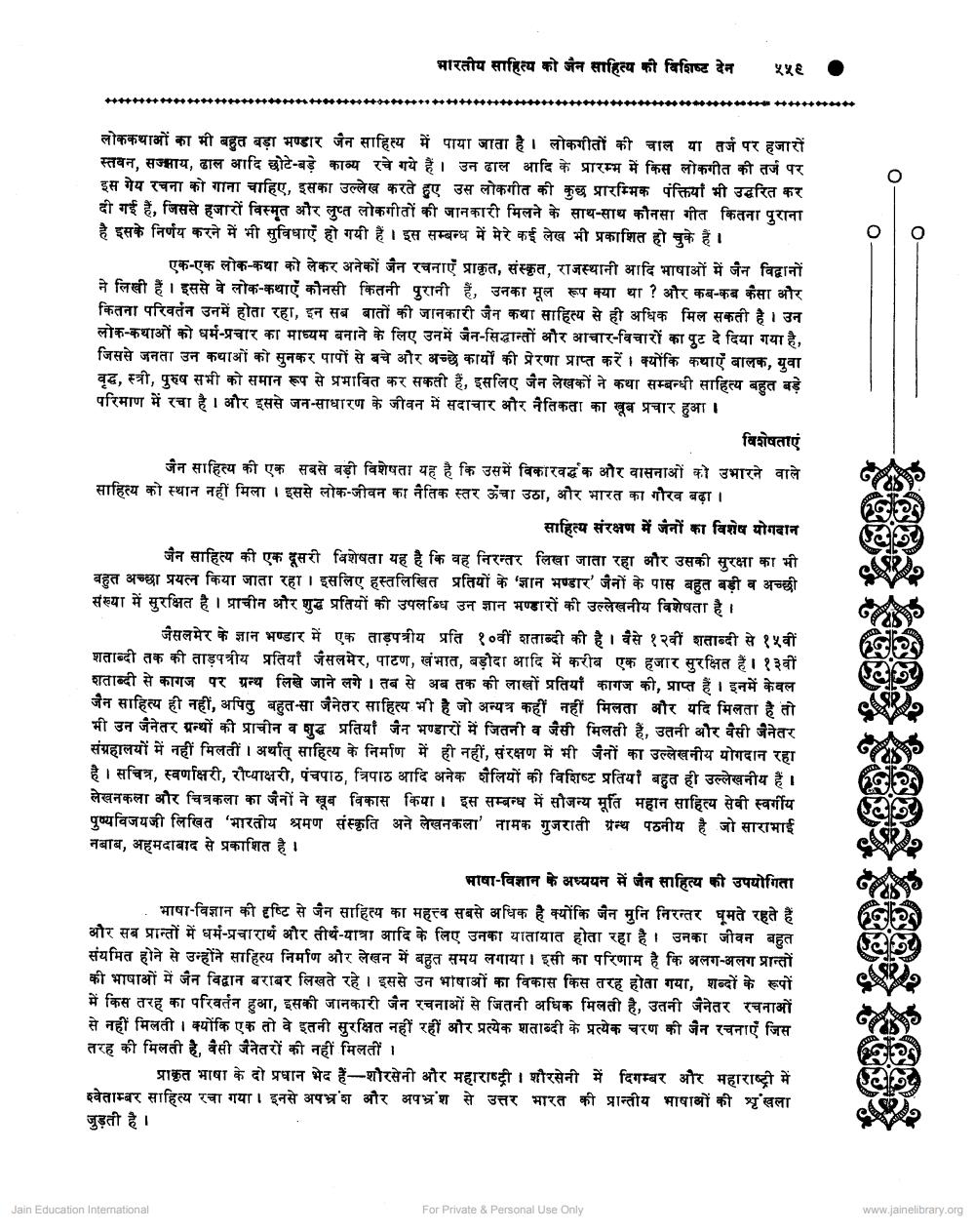________________
भारतीय साहित्य को जैन साहित्य की विशिष्ट देन
५५९
.
०
०
लोककथाओं का भी बहुत बड़ा भण्डार जैन साहित्य में पाया जाता है। लोकगीतों की चाल या तर्ज पर हजारों स्तवन, सज्झाय, ढाल आदि छोटे-बड़े काव्य रचे गये हैं। उन ढाल आदि के प्रारम्भ में किस लोकगीत की तर्ज पर इस गेय रचना को गाना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए उस लोकगीत की कुछ प्रारम्भिक पंक्तियां भी उद्धरित कर दी गई हैं, जिससे हजारों विस्मृत और लुप्त लोकगीतों की जानकारी मिलने के साथ-साथ कौनसा गीत कितना पुराना है इसके निर्णय करने में भी सुविधाएं हो गयी हैं। इस सम्बन्ध में मेरे कई लेख भी प्रकाशित हो चुके हैं।
एक-एक लोक-कथा को लेकर अनेकों जैन रचनाएं प्राकृत, संस्कृत, राजस्थानी आदि भाषाओं में जैन विद्वानों ने लिखी हैं । इससे वे लोक-कथाएं कोनसी कितनी पुरानी हैं, उनका मूल रूप क्या था? और कब-कब कैसा और कितना परिवर्तन उनमें होता रहा, इन सब बातों की जानकारी जैन कथा साहित्य से ही अधिक मिल सकती है। उन लोक-कथाओं को धर्म-प्रचार का माध्यम बनाने के लिए उनमें जन-सिद्धान्तों और आचार-विचारों का पुट दे दिया गया है, जिससे जनता उन कथाओं को सुनकर पापों से बचे और अच्छे कार्यों की प्रेरणा प्राप्त करें। क्योंकि कथाएँ बालक, युवा वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी को समान रूप से प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए जैन लेखकों ने कथा सम्बन्धी साहित्य बहुत बड़े परिमाण में रचा है। और इससे जन-साधारण के जीवन में सदाचार और नैतिकता का खूब प्रचार हुआ ।
विशेषताएं जैन साहित्य की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें विकारवर्द्धक और वासनाओं को उभारने वाले साहित्य को स्थान नहीं मिला । इससे लोक-जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा उठा, और भारत का गौरव बढ़ा ।
साहित्य संरक्षण में जैनों का विशेष योगदान जैन साहित्य की एक दूसरी विशेषता यह है कि वह निरन्तर लिखा जाता रहा और उसकी सुरक्षा का भी बहुत अच्छा प्रयल किया जाता रहा । इसलिए हस्तलिखित प्रतियों के 'ज्ञान भण्डार' जैनों के पास बहुत बड़ी व अच्छी संख्या में सुरक्षित है। प्राचीन और शुद्ध प्रतियों की उपलब्धि उन ज्ञान भण्डारों की उल्लेखनीय विशेषता है।
जैसलमेर के ज्ञान भण्डार में एक ताडपत्रीय प्रति १०वीं शताब्दी की है। वैसे १२वीं शताब्दी से १५वीं शताब्दी तक की ताडपत्रीय प्रतियां जैसलमेर, पाटण, खंभात, बड़ौदा आदि में करीब एक हजार सुरक्षित हैं। १३वीं शताब्दी से कागज पर ग्रन्थ लिखे जाने लगे । तब से अब तक की लाखों प्रतियां कागज की, प्राप्त हैं । इनमें केवल जैन साहित्य ही नहीं, अपितु बहुत-सा जैनेतर साहित्य भी है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता और यदि मिलता है तो भी उन जैनेतर ग्रन्थों की प्राचीन व शुद्ध प्रतियां जैन भण्डारों में जितनी व जैसी मिलती हैं, उतनी और वैसी जैनेतर संग्रहालयों में नहीं मिलतीं । अर्थात् साहित्य के निर्माण में ही नहीं, संरक्षण में भी जैनों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। सचित्र, स्वर्णाक्षरी, रौप्याक्षरी, पंचपाठ, त्रिपाठ आदि अनेक शैलियों की विशिष्ट प्रतियां बहुत ही उल्लेखनीय हैं । लेखनकला और चित्रकला का जैनों ने खूब विकास किया। इस सम्बन्ध में सौजन्य मूर्ति महान साहित्य सेवी स्वर्गीय पुण्यविजयजी लिखित 'भारतीय श्रमण संस्कृति अने लेखनकला' नामक गुजराती ग्रन्थ पठनीय है जो साराभाई नबाब, अहमदाबाद से प्रकाशित है।
भाषा-विज्ञान के अध्ययन में जैन साहित्य की उपयोगिता . भाषा-विज्ञान की दृष्टि से जैन साहित्य का महत्त्व सबसे अधिक है क्योंकि जैन मुनि निरन्तर घूमते रहते हैं और सब प्रान्तों में धर्म-प्रचारार्थ और तीर्थ-यात्रा आदि के लिए उनका यातायात होता रहा है। उनका जीवन बहुत संयमित होने से उन्होंने साहित्य निर्माण और लेखन में बहुत समय लगाया। इसी का परिणाम है कि अलग-अलग प्रान्तों की भाषाओं में जैन विद्वान बराबर लिखते रहे। इससे उन भाषाओं का विकास किस तरह होता गया, शब्दों के रूपों में किस तरह का परिवर्तन हुआ, इसकी जानकारी जैन रचनाओं से जितनी अधिक मिलती है, उतनी जैनेतर रचनाओं से नहीं मिलती। क्योंकि एक तो वे इतनी सुरक्षित नहीं रहीं और प्रत्येक शताब्दी के प्रत्येक चरण की जैन रचनाएं जिस तरह की मिलती है, वैसी जैनेतरों की नहीं मिलती।
प्राकृत भाषा के दो प्रधान भेद हैं-शौरसेनी और महाराष्ट्री । शौरसेनी में दिगम्बर और महाराष्ट्री में श्वेताम्बर साहित्य रचा गया। इनसे अपभ्रश और अपभ्रंश से उत्तर भारत की प्रान्तीय भाषाओं की श्रृंखला जुड़ती है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org