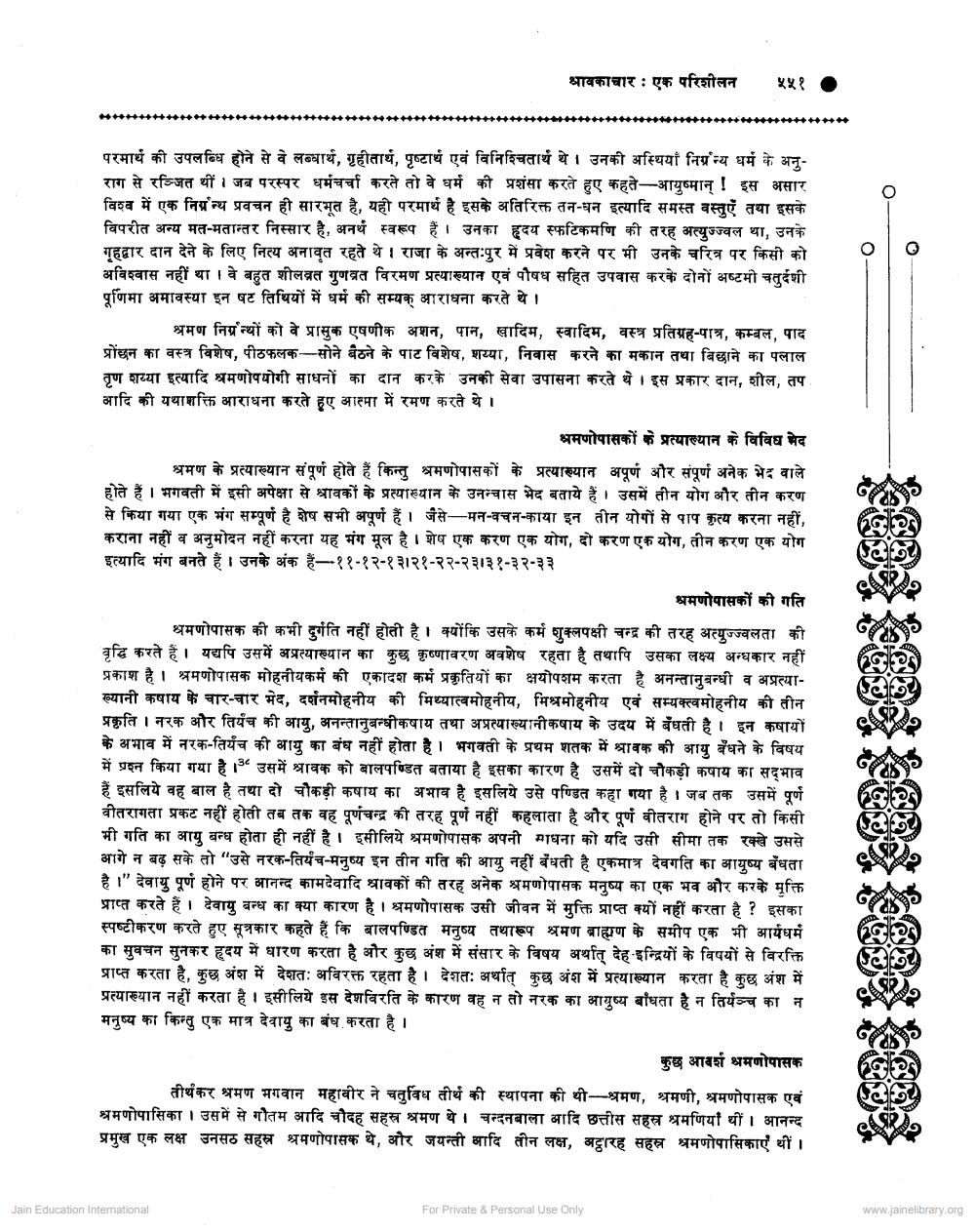________________
श्रावकाचार : एक परिशीलन
परमार्थ की उपलब्धि होने से वे लब्धार्थ, गृहीतार्थ, पृष्टार्थ एवं विनिश्चितार्थ थे। उनकी अस्थियाँ निग्रंन्य धर्म के अनुराग से रञ्जित थीं। जब परस्पर धर्मचर्चा करते तो वे धर्म की प्रशंसा करते हुए कहते-आयुष्मान् ! इस असार विश्व में एक निग्रन्थ प्रवचन ही सारभूत है, यही परमार्थ है इसके अतिरिक्त तन-धन इत्यादि समस्त वस्तुएं तथा इसके विपरीत अन्य मत-मतान्तर निस्सार है, अनर्थ स्वरूप हैं। उनका हृदय स्फटिकमणि की तरह अत्युज्ज्वल था, उनके गृहद्वार दान देने के लिए नित्य अनावृत रहते थे । राजा के अन्तःपुर में प्रवेश करने पर भी उनके चरित्र पर किसी को अविश्वास नहीं था । वे बहुत शीलव्रत गुणव्रत विरमण प्रत्याख्यान एवं पौषध सहित उपवास करके दोनों अष्टमी चतुर्दशी पूर्णिमा अमावस्या इन षट तिथियों में धर्म की सम्यक् आराधना करते थे।
श्रमण निर्ग्रन्थों को वे प्रासुक एषणीक अशन, पान, खादिम, स्वादिम, वस्त्र प्रतिग्रह-पात्र, कम्बल, पाद प्रोंछन का वस्त्र विशेष, पीठफलक-सोने बैठने के पाट विशेष, शय्या, निवास करने का मकान तथा बिछाने का पलाल तृण शय्या इत्यादि श्रमणोपयोगी साधनों का दान करके उनकी सेवा उपासना करते थे । इस प्रकार दान, शील, तप आदि की यथाशक्ति आराधना करते हुए आत्मा में रमण करते थे।
श्रमणोपासकों के प्रत्याख्यान के विविध भेद श्रमण के प्रत्याख्यान संपूर्ण होते हैं किन्तु श्रमणोपासकों के प्रत्याख्यान अपूर्ण और संपूर्ण अनेक भेद वाले होते हैं। भगवती में इसी अपेक्षा से धावकों के प्रत्याख्यान के उनन्चास भेद बताये हैं। उसमें तीन योग और तीन करण से किया गया एक भंग सम्पूर्ण है शेष सभी अपूर्ण हैं। जैसे-मन-वचन-काया इन तीन योगों से पाप कृत्य करना नहीं, कराना नहीं व अनुमोदन नहीं करना यह मंग मूल है । शेष एक करण एक योग, दो करण एक योग, तीन करण एक योग इत्यादि मंग बनते हैं। उनके अंक हैं--११-१२-१३।२१-२२-२३६३१-३२-३३
श्रमणोपासकों की गति श्रमणोपासक की कभी दुर्गति नहीं होती है। क्योंकि उसके कर्म शुक्लपक्षी चन्द्र की तरह अत्युज्ज्वलता की बृद्धि करते हैं। यद्यपि उसमें अप्रत्याख्यान का कुछ कृष्णावरण अवशेष रहता है तथापि उसका लक्ष्य अन्धकार नहीं प्रकाश है। श्रमणोपासक मोहनीयकर्म की एकादश कर्म प्रकृतियों का क्षयोपशम करता है अनन्तानुबन्धी व अप्रत्याख्यानी कषाय के चार-चार भेद, दर्शनमोहनीय की मिथ्यात्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय एवं सम्यक्त्वमोहनीय की तीन प्रकृति । नरक और तिर्यच की आयु, अनन्तानुबन्धीकषाय तथा अप्रत्याख्यानीकषाय के उदय में बँधती है। इन कषायों के अभाव में नरक-तिर्यंच की आयु का बंध नहीं होता है। भगवती के प्रथम शतक में श्रावक की आयु बँधने के विषय में प्रश्न किया गया है। उसमें श्रावक को बालपण्डित बताया है इसका कारण है उसमें दो चौकड़ी कषाय का सद्भाव हैं इसलिये वह बाल है तथा दो चौकड़ी कषाय का अभाव है इसलिये उसे पण्डित कहा गया है। जब तक उसमें पूर्ण वीतरागता प्रकट नहीं होती तब तक वह पूर्णचन्द्र की तरह पूर्ण नहीं कहलाता है और पूर्ण वीतराग होने पर तो किसी भी गति का आयु बन्ध होता ही नहीं है। इसीलिये श्रमणोपासक अपनी माधना को यदि उसी सीमा तक रक्खे उससे आगे न बढ़ सके तो "उसे नरक-तिर्यच-मनुष्य इन तीन गति की आयु नहीं बंधती है एकमात्र देवगति का आयुष्य बँधता है।" देवायु पूर्ण होने पर आनन्द कामदेवादि श्रावकों की तरह अनेक श्रमणोपासक मनुष्य का एक भव और करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। देवायु बन्ध का क्या कारण है । श्रमणोपासक उसी जीवन में मुक्ति प्राप्त क्यों नहीं करता है ? इसका स्पष्टीकरण करते हए सूत्रकार कहते हैं कि बालपण्डित मनुष्य तथारूप श्रमण ब्राह्मण के समीप एक भी आर्यधर्म का सुवचन सुनकर हृदय में धारण करता है और कुछ अंश में संसार के विषय अर्थात् देह इन्द्रियों के विषयों से बिरक्ति प्राप्त करता है, कुछ अंश में देशतः अविरक्त रहता है। देशत: अर्थात् कुछ अंश में प्रत्याख्यान करता है कुछ अंश में प्रत्याख्यान नहीं करता है । इसीलिये इस देशविरति के कारण वह न तो नरक का आयुष्य बाँधता है न तिर्यञ्च का न मनुष्य का किन्तु एक मात्र देवायु का बंध करता है ।
कुछ आवर्श श्रमणोपासक तीर्थकर श्रमण भगवान महावीर ने चतुर्विध तीर्थ की स्थापना की थी-श्रमण, श्रमणी, श्रमणोपासक एवं श्रमणोपासिका । उसमें से गौतम आदि चौदह सहस्र श्रमण थे। चन्दनबाला आदि छत्तीस सहस्र श्रमणियां थीं। आनन्द प्रमुख एक लक्ष उनसठ सहस्र श्रमणोपासक थे, और जयन्ती आदि तीन लक्ष, अट्ठारह सहस्र श्रमणोपासिकाएं थीं।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org