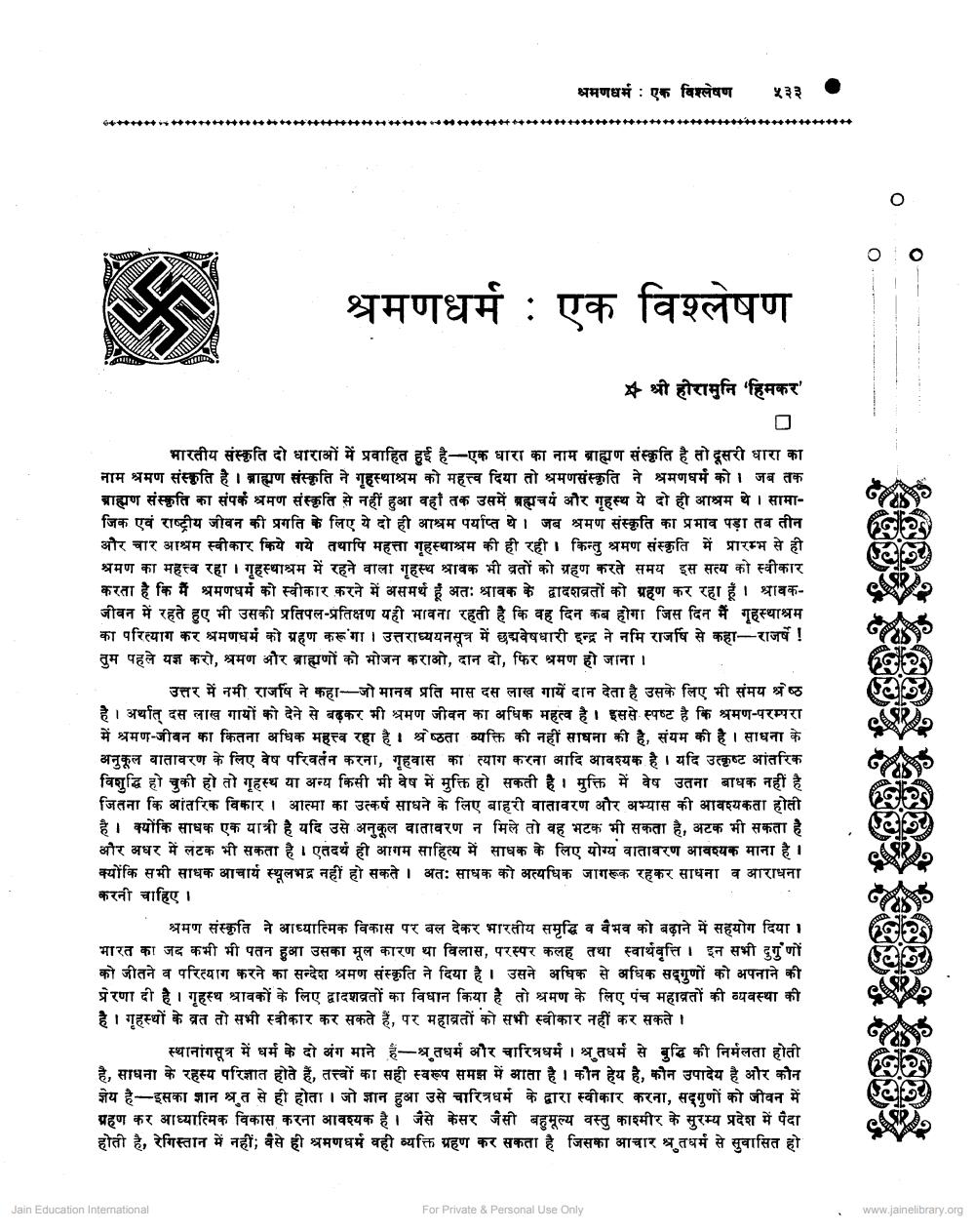________________
श्रमणधर्म : एक विश्लेषण
५३३
+
+
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
+
+++
++++
+
+
++
+
++++
+++++++
++
+
++
++
००
श्रमणधर्म : एक विश्लेषण
* श्री होरामुनि 'हिमकर'
ति ने गृहस्थाहाँ तक उस
तो श्रमणसंस्कृति में दो ही आश्रमशा तब तीन जब श्रा
भारतीय संस्कृति दो धाराओं में प्रवाहित हुई है-एक धारा का नाम ब्राह्मण संस्कृति है तो दूसरी धारा का नाम श्रमण संस्कृति है। ब्राह्मण संस्कृति ने गृहस्थाश्रम को महत्त्व दिया तो श्रमणसंस्कृति ने श्रमणधर्म को। जब तक ब्राह्मण संस्कृति का संपर्क श्रमण संस्कृति से नहीं हुआ वहाँ तक उसमें ब्रह्मचर्य और गृहस्थ ये दो ही आश्रम थे । सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन की प्रगति के लिए ये दो ही आश्रम पर्याप्त थे। जब श्रमण संस्कृति का प्रभाव पड़ा तब तीन और चार आश्रम स्वीकार किये गये तथापि महत्ता गृहस्थाश्रम की ही रही। किन्तु श्रमण संस्कृति में प्रारम्भ से ही श्रमण का महत्त्व रहा । गृहस्थाश्रम में रहने वाला गृहस्थ श्रावक भी व्रतों को ग्रहण करते समय इस सत्य को स्वीकार करता है कि मैं श्रमणधर्म को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ अतः श्रावक के द्वादशव्रतों को ग्रहण कर रहा हूँ। श्रावकजीवन में रहते हुए भी उसकी प्रतिपल-प्रतिक्षण यही भावना रहती है कि वह दिन कब होगा जिस दिन मैं गृहस्थाश्रम का परित्याग कर श्रमणधर्म को ग्रहण करूंगा। उत्तराध्ययनसूत्र में छद्मवेषधारी इन्द्र ने नमि राजर्षि से कहा-राजर्षे ! तुम पहले यज्ञ करो, श्रमण और ब्राह्मणों को भोजन कराओ, दान दो, फिर श्रमण हो जाना।
उत्तर में नमी राजर्षि ने कहा-जो मानव प्रति मास दस लाख गायें दान देता है उसके लिए भी संमय श्रेष्ठ है । अर्थात् दस लाख गायों को देने से बढ़कर भी श्रमण जीवन का अधिक महत्व है। इससे स्पष्ट है कि श्रमण-परम्परा में श्रमण-जीवन का कितना अधिक महत्त्व रहा है। श्रेष्ठता व्यक्ति की नहीं साधना की है, संयम की है । साधना के अनुकूल वातावरण के लिए वेष परिवर्तन करना, गृहवास का त्याग करना आदि आवश्यक है । यदि उत्कृष्ट आंतरिक विशुद्धि हो चुकी हो तो गृहस्थ या अन्य किसी भी वेष में मुक्ति हो सकती है। मुक्ति में वेष उतना बाधक नहीं है जितना कि आंतरिक विकार । आत्मा का उत्कर्ष साधने के लिए बाहरी वातावरण और अभ्यास की आवश्यकता होती है। क्योंकि साधक एक यात्री है यदि उसे अनुकूल वातावरण न मिले तो वह भटक भी सकता है, अटक भी सकता है और अधर में लटक भी सकता है । एतदर्थ ही आगम साहित्य में साधक के लिए योग्य वातावरण आवश्यक माना है। क्योंकि सभी साधक आचार्य स्थूलभद्र नहीं हो सकते । अतः साधक को अत्यधिक जागरूक रहकर साधना व आराधना करनी चाहिए।
श्रमण संस्कृति ने आध्यात्मिक विकास पर बल देकर भारतीय समृद्धि व वैभव को बढ़ाने में सहयोग दिया। भारत का जद कभी भी पतन हुआ उसका मूल कारण था विलास, परस्पर कलह तथा स्वार्थवृत्ति । इन सभी दुर्गुणों को जीतने व परित्याग करने का सन्देश श्रमण संस्कृति ने दिया है। उसने अधिक से अधिक सद्गुणों को अपनाने की प्रेरणा दी है। गृहस्थ श्रावकों के लिए द्वादशव्रतों का विधान किया है तो श्रमण के लिए पंच महाव्रतों की व्यवस्था की है । गृहस्थों के व्रत तो सभी स्वीकार कर सकते हैं, पर महाव्रतों को सभी स्वीकार नहीं कर सकते ।
स्थानांगसूत्र में धर्म के दो अंग माने हैं-श्रुतधर्म और चारित्रधर्म । श्रुतधर्म से बुद्धि की निर्मलता होती है, साधना के रहस्य परिज्ञात होते हैं, तत्त्वों का सही स्वरूप समझ में आता है। कौन हेय है, कौन उपादेय है और कौन ज्ञेय है-इसका ज्ञान श्रुत से ही होता । जो ज्ञान हुआ उसे चारित्रधर्म के द्वारा स्वीकार करना, सद्गुणों को जीवन में ग्रहण कर आध्यात्मिक विकास करना आवश्यक है। जैसे केसर जैसी बहुमूल्य वस्तु काश्मीर के सुरम्य प्रदेश में पैदा होती है, रेगिस्तान में नहीं; वैसे ही श्रमणधर्म वही व्यक्ति ग्रहण कर सकता है जिसका आचार श्रुतधर्म से सुवासित हो
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org