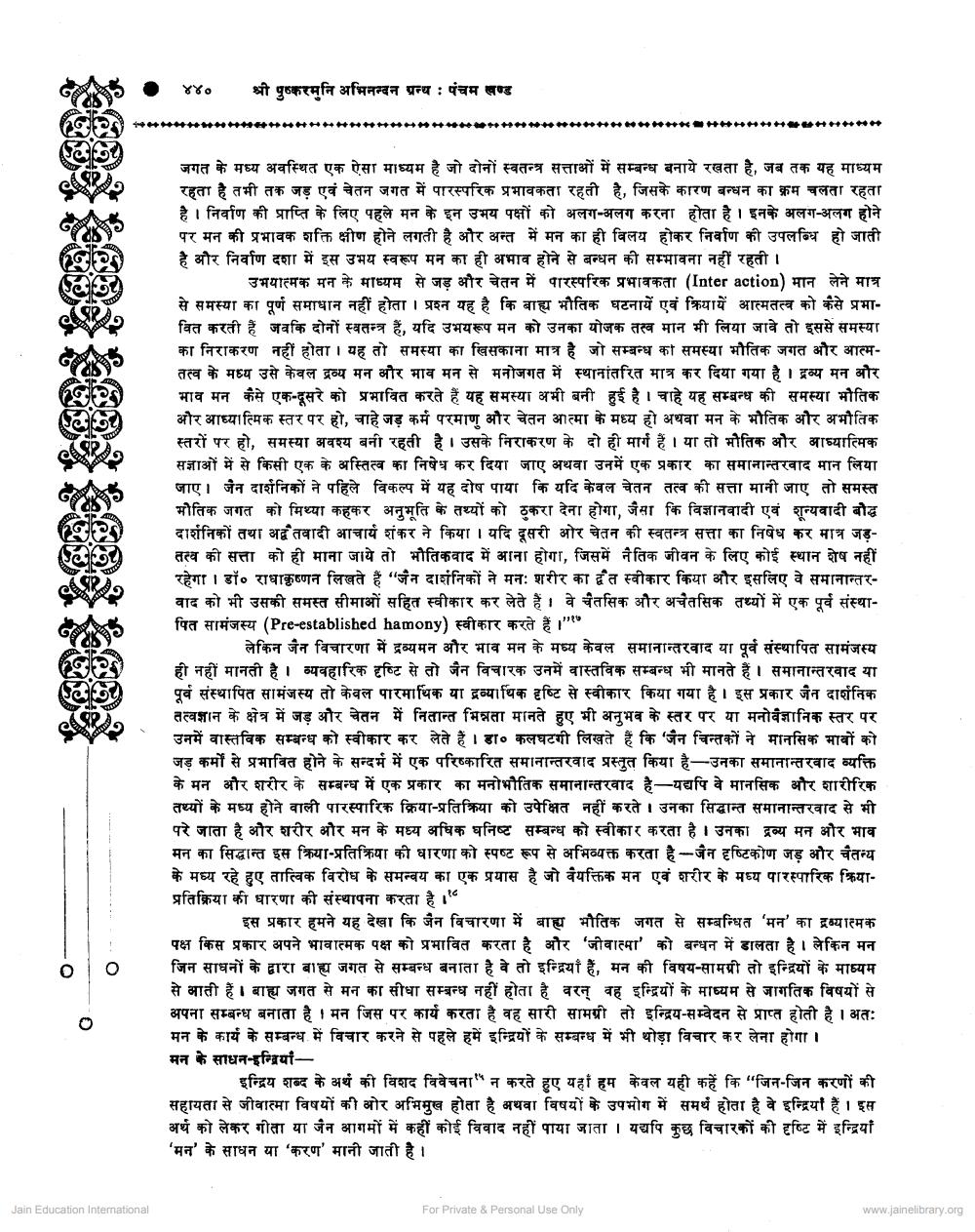________________
४४०
श्री पुष्करमुनि अभिनन्दन ग्रन्थ : पंचम खण्ड
immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm-----
जगत के मध्य अवस्थित एक ऐसा माध्यम है जो दोनों स्वतन्त्र सत्ताओं में सम्बन्ध बनाये रखता है, जब तक यह माध्यम रहता है तभी तक जड़ एवं चेतन जगत में पारस्परिक प्रभावकता रहती है, जिसके कारण बन्धन का क्रम चलता रहता है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए पहले मन के इन उभय पक्षों को अलग-अलग करना होता है। इनके अलग-अलग होने पर मन की प्रभावक शक्ति क्षीण होने लगती है और अन्त में मन का ही विलय होकर निर्वाण की उपलब्धि हो जाती है और निर्वाण दशा में इस उभय स्वरूप मन का ही अभाव होने से बन्धन की सम्भावना नहीं रहती।
उभयात्मक मन के माध्यम से जड़ और चेतन में पारस्परिक प्रभावकता (Inter action) मान लेने मात्र से समस्या का पूर्ण समाधान नहीं होता । प्रश्न यह है कि बाह्य भौतिक घटनायें एवं क्रियायें आत्मतत्व को कैसे प्रमावित करती हैं जबकि दोनों स्वतन्त्र हैं, यदि उभयरूप मन को उनका योजक तत्व मान भी लिया जावे तो इससे समस्या का निराकरण नहीं होता । यह तो समस्या का खिसकाना मात्र है जो सम्बन्ध को समस्या भौतिक जगत और आत्मतत्व के मध्य उसे केवल द्रव्य मन और भाव मन से मनोजगत में स्थानांतरित मात्र कर दिया गया है । द्रव्य मन और भाव मन कैसे एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं यह समस्या अभी बनी हुई है । चाहे यह सम्बन्ध की समस्या भौतिक और आध्यात्मिक स्तर पर हो, चाहे जड़ कर्म परमाणु और चेतन आत्मा के मध्य हो अथवा मन के भौतिक और अभौतिक स्तरों पर हो, समस्या अवश्य बनी रहती है। उसके निराकरण के दो ही मार्ग हैं । या तो भौतिक और आध्यात्मिक सज्ञाओं में से किसी एक के अस्तित्व का निषेध कर दिया जाए अथवा उनमें एक प्रकार का समानान्तरवाद मान लिया जाए। जैन दार्शनिकों ने पहिले विकल्प में यह दोष पाया कि यदि केवल चेतन तत्व की सत्ता मानी जाए तो समस्त भौतिक जगत को मिथ्या कहकर अनुभूति के तथ्यों को ठुकरा देना होगा, जैसा कि विज्ञानवादी एवं शून्यवादी बौद्ध दार्शनिकों तथा अद्वैतवादी आचार्य शंकर ने किया । यदि दूसरी ओर चेतन की स्वतन्त्र सत्ता का निषेध कर मात्र जड़तत्व की सत्ता को ही माना जाये तो भौतिकवाद में आना होगा, जिसमें नैतिक जीवन के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहेगा । डॉ. राधाकृष्णन लिखते हैं "जैन दार्शनिकों ने मनः शरीर का द्वंत स्वीकार किया और इसलिए वे समानान्तरवाद को भी उसकी समस्त सीमाओं सहित स्वीकार कर लेते हैं। वे चैतसिक और अचैतसिक तथ्यों में एक पूर्व संस्थापित सामंजस्य (Pre-established hamony) स्वीकार करते हैं।"१७
लेकिन जैन विचारणा में द्रव्यमन और भाव मन के मध्य केवल समानान्तरवाद या पूर्व संस्थापित सामंजस्य ही नहीं मानती है। व्यवहारिक दृष्टि से तो जैन विचारक उनमें वास्तविक सम्बन्ध भी मानते हैं। समानान्तरवाद या पूर्व संस्थापित सामंजस्य तो केवल पारमार्थिक या द्रव्याथिक दृष्टि से स्वीकार किया गया है। इस प्रकार जैन दार्शनिक तत्वज्ञान के क्षेत्र में जड़ और चेतन में नितान्त भिन्नता मानते हुए भी अनुभव के स्तर पर या मनोवैज्ञानिक स्तर पर उनमें वास्तविक सम्बन्ध को स्वीकार कर लेते हैं । डा० कलघटगी लिखते हैं कि 'जैन चिन्तकों ने मानसिक भावों को जड़ कर्मों से प्रभावित होने के सन्दर्भ में एक परिष्कारित समानान्तरवाद प्रस्तुत किया है उनका समानान्तरवाद व्यक्ति के मन और शरीर के सम्बन्ध में एक प्रकार का मनोभौतिक समानान्तरवाद है-यद्यपि वे मानसिक और शारीरिक तथ्यों के मध्य होने वाली पारस्पारिक क्रिया-प्रतिक्रिया को उपेक्षित नहीं करते । उनका सिद्धान्त समानान्तरवाद से भी परे जाता है और शरीर और मन के मध्य अधिक घनिष्ट सम्बन्ध को स्वीकार करता है। उनका द्रव्य मन और भाव मन का सिद्धान्त इस क्रिया-प्रतिक्रिया की धारणा को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करता है-जैन दृष्टिकोण जड़ और चैतन्य के मध्य रहे हुए तात्विक विरोध के समन्वय का एक प्रयास है जो वैयक्तिक मन एवं शरीर के मध्य पारस्पारिक क्रियाप्रतिक्रिया की धारणा की संस्थापना करता है।
इस प्रकार हमने यह देखा कि जैन विचारणा में बाह्य भौतिक जगत से सम्बन्धित 'मन' का द्रव्यात्मक पक्ष किस प्रकार अपने भावात्मक पक्ष को प्रभावित करता है और 'जीवात्मा' को बन्धन में डालता है। लेकिन मन जिन साधनों के द्वारा बाह्य जगत से सम्बन्ध बनाता है वे तो इन्द्रियाँ हैं, मन की विषय-सामग्री तो इन्द्रियों के माध्यम से आती हैं। बाह्य जगत से मन का सीधा सम्बन्ध नहीं होता है वरन् वह इन्द्रियों के माध्यम से जागतिक विषयों से अपना सम्बन्ध बनाता है । मन जिस पर कार्य करता है वह सारी सामग्री तो इन्द्रिय-सम्वेदन से प्राप्त होती है । अतः मन के कार्य के सम्बन्ध में विचार करने से पहले हमें इन्द्रियों के सम्बन्ध में भी थोड़ा विचार कर लेना होगा। मन के साधन-इन्द्रियां
इन्द्रिय शब्द के अर्थ की विशद विवेचना न करते हुए यहाँ हम केवल यही कहें कि "जिन-जिन करणों की सहायता से जीवात्मा विषयों की ओर अभिमुख होता है अथवा विषयों के उपभोग में समर्थ होता है वे इन्द्रियाँ हैं । इस अर्थ को लेकर गीता या जैन आगमों में कहीं कोई विवाद नहीं पाया जाता । यद्यपि कुछ विचारकों की दृष्टि में इन्द्रियाँ 'मन' के साधन या 'करण' मानी जाती है।
००
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org