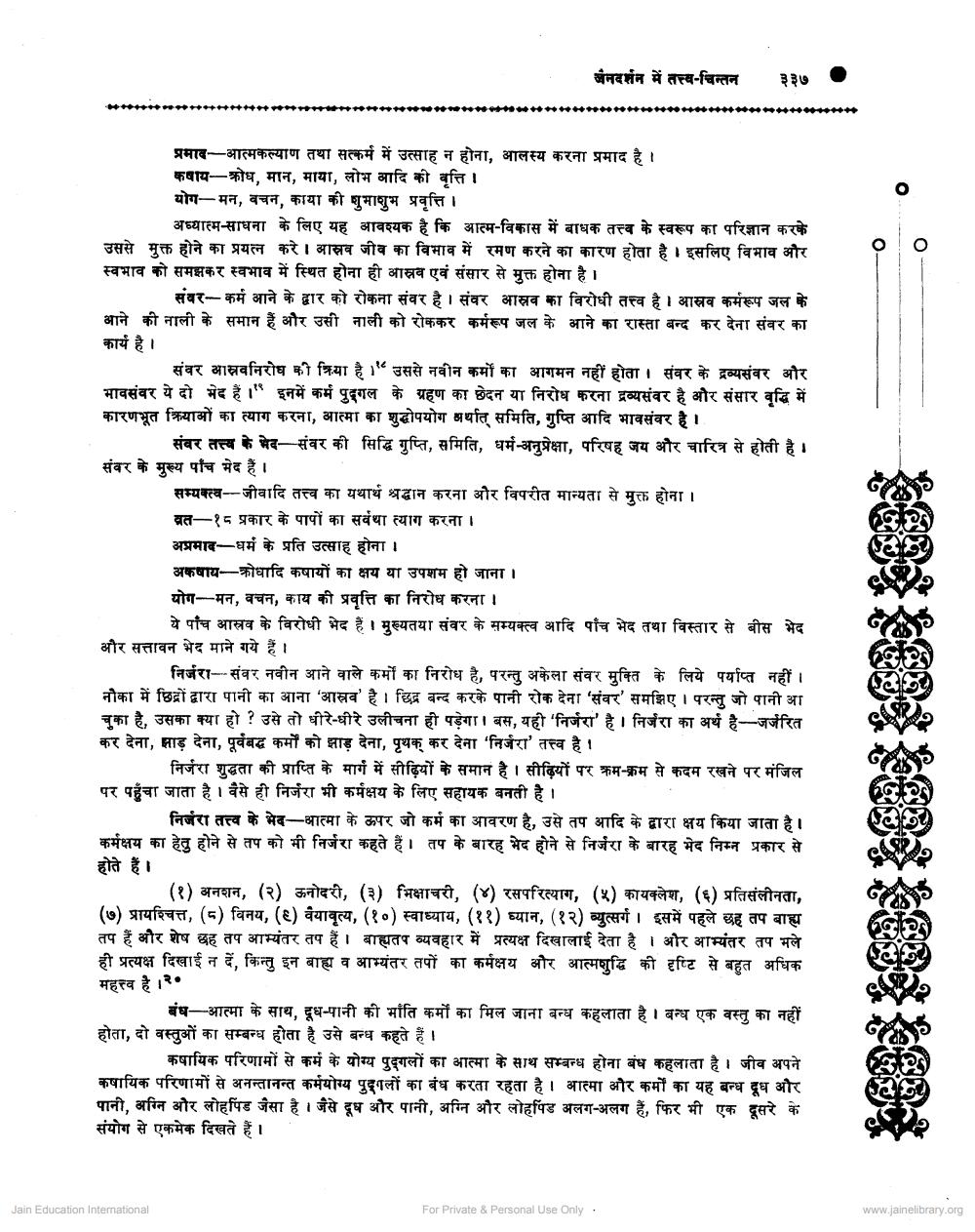________________
जैनदर्शन में तत्त्व-चिन्तन
३३७
प्रमाव-आत्मकल्याण तथा सत्कर्म में उत्साह न होना, आलस्य करना प्रमाद है। कषाय-क्रोध, मान, माया, लोभ आदि की वृत्ति । योग-मन, वचन, काया की शुभाशुभ प्रवृत्ति ।।
अध्यात्म-साधना के लिए यह आवश्यक है कि आत्म-विकास में बाधक तत्त्व के स्वरूप का परिज्ञान करके उससे मुक्त होने का प्रयत्न करे । आस्रव जीव का विभाव में रमण करने का कारण होता है। इसलिए विभाव और स्वभाव को समझकर स्वभाव में स्थित होना ही आस्रव एवं संसार से मुक्त होना है।
संवर-कर्म आने के द्वार को रोकना संवर है। संवर आस्रव का विरोधी तत्त्व है। आस्रव कर्मरूप जल के आने की नाली के समान हैं और उसी नाली को रोककर कर्मरूप जल के आने का रास्ता बन्द कर देना संवर का कार्य है।
संवर आनवनिरोध की क्रिया है।" उससे नवीन कर्मों का आगमन नहीं होता। संवर के द्रव्यसंवर और भावसंवर ये दो भेद हैं। इनमें कर्म पुद्गल के ग्रहण का छेदन या निरोध करना द्रव्यसंवर है और संसार वृद्धि में कारणभूत क्रियाओं का त्याग करना, आत्मा का शुद्धोपयोग अर्थात् समिति, गुप्ति आदि भावसंवर है।
___संबर तत्त्व के भेद-संवर की सिद्धि गुप्ति, समिति, धर्म-अनुप्रेक्षा, परिषह जय और चारित्र से होती है। संवर के मुख्य पाँच भेद हैं।
सम्यक्त्व-जीवादि तत्त्व का यथार्थ श्रद्धान करना और विपरीत मान्यता से मुक्त होना। व्रत-१८ प्रकार के पापों का सर्वथा त्याग करना । अप्रमाद-धर्म के प्रति उत्साह होना । अकषाय-क्रोधादि कषायों का क्षय या उपशम हो जाना। योग-मन, वचन, काय की प्रवृत्ति का निरोध करना।
ये पाँच आस्रव के विरोधी भेद हैं । मुख्यतया संवर के सम्यक्त्व आदि पाँच भेद तथा विस्तार से बीस भेद और सत्तावन भेद माने गये हैं।
निर्जरा-संवर नवीन आने वाले कर्मों का निरोध है, परन्तु अकेला संवर मुक्ति के लिये पर्याप्त नहीं। नौका में छिद्रों द्वारा पानी का आना 'आस्रव है। छिद्र बन्द करके पानी रोक देना 'संवर' समझिए । परन्तु जो पानी आ चुका है, उसका क्या हो ? उसे तो धीरे-धीरे उलीचना ही पड़ेगा। बस, यही 'निर्जरा' है । निर्जरा का अर्थ है-जर्जरित कर देना, झाड़ देना, पूर्वबद्ध कर्मों को झाड़ देना, पृथक् कर देना 'निर्जरा' तत्त्व है।
निर्जरा शुद्धता की प्राप्ति के मार्ग में सीढ़ियों के समान है । सीढ़ियों पर क्रम-क्रम से कदम रखने पर मंजिल पर पहुँचा जाता है । वैसे ही निर्जरा भी कर्मक्षय के लिए सहायक बनती है ।
निर्जरा तत्त्व के भेद-आत्मा के ऊपर जो कर्म का आवरण है, उसे तप आदि के द्वारा क्षय किया जाता है। कर्मक्षय का हेतु होने से तप को भी निर्जरा कहते हैं। तप के बारह भेद होने से निर्जरा के बारह भेद निम्न प्रकार से होते हैं।
(१) अनशन, (२) ऊनोदरी, (३) भिक्षाचरी, (४) रसपरित्याग, (५) कायक्लेश, (६) प्रतिसंलीनता, (७) प्रायश्चित्त, (८) विनय, (९) वैयावृत्य, (१०) स्वाध्याय, (११) ध्यान, (१२) व्युत्सर्ग। इसमें पहले छह तप बाह्य तप हैं और शेष छह तप आभ्यंतर तप हैं। बाह्यतप व्यवहार में प्रत्यक्ष दिखालाई देता है । और आभ्यंतर तप भले ही प्रत्यक्ष दिखाई न दें, किन्तु इन बाह्य व आभ्यंतर तपों का कर्मक्षय और आत्मशुद्धि की दृष्टि से बहुत अधिक महत्त्व है।
बंध-आत्मा के साथ, दूध-पानी की भांति कर्मों का मिल जाना बन्ध कहलाता है। बन्ध एक वस्तु का नहीं होता, दो वस्तुओं का सम्बन्ध होता है उसे बन्ध कहते हैं।
कषायिक परिणामों से कर्म के योग्य पुद्गलों का आत्मा के साथ सम्बन्ध होना बंध कहलाता है। जीव अपने कषायिक परिणामों से अनन्तानन्त कर्मयोग्य पुद्गलों का बंध करता रहता है। आत्मा और कर्मों का यह बन्ध दूध और पानी, अग्नि और लोहपिंड जैसा है । जैसे दूध और पानी, अग्नि और लोहपिंड अलग-अलग हैं, फिर भी एक दूसरे के संयोग से एकमेक दिखते हैं।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only.
www.jainelibrary.org