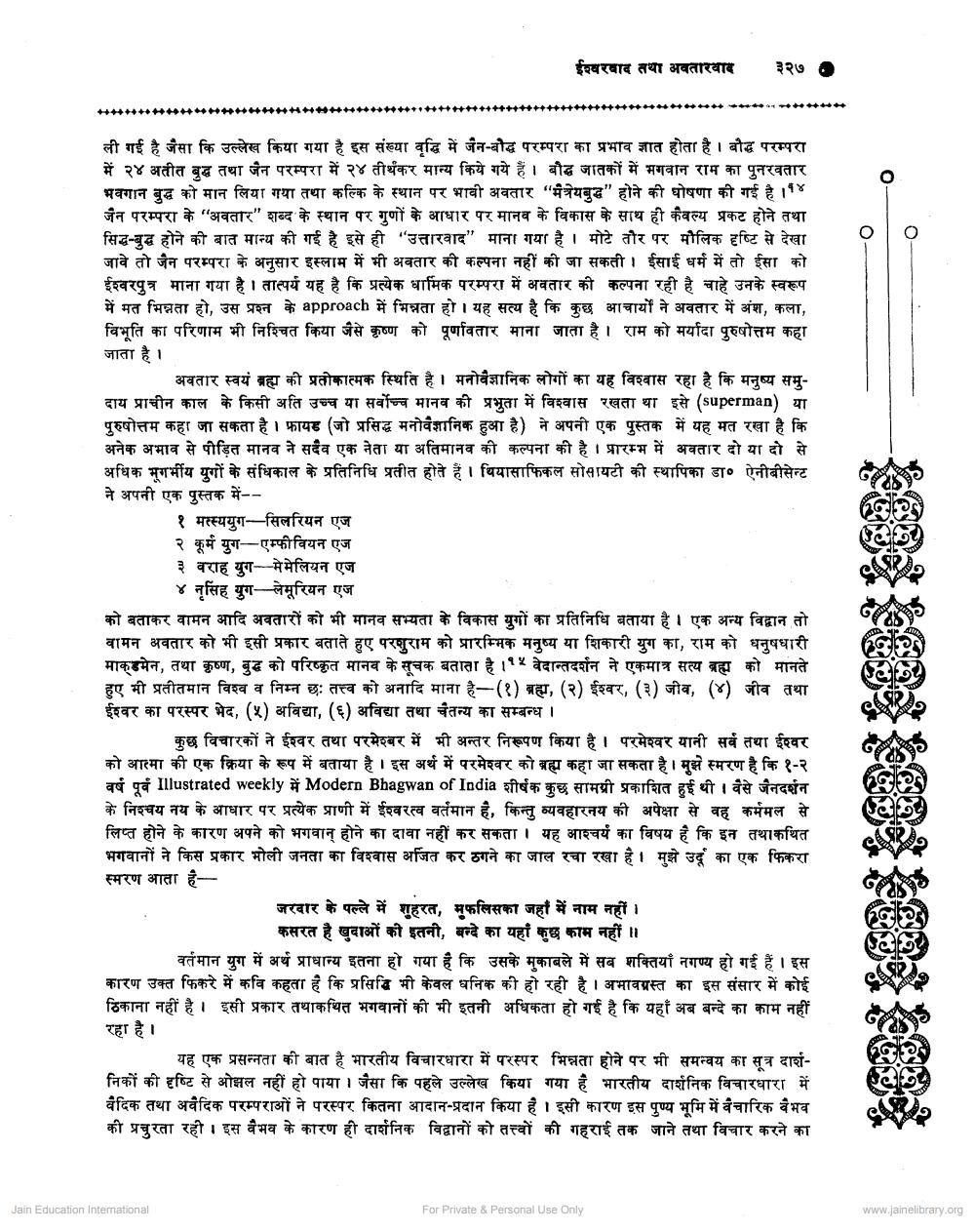________________
ईश्वरवाद तथा अवतारवाद
३२७.
olo
ली गई है जैसा कि उल्लेख किया गया है इस संख्या वृद्धि में जैन-बौद्ध परम्परा का प्रभाव ज्ञात होता है । बौद्ध परम्परा में २४ अतीत बुद्ध तथा जैन परम्परा में २४ तीर्थंकर मान्य किये गये हैं। बौद्ध जातकों में भगवान राम का पुनरवतार भवगान बुद्ध को मान लिया गया तथा कल्कि के स्थान पर भावी अवतार "मैत्रेयबुद्ध" होने की घोषणा की गई है ।१४ जैन परम्परा के “अवतार" शब्द के स्थान पर गुणों के आधार पर मानव के विकास के साथ ही कैवल्य प्रकट होने तथा सिद्ध-बुद्ध होने की बात मान्य की गई है इसे ही "उत्तारवाद" माना गया है । मोटे तौर पर मौलिक दृष्टि से देखा जावे तो जैन परम्परा के अनुसार इस्लाम में भी अवतार की कल्पना नहीं की जा सकती। ईसाई धर्म में तो ईसा को ईश्वरपुत्र माना गया है । तात्पर्य यह है कि प्रत्येक धार्मिक परम्परा में अवतार की कल्पना रही है चाहे उनके स्वरूप में मत भिन्नता हो, उस प्रश्न के approach में भिन्नता हो। यह सत्य है कि कुछ आचार्यों ने अवतार में अंश, कला, विभूति का परिणाम भी निश्चित किया जैसे कृष्ण को पूर्णावतार माना जाता है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है।
अवतार स्वयं ब्रह्म की प्रतीकात्मक स्थिति है। मनोवैज्ञानिक लोगों का यह विश्वास रहा है कि मनुष्य समुदाय प्राचीन काल के किसी अति उच्च या सर्वोच्च मानव की प्रभुता में विश्वास रखता था इसे (superman) या पुरुषोत्तम कहा जा सकता है। फ्रायड (जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुआ है) ने अपनी एक पुस्तक में यह मत रखा है कि अनेक अभाव से पीड़ित मानव ने सदैव एक नेता या अतिमानव की कल्पना की है। प्रारम्भ में अवतार दो या दो से अधिक भूगर्भीय युगों के संधिकाल के प्रतिनिधि प्रतीत होते हैं। थियासाफिकल सोसायटी की स्थापिका डा. ऐनीबीसेन्ट ने अपनी एक पुस्तक में--
१ मत्स्ययुग-सिलरियन एज २ कूर्म युग-एम्फीवियन एज ३ वराह युग-मेमेलियन एज
४ नृसिंह युग-लेमूरियन एज को बताकर वामन आदि अवतारों को भी मानव सभ्यता के विकास युगों का प्रतिनिधि बताया है। एक अन्य विद्वान तो वामन अवतार को भी इसी प्रकार बताते हुए परशुराम को प्रारम्भिक मनुष्य या शिकारी युग का, राम को धनुषधारी माक्डमेन, तथा कृष्ण, बुद्ध को परिष्कृत मानव के सूचक बताता है । १५ वेदान्तदर्शन ने एकमात्र सत्य ब्रह्म को मानते हुए भी प्रतीतमान विश्व व निम्न छः तत्त्व को अनादि माना है-(१) ब्रह्म, (२) ईश्वर, (३) जीव, (४) जीव तथा ईश्वर का परस्पर भेद, (५) अविद्या, (६) अविद्या तथा चैतन्य का सम्बन्ध ।
कुछ विचारकों ने ईश्वर तथा परमेश्वर में भी अन्तर निरूपण किया है। परमेश्वर यानी सर्व तथा ईश्वर को आत्मा की एक क्रिया के रूप में बताया है । इस अर्थ में परमेश्वर को ब्रह्म कहा जा सकता है। मुझे स्मरण है कि १-२ वर्ष पूर्व Illustrated weekly में Modern Bhagwan of India शीर्षक कुछ सामग्री प्रकाशित हुई थी। वैसे जैनदर्शन के निश्चय नय के आधार पर प्रत्येक प्राणी में ईश्वरत्व वर्तमान है, किन्तु व्यवहारनय की अपेक्षा से वह कर्ममल से लिप्त होने के कारण अपने को भगवान् होने का दावा नहीं कर सकता। यह आश्चर्य का विषय है कि इन तथाकथित भगवानों ने किस प्रकार भोली जनता का विश्वास अजित कर ठगने का जाल रचा रखा है। मुझे उर्दू का एक फिकरा स्मरण आता है
जरवार के पल्ले में शुहरत, मुफलिसका जहाँ में नाम नहीं ।
कसरत है खुदाओं की इतनी, बन्दे का यहां कुछ काम नहीं ॥ वर्तमान युग में अर्थ प्राधान्य इतना हो गया है कि उसके मुकाबले में सब शक्तियाँ नगण्य हो गई हैं । इस कारण उक्त फिकरे में कवि कहता है कि प्रसिद्धि भी केवल धनिक की हो रही है । अभावग्रस्त का इस संसार में कोई ठिकाना नहीं है। इसी प्रकार तथाकथित भगवानों की भी इतनी अधिकता हो गई है कि यहाँ अब बन्दे का काम नहीं
यह एक प्रसन्नता की बात है भारतीय विचारधारा में परस्पर भिन्नता होने पर भी समन्वय का सूत्र दार्शनिकों की दृष्टि से ओझल नहीं हो पाया। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है भारतीय दार्शनिक विचारधारा में वैदिक तथा अवैदिक परम्पराओं ने परस्पर कितना आदान-प्रदान किया है । इसी कारण इस पुण्य भूमि में वैचारिक वैभव की प्रचुरता रही। इस वैभव के कारण ही दार्शनिक विद्वानों को तत्त्वों की गहराई तक जाने तथा विचार करने का
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org