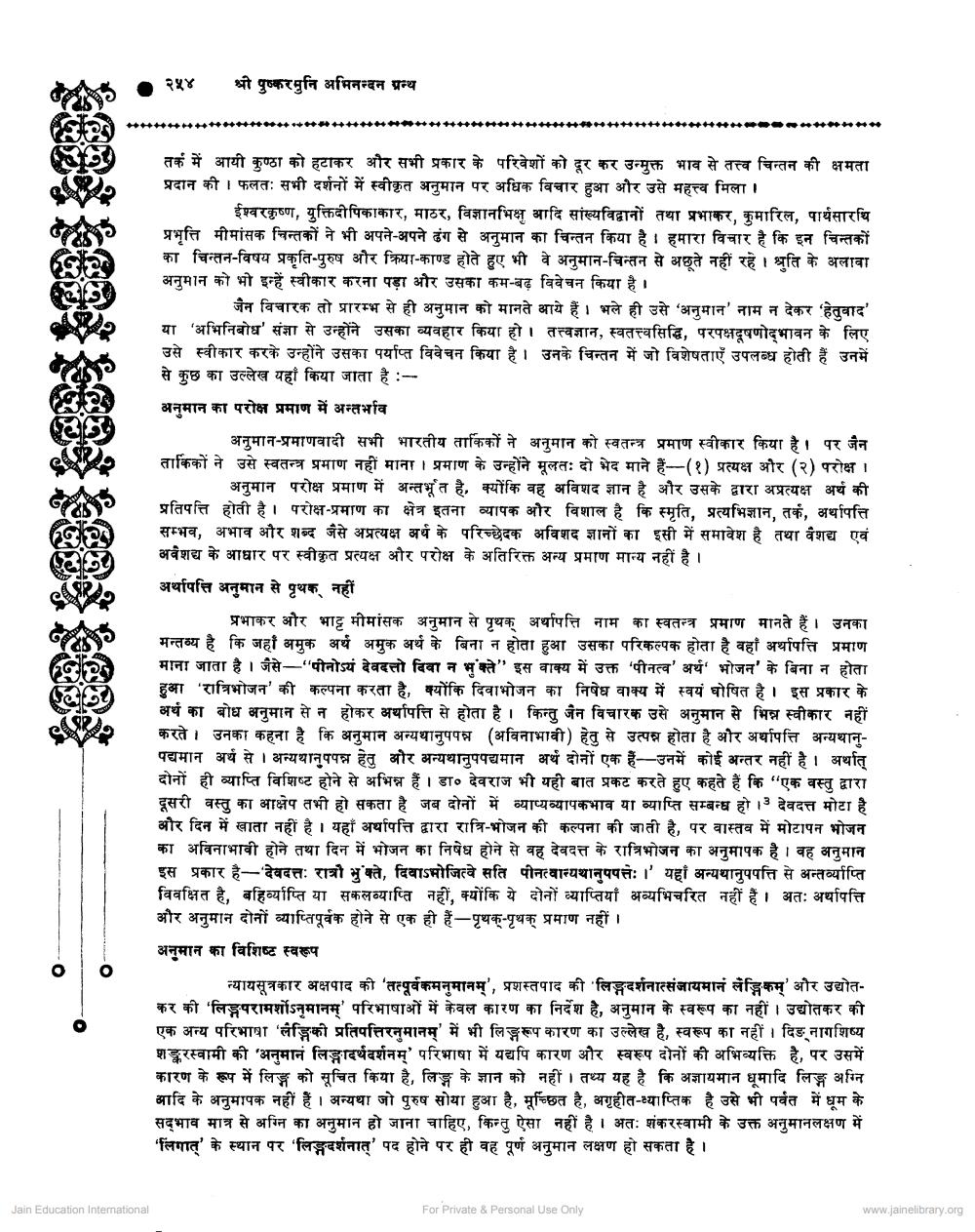________________
Jain Education International
२५४
श्री पुष्कर मुनि अभिनन्दन ग्रन्थ
तर्क में आयी कुण्ठा को हटाकर और सभी प्रकार के परिवेशों को दूर कर उन्मुक्त भाव से तत्त्व चिन्तन की क्षमता प्रदान की । फलतः सभी दर्शनों में स्वीकृत अनुमान पर अधिक विचार हुआ और उसे महत्त्व मिला।
ईश्वरकृष्ण, युक्तिदीपिकाकार, माठर, विज्ञानभिक्षु आदि सांख्यविद्वानों तथा प्रभाकर, कुमारिल, पार्थसारथि प्रभृत्ति मीमांसक चिन्तकों ने भी अपने-अपने ढंग से अनुमान का चिन्तन किया है। हमारा विचार है कि इन चिन्तकों का चिन्तन- विषय प्रकृति-पुरुष और क्रिया काण्ड होते हुए भी वे अनुमान चिन्तन से अछूते नहीं रहे। श्रुति के अलावा अनुमान को भी इन्हें स्वीकार करना पड़ा और उसका कम बढ़ विवेचन किया है।
जैन विचारक तो प्रारम्भ से ही अनुमान को मानते आये हैं। भले ही उसे 'अनुमान' नाम न देकर 'हेतुवाद' या 'अभिनिबोध' संज्ञा से उन्होंने उसका व्यवहार किया हो । तत्त्वज्ञान, स्वतत्त्वसिद्धि, परपक्षदूषणोद्भावन के लिए उसे स्वीकार करके उन्होंने उसका पर्याप्त विवेचन किया है। उनके चिन्तन में जो विशेषताएँ उपलब्ध होती हैं उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ किया जाता है :
अनुमान का परोक्ष प्रमाण में अन्तर्भाव
अनुमान प्रमाणवादी सभी भारतीय तार्किकों ने अनुमान को स्वतन्त्र प्रमाण स्वीकार किया है। पर जैन तार्किकों ने उसे स्वतन्त्र प्रमाण नहीं माना । प्रमाण के उन्होंने मूलतः दो भेद माने हैं-- (१) प्रत्यक्ष और ( २ ) परोक्ष । क्योंकि वह अविशद ज्ञान है और उसके द्वारा अप्रत्यक्ष अर्थ की व्यापक और विशाल है कि स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अर्थापत्ति परिच्छेदक अविशद ज्ञानों का इसी में समावेश है तथा वैशद्य एवं
अनुमान परोक्ष प्रमाण में अन्तर्भूत है, प्रतिपत्ति होती है । परोक्ष प्रमाण का क्षेत्र इतना सम्भव, अभाव और शब्द जैसे अप्रत्यक्ष अर्थ के अवैद्य के आधार पर स्वीकृत प्रत्यक्ष और परोक्ष के अतिरिक्त अन्य प्रमाण मान्य नहीं है ।
अर्थापत्ति अनुमान से पृथक नहीं
प्रभाकर और भाट्ट मीमांसक अनुमान से पृथक् अर्थापत्ति नाम का स्वतन्त्र प्रमाण मानते हैं। उनका मन्तव्य है कि जहाँ अमुक अर्थ अमुक अर्थ के बिना न होता हुआ उसका परिकल्पक होता है वहाँ अर्थापत्ति प्रमाण माना जाता है। जैसे- "पीनोऽयं देवदत्तो दिवा न भुंक्ते" इस वाक्य में उक्त 'पीनत्व' अर्थ' भोजन' के बिना न होता हुआ 'रात्रिभोजन' की कल्पना करता है, क्योंकि दिवाभोजन का निषेध वाक्य में स्वयं घोषित है । इस प्रकार के अर्थ का बोध अनुमान से न होकर अर्थापत्ति से होता है। किन्तु जैन विचारक उसे अनुमान से भित्र स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि अनुमान अन्यथानुपपन्न (अविनाभावी) हेतु से उत्पन्न होता है और अर्थापत्ति अन्यथा - पद्यमान अर्थ से । अन्यथानुपपन्न हेतु और अन्यथानुपपद्यमान अर्थं दोनों एक हैं—उनमें कोई अन्तर नहीं है । अर्थात् दोनों ही व्याप्ति विशिष्ट होने से अभिन्न हैं । डा० देवराज भी यही बात प्रकट करते हुए कहते हैं कि “एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु का आक्षेप तभी हो सकता है जब दोनों में व्याप्यव्यापकभाव या व्याप्ति सम्बन्ध हो । 3 देवदत्त मोटा है और दिन में खाता नहीं है । यहाँ अर्थापत्ति द्वारा रात्रि भोजन की कल्पना की जाती है, पर वास्तव में मोटापन भोजन का अविनाभावी होने तथा दिन में भोजन का निषेध होने से वह देवदत्त के रात्रिभोजन का अनुमापक है। वह अनुमान इस प्रकार है - 'देवदत्तः रात्रौ भुंक्ते, दिवाऽमोजित्वे सति पीनत्वान्यथानुपपत्तेः ।' यहाँ अन्यथानुपपत्ति से अन्तर्व्याप्ति विवक्षित है, बहिर्व्याप्ति या सकलव्याप्ति नहीं, क्योंकि ये दोनों व्याप्तियां अव्यभिचरित नहीं है। अतः अर्थापत्ति और अनुमान दोनों व्याप्तिपूर्वक होने से एक ही हैं- पृथक् पृथक् प्रमाण नहीं ।
अनुमान का विशिष्ट स्वरूप
न्यायसूत्रकार अक्षपाद की 'तत्पूर्वकमनुमानम् प्रशस्तपाद की सिङ्गदर्शनात्संजायमानं लैङ्गिकम्' और यो कर की 'लिङ्गपरामशऽनुमानम् परिभाषाओं में केवल कारण का निर्देश है, अनुमान के स्वरूप का नहीं। उद्योतकर की एक अन्य परिभाषा 'लैङ्गिकी प्रतिपत्तिरनुमानम्' में भी लिङ्गरूप कारण का उल्लेख है, स्वरूप का नहीं । दिङ्नागशिष्य शङ्करस्वामी की 'अनुमानं लिङ्गादर्थदर्शनम्' परिभाषा में यद्यपि कारण और स्वरूप दोनों की अभिव्यक्ति है, पर उसमें कारण के रूप में लिङ्ग को सूचित किया है, लिङ्ग के ज्ञान को नहीं। तथ्य यह है कि अज्ञायमान धूमादि लिङ्ग अग्नि आदि के अनुमापक नहीं है। अन्यथा जो पुरुष सोया हुआ है, मूच्छित है, अग्रगृहीतश्याप्तिक है उसे भी पर्वत में धूम के सद्भाव मात्र से अग्नि का अनुमान हो जाना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं है । अतः शंकरस्वामी के उक्त अनुमानलक्षण में 'लिंगात्' के स्थान पर 'लिङ्गदर्शनात्' पद होने पर ही वह पूर्ण अनुमान लक्षण हो सकता है ।
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org