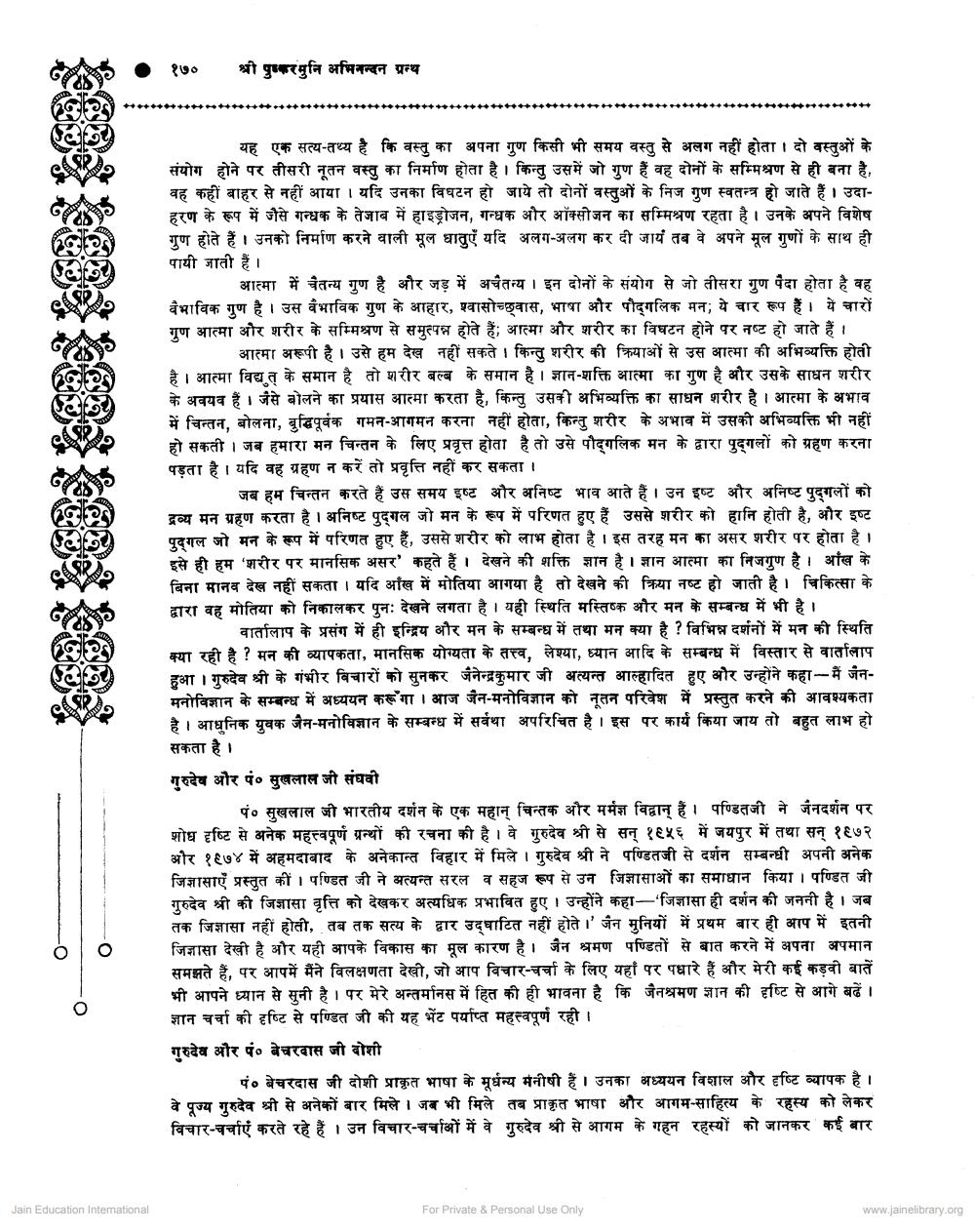________________
१७०
श्री पुष्करमुनि अभिनन्दन ग्रन्थ
+++
+++++++++++++++++++++++++++
+++
++++++
+
+
+++
+
+
+
+
+
++
++
+++++++++
++
+++
+++++
+
+++
यह एक सत्य-तथ्य है कि वस्तु का अपना गुण किसी भी समय वस्तु से अलग नहीं होता। दो वस्तुओं के संयोग होने पर तीसरी नूतन वस्तु का निर्माण होता है। किन्तु उसमें जो गुण हैं वह दोनों के सम्मिश्रण से ही बना है, वह कहीं बाहर से नहीं आया । यदि उनका विघटन हो जाये तो दोनों वस्तुओं के निज गुण स्वतन्त्र हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे गन्धक के तेजाब में हाइड्रोजन, गन्धक और ऑक्सीजन का सम्मिश्रण रहता है। उनके अपने विशेष गुण होते हैं। उनको निर्माण करने वाली मूल धातुएँ यदि अलग-अलग कर दी जायं तब वे अपने मूल गुणों के साथ ही पायी जाती हैं।
आत्मा में चैतन्य गुण है और जड़ में अचैतन्य । इन दोनों के संयोग से जो तीसरा गुण पैदा होता है वह वैभाविक गुण है । उस वैभाविक गुण के आहार, श्वासोच्छ्वास, भाषा और पौद्गलिक मन, ये चार रूप हैं। ये चारों गुण आत्मा और शरीर के सम्मिश्रण से समुत्पन्न होते हैं; आत्मा और शरीर का विघटन होने पर नष्ट हो जाते हैं।
आत्मा अरूपी है। उसे हम देख नहीं सकते । किन्तु शरीर की क्रियाओं से उस आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। आत्मा विद्य त् के समान है तो शरीर बल्ब के समान है। ज्ञान-शक्ति आत्मा का गुण है और उसके साधन शरीर के अवयव हैं । जैसे बोलने का प्रयास आत्मा करता है, किन्तु उसकी अभिव्यक्ति का साधन शरीर है । आत्मा के अभाव में चिन्तन, बोलना, बुद्धिपूर्वक गमन-आगमन करना नहीं होता, किन्तु शरीर के अभाव में उसकी अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती । जब हमारा मन चिन्तन के लिए प्रवृत्त होता है तो उसे पौद्गलिक मन के द्वारा पुद्गलों को ग्रहण करना पड़ता है । यदि वह ग्रहण न करें तो प्रवृत्ति नहीं कर सकता।
जब हम चिन्तन करते हैं उस समय इष्ट और अनिष्ट भाव आते हैं। उन इष्ट और अनिष्ट पुद्गलों को दव्य मन ग्रहण करता है। अनिष्ट पूदगल जो मन के रूप में परिणत हए हैं उससे शरीर को हानि होती है, और इष्ट पुदगल जो मन के रूप में परिणत हुए हैं, उससे शरीर को लाभ होता है । इस तरह मन का असर शरीर पर होता है। इसे ही हम 'शरीर पर मानसिक असर' कहते हैं। देखने की शक्ति ज्ञान है। ज्ञान आत्मा का निजगुण है। आँख के बिना मानव देख नहीं सकता । यदि आँख में मोतिया आगया है तो देखने की क्रिया नष्ट हो जाती है। चिकित्सा के द्वारा वह मोतिया को निकालकर पुनः देखने लगता है । यही स्थिति मस्तिष्क और मन के सम्बन्ध में भी है।
वार्तालाप के प्रसंग में ही इन्द्रिय और मन के सम्बन्ध में तथा मन क्या है ? विभिन्न दर्शनों में मन की स्थिति क्या रही है ? मन की व्यापकता, मानसिक योग्यता के तत्त्व, लेश्या, ध्यान आदि के सम्बन्ध में विस्तार से वार्तालाप हुआ । गुरुदेव श्री के गंभीर विचारों को सुनकर जैनेन्द्रकुमार जी अत्यन्त आल्हादित हुए और उन्होंने कहा-मैं जनमनोविज्ञान के सम्बन्ध में अध्ययन करूंगा । आज जैन-मनोविज्ञान को नूतन परिवेश में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आधुनिक युवक जैन-मनोविज्ञान के सम्बन्ध में सर्वथा अपरिचित है। इस पर कार्य किया जाय तो बहुत लाभ हो सकता है। गुरुदेव और पं० सुखलाल जी संघवी
पं० सुखलाल जी भारतीय दर्शन के एक महान् चिन्तक और मर्मज्ञ विद्वान् हैं। पण्डितजी ने जनदर्शन पर शोध दृष्टि से अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की है। वे गुरुदेव श्री से सन् १९५६ में जयपुर में तथा सन् १९७२
और १९७४ में अहमदाबाद के अनेकान्त विहार में मिले । गुरुदेव श्री ने पण्डितजी से दर्शन सम्बन्धी अपनी अनेक जिज्ञासाएँ प्रस्तुत की। पण्डित जी ने अत्यन्त सरल व सहज रूप से उन जिज्ञासाओं का समाधान किया। पण्डित जी गुरुदेव श्री की जिज्ञासा वृत्ति को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने कहा-'जिज्ञासा ही दर्शन की जननी है। जब तक जिज्ञासा नहीं होती, तब तक सत्य के द्वार उद्घाटित नहीं होते।' जैन मुनियों में प्रथम बार ही आप में इतनी जिज्ञासा देखी है और यही आपके विकास का मूल कारण है। जैन श्रमण पण्डितों से बात करने में अपना अपमान समझते हैं, पर आपमें मैंने विलक्षणता देखी, जो आप विचार-चर्चा के लिए यहां पर पधारे हैं और मेरी कई कड़वी बातें भी आपने ध्यान से सुनी है। पर मेरे अन्तर्मानस में हित की ही भावना है कि जैनश्रमण ज्ञान की दृष्टि से आगे बढ़ें। ज्ञान चर्चा की दृष्टि से पण्डित जी की यह भेंट पर्याप्त महत्त्वपूर्ण रही। गुरुदेव और पं० बेचरदास जी बोशी
पं० बेचरदास जी दोशी प्राकृत भाषा के मूर्धन्य मनीषी हैं । उनका अध्ययन विशाल और दृष्टि व्यापक है। वे पूज्य गुरुदेव श्री से अनेकों बार मिले। जब भी मिले तब प्राकृत भाषा और आगम-साहित्य के रहस्य को लेकर विचार-चर्चाएं करते रहे हैं । उन विचार-चर्चाओं में वे गुरुदेव श्री से आगम के गहन रहस्यों को जानकर कई बार
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org